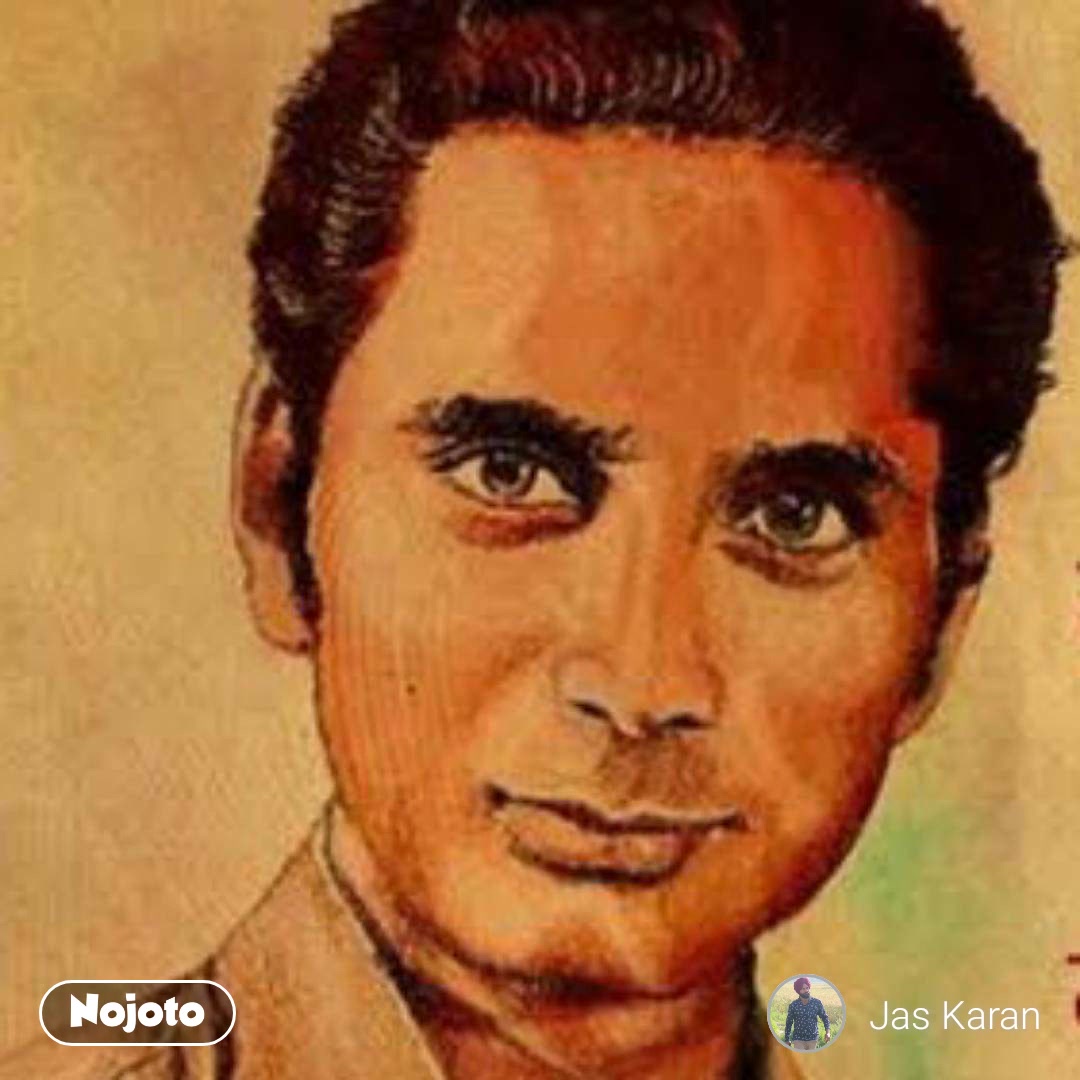सुधीर सुमन
महादेवी वर्मा ने ‘शृंखला की कड़ियाँ’ में लिखा है- ‘‘स्त्री के व्यक्तित्व में कोमलता और सहानुभूति के साथ साहस और विवेक का ऐसा सामंजस्य होना आवश्यक है जिससे हृदय के सहज स्नेह की अजस्र वर्षा करते हुए भी वह किसी अन्याय को प्रश्रय न देकर उसके प्रतिकार में तत्पर रह सके।’’
गुंजन उपाध्याय पाठक की कविताओं को पढ़ते हुए यह महसूस होता है कि उनकी कविता में इसी तरह की स्त्री दृष्टि मौजूद है।
जैसा कि एक कविता का शीर्षक है- मैं तो हिंदू हूँ। तो यह स्त्री इस देश के बहुसंख्यक समुदाय की है, उसकी रूढ़ियों और पुरुषसत्तात्मक परंपराओं से आजादी चाहती है। मिथ, इतिहास और वर्तमान सबके भीतर मौजूद वर्चस्वकारी और हिंसक पुरुष नजरिये से उसकी बहस है। इसलिए हिन्दू समुदाय में जन्म लेने के बावजूद उसका हिन्दुत्ववादी सांप्रदायिक राजनीतिक-सामाजिक दृष्टि से प्रत्यक्ष टकराव है। यह जो हिंदुत्व है, वह गैरबराबरी, दमन और नृंशसता की तमाम पुरानी परंपराओं के साथ-साथ आधुनिक पूंजीवादी दौर की बर्बरता के मेल से निर्मित है। जाहिर है कि हिंदुत्ववाद के आधार पुरुषसत्तात्मक नैतिकताएँ और तथाकथित संस्कार भी हैं, जो स्त्री की स्वतंत्रता, स्वत्व और आत्मनिर्णय के अधिकार के पक्ष में नहीं हैं।
आज कोई भी शहर ऐसा नहीं है, जहाँ दंगे की आशंका नहीं है, स्त्री हर जगह असुरक्षित है। ऐसी स्थिति में रामनवमी की छुट्टियों में किसी ऐसे शहर में जाने की तमन्ना जहाँ कोई परिचित पुरुष है, है तो स्वतंत्रता की कामना और साहस ही, पर आशंका बलवती है, क्योंकि
‘… माथे से नदारद सिंदूर, बिंदिया ,पैरों की अंगुली से गायब बिछुआ/
काफी है किसी भी कटघरे में खड़े करने को नोंचे जाने को।’
जो आशंका है, दरअसल वह हकीकत के अहसास से उपजा है, पुरुष संदिग्ध है, वह सांप्रदायिकता के वायरस के असर में हो सकता है। वह दंगाइयों की पीठ थपथपा सकता है। स्पष्ट है कि वह पुरुष भी हिंदू है और उसकी हिंदुत्ववादी दृष्टि से वह स्त्री अनभिज्ञ नहीं है। वह स्त्री जो विवेकवान है, जो छुट्टियों में किसी परिचित के शहर में जाकर उससे मिलने का साहस रखती है। लेकिन गौर से देखा जाए तो यह कविता ही एक विवेकवान स्त्री के इनकार की कविता है, वह कहना चाहती है कि मैं तुम्हारे शहर आ तो सकती थी, पर तुम्हारी सोच जिस तरह की है, उसे महसूस कर मैं आ नहीं रही हूँ। पुरुष के सांप्रदायिक होने के पीछे स्त्री का कोई पक्का यकीन है। जो इस तरह अभिव्यक्त होता है कि ‘यह दोगलेपन की कोर्स/ कहाँ होती है मेरी जान?’ वैसे इस ‘दोगलेपन’ शब्द के इस्तेमाल पर गुंजन को सोचना चाहिए, क्योंकि यह स्वयं पुरुषवादी यौन नैतिकता से बना शब्द है।
मिथ जिसे इतिहास बनाने पर हिंदुत्व की राजनीति तुली हुई है, वह ढाँचा ही पुरुषों के वर्चस्व और स्त्री के दमन पर टिका हुआ है। ‘हे तुलसीदास प्रेमी’ में गुंजन दो टूक लिखती हैं-
‘‘ढोल, गंवार, शूद्र, पशु लिखते बाँचते
तुम देते हो अपनी ही प्रिया और माँ को
ताड़न का उपहार
ताकि तुम लेते रहो हर युग में
प्रीत की अग्नि परीक्षा का प्रमाण…’’
जाने कितनी सदियों से प्रीत से भरी हुई स्त्री किसी ऐसे प्रिय का इंतजार करती है, जिसकी गंध को हवा पहचानती है, जिससे शहर या किसी जगह की पहचान है, जिसके स्पर्श की भाषा हर बारिश में मौजूद होती है। लेकिन उसे प्रायः विरह, उदासी और अवसाद ही मिलता रहता है। केवल मुहब्बत की यादें ही उसका साथ देती हैं, फिर भी वह प्रेम को ‘चवन्नी’ की तरह लुटाती रहती है। यह जानते हुए भी कि आज के जमाने में प्रेम के बदले में कोई उस तरह जहर भी नहीं देगा, जैसा मीरा को दिया गया था। मीरा के समय से लेकर आज तक की स्त्री की नियति में बहुत बदलाव नहीं हुआ है, पर प्रेम ज्यादा जटिल और मुश्किल हो गया है, प्रेम के लिए प्रतिरोध भी आसान नहीं रह गया है। किसी जमाने में स्त्री को लगता था कि रेलिया बैरिन पिया को लेके चली जा रही है, आगे चलकर मामला और स्पष्ट हुआ कि रेलिया और जहजिया बैरी नहीं है, बल्कि पैसा बैरी है, जो पिया को दूर लिए जा रहा है। आज के दौर में यह दूरी महज जीवन की बुनियादी जरूरतों के कारण ही नहीं पैदा होती, बल्कि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाएँ भी एक-दूसरे से दूर ले जाती हैं, क्योंकि जीवन में संबंधों से ज्यादा जरूरी आर्थिक समृद्धि हो गयी है। हालाँकि दूरी का तर्क भी प्रेम ही है, पर होता ठीक उलट है। स्त्री अपने अनुभव से कहती है-
प्रेम को मिलाने निकले वो समुद्री जहाज
जो निगल गए आँखें मेरी तुम्हारी
जाहिर है जिन आँखों में गहरा प्रेम होता था, अब वहाँ वैसी गहराई न रही। वैसे भी दूर जाना आज भी पुरुष के लिए ही ज्यादा सहज है। स्त्री के लिए वैसे अवसर अब भी कम हैं। तर्क भले रोजी-रोटी और जीवन के साधनों का हो।
स्त्री को लगता है कि उसके ‘सपने’ गायब हो गये हैं, जीवन की बेहद बुनियादी जरूरतों में उलझने के कारण वह प्रेम नहीं कर सकी या जिस हद तक प्रेम को समय देना चाहिए था, वह दे नहीं पायी। वैसे यह समस्या तो आज की स्त्री और पुरुष दोनों के साथ है। ‘थक रहा है प्रेम’ की अनुभूतियाँ भी प्रायः स्त्री-पुरुष दोनों को ही होती है। आलोकधन्वा की अत्यंत चर्चित कविता ‘भागी हुई लड़कियाँ’ की पंक्तियाँ कौंधती है- ‘अब तो वह कहीं भी हो सकती है/ उन आगामी देशों में/ जहाँ प्रणय एक काम होगा पूरा का पूरा।’ बेशक लड़कियों का भागना जारी रहा, पर प्रणय को लेकर जो सपना था, उसे नई परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। जीवन की तल्ख हकीकत और जीवित रहने भर के लिए जद्दोजहद ने इस कवि के उस भविष्य-स्वप्न को साकार नहीं होने दिया, जहाँ प्रणय पूरा का पूरा एक काम हो। गुंजन अपनी कविता में इस स्थिति को इस तरह व्यक्त करती हैं-
अब ख्वाबों के मरू में
जलते छाले लिए नृत्यरत है काल
ऊब के जीवाश्म पर मुँह फेरकर खड़ा है
एक और ख्वाब
जिसमें तुम्हारी परछाई तक नहीं है
दरअसल आज भी स्त्री को जिस तरह के स्वच्छंद, सहज, अकृत्रिम और गहरे प्रेम की दरकार है, उसके न होने की बेचैनी और उसके कारण पैदा विडंबनाबोध और अवसाद गुंजन उपाध्याय पाठक की कविताओं का केंद्रीय स्वर है। यहाँ प्रेम में खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाला पूराना भावबोध नहीं है, बल्कि प्रेम में अपनी पहचान और हक की आकांक्षा भी है, जिससे स्त्री वंचित है। जहाँ पानी के पारदर्शी आईने में उसका अपना ही प्रतिबिंब भी गायब है, जहाँ ‘प्रेम की हत्या का पाप है,/ वक्त के माथे की सलवटों पर’। जाहिर है यह ‘माँ’ के जमाने से भिन्न स्थिति है और चेतना के साथ-साथ अपनी नियति का स्वीकार भी भिन्न तरीके का है। पूजनीय होने के लिए खुद को बलिदान करने को वह तैयार नहीं है। जहाँ सारे बदलाव अवांछित या प्रतिकूल हैं, वहाँ वह उस छोटी-सी चिड़िया की तरह खुद को महसूस करती है, जिसके सीने में पता नहीं मीठा सा कौन दर्द है। वह उसी की तरह नेचुरल होना चाहती है, पूरी तरह सहज मनुष्य, उसे फरिश्ता होना मंजूर नहीं है- फरिश्ता मत बनना कभी भी/ जो लोगों की हसरतों को / तेंदू की पत्तियों में लपेटकर पीता है।
गुंजन की कविताओं में गहरा अवसाद है, जिससे मन ही नहीं, तन भी ग्रस्त प्रतीत होता है। पाठकों को भी ऐसी कविताएँ अवसाद में धकेल देती हैं। विरह वर्णन वाली पुरानी कविताओं से ये अधिक त्रासद हैं। यहाँ अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि यथार्थ की अभिव्यक्ति है-
हर बार की शल्य चिकित्सा के बाद
न जाने ऐसा क्या कर गुजरता था चिकित्सक
कि वह ढूँढती थी खुद को ही
और अपनी अनुपस्थिति का अंदाजा होते ही
गढ़ने लगती थी
अपना ही सा कुछ कुछ
‘इल्म’ शीर्षक कविता भी गहरे अवसाद की कविता है, जिसमें अंदेशों की झालर है, चैतन्य की कुटिलता है, बासी बसंत की गंध से महकती देह है और मौत की देहरी पर सर पटकते हुए अपनी ही मुक्ति की चाह है। मृत्यु का अंदेशा इनकी कई कविताओं में महसूस किया जा सकता है। मृत्यु की आशंका और प्रेम के अभाव से पैदा अवसाद इनकी कविताओं में प्रायः हर जगह मौजूद है। यह ऐसे प्रेमियों, खासकर प्रेम की चाह वाली स्त्री की दुनिया है, जिसमें किसी ईश्वर का सहारा भी नहीं है, बस प्रेम ही सहारा हो सकता है। वे लिखती हैं- ‘‘उदास है ईश्वर/ उसका गुड़ खट्टा हो चुका है/ बस प्रेमियों का होना भर ही/ इस जगत में अवसाद को आस में बदलता है।’’ हम कह सकते हैं कि प्रेम से उत्पन्न अवसाद से मुक्ति भी प्रेम के जरिए ही संभव है। लेकिन इस प्रेम की परख भी जरूरी है, इसकी अपनी विशिष्टता है, इसका ठोस वैचारिक आधार है, जिसे वली दक्किनी को याद करते हुए लिखी गयी कविता ‘हस्तांतरण’ को पढ़ते हुए भी बखूबी महसूस किया जा सकता है।
गुंजन उपाध्याय पाठक की कविताएँ
1. मैं तो हिंदू हूँ
रामनवमी की छुट्टियों में
सोचा तुम्हारे शहर आऊं
सीट आरक्षित होने के बावजूद भी रीढ़ में झुरझुरी सी रही
दंगो के इस दौर में
मारे जाने से पहले
किया जा सकता है बलत्कृत
मानसिक प्रताड़ना जिसकी मान कम है शारीरिक से
मुझे याद आता है
मैं तो हिन्दू हूँ
डरने की जरूरत ही क्या है
मगर माथे से नदारद सिंदूर, बिंदिया ,पैरों की अंगुली से गायब बिछुआ
काफी है किसी भी कटघरे में खड़े करने को नोंचे जाने को
और फिर भी किसी तरह पहुंच भी सकी तो,
तुम्हें, दंगाइयों की पीठ थपथपाते देख
उबकाई आने की भनक पाते
बौखला पड़ोगे
जबकि हजारों लाखों लाशों की
चलती फिरती सच्चाई को तुम
इक मजाक में उड़ा सकते हो
इस दोगलेपन की कोर्स
कहां होती हैं मेरी जान?
2. हे तुलसीदास प्रेमी
हारकर उसकी विद्वता से
तुम ढूंढ लाते हो कालिदास
छाती पीटते हुए
धर्म कर्म के मर्म पर
रच बैठते हो रामचरित
मानस का पाठ
ढोल, गंवार, शूद्र, पशु लिखते बांचते
तुम देते हो अपनी ही प्रिया और मां को
ताड़न का उपहार
ताकि तुम लेते रहो हर युग में
प्रीत की अग्नि परीक्षा का प्रमाण
तुम्हारी हीनता, तुम्हारा रोपा गया डर
देता रहा है गवाही युगों से,
तुम्हारे भीतर रहा होगा
कितना भीरूता का असर ।
3. प्रतिजैविक
मेरे हाथ टटोलते हुए अपने ही गले को
कर लेना चाहते हैं अपनी पकड़ मजबूत
कि तुम्हारी ऐनक वाली आंखें चमक उठती हैं
और यकबयक दोनो हथेलियां नाभी पर रख
याद करती हूँ तुम्हारी सरफिरी बातें
अस्फुट मंत्रोच्चार सी फूट पड़ती हैं बतकहिया हमारी
और किसी एंबुलेंस की तीखी गंध को
अपनी ही शिराओं से बहते हुए महसूस करती
औचक सी देखती हूँ तुम्हें
दूर कोई सायरन की आवाज सुनकर
पुकारती हूँ तुम्हें और प्रतिउत्तर में
उभर आए मेरे नाम से चिमटकर
मुस्कुरा उठती हूँ
हसरत का एक टुकड़ा जो चक्खा था कभी
अब भी प्रतिजैविक की तरह मुझमें फलता फूलता है
हालाँकि ईश्वर की बेबसी
चिपकी हुई रहती है किसी दुआ मागंते होठों पर
और बच्चो की सिसकियां
उसे चुभती हैं रात भर
4. चवन्नी
कभी आना हुआ
तो आना इस शहर भी
जहाँ की हवा बिना तुम्हे देखे
पहचानती है तुम्हारी गंध
और यहाँ की हर बारिश में छुपी हुई है
तुम्हारे स्पर्श की भाषा
कभी आना हुआ
तो आना इस शहर भी
जहाँ बदरंग हो गए हैं
पंख तितलियों के
जुगनुओं की रोशनी को
वक्त से पहले लग गई है ऐनक
और जहाँ गोरैया से किये जाते हैं
उनके पंखों के सौदे
उनकी हंसी के बदले।
कभी आना हुआ
तो आना इस शहर भी
जहाँ जीवन के हाट बाज़ार में
तुम्हारी प्रेम चवन्नी के बदले
मैं आज भी लुटाती हूँ
मौसम बेबरस के…….
5. हुक्का
बेकली सी रातों में नाचते हैं गिद्ध
पारिस्थितिकी का हुक्का पीते हुए चीखते हैं प्रेत
हवाला देती है ठिठुरती ठंड
रूठी चांदनी की आंखों में बहता है रक्त
समेट कर रख लेती हूँ आसमां सिरहाने अपने
ह्रदय के अगल बगल लगी चिमटी
जोकि नापती है नमी मुहब्बत की
और सुलग जाते हैं बुरांश मेरे होठों पर
बेदिली में झकझोरती हैं यादें
उन लम्हों को
जो किस्मत में मेरी कभी थे ही नहीं
6. किस्सागोई
रीढ़हीन कोशिकाओं की शिराओं में
रक्त की जगह बज उठती है
कॉफी की सुरसुराहट
दीवारों पर डूब जाती है इक परछाई
और जहाज उभर आते हैं तुम्हारे नवीनीकृत ऐनक पर
पर अफ़सोस
सुकून की बंदिशें
खदबदाती हैं जेहन में
मगर कुछ बातें, रातें सिर्फ़ और सिर्फ़
किस्सागोई होते हैं
7. तिल गुड़
इस जीवन के बीते कितने ही कालखण्डों में
एक ख्वाहिश बार बार दस्तक देती रही
तेरे हाथों से खा कर गुड़ तिल
मैं होना चाहती रही हूँ तुम्हारी ऋणी
उस पल की जो हमारे जीवन में कभी रहा ही नहीं
उदास है ईश्वर
उसका गुड़ खट्टा हो चुका है
बस प्रेमियों का होना भर ही
इस जगत में अवसाद को आस में बदलता है
तुम जो अपने शब्दों में सोचते हो मुझे
अनजाने ही
उन लम्हों में
रचते हो कोई भूला बिसरा गीत
और फिर उन तरंगों पर
नृत्य करता कोई तय करता है
अपने अस्तित्व से अनस्तित्व की यात्रा
8. भोले प्रेम
रिपोर्ट जिसमें टंका था
आत्मा की दीवारों पर सीलन से
जम गई थी फफूंद और
धड़कनों की फिसलन पर
छाती से उठती हौल के वक्त,
कराहती हुई जब देखा वक्त
तो चाहा यही कि
यह चाहे कोई भी दिन हो
तुम रहो कार्यालय में
बहुतेरे फाइलों और योजनाओं के प्रति
निभाते हुए अपनी प्रतिबद्धता
जब देखो, मेरे मरने की ख़बर
रो सको, चीख मारकर
वरना गुमसुम जो यूं ही रहोगे
और कोसोगे खुद को
ओ मेरे भोले प्रेम
क्या तुम जानते नही थे
यह एक बेहद निर्ल्लज राज्य था
जहाँ कोई तुम्हें मीरा की तरह विष भी न देगा
9. सपने
पेंसिल से पेपर पर कुछ उकेरते हुए
पूछता है
आपके सपने?
मैं हड़बड़ाते हुए टटोलती हूँ
रात के आले से गायब हो चुके सपनों को
कोई शौक़?
मैं जोर डालती हूँ दिमाग़ पर
मगर वह भी नदारद
जी आपके दोस्त?
सब खैरियत से हैं और जी रहे हैं
प्रेम?
कर न सकी,
बेहद बुनियादी जरूरतों में उलझी
कोई रंग?
मैं जल्दी से .. नीला !
दवाईयो की पर्ची देते हुए दुकानदार
सवालिया निगाहों से टटोलता है
मैं, और भाई कहां, किस गांव के हो तुम….?
जबकि सवालों की मुस्तैदी
और जवाबों के नदारद होने को
बीते कुछ बरस हो चुके थे .. !
10. थक रहा है प्रेम
खिड़कियों पर चांदनी थपकी देती है
चांद ने सारी किताबे फेंक दी है
चिड़ियों को माइग्रेन हुआ है
और पेड़ चीखता हुआ बोलता है
सांझ आत्महत्या के बहाने ढूंढती है
परखनली सूख गई है आंसुओ में डूबी रात की
पहर पहर चाक पर घूमता ही नही है वक्त
कट कर गिरते हैं उसके जज़्बात भी
कवयित्री गुंजन उपाध्याय पाठक नई पीढ़ी की समर्थ व सशक्त कवयित्री हैं। पीएचडी (इलेक्ट्रॉनिक्स) मगध विश्वविद्यालय। दो कविता संग्रह १.अधखुलीआंखों के ख़्वाब
२.दो तिहाई चांद
(बोधि प्रकाशन से प्रकाशित)
समकालीन स्त्री कविता में एक उभरता हुआ नाम उनसे gunji.sophie@gmail.com पर बात की जा सकती है।
टिप्पणीकार सुधीर सुमन साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यकर्ता. ‘समकालीन जनमत’ का लगभग 15 वर्षों तक संपादन, फिलहाल संपादक मंडल में।
लगभग 20 मंचीय और नुक्कड़ नाटकों में अभिनय। नुक्कड़ नाटकों और बाल नाटकों का लेखन। लगभग अस्सी समीक्षाएँ, आलोचनात्मक लेख और समसामयिक विषयों पर आलेख, कविताएँ और टिप्पणियाँ विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित। लंबे समय तक जन संस्कृति मंच, बिहार के सचिव की जिम्मेदारी निभायी। दूरदर्शन के सेंट्रल आर्काइव में पाँच साल से अधिक समय तक भाषा विशेषज्ञ और ट्रांस्क्राइबर का काम किया। सिनेमा, डाक्यूमेंट्री और चित्रकला से संबंधित छिटपुट लेखन। संजीव की कहानियों पर पी-एच. डी.। यशपाल की कहानियों में नैतिकता बोध विषय पर लघु शोध प्रबंध।
फिलहाल झारखंड के एक काॅलेज में अतिथि शिक्षक के बतौर हिन्दी साहित्य का अध्यापन। सम्पर्क: 09431685572