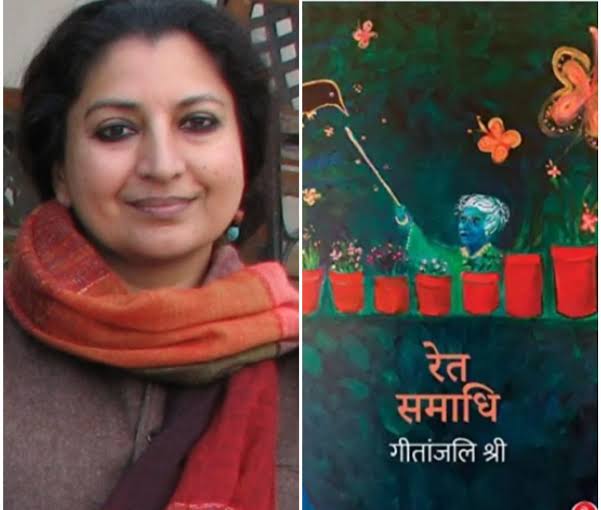प्रियदर्शन
अपने जीवन के उत्तरार्ध में श्रीकांत वर्मा सत्ता-संस्कृति के प्रति अपने आकर्षण और कांग्रेस से अपने जुड़ाव की वजह से हिंदी साहित्य में पर्याप्त- और काफी कुछ उचित- भर्त्सना झेलते रहे। उसी दौर में शायद किसी रचनात्मक पश्चाताप की तरह, राजनीतिक विचारहीनता के ऊसर को बहुत करीब देखते हुए और सत्ता तंत्र के खोखले होते जाने के अनुभव को महसूस करते हुए उन्होंने ‘मगध’ संग्रह की कविताएं लिखीं। मगर आज की तारीख़ में उनके राजनीतिक हस्तक्षेप की कोई स्मृति शेष नहीं है जबकि उनकी कविता लगातार प्रासंगिक बनी हुई है।
रविवार को दिल्ली के एलटीजी प्रेक्षागृह में उनकी कविताओं पर आधारित नाट्य प्रस्तुति ‘मगध’ देखते हुए खयाल आता रहा कि 80 के दशक में श्रीकांत वर्मा जिस संकट की शिनाख्त कर रहे थे, वह 21वीं सदी के दूसरे दशक में कुछ और गहरा गया है। हमारे समय में विचारों की कमी है, नागरिकों का प्रश्न पूछना निषिद्ध है और राज्य की सुरक्षा और शांति के लिए यह जरूरी है कि सब भयभीत रहें, सत्ता से डरें।
कविताओं का नाट्य रूपांतरण कभी आसान नहीं होता, लेकिन उनमें निहित आंतरिक तनाव की स्थिति और उससे पैदा हो सकने वाली नाटकीयता अक्सर रंगकर्मियों को कविताओं की ओर खींचती हैं। खास तौर पर राजनीतिक आशयों और समकालीन संदर्भों से लैस कविताएं दृश्य और संवाद दोनों की बड़ी संभावना पैदा करती हैं। ऐसी बहुत सारी कविताएं और रंग प्रस्तुतियां हैं जिन्हें इस सिलसिले में याद किया जा सकता है।
यह स्वीकार करूं कि रविवार को ‘मगध’ का मंचन देखते हुए जो बिल्कुल प्राथमिक ख़याल आया, वह यही था कि श्रीकांत वर्मा की कविता जो स्वायत्त अर्थ देती है, यह नाट्य प्रस्तुति उससे अलग अपने एक अर्थ का संधान करने की कोशिश कर रही है- शायद इसलिए कि कविताओं में जो संशय, करुणा और हिचक है वह प्रस्तुति में एक तरह के निश्चय कुछ ‘लाउड’ किस्म के अनुभव में बदल रही है। शायद इस राय की एक वजह वह प्रारंभिक पार्श्व संगीत और ध्वनि प्रभाव भी था जो कुछ हल्का होता तो ज़्यादा संप्रेषणीय होता।
लेकिन कहना होगा कि नाटक जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया, कविता और प्रस्तुति का तारतम्य आपस में जुड़ता गया। अब हमारे सामने बस संवादों में बदली कविता नहीं थी या उन पर निर्मित दृश्य नहीं थे, बल्कि एक पूरी समग्रता थी जिसमें श्रीकांत वर्मा का काव्य तत्व अपनी बहुत सारी अनुगूंजों के साथ मौजूद था और अर्थों की वे परतें खोल रहा था जिन्हें सामने लाना इन कविताओं का ध्येय रहा होगा। हमारे सामने मगध, कोसल, काशी, अवंती, श्रावस्ती, हस्तिनापुर इतिहास और स्मृति से बाहर आकर बिल्कुल आज का यथार्थ रच रहे थे। निरे राजनीतिक अर्थों में नहीं, बल्कि गहरे मानवीय अर्थों में भी यह प्रस्तुति आज के बंजर को कुछ इस तरह सामने ला रही थी जिस तरह किसी और माध्यम में संभव नहीं हो पाता। जो समाज सच कहने का साहस न रखता हो, सच सुनने को तैयार न हो, सच को समझने का विवेक खो चुका हो, जहां एक हिंसक आक्रामकता सारे विचार-विमर्श को विस्थापित कर उसकी जगह ले चुकी हो, जहां भय को एक मूल्य की तरह प्रस्तावित किया जा रहा हो, वहां सच को इसी तरह रखा जा सकता है कि वह बाहर से पकड़ में न आए लेकिन बिल्कुल अंतर तक चोट करे।
प्रस्तुति में सिर्फ़ ‘मगध’ की ही नहीं, श्रीकांत वर्मा की दूसरी कुछ कविताओं का भी इस्तेमाल था। निर्देशक ने बहुत कल्पनाशील ढंग से कभी इन्हें छोटे संवादों की तरह इस्तेमाल किया, कहीं-कहीं एकालाप की तरह और कहीं कहीं सामूहिक अभिव्यक्ति की तरह।
इन कविताओं को जोड़ते हुए 75 मिनट तक दर्शकों को बांधे रखना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन मानना होगा कि दर्शक प्रस्तुति से बंधे रहे। कोसल की विचारविपन्नता, बिखरी हुई वैशाली में अंबापाली का अकेलापन, बार-बार पकड़ में न आता मगध, अश्वारोहियों की बेचैनी, मणिकर्णिका का दुख, जीवित और मृत के बीच का भेद भूल गई काशी, मारा गया रोहिताश्व और रोहिताश्व को पुकारते एक पिता का कातर विलाप- यह सब एक बड़ा दुख रचते रहे- जिसमें इतिहास की स्मृति भी थी और वर्तमान के संकट की अभिव्यक्ति भी।
हालांकि नाटक जहां खत्म होता है, वहां शायद कुछ खालीपन रह जाता है जो अमूमन नाटकों के स्थूल व्याकरण के विरुद्ध मालूम पड़ता है। फिर भी पूरी प्रस्तुति असंदिग्ध तौर पर प्रभावशाली है। यह ज़रूरी है कि हम इस मगध को पहचानें।
फिल्मेरा नाटक की इस प्रस्तुति के लिए कविताओं का नाट्य रूपांतर अमितेश कुमार और दिलीप गुप्ता ने किया, निर्देशक भी दिलीप गुप्ता ही थे।