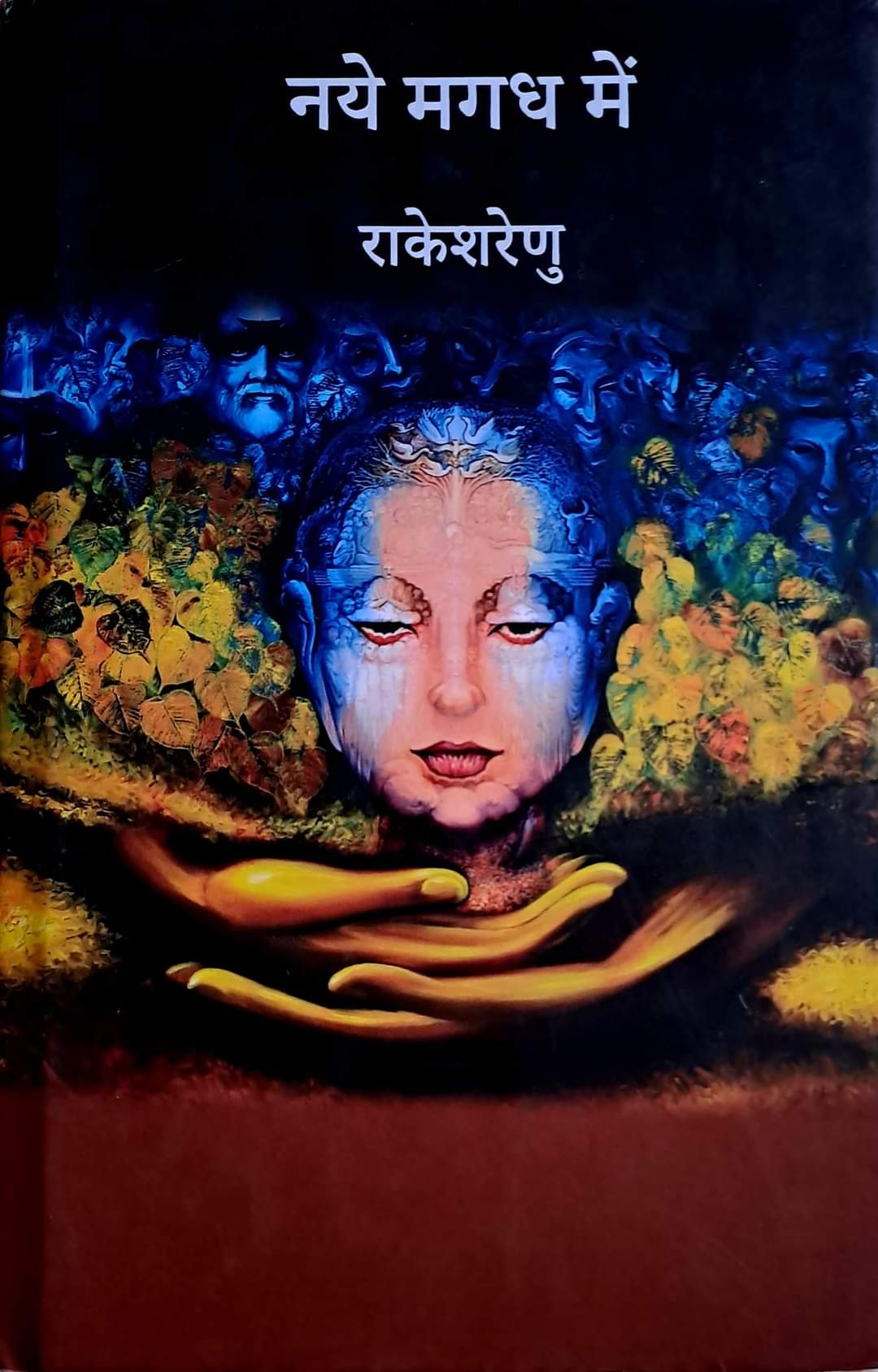योगेश प्रताप शेखर
श्रीधर करुणानिधि के दो कविता–संग्रह प्रकाशित हुए हैं | ‘खिलखिलाता हुआ कुछ’ और ‘पत्थर से निकलती कराह’ | उन का पहला कविता – संग्रह ‘खिलखिलाता हुआ कुछ’ 2018 ई. में प्रकाशित हुआ था | दूसरा संग्रह 2020 ई. में जहाँ पहले संग्रह में श्रीधर जी की अधिकांश कविताएँ प्रकृति और जीवन के कोमल प्रसंगों से जुड़ी थीं वहीं दूसरे संग्रह की कविताएँ वर्तमान समय के क्रूर, हिंसक और कुटिल स्वरूप को स्पष्ट करती हैं | उस की कविता यथार्थ के अनेक रूपों को पकड़ हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं |
पिछले कुछ वर्षों में भारत में सांप्रदायिकता का नए सिरे से उभार हुआ है | आज का समय हमारे सामने अनेक तरह के संघर्ष और चुनौतियाँ लाया है | घोर निराशा–हताशा के वातावरण में असली समस्या इनसे मुक़ाबले की है| निश्चय ही यह मुक़ाबला ठोस वैचारिकता और सामूहिकता से ही संभव है | श्रीधर की कविताओं में सामूहिक संघर्ष की बात भी हैं और प्रतिरोध की वैचारिकता भी|
कोई भी लड़ाई सब से पहले सवाल पूछने से शुरू होती है | व्यवस्था, तंत्र, बाज़ार और सत्ता यह कभी नहीं चाहते कि सवालों को सामने लाया जाए | इसीलिए सत्ताएँ हर युग में सवाल पूछने वालों को सजा देती आई हैं | सत्ता यही चाहती है कि उसे सवालों से परे मानकर देवता का दर्ज़ा दे दिया जाए | वास्तविकता यह है कि इंसान का पूरा विकास ही उस के सोचने और सवाल पूछने से हुआ है | सवाल इंसान के प्राण हैं |
आज भारत में लोकतंत्र है | पर यह लोकतंत्र भी तभी बचेगा जब हर व्यक्ति बिना किसी डर के सवाल पूछ पाए | यह अत्यंत दुखद है कि भारत में अभी सवाल पूछ्नेवालों को ‘देशद्रोही’ तक कहा जा रहा है | कवि ने सत्ता से सवाल करने की प्रक्रिया और सत्ता में विलुप्त होती मानवीयता का बेबाकी से चित्रण किया है |
भूमंडलीकरण और पूँजीवाद के गठजोड़ ने समकालीन समय में मानवीयता को एकदम किनारे-सा कर दिया है | इस सच्चाई से अभी का कोई भी कवि मुँह नहीं मोड़ सकता | इस कठोर सच का सामना रोज़ करना होता है | मानवीयता को हर दिन जैसे क्षरण का शिकार होना पड़ता है | एक ऐसी चकाचौंध हमारे इर्द– गिर्द है कि रोशनी का कहीं कुछ पता नहीं | मनुष्य तो मनुष्य इस निर्दयी स्थिति के शिकार पशु, पक्षी और पर्यावरण, सभी हो रहे हैं| जैसे-जैसे मानवीय सभ्यता आगे बढ़ती जा रही है वैसे–वैसे पिछली शताब्दियों में अर्जित आधुनिकता और विकास के पैमानों पर सवाल भी खड़े होते जा रहे हैं | इन में सब से प्रमुख पर्यावरण का मुद्दा है |
विकास और प्रगति की मनुष्य केंद्रित अवधारणा ने न केवल दूसरे जीवों के बल्कि पूरी पृथ्वी के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया है | दूसरा मुद्दा मनुष्य की संवेदनशीलता का है| इन सब को ख़ूब अच्छी तरह से समझते हुए श्रीधर करुणानिधि अपनी कविताओं में इस की आलोचना प्रस्तुत करते हैं |
किसी भी कवि के विकास के लिए ज़रूरी है कि वह यह सवाल बार- बार ख़ुद से पूछता रहे कि जीवन और कविता का रिश्ता क्या है ? साहित्य की मूल प्रकृति पर भी वह बार – बार विचार करता रहे| हर कला और साहित्य एक ही साथ अभिव्यक्ति और प्रतिरोध दोनों है| हर कला अपने माध्यम को उस की जड़ता से मुक्त कर के उसे एक अलग स्वरूप देती है| यही उस का प्रतिरोधी रूप है| उदाहरण के लिए यदि हम कागज़ पर चित्र बनाते हैं तो उस पर उकेरा गया रंग उस कोरे कागज़ को निपट ‘कागज़पन’ से मुक्त कर देता है| चित्रांकन के बाद वह केवल कोरा कागज़ ही नहीं रह जाता| यही स्थिति शब्दों की भी है| साहित्य में प्रयुक्त शब्द केवल शब्द रह नहीं जाते वे संघर्ष, यथार्थ और स्वप्नों के वाहक हो जाते हैं|
श्रीधर जी की प्रेम कविताओं में निश्चय ही कोमलता है पर उन में भोलापन नहीं है| इन कविताओं में हृदय की गहरी संवेदना तो है ही पर साथ ही कई जगहों पर इस दुनिया के लगातार प्रेम विरोधी होते जा रहे स्वरूप का कठोर साक्षात्कार भी है|
श्रीधर करुणानिधि की कविताएँ निश्चय ही हमारे समय के यथार्थ का अंकन करती हैं| ये कविताएँ इंसानियत को बचाए रहने की जद्दोजहद और मानवीय अस्तित्व को बरक़रार रखने की प्रक्रिया के साथ खड़ी हैं | यह इस ज़िद को भरोसा तथा हिम्मत देता है कि समकालीन समय, तंत्र, सत्ता एवं बाज़ार हम मनुष्यों को जितना भी ‘पत्थर’ बनाना चाहें, हम इस से इनकार कर जीवन की सहजता, सहजीविता और साहचर्य के पक्ष में संघर्ष करते रहेंगे|
श्रीधर करुणानिधि की कविताएँ
1.गुमाश्ते नींद के
नींद के गुमाश्ते
रात के आखिरी पहर में
मौका देखकर आ धमकते हैं
और रतजगा छीन ले जाते हैं
रतजगों की भी अपनी दुनिया होती है
कई बार रतजगों पर चाँद की भी बेतरह नजर होती है
सुबह होते ही वह
छुपते-छुपाते सारी स्याह खबरें इकट्ठी कर लेता है
गुमाश्ते अक्सर अपनी जकड़ में लेने के बाद
हाथ-पैर फैलाकर सोने की तसदीक करते हुए
सरकारी मुलाजिम की तरह व्यवहार करते हैं
जिसे सिर्फ महँगाई भत्तों और वेतन वृद्धि से मतलब होता है
कौन कहाँ मर रहा?
भीड़ की हत्याएं?
बेरोजगारी?
वे हँसते हैं और कहते हैं
“बकवास सुनते हुए तुम्हारा कान नहीं पकता?”
मौसम ठंडा है
चुपचाप सो जाओ
कुछ नहीं हो रहा….
2. ऐ रात के काफिर!
यकीन मानो
मैंने नहीं पुकारा तुम्हें
तुम हो या नहीं हो
चाँद की आग में हो
या नींद की धूप में…
धागा जो रेशम का
उड़ रहा है
हो उसमें
या हो
काले आसमां में उड़ते परिंदे
के रोएँदार पँखों में
अगर नहीं तो
क्यों अँधेरे को जिलाए रखने में
चाँद की साज़िश ढूंढता हूँ
और फिर उसी की खातिर
नीम के पत्तों में घुसता हूँ
हवा होकर
तुम्हारे लिए
तुम्हीं को
सिफारिश के दो शब्द कहता हूँ
3. आकार
हर प्यारी चीज भरोसा देती है
अगर यह वाक्य गलत नहीं है
तो तमाम ‘नहीं’ के बीच जरूर
एक छोटी सी ‘हाँ’ भी रहती होगी
असंख्य लम्बी पैदल यात्राओं की शुरुआत के
एक नन्हे कदम की तरह
घर में रखे तमाम संदूकों में से
एक छोटे से गुल्लक को
प्यार का भरोसा देकर
कभी मैंने कहा था ‘हाँ’
‘हाँ’ बहुत छोटा था
शब्द के औसत आकार से भी छोटा
वह सफेद ही था
बिलकुल सफेद
लेकिन उसे कोई काला भी कह देता तो
इससे इस बात से वास्ता नहीं होता
कि ‘काली दिखती वस्तु सफेद नहीं हो सकती’
या ‘सफेद दिखती वस्तु में कालिख नहीं खो सकती’
काश कि भरोसे के दर्द को समझ कर
मैं एक शब्द ‘हाँ’ के आकार का
फिर से बचपन की तरह लिख पाता
4. कबूतर की बंद आँखें
छुट्टा सांड को पुचकारने से
वह फुफकारने लगता है
उसकी जांघ फड़कने लगती है
उसके नथुनों की गर्म हवा से
इतिहास के नाजुक अध्याय जलने लगते हैं
और वह नरभक्षी हो जाता है
अब वह चारों ओर दौड़ता जाता है
रौंदते हुए…चिन्हित जगहों को
अपनी पीठ की खुजली के लिए इस्तेमाल करते हुए
मजे से पागुर करता है
उसकी दिग्विजय यात्रा का गुण गाते भांड
जब उसकी छाती को चौड़ी और सींग को
ब्रह्मास्त्र बताने की परले दर्जे की हरामखोरी में
दिन-रात जुटे होते है
तब वह लोगों के मुंह में
अपनी सिंग धुसेड़ रहा होता है
उसे चीथ रहा होता है
ये इत्तेफाक है कि साजिश
सारे कैमरे और सारी चौकन्नी आँखें
बकरी की तरह घास चरने चली गई हैं
सारे कबूतरों ने अपनी-अपनी आँखें बंद कर ली हैं
आपस में यह गुटरगूं करते हुए
कि नहीं…आँखों के सामने कुछ नहीं हो रहा है….. कुछ नहीं
कोई सांड फुफकार नहीं रहा
अपने खुरों से रौंद नहीं रहा
5. अंधेरे के हादसे
सबकी अपनी रातें होती हैं
सबके अपने दिन
हादसों वाली शामों के बारे में
हमारे ख्याल
ऑक्सीजन उगलती पत्तियों में
दुबकी हुई एक सुबह की तरह होती है
जिसे पतझड़ का पता नहीं होता
वैसे तो हर सुबह की आँखों में
एक शाम का अंखुवाया मंजर छिपा होता है
हर शाम की अंधियारी हवा में
एक सुबह का फतिंगा फड़फड़ा उठता है
गर्दिश में चले गए उल्लास में
अब हादसे ही इतने सहज हो गए हैं
कि उनसे कभी भी हाथ मिलाया जा सकता है
जब रात
दिन के वक्त भी
किसी अनजान पक्षी की तरह
पंख तौलती हुई आती है
भय के पार
एक और बड़ा भय
चमगादड़ों की तरह लटक कर
करता है इंतजार….
हादसों के आगे….
6. दिया गया बयान
कानून की धाराएँ अपनी जगह थीं
दुनियादारी अपनी जगह
एक हत्यारे के न्यायकर्ता बन जाने के लिए
जिस इल्म की जरुरत थी
वह किसी शिल्पी के पास नहीं
उसी स्वनामधन्य हत्यारे के पास था
कानून की सारी किताबों को धता बताते हुए
जब उसने एक सधी हुई भाषा में बयान दिया
न्याय की गुहार लगाने वालों के ऐन सामने
तब छंद और लय के दीवानों ने कहा
आज से एक नया युग शुरू हो रहा है
कवियों ने कहा ‘सच’ और ‘झूठ’ के बीच
भाषा की नाजुक दीवार आज गिर गई है
इतिहासकार हैरान परेशान काल की गणनाओं में
मशरूफ हो गए हक्के बक्के…
हाथ जोड़कर खड़े हुए
न्याय की गुहार लगाने वालों के सामने
उसने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा
“निराश न हो ! अब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे”
मित्रो! न्याय के पक्ष में दिया गया
उसका आखिरी बयान नहीं है
जयघोष के साथ इस बयान की एक-एक कॉपी
न्याय की गुहार लगाने वाले को थमाकर
वह न्यायकर्ता
दूर यात्रा पर
किसी और को न्याय सुलभ कराने
निकल गया है….
7.प्यास ही ठहरती है प्रश्न की तरह
जितने आए उतने ही नहीं गए बाहर
कुछ सड़-गल गए
कुछ टिक गए..
जो टिका कर बैठ गए ‘अब उठा के तो देखो’ वाली मुद्रा में
वे बिके जा रहे हैं रोज थोड़ा-थोड़ा
क्रांति को अपनी कांख में दबाकर
ऐन चौराहे पर पटखनी दे देते हैं
और मुंह बिचकाए शामिल हो जाते हैं
उस भीड़ में जिसे जनतांत्रिक भाषा में ‘अवसर’ कहते हैं
एक प्यास ही थी
जो गले में प्रश्न की तरह ठहर सकती थी
उसे भी मीडिया की भड़वागिरी ने निगल लिया
सिर्फ एक आदमी की इच्छा इतनी बड़ी हो गई
सारे चैनलों को चिल्ला-चिल्ला कर
हर नागरिक के माथे पर गोबर की तरह
मैं ‘राष्ट्रप्रेम’ हूँ, ‘मैं राष्ट्र प्रेम हूँ’ का स्लोगन थोपना पड़ा
जिसे तुम इशारा कहते हो
वह एक आदेश है जिसे
हर कोई इतनी आसानी से मान जाता है
कि उस प्यास के पास भी वो प्रश्न नहीं बचता
बचती है खाली एक तरलता
जिसे गले की खराश के लिए बचा के रखना होता है
कि कोई प्रश्न
जिसे राजनीति कहते हैं
उस तरफ से ‘देशद्रोह’ की तरह टंग न जाए..
8.मनौअल
उसने कहा ‘यही’ सही है
फिर कहा भला इसी में है कि
मैं सच को ‘ऐसा ही’ मान लूँ
ऐसा कहते वक्त वह मुझे इस दुनिया में
सच का एकमात्र ठेकेदार लगा
उसने मेरी सारी पुरानी गलतियाँ
तस्तरी में सजा कर
मेरे सामने नाश्ते की तरह रखीं
और हौले से मुस्कराया
रोने को हँसना मान लेने
और मौत के आंकड़े को छिपाने की खातिर
मेरे मुँह पर नोटों की गड्डी फेंकने की तरह
मलमल का रूमाल फेंका
जैसे वह कोई जादूगर हो
वह मुझे ‘ऐसा ही’ मानने के लिए
और ‘ऐसा ही’ कहने के लिए
किसी फाइव स्टार होटल में
डील के लिए ले जाता है..
इस तरह कार्पोरेट मैनेजमेंट का उस्ताद वह
कोई भी डील छुट्टा जाने नहीं देता
माना कि बहुत नखरेबाजी में यकीन नहीं करता
सीधे काम करता है
मनाने की खातिर
वह अपने गोडाउन से
बोरे का बोरा भिजवाता है
पेट की क्षमता से
ज्यादा ही ढूंस देता है मुंह में
शालीनता से बात करता है
और गाहे बगाहे यह भी कह देता है
कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भाई!
मानना न मानना तुम्हारे हाथ में है….
9. झुनझुने का पेड़
वह था तो एक पेड़ ही
लेकिन साबुत पेड़ को झूठ से फेंट देने पर बना हुआ
थोड़ा ‘टनकाहा’, चढ़ो तो डाल ही ‘लचक’ जाए
फल से कोसों दूर बेकाम का..
.
बचपन इस नाम के खिलौने से शुरू होता था
तब झूठे दिलासे की झूठी आँच
वहाँ नहीं पहुँची होती थी….
कथा-कहानियों के रास्ते घूम फिर कर
झूठे से चाँद की ओट से वह बचपन में कैसे घुसता
यह ओट देने वाले चाँद
को भी नहीं पता…
हमें या तो पेड़ों के फल से प्यार होता
या उसकी मजबूत देह से
उसके हरेपन को हम सपनों में भी बिछा नहीं सकते
हरे पत्ते भी किसी काम के नहीं
हम तो अपने किवाड़, खिड़कियाँ, पलंग
मजबूत और इमारती दरख्त की उम्मीद से निकालने की सोचते
लेकिन झुनझुने का पेड़!
झूठ की उम्मीद पर कमजोर देह की तरह बड़ा होता
वह कटकर गिरता नहीं कभी
बस झूठी उम्मीद की तरह
चोर दरवाजे से बचपन से लेकर जवानी तक
झूठे दिलासे की तरह बड़ा होता रहता…
वह तो अपनी जगह कायम था
बस झूठ ही बढ़ रहा था हर वक्त…
10. चीखें कहीं गुम हो जाती हैं
आवाजें शोर में बदल जाती हैं
पुकार धीरे-धीरे कराहों में
तब चीखों के लिए चीखने का
और समय के पास
क्षत-विक्षत शवों की शिनाख्त कर सकने का
वक्त नहीं रह जाता
बहुत दूर जाकर
एक बच्चे ने कहा कि अब घर केवल सपनों में दिखता है
अपनी पटरियों पर अनंत काल तक चलती हुई
ट्रेन ने जब भटककर पूछा यह कौन सी जगह है
तभी लगा स्थापित चीजें गड्ड-मड्ड हो गईं हैं…
हँसी ने होठों से कहा अपनी पपड़ी का ध्यान करो
भूख ने पेट से कहा सब्र करो यह जानते हुए
कि सब्र भी सीमाओं से परे नहीं है…
प्यास ने किसी से कुछ नहीं कहा
वह किसी सूखे गले में मल्हार की तरह बजने लगी…
चीख के भीतर खुद इतनी चीख थी कि
वह चीख भी न सकी
घर अब सुकून का इत्र हो गया
सारे बेघरों के लिए…
फैक्ट्री और दफ्तर के सामने
एक बेचैनी की पोटली उम्मीद की तरह रखी है
कि खुलते हीं जाने उससे क्या निकले?
एक ठेला-गाड़ी
एक रिक्शा
एक साइकिल
एक ट्रक
सब चल रहे हैं बेहोश चालकों के सहारे
जो नींद में भी बुदबुदाते हुए
पुकारते हैं घर को
भूख और प्यास को आवाज लगाते हैं
जिंदगी के महीन धागों को पकड़े हुए…
आवाजें कहाँ पहुंच रही हैं!
कहीं पटरियों पर बिछी नींद में
खून के छींटें उड़ते हैं
कहीं सड़कों पर रफ्तार की गिरफ्त में आए
हुए लोगों की आहें
हवा में तैरती रहती हैं ध्वनि तरंगों की तरह
पर हम तक नहीं पहुंच पातीं…
कवि श्रीधर करुणानिधि
जन्म पूर्णिया ,बिहार के एक गाँव में
देश भर की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं और वेब मेगजीन आदि में कविताएँ, कहानियाँ और आलेख प्रकाशित। आकाशवाणी पटना से कहानियों का तथा दूरदर्शन, पटना से काव्यपाठ का प्रसारण।
प्रकाशित पुस्तकें-
1. ’’वैश्वीकरण और हिन्दी का बदलता हुआ स्वरूप‘‘(आलोचना पुस्तक, अभिधा प्रकाशन, मुजफ्फरपुर, बिहार
2. ’’खिलखिलाता हुआ कुछ‘‘(कविता-संग्रह, साहित्य संसद प्रकाशन, नई दिल्ली)
3. “पत्थर से निकलती कराह”(कविता संग्रह, बोधि प्रकाशन, जयपुर से प्रकाशित)
4. ‘अँधेरा कुछ इस तरह दाखिल हुआ(कहानी-संग्रह), बोधि प्रकाशन से रामकुमार ओझा पांडुलिपि प्रकाशन योजना 2021 के तहत प्रकाशित
संप्रति-
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, गया कालेज, गया( मगध विश्वविद्यालय)
सम्पर्क: 09709719758, 7004945858
Email id- shreedhar0080@gmail.com
टिप्पणीकार योगेश प्रताप शेखर दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया(बिहार) में हिंदी के सहायक प्राध्यापक हैं. ‘हिंदी के रचनाकार आलोचक’ पुस्तक प्रकाशित है. विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में समसामयिक एवं उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर लेखन।
सम्पर्क:9631952649
ईमेल: ypshekhar000@gmail.com