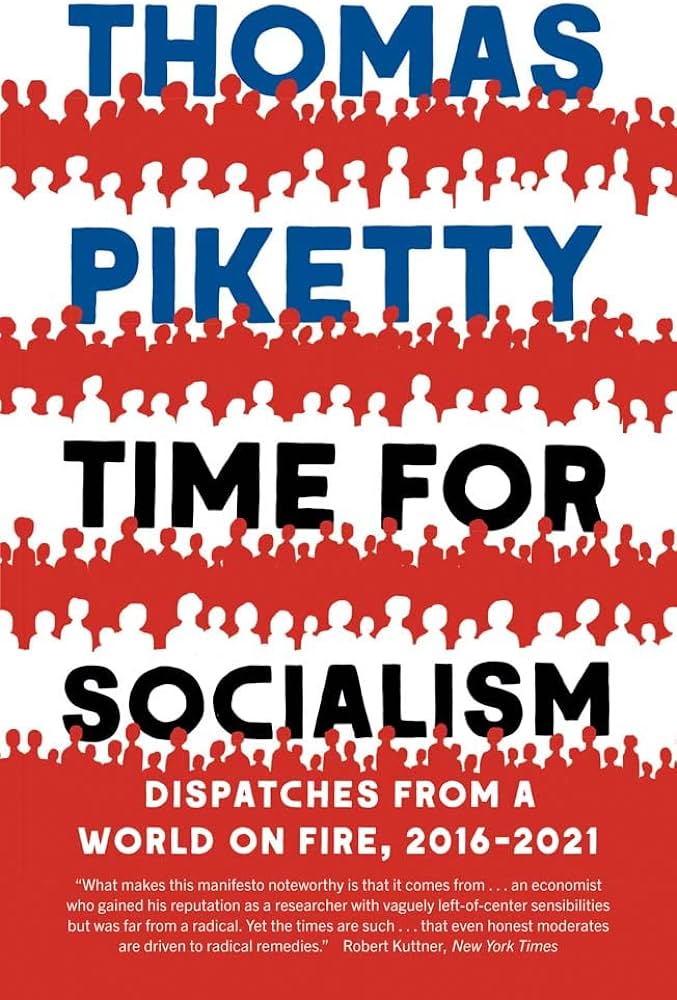2021 में येल यूनिवर्सिटी प्रेस से थामस पिकेटी की फ़्रांसिसी में 2020 में छपी किताब का अंग्रेजी अनुवाद ‘टाइम फ़ार सोशलिज्म: डिसपैचेज फ़्राम ए वर्ल्ड आन फ़ायर, 2016-2021’ का प्रकाशन हुआ । अनुवाद क्रिस्टीन कूपर ने किया है । पिकेटी का कहना है कि अगर तीस साल पहले किसी ने इस किताब के लेखन की भविष्यवाणी की होती तो उसे वे भद्दा मजाक ही समझते । उस समय तो समाजवादी सत्ता के ढहने की खबरें सुनायी देती थीं । उस समय लेखक उदारपंथी थे । इस नाते वे रोमानिया के चाउसेस्कू से मुक्ति की खुशी में शामिल थे । 1971 में लेखक का जन्म हुआ था इसलिए वे उस पीढ़ी के नहीं थे जिसे कम्युनिज्म का आकर्षण था और युवा होने तक समाजवाद की समस्या प्रत्यक्ष हो चली थी । उन्हें बुजुर्गों के अतीतमोह से चिढ़ होती थी । बाजार अर्थतंत्र और निजी पूंजी को ही समाधान न मानने वालों से उनकी सहमति नहीं थी । अब तीस साल बाद पूंजीवाद की गति देखकर उन्हें शंका हो रही है । अब तो पूंजीवाद का कोई विकल्प ही नयी राह खोल सकता है । अब नये तरह के समाजवाद की जरूरत है जो भागीदारीपरक और विकेंद्रित, संघीय और लोकतांत्रिक, पारिस्थितिकीय, बहुनस्ली और नारीवादी होगा । समाजवाद की धारणा को बचाने और फिर से जगाने की जरूरत महसूस हो रही है । पूंजीवाद के विकल्प के बतौर खड़ा होने वाली अर्थव्यवस्था को यही नाम देना होगा । फिलहाल पूंजीवाद या नवउदारवाद का विरोध ही पर्याप्त नहीं है । इनका विरोध करते हुए किसी पक्ष में होना होगा । उस आदर्श अर्थव्यवस्था और उस न्यायपूर्ण समाज को कोई नाम देना होगा । विषमता को बढ़ावा देने और धरती को नष्ट करने के कारण वर्तमान पूंजीवाद की समग्र ही सम्भावना चुक जाने की बात सभी करते हैं । बात तो सही है लेकिन उचित विकल्प के अभाव में अभी इसके जारी रहने की ही आशा की जा सकती है । लेखक खुद को विषमता के इतिहास का अध्येता और आर्थिक विकास, संपत्ति के वितरण तथा राजनीतिक टकराव के बीच संबंध तलाशने वाला कहते हैं । इस नाते उन्होंने एकाधिक मोटी किताबों का प्रणयन किया है और ऐसे विश्व विषमता कोश का निर्माण करने में मदद की है जिससे दुनिया के विभिन्न समाजों में आय और संपत्ति की विषमता का इतिहास पारदर्शी हो सके ।
इस ऐतिहासिक शोध के आधार पर और पिछले तीस सालों के अनुभव के आधार पर उन्होंने भागीदारीपरक समाजवाद की रूपरेखा तैयार करने की कोशिश की थी । उसके मुख्य विंदुओं को इसमें दोहराया गया है । लेखक का मानना है कि इस मामले में सामूहिक व्याख्या, खुली बहस और सामाजिक तथा राजनीतिक प्रयोगों की लम्बी प्रक्रिया चलेगी । इस प्रक्रिया की शुरुआत उन्होंने अपनी बात से की है । इस प्रक्रिया को विनम्रता और लचीलेपन के साथ चलाना होगा क्योंकि पिछले प्रयोग की विफलता तो भारी है ही आगामी चुनौती भी कुछ कम बड़ी नहीं है । इस किताब में लेखक द्वारा सितम्बर 2016 से फ़रवरी 2021 तक प्रतिमाह ले मोंद में लिखे लेख संग्रहित हैं इसलिए इनसे उनके हालिया विचारों को समझने में भी मदद मिलेगी । इनमें कुछ दोहराव भी होने की आशंका लेखक को है । इसके बावजूद उनको उम्मीद है कि पाठकों को सोचने विचारने के कुछ मुद्दे मिलेंगे ।
सबसे पहली बात कि समता और भागीदारीपरक समाजवाद की दिशा में यात्रा की शुरुआत हो चुकी है । इतिहास से साबित हो चुका है कि विषमता वैचारिक और राजनीतिक होती है, आर्थिक या तकनीकी नहीं । निराशा के वर्तमान माहौल में लेखक का यह आशावाद विरोधाभासी लग सकता है फिर भी उनकी बात सच के करीब है । लम्बे समय के हिसाब से विषमता में कमी आयी है । इसकी विशेष वजह बीसवीं सदी में लागू की गयी नयी सामाजिक और राजकोषीय नीतियां हैं । इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है लेकिन इस इतिहास से सीखकर हम काफी आगे बढ़ सकते हैं । मिसाल के लिए संपत्ति के संकेंद्रण की हालत पिछली दो सदियों में देखने से पता चलता है कि समूची संपत्ति में सबसे अमीर एक फ़ीसद लोगों का हिस्सा समूची उन्नीसवीं सदी में बहुत अधिक रहा । फ़्रांसिसी क्रांति की समानता की घोषणा बहुत कुछ सैद्धांतिक ही रही अगर इसका अर्थ संपत्ति का पुनर्वितरण समझा जाय । बीसवीं सदी में उनका हिस्सा तेजी से कम होता हुआ नजर आता है । प्रथम विश्वयुद्ध के समय समूची संपत्ति में एक फ़ीसद अमीरों का हिस्सा 55 फ़ीसद था और अब यह 25 फ़ीसद के आसपास है । इसके बावजूद ध्यान रखना चाहिए कि नीचे की आधी आबादी का हिस्सा महज पांच फ़ीसद है इसलिए एक फ़ीसद अमीरों का हिस्सा उनके हिस्से का पांच गुना है । दुखद यह है कि नीचे की आधी आबादी का हिस्सा 1980 या 1990 दशक से लगातार लगातार कम होता जा रहा है । यह प्रवृत्ति भारत, रूस और चीन के साथ ही अमेरिका, जर्मनी और शेष यूरोप में भी जारी है ।
मतलब कि स्वामित्व और नतीजतन आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण पिछली सदी में कुछ कम तो हुआ है लेकिन अब भी बहुत अधिक है । विषमता में कमी का सबसे अधिक लाभ उस चालीस फ़ीसद मध्य वर्ग को हुआ है जो नीचे की आधी आबादी और ऊपर के दस फ़ीसद अमीरों के बीच में रहता है । इस कमी का सबसे कम लाभ नीचे की गरीब आधी आबादी को हुआ । ऊपर के दस फ़ीसद लोगों का हिस्सा 80 या 90 फ़ीसद से घटकर 50 या 60 फ़ीसद रह गया है लेकिन नीचे की आधी आबादी का हिस्सा अब भी अत्यल्प ही है । उनकी आमदनी तो बढ़ी है लेकिन संपत्ति में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ है ।
सवाल यह है कि पिछली सदी में विषमता में जो कमी आयी उसकी व्याख्या कैसे की जाय । इसका एक कारण तो यह है कि दोनों विश्वयुद्धों में बड़े पैमाने पर संपत्ति का विनाश हुआ लेकिन इसके साथ ही बहुत बड़ी वजह बीसवीं सदी में अनेक यूरोपीय देशों द्वारा कानूनी, सामाजिक और कराधान संबंधी नीतियों में बदलाव भी है । इसका सबसे निर्णायक कारक 1910-20 से लेकर 1980-90 तक का कल्याणकारी राज्य था जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, अवकाश और विकलांगता पेंशन के साथ ही भत्ता, आवास जैसे बहुतेरे सामाजिक सुरक्षा उपायों में भारी निवेश किया । 1910 की शुरुआत में पश्चिमी यूरोप में सार्वजनिक व्यय सकल राष्ट्रीय आय का मुश्किल से दस फ़ीसद था और इसका भी बड़ा हिस्सा पुलिस, फौज और औपनिवेशिक विस्तार में चला जाता था । यही हिस्सा 1980 तक आते आते राष्ट्रीय आय का 40 से 50 फ़ीसद तक पहुंच गया और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा बड़ा था । इसके कारण बीसवीं सदी में यूरोप में शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों तक पहुंच के मामले में कुछ समानता आयी । इससे पहले के समाजों में इस स्तर की समानता नहीं थी । बहरहाल 1980-90 के दशक से ही कल्याणकारी राज्य में ठहराव आ गया है जबकि जीवन प्रत्याशा और स्कूली शिक्षा का खर्च बढ़ने के चलते जरूरत में कमी नहीं आयी है । इससे साबित होता है कि किसी भी उपलब्धि को स्थायी नहीं मानना चाहिए । कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ के खतरों को भली तरह उजागर कर दिया । उसके बाद तो सवाल यही उठा है कि अमीर देशों में सामाजिक राज्य की वापसी और गरीब देशों में उसकी ओर त्वरण कैसे हासिल किया जाए ।
इसके बाद वे शिक्षा में निवेश की चर्चा करते हैं । बीसवीं सदी की शुरुआत में सभी स्तरों की शिक्षा पर निवेश पश्चिमी यूरोप में राष्ट्रीय आय का महज 0.5 प्रतिशत था । इसका मतलब था कि शिक्षा बेहद कुलीन और बहिष्कारी थी । अधिकतर लोगों को भीड़ भरे और संसाधनहीन प्राथमिक स्कूलों में जाना होता था और मुट्ठी भर लोग ही माध्यमिक या उच्च शिक्षा तक पहुंच पाते थे । बीसवीं सदी में शिक्षा में निवेश दस गुना बढ़ा और 1980 आते आते औसतन राष्ट्रीय आय के 5 या 6 प्रतिशत तक चला गया । इसके कारण शिक्षा का बहुत प्रसार हुआ । तमाम सबूतों से जाहिर होता है कि पिछली सदी की समृद्धि और समता का सबसे मजबूत कारक शिक्षा ही थी । इसी प्रकार हाल के दशकों में जब शिक्षा के क्षेत्र में निवेश अवरुद्ध हुआ है तो विषमता बढ़ी है और औसत आमदनी में वृद्धि मंद हुई है । लेखक को इसका भी उल्लेख जरूरी लगा कि शिक्षा तक पहुंच के मामले में बहुत ही अधिक सामाजिक भेदभाव बना हुआ है । अमेरिका में उच्च शिक्षा हासिल करने का सुयोग माता-पिता की आमदनी पर निर्भर हो गया है । फ़्रांस में भी अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए अनुदान के मामले में भेदभाव होने के कारण भारी विषमता पैदा हो रही है । एक ओर शिक्षा की चाहत में बढ़ोत्तरी आयी है और दूसरी ओर उस पर निवेश में कमी हो रही है ।
लेखक का कहना है कि असली समानता प्राप्त करने के लिए शैक्षिक समता और कल्याणकारी राज्य ही पर्याप्त नहीं हैं । इसके लिए सत्ता और शक्ति के तमाम संबंधों पर पुनर्विचार करना होगा । इसके लिए शक्ति के सहकारी बंटवारे के बारे में सोचना होगा । लेखक ने इस क्षेत्र में भी बीसवीं सदी से सीखने की सलाह दी है । अनेक यूरोपीय देशों खासकर जर्मनी और स्वीडेन में ट्रेड यूनियन आंदोलन और सामाजिक जनवादी पार्टियों ने बीसवीं सदी के मध्य में तथाकथित सह प्रबंधन की व्यवस्था के रूप में भागीदारों के बीच नया शक्ति विभाजन लागू करने में सफलता पायी थी । बड़ी बड़ी कंपनियों के निदेशक मंडल में आधे सदस्य कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते थे । हालांकि इनके पास कंपनी का कोई हिस्सा नहीं होता था और किसी विवाद की स्थिति में हिस्सेदारों के मत ही गिने जाते थे । इसे लेखक ने आदर्श नहीं माना है लेकिन हिस्सेदारी की व्यवस्था में एक बदलाव के बतौर देखने का अनुरोध किया है । उनका कहना है कि कर्मचारियों के पास पूंजी में 10 या 20 फ़ीसद हिस्सेदारी होने से भी नाजुक मौकों पर प्रभाव डाला जा सकता है । सही बात है कि इस प्रावधान पर बहुत हो हल्ला मचा था और इसके लिए तीखी सामाजिक, राजनीतिक तथा कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी लेकिन इससे आर्थिक विकास में कोई बाधा नहीं आयी थी बल्कि विकास तेज ही हुआ था । सबूत इस बात के हैं कि अधिकारों के मामले में समानता होने से कंपनी की दीर्घकालीन रणनीति में कर्मचारियों की भागीदारी होती है । दुर्भाग्य से कंपनियों के हिस्सेदारों के कड़े प्रतिरोध की वजह से इन नियमों का प्रसार नहीं हो सका है । फ़्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में सारी ताकत इन कंपनियों के हिस्सेदार ही अपने पास रखना चाहते हैं । फ़्रांस के समाजवादी भी इंग्लैंड के लेबर प्रतिनिधियों के समान 1980 तक राष्ट्रीकरण के पक्षधर रहे और स्वीडेन तथा जर्मनी के सामाजिक जनवादियों की उपर्युक्त रणनीतियों को अपर्याप्त समझते रहे हैं । सोवियत संघ के पतन के बाद से राष्ट्रीकरण की मांग गायब हो गयी और फिलहाल स्वामित्व में बदलाव की सारी बात ही फ़्रांस और इंग्लैंड में सुनायी नहीं देती । ऐसे में पिकेटी भागीदारी के इस विकल्प के बारे में सोचने का अनुरोध करते हैं ।
सत्ता में भागीदारी के इस आंदोलन को विस्तारित करना उन्हें सम्भव लगता है । मसलन सोचा जा सकता है कि सभी कंपनियों में कर्मचारियों के इन मतों के अतिरिक्त भी किसी निजी हिस्सेदार के मतों की संख्या सीमित कर दी जाय । इससे सभी हिस्सेदारों को आपस में सहयोग करने की प्रेरणा मिलेगी । उन्हें लगता है कि इस मामले में कानूनी बदलाव ही पर्याप्त नहीं होंगे । सत्ता के असली वितरण के लिए कराधान और विरासत की व्यवस्था भी ऐसी बनानी होगी जिससे संपत्ति का वृहत्तर वितरण हो सके । ऊपर ही कहा गया कि आधी गरीब आबादी के पास वस्तुत: कुछ भी नहीं है और सकल संपत्ति में उनका हिस्सा भी ऊन्नीसवीं सदी के ही स्तर पर ठहरा हुआ है । यह सोच व्यर्थ लगती है कि संपत्ति की आम बढ़ोत्तरी से स्वामित्व में व्यापकता आयेगी । अगर यह सच होता तो बहुत पहले ऐसा हो जाना चाहिए था । इसी वजह से लेखक को शासन से सक्रिय कदम उठाने की उम्मीद है । उनका प्रस्ताव है कि प्रत्येक बालिग व्यक्ति को देश की औसत संपत्ति का भुगतान करना चाहिए । सबके लिए इस तरह की विरासत का खर्च वार्षिक संपत्ति कर और वर्धमान विरासत कर लगाकर प्राप्त किया जायेगा । इस सिलसिले में वे विस्तार से तमाम सुझाव प्रस्तावित करते हैं जिन्हें लागू किया जाना चाहिए ।
उनका कहना है कि कोई भी जायज पर्यावरण नीति बिना वैश्विक समाजवादी परियोजना के लागू नहीं की जा सकती । इस वैश्विक परियोजना का आधार विषमता में कमी, सत्ता और संपत्ति का स्थायी वितरण तथा आर्थिक संकेतकों की पुन:परिभाषा होगा । आर्थिक लक्ष्य अगर पूर्ववत ही बने रहते हैं तो सत्ता का वितरण बेमानी हो जायेगा । स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन के उपभोग पर रोक लगाने का ढांचा खड़ा करना होगा । तयशुदा सीमा से अधिक कार्बन उत्सर्जन पर कड़ाई से प्रतिबंध और दंड लगाने होंगे । सकल घरेलू उत्पाद की जगह राष्ट्रीय आय की धारणा लानी होगी । औसत की जगह वितरण पर ध्यान केंद्रित करना होगा । आय के इन संकेतकों का पूरक कार्बन उत्सर्जन जैसे पर्यावरणिक संकेतकों को बनाना होगा । इनके आधार पर न्याय का सर्वसम्मत मानक भी गढ़ना होगा ।
प्रत्येक व्यक्ति को देश की औसत संपत्ति के भुगतान से सार्वजनिक व्यय में बहुत वृद्धि नहीं होगी क्योंकि किसी भी न्यायपूर्ण समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, आवास और पर्यावरण जैसी बुनियादी सुविधाओं तक सबकी पहुंच होगी । इससे सभी लोग देश के समाजार्थिक जीवन में पूरी तरह भागीदारी कर सकेंगे । संपत्तिहीन होने या कर्ज से दबे होने की वजह से इस समय बहुतेरे लोग राष्ट्रीय आय में उचित योगदान नहीं कर पाते । जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आप कोई भी वेतन और काम के कैसे भी हालात स्वीकार कर लेते हैं ताकि किराया चुका सकें और परिवार चला सकें । इसके उलट यदि आपके पास संपत्ति हो तो आप बुरे विकल्प को अस्वीकार करके समूचे माहौल में सुधार की प्रेरणा पैदा कर सकते हैं । इससे न्याय पर आधारित समाज के निर्माण की राह सुगम होगी ।
अमीरों पर भारी कराधान के उनके प्रस्ताव पर बहुत विवाद हुआ है । उनका कहना है कि बहुतेरे देशों में ऐसा हो चुका है । इसके लिए वे 1930 से 1980 तक के अमेरिकी कराधान का उदाहरण देते हैं । उनका यह भी कहना है कि इस नीति का बेहद सकारात्मक असर उस दौरान रहा था । अमेरिका में समृद्धि का वाहक शिक्षा रही है न कि विकराल सामाजिक विषमता । लेखक का आदर्श समाज सबके पास कुछ न कुछ धन वाला होगा । जिसमें व्यक्तियों की अमीरी अस्थायी होगी और कराधान के जरिये उन्हें समाज के लिए उपयोगी स्तर तक ले आया जायेगा । उनका मानना है कि अवसरों की समानता की उद्घोषणाओं को यथार्थ की जमीन पर उतारने के लिए इस दिशा में और भी आगे जाना होगा ।
यह बात वे साफ साफ कहते हैं कि सारे संसार में सर्वसम्मति का इंतजार किये बिना भी अलग अलग देशों में कानूनी, राजकोषीय और सामाजिक बदलाव के जरिये भागीदारीपरक समाजवाद की ओर धीरे धीरे अग्रगति सम्भव है । इसी तरह बीसवीं सदी में सामाजिक राज्य का निर्माण हुआ था और विषमता में कमी आयी थी । शैक्षिक समानता और सामाजिक राज्य को देश दर देश फिर से लाया जा सकता है । इसके लिए किसी की अनुमति या आदेश की जरुरत नहीं है । साथ ही अगर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी विकसित कर लिया जाय तो इस काम में तेजी लायी जा सकती है । इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी बेहतर आधार मिलेगा । इसके लिए मुक्त व्यापार पर आधारित हालिया वैश्वीकरण की विचारधारा से छुट्टी पानी होगी और आर्थिक, राजकोषीय तथा पर्यावरणिक न्याय की स्पष्ट नीतियों पर आधारित विकास के माडल और वैकल्पिक अर्थव्यवस्था को अपनाना होगा । इस व्यवस्था का लक्ष्य तो अंतर्राष्ट्रीय होगा लेकिन उसका व्यवहार संप्रभुता पर आधारित होगा । तात्पर्य कि प्रत्येक देश शेष दुनिया के साथ व्यापार की शर्तें तय करने को स्वतंत्र होगा । सार्वभौमिक संप्रभुता की इस व्यवस्था को वर्तमान उग्र और संकीर्ण राष्ट्रवादी उन्माद की जगह लेनी होगी ।
इस नये अंतर्राष्ट्रवाद में अधिकतर देशों को सामाजिक न्याय, विषमता में कमी और पृथ्वी की संरक्षा के सार्वभौमिक मूल्यों का पालन सहकारी आधार पर करना होगा और सामाजिक, राजकोषीय तथा पर्यावरणिक रूप से नुकसानदेह रास्ते पर चलने वाले देशों को ऐसा करने से रोकना होगा । रोकने के तरीके प्रतिबंधात्मक होने की जगह प्रोत्साहनपरक होने होंगे । इसके लिए मनमानी और बंद दरवाजों के पीछे की दुरभिसंधियों का चलन समाप्त करना होगा । यूरोप के लोकतंत्रीकरण के घोषणापत्र के प्रस्ताव इसी दिशा में लक्षित हैं । फ़्रांस और जर्मनी की संयुक्त संसदीय प्रणाली से सबकी सहमति का इंतजार किये बिना भी विभिन्न देशों के उप समूहों द्वारा नयी संस्थाओं के निर्माण का रास्ता खुला है । यूरोप से बाहर भी सामाजिक संघीयता की धारणा को अपनाया जा सकता है । मसलन पश्चिमी अफ़्रीका के देशों ने अपनी संयुक्त मुद्रा चलाने का प्रयास किया है और इसके सहारे वे औपनिवेशिक विरासत को तिलांजलि भी देना चाहते हैं । लेखक का कहना है कि इस मुद्रा को पूंजी और अमीरी की सेवा में लगाने की जगह युवकों और अधिरचना में निवेशित करना चाहिए । यूरोप के अक्सर भुला दिया जाता है कि यह पश्चिम अफ़्रीकी सहकार यूरोपीय संघ से आगे की बात है । 2008 में ही इसने साझा कारपोरेट टैक्स लगाने का निर्देश दिया और इसकी दर 25 से 30 प्रतिशत के बीच रखने का फैसला किया । यूरोपीय संघ ऐसी कोई सहमति बना ही नहीं सका । दुनिया के पैमाने पर सामाजिक संघीयता और पारदेशीय संसदें जरूरी हो गयी हैं ताकि साझा समुचित वित्तीय, राजकोषीय और पर्यावरणिक नियम बनाये और चलाए जा सकें ।
भागीदारीपरक समाजवाद को एकाधिक स्तम्भों पर खड़ा करना होगा । शैक्षिक समानता और सामाजिक राज्य, सत्ता और संपत्ति का स्थायी वितरण, सामाजिक संघीयता और टिकाऊ तथा न्यायपूर्ण वैश्वीकरण उसके महत्वपूर्ण घटक होंगे । इन सभी पैमानों पर बीसवीं सदी के समाजवाद और सामाजिक जनवाद की बेहिचक कड़ी परीक्षा करनी होगी । यह बात रेखांकित करनी होगी कि पितृसत्ता और औपनिवेशिक विकृतियों के सवाल पर यथोचित ध्यान नहीं दिया गया था । उनके मुताबिक इन सवालों को एक दूसरे से काटकर नहीं देखा जा सकता । समाजार्थिक और राजनीतिक अधिकारों की वास्तविक समानता पर आधारित किसी समग्र समाजवादी परियोजना के भीतर ही इन पर विचार करना होगा । इसके बाद वे इन दोनों सवालों की विस्तार से चर्चा करते हैं ।
सभी मानव समाज किसी न किसी रूप में पितृसत्ताक रहे हैं । बीसवीं सदी के आरम्भ तक जितने भी असमानतामूलक विचार रहे हैं उन सबमें पुरुष वर्चस्व की केंद्रीय भूमिका रही है । बीसवीं सदी के दौरान इस वर्चस्व का स्वरूप अधिक सूक्ष्म हुआ । अधिकारों की औपचारिक समानता तो धीरे धीरे स्थापित हुई लेकिन यह विचार भी मजबूत बना रहा कि स्त्री की जगह उसका घर ही है । 1970 के पूर्वार्ध में कमाई करने वालों में 80 प्रतिशत पुरुष ही हुआ करते थे । समान काम के लिए पुरुष और स्त्री के वेतन में 15 से 20 प्रतिशत तक का अंतर था । प्रगति की वर्तमान दर पर ही कायम रहा जाय तो स्त्री और पुरुष के वेतन में समानता 2102 तक जाकर आ पायेगी । अगर इस दिशा में तेजी से वास्तविक प्रगति करनी है तो कंपनी, प्रशासन, विश्वविद्यालय और संसद में जिम्मेदार पदों पर उनकी नियुक्ति को अनिवार्य बनाना होगा । देखने में यह भी आया है कि स्त्रियों के प्रतिनिधित्व में बढ़ोत्तरी के साथ ही सभी वंचित सामाजिक समूहों की भागीदारी में भी सुधार आता है । इसका मतलब है कि लैंगिक समता के साथ सामाजिक समता का भी विस्तार होगा ।
इसके ही साथ रोजगार तक पहुंच के मामले में जातीय और नस्ली भेदभाव से भी टकराना होगा । इसके लिए औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक इतिहास पर भी दावा जताना लेखक को जरूरी लगता है । गुलामों का व्यापार करने वालों की यूरोपीय और अमेरिकी शहरों में स्थापित मूर्तियों पर लोगों का हमला आश्चर्यचकित करता है लेकिन इतिहास पर दावेदारी का यह अनिवार्य अंग है । सभी उपनिवेशित देशों के संसाधनों का यूरोपीय देशों द्वारा भारी दोहन किया गया था इसलिए क्षतिपूर्ति की उनकी वर्तमान मांग पूरी तरह जायज है । इस सिलसिले में याद रखना होगा कि गुलामी के उन्मूलन के लिए गुलामों का व्यापार करने वालों की क्षतिपूर्ति की गयी थी । नस्लवाद और उपनिवेशवाद से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के सवाल पर भी लेखक ने भविष्य में ऐसी आर्थिक व्यवस्था का पक्ष लिया है जिससे विषमता में कमी आये और शिक्षा, रोजगार तथा संपत्ति तक सबकी पहुंच बने । क्षतिपूर्ति और सार्वभौमिक अधिकार को एक दूसरे के विरोध में खड़ा करने की जगह उन्हें एक साथ जोड़ा जाना चाहिए । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्षतिपूर्ति की ऐसी जायज व्यवस्था के बारे में सोचा जा सकता है जिसमें संसार के सभी व्यक्तियों को शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में अच्छी सुविधा हासिल हो । वर्तमान कोरोना महामारी इस दिशा में सोचने का सही मौका मुहैया कराती है । इसका खर्च अमीर देशों पर टैक्स लगाकर निकाला जाना चाहिए । उनकी समृद्धि आखिरकार वैश्विक अर्थतंत्र पर आधारित है । सदियों तक दुनिया के मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों के अबाध दोहन का ही नतीजा उनकी वर्तमान समृद्धि है ।
अंत में लेखक का कहना है कि भागीदारीपरक समाजवाद लाने के लिए किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है । लेखक ने इस किताब के जरिये उसकी दिशा में नागरिकों की सोच को उन्मुख करने की कोशिश की है क्योंकि उनका मानना है कि समाजार्थिक सवालों पर संगठित सामूहिक विचार विमर्श से ही असली बदलाव आ सकता है ।