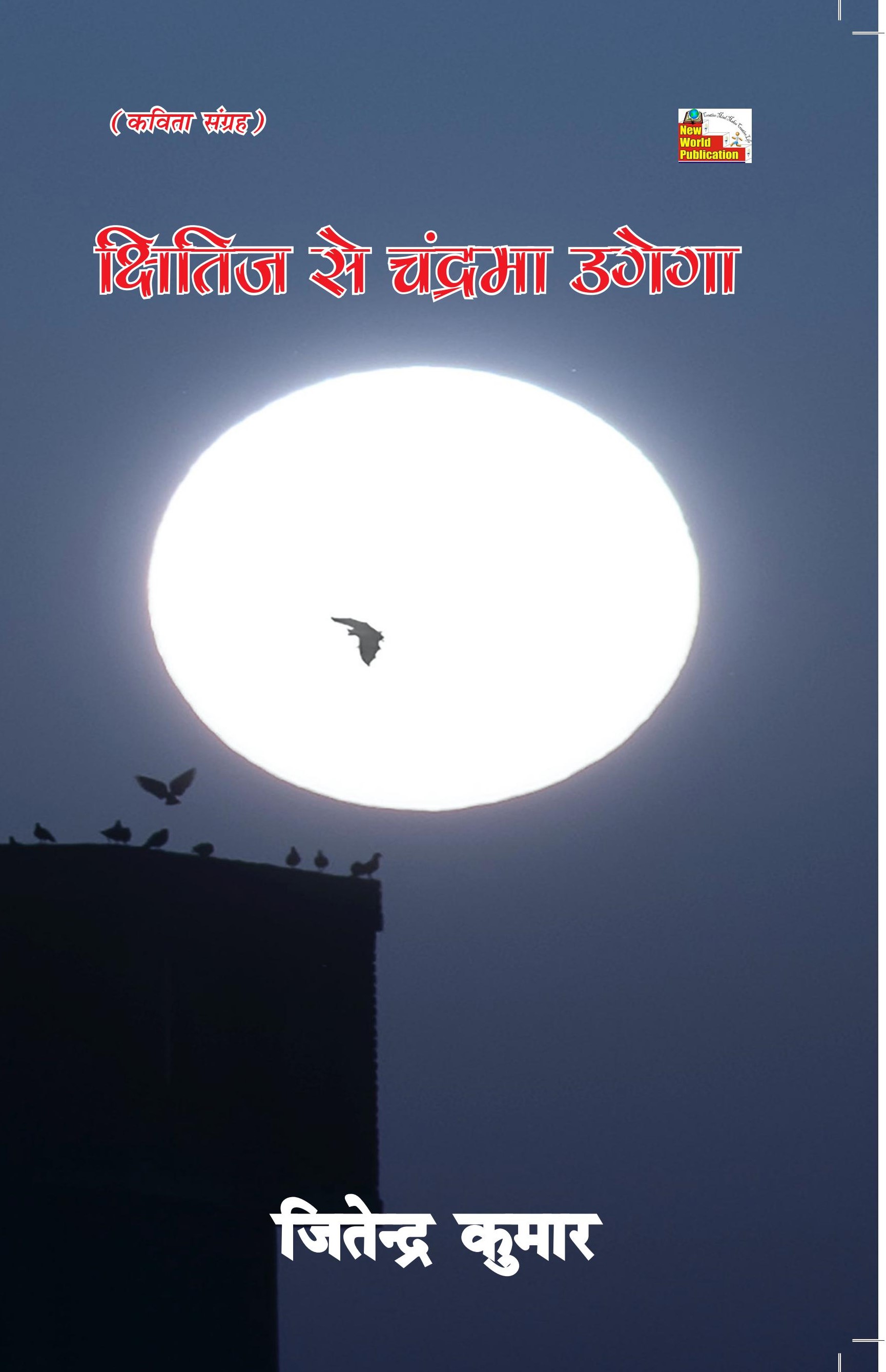जितेन्द्र कुमार कविता की दुनिया के सजग और सचेत नागरिक हैं। इनकी पहली कविता पुस्तक ‘रात भर रोई होगी धरती’ करीब 25 साल पहले आई थी। ‘क्षितिज से उगेगा चंद्रमा’ कविताओं की पांचवी पुस्तक है। इनकी चिंता में धरती और उस पर रहने व बसने वाले जीव, प्रकृति, मनुष्य और जीवन है। आम आदमी की जीवनचर्या हो या दूर पूर्वी छोर पर नए दिवस के आरंभ के रूप में सूरज का दस्तक देना जैसी प्राकृतिक क्रिया हो, इनके लिए कविता लिखने का यही वक्त है। अर्थात कविता जीवन के क्रिया-कलापों के साथ क़दम मिलाती है, उसके साथ चलती है। जितेन्द्र कुमार के लिए कविता लिखना बैठे ठाले का शगल नहीं है। इस संबंध में वे कहते हैंः
‘ कविताई इसलिए/कि बचा रहे नदियों में जल/बचे रहे जंगल और पहाड़/बची रहे पृथ्वी की हरियाली/बची रहे बेटियां/घर आंगन में गूंजती रहे बच्चों की किलकारियां/और जब कभी विध्वंस का सामना करना पड़े/हम एकजुट हो जाएं ’
इस कविता से जितेन्द्र कुमार के सरोकार, रचनात्मक संघर्ष और जमीन को समझा जा सकता है। इसमें कवि की मात्र सदिच्छा और कामना ही नहीं है बल्कि जन-जीवन में ‘विध्वंस’ के कारकों तथा इसे पैदा करने वाली ताकतों की पड़ताल व पहचान भी है। साथ ही इसके प्रति हमारा नजरिया व व्यवहार क्या हो ? कैसे निपटा जाए ? ‘ एकजुटता ’ के संदेश के साथ इसकी राह भी है। जितेंद्र कुमार की रचनात्मक स्थितियां इसी द्वंद से निर्मित होती हैं जिसमें हमारा वर्तमान है, उसकी राजनीति, समाज व संस्कृति है। वे समकालीन यथार्थ को अपने निजी अनुभव, ज्ञान-विवेक तथा कलात्मक क्षमता से मूर्त करते हैं।
हिंदी की समकालीन कविता मध्यवर्गीय व महानगरीय हुई है। बौद्धिकता को ही कला-प्रतिमान के रूप में प्रतिष्ठा मिली है। इससे उसकी पहुंच का दायरा सीमित हुआ है। वैसे कविताएं लिखी तो खूब जा रही हैं पर वह पाठकों तक कम पहुंच रही हैं। आमतौर पर कवि वैचारिक धरातल पर अपने को प्रगतिशील और जनवादी के रूप में पेश करते हैं परन्तु कविता का जनवादी मॉडल क्या हो, आज भी यह बहस और विचार का विषय है। इस संबंध में जितेन्द्र कुमार की कविताओं से हम उम्मीद कर सकते हैं। समय और समाज का जटिल यथार्थ जिस सहज व सरल तरीके से इनकी कविता में व्यक्त हुआ है, यह इनकी काव्य-कला है। भाषा आम बोलचाल के करीब है तथा शैली अभिधात्मक के साथ व्यंजनात्मक है। इससे अभिव्यक्ति धारदार हुई है। यहां ढ़ूढ़ें भी शायद ही कोई कविता मिले, जिसे समझने के लिए मानसिक कसरत करनी पड़े। ऐसी ही कविताओं का यह संग्रह है।
इस संग्रह से गुजरते ही सबसे पहले ऐसी कविताओं से हमारी मुलाकात होती है जिसकी विषय वस्तु स्त्री जीवन, उसकी दशा-दुर्दशा, मर्दाना समाज और पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों का साहस व संघर्ष है। हमारे समाज में स्त्री जीवन के कई स्तर हैं। जितेन्द्र कुमार की कविताएं उनसे रूबरू है। इनमें खेतों में काम करने वाली श्रमिक स्त्रियां हैं जो खेत व घर से लेकर बाजार तक अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हैं, तमाम बाधाओं को पार करती हैं और ज़िन्दगी की छोटी-छोटी खुशियों को बड़ी मुश्किल से बटोर कर लाती हैं।
जितेन्द्र कुमार की नजर गांव के अंदर लड़कियों में आ रहे बदलाव पर है जो पढ़ाई में लड़कों से अव्वल आ रही हैं और उन्हें घर की चहारदीवारी के भीतर कैद करने के तमाम उपक्रम किये जा रहे हैं। लेकिन वे बंदिशों के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें कैद नहीं आजादी चाहिए। इसी का प्रखर रूप ‘बीएचयू की लड़कियां’ में उनका छेड़खानी और गुंडागर्दी के खिलाफ संघर्ष में मुखरता से सामने आता है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा की ‘बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ’ का नारा देने वाली सरकार के प्रधान जो स्थानीय सांसद भी हैं, उन दिनों बनारस में होते हैं और रास्ता बदलकर निकले जाते हैं । जितेंद्र कुमार सत्ता के इस दोहरे चरित्र तथा ‘दीपा मुर्मू’ और ‘रंजन मिश्रा कहां जाए’ के माध्यम से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में फलते-फूलते पितृसत्तात्मक व्यवस्था की क्रूर सच्चाई को सामने लाते हैं।
संग्रह में एक कविता है ‘ मेरे गांव की अंगूठा छाप औरतें ’। इस कविता को पढ़ते हुए गोरख पांडे की ‘ कैथरकलां की औरतें ’ कविता की बरबस याद हो आती है। शोषण और उत्पीड़न की परिस्थितियां अन्याय के प्रतिकार और संघर्ष की चेतना का मुख्य स्रोत है। यह ग्रामीण स्त्रियों में आ रहे बदलाव का भी कारण है। यह भाव कुछ यूं व्यक्त होता हैः
‘ चूल्हे की आग में भात की तरह/पकती है गांव की स्त्रियां/कुटान पिसान करती हैं/सावन में रोपनी के गीत गाती हैं/… नरम देह वाली नदी/शिकायत करने लगी हैं/मुखिया से/सुखिया से /राजशाही से/तानाशाही से/… खाकी वर्दी से नहीं डरती अब/हाथ में हंसिया लेकर/विधानसभा का घेराव करने/राजधानी चली जाती हैं ’
यहां जितेन्द्र कुमार अपने साहित्य समाज से भी मुखातिब है। उनका यह कहना कि ‘ अधूरा होगा कवि का अनुभव संसार/मेरे गांव की अंगूठा छाप औरतों के जिक्र के बिना’ वास्तव में साहित्य के मध्यवर्गीय समाज से कवि की अपेक्षा है। यह प्रगतिशील और जनवादी साहित्य समाज के डी-क्लास व डी-कास्ट होने से भी जुड़ा है।
जितेन्द्र कुमार लोकधर्मी-जनधर्मी कवि हैं। इनकी कर्मभूमि भोजपुर का अंचल है जो सामंतवाद विरोधी किसान संघर्ष के लिए ख्यात रहा है। बाथे, बथानी टोला जैसी अनगिनत घटनाएं घटित हुईं, जो सामंती जुल्म और नृशंसता को सामने लाती हैं। भोजपुर ने जुल्म के आगे कभी घुटने नहीं टेके। दमन-उत्पीड़न के प्रतिकार-प्रतिरोध ने जन चेतना को नयी ऊंचाई दी। उसे व्यापक बनाया। जितेन्द्र कुमार की कविता की यही जमीन है। उनकी वैचारिकी तथा प्रतिरोधी काव्य चेतना की निर्मिति में इसकी भूमिका है।
इस कविता संग्रह में ‘ बाथे ’ शीर्षक से उनकी चार कविताएं हैं जो उस अमानवीय कृत्य के विविध पहलुओं तथा जघन्यतम हत्याकांड को हमारे सामने सजीव करती हैं। ये मन को विह्वल ही नहीं करती बल्कि आक्रोश से भर देती हैं । जितेन्द्र कुमार का दमन-उत्पीड़न की शिकार जनता से भावनात्मक लगाव सामने आता है। उनका दृढ़ मत है कि भोजपुर के संघर्ष में जन समुदाय ने मुक्ति का जो स्वप्न देखा, उसे इस तरह की घटनाएं खत्म नहीं कर सकती। इससे प्रतिकार की जमीन को विस्तार ही मिला। इस भाव-विचार को वे कविता में कुछ यूं व्यक्त करते हैंः
‘ रक्त में सने सपनों के पंख फड़फड़ाने लगे/सोन के अरार पर पीपल के विशाल वृक्ष पर बगुले बैठने लगे/बाथे की धरती प्रतिरोध की लिए/और उर्वर हो गई है ’
जितेन्द्र कुमार की कविता का फलक बड़ा है। वह विविधता लिए हुए है। उनके अंदर ‘आम का पेड़ हो जाऊं’ जैसी चाह है। इसके मूल में पेड़-पौधे, बाग-बगीचे, माल-मवेशी, गांव-कस्बा, प्रकृति-जंगल आदि से गहरा अनुराग और जिस तरह प्रकृति का दोहन व पर्यावरण को नष्ट-भ्रष्ट किया जा रहा है, उसके विरुद्ध संघर्ष है। वहीं, ‘ यूकेलिप्टस’ जो धरती को उसर बना रहा है, गोराशाही व उपनिवेशवाद प्रतीक है। इनकी कविताएं दलित, आदिवासी, बाल मजदूर, कचड़ों में मूल्यवान बीनने वाले बच्चे, निद्रालीन शिशु, यहूदी, पिहू, रतिनाथ की चाची, राम बुझावन की रुलाई, दशरथ मांझी आदि के जीवन-संघर्ष से पाठकों को जोड़ती है और उन्हें प्रेमचंद, रेणु तथा नागार्जुन के पास ले जाती हैं।
यह समय है जब वैश्विक पूंजी का दबदबा बढ़ा है। उसने गांव, समाज व देश को अपना आहार बनाया है। नस्लवाद, अंधराष्ट्रवाद, कारपोरेट फासीवाद – जैसे प्रतिक्रियावादी विचारों व मूल्यों को खाद-पानी मिला है। भारत गंभीर रूप से इसकी चपेट में हैं। आजादी के मूल्य, आम आदमी का जीवन, संविधान, लोकतंत्र, न्याय, प्रेम व भाईचारा आदि संकट में है। समाज से लेकर इतिहास तक का सांप्रदायिकरण किया जा रहा है। लोकतंत्र उनके रहमो करम पर है, कुछ ऐसा
‘जो विरोध करेगा/वह देशद्रोही घोषित होगा/भगवा जैकेट वाहिनी उसे धूल-धूसरित करेगी/नया लोकतंत्र यही होगा’
तुर्रा तो यह कि इसे वर्तमान सत्ता ने ‘विकास’ का नाम दिया है। खेती-किसानी खत्म हो रही है। नौजवान गांव-कस्बा छोड़ शहर और महानगर की डगर पकड़ रहे हैं। दरअसल, यह विकास नहीं विपदा है। देखेंः
‘उल्लू बोलते हैं/खंडहर बने घरों में/विकास की आंधी बहती है/कागजों में’।
‘उल्लू बोलते हैं/खंडहर बने घरों में/विकास की आंधी बहती है/कागजों में’।
जितेन्द्र कुमार की कविता शोषक-प्रतिक्रियावादी सत्ता से मोर्चा लती है। आम जन के पक्ष में खड़ी होती है। टीपू सुल्तान जैसे नायकों को प्रतिष्ठित करती है। ऐसा करते हुए वह अपने समय का आख्यान रचती है। वह संवाद करती है और सवाल भी उठाती है:
‘क्या फोरलेन के नीचे/गांव के सपनों की सड़क दम तोड़ देगी?’, ‘आदिवासी जानना चाहते हैं कि/सोनभद्र में आदिवासी किसानों की हत्याओं का वर्ग चरित्र क्या है? हत्यारे किसके दामन में छुपे हैं?’, ‘वह कौन है, जो दोस्ती करता है अमेरिका से, सेमिनार करता है राष्ट्रवाद पर, एक भाषा, एक खान-पान, एक पोशाक की बात करता है/वह कौन है?’
यहां आशावाद भी हैः
‘एक दिन जनता उठ खड़ी होगी/इस अत्याचार के खिलाफ’, ‘जनतंत्र और संविधान के लिए लड़ना ही होगा’, ‘अपमान और मौत में एक को चुनने की मजबूरी हो/तो लड़ते हुए मरना सर्वाेत्तम विकल्प है’, ‘नाचती है पृथ्वी/हांफती अस्त-व्यस्त केशोंवाली/औरत के खुरदुरे पैरों के आघात से’ और ‘…. लड़कियों को इंतजार है जुल्म की रात के बीतने का’
इस इंतजार में मुक्ति का स्वप्न और संघर्ष दोनों शामिल है। जितेंद्र कुमार के अंदर बदलाव की अदम्य आकांक्षा है। वे द्वन्द्व को तार्किक परिणति तक ले जाते हैं। उनका दृढ़ मत है कि सनातन जैसा कुछ नहीं होता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसी से मनुष्यता का पथ आलोकित होगा। वह कहते हैंः
‘सनातन जैसा कुछ भी नहीं है/ना धर्म ना राजनीति/प्रकृति में परिवर्तन की लय है/अंतत मनुष्यता की जय है’
जितेन्द्र कुमार की कविताएं परिवर्तन के पक्ष में हैं। वे मनुष्यता का गीत गाती हैं, समय, समाज और जीवन को समझने में मदद करती हैं और सामाजिक बदलाव के लिए पाठकों को सांस्कृतिक रूप से तैयार करती हैं। यह कवि और कविता का एक जरूरी काम है। इम उम्मीद करते हैं कि संग्रह की कविताएं पढ़ी जाएंगी और पसन्द की जाएंगी।