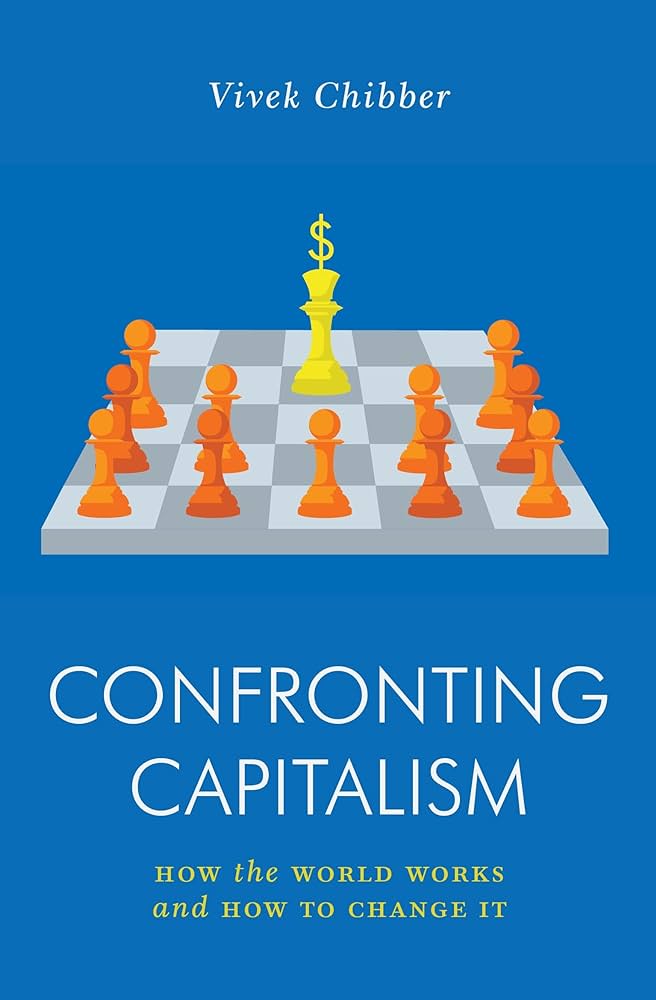2022 में वर्सो से विवेक छिब्बर की किताब ‘कनफ़्रंटिंग कैपिटलिज्म: हाउ द वर्ल्ड वर्क्स ऐंड हाउ टु चेंज इट’ का प्रकाशन हुआ । लेखक का कहना है कि पिछले पांच सालों में विकसित पूंजीवादी दुनिया में पूंजीवाद के नवउदारवादी स्वरूप की वैचारिक वैधता समाप्त हो गयी है । चालीस साल के प्रभुत्व के बाद मुक्त बाजार की सोच पर हमले हो रहे हैं । हमलावर वामपंथी ही नहीं, मुख्य धारा के बौद्धिक भी हैं । तमाम तरह के कामगार विकल्पहीनता के दावे के विपरीत पूंजी के शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प जाहिर कर रहे हैं । इस ऊब की अभिव्यक्ति अभी संगठित वर्ग संघर्ष की जगह अन्य तरीकों से हो रही है । इसके बावजूद इसकी व्यापकता के चलते नये समय के आगमन की अनुभूति हो रही है । विचित्र बात कि इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई । 2011 के अकुपाइ आंदोलनों में इसकी थोड़ी सुगबुगाहट नजर आयी लेकिन 2016 और 2020 के राष्ट्रपति चुनावों में बर्नी सांडर्स के प्रत्याशी बनाने के अभियान से इसे ठोस शक्ल मिली । पूंजीवाद विरोधी वामपंथी बातें जिस तरह हो रही हैं वैसा विगत दो पीढ़ियों के दौरान कभी नहीं सुनी गयी थीं । उनके प्रत्याशी न होने के बावजूद यह उभार बना रहा । वामपंथी संगठनों की सदस्यता में भारी इजाफ़ा हुआ है । इनमें अमूर्त दार्शनिक विवादों की जगह रणनीति और कार्यनीति संबंधी बहसें हो रही हैं । इसके साथ ही मजदूरों के संगठन भी मजबूत हो रहे हैं ।
ऐसे समय पूंजीवाद की बुनियादी गतिकी के बारे में सरल किताबों की कमी को देखते हुए यह किताब तैयार की गयी है । पहले आम शिक्षण को ध्यान में रखते हुए ऐसी पुस्तिकाओं के प्रकाशन का चलन था लेकिन 1980 के बाद से यह परम्परा खत्म हो गयी । इसकी वजह एक ओर संगठित वाम की पराजय था तो दूसरी ओर क्रांतिकारी विमर्श की दुनिया में गैर सरकारी संगठन और विद्वानों का भर जाना था । क्रांतिकारी सोच के भीतर राजनीतिक बदलाव की सम्भावना की आशा भी नहीं रह गयी थी । विद्वानों का प्रवेश कोई बुरी बात नहीं थी और उन्होंने सैद्धांतिक मोर्चे पर कुछ अग्रगति भी हासिल की लेकिन मजदूर वर्ग के साथ रिश्ते टूट जाने के चलते ये तमाम अध्ययन पुस्तकों और पत्रिकाओं में दबे रहे । अब चुनौती सिद्धांत को संगठन के साथ जोड़ने की है । उसे अद्यतन तो होना ही होगा, ऐसी भाषा भी अपनानी होगी जो सत्तर के दशक के मुकाबले आज की लगे । नवउदारवाद के चालीस सालों के बाद होश आने में वक्त लगेगा । उसका आ जाना तय नहीं है । मुक्त बाजार की विचारधारा कमजोर पड़ी है लेकिन अब भी मजबूत राजनीतिक ताकत बनी हुई है । हालात बदलने के लिए वामपंथ को पचास के दशक जैसी ताकत जुटानी होगी । वैचारिक रूप से आगे बढ़ने के बावजूद समाजवादी वाम राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ है । लेखक को उम्मीद है कि उनकी इस किताब से उसके पुनरुत्थान में कुछ तो मदद मिलेगी ।
लेखक का कहना है कि कोरोना की महामारी के आगमन से पहले ही दैनन्दिन जीवन बाधादौड़ बन गया था । 2015 में जब अमेरिकी लोगों से उनकी वित्तीय सुरक्षा के बारे में पूछा गया तो आधे लोगों ने वित्तीय सुरक्षा के बारे में अनिश्चितता जतायी । 71 फ़ीसद लोग बिल नहीं चुका सके थे और 70 फ़ीसद लोग अवकाश के बाद के लिए बचत नहीं कर सके थे । भविष्य की असुरक्षा इतनी अधिक थी कि 92 फ़ीसद लोग आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रोन्नति भी कुर्बान करने को तैयार थे । ऐसा नहीं कि उन्हें प्रोन्नति की चाह नहीं थी लेकिन तत्काल स्थिरता के लिए वे भविष्य के आर्थिक लाभ छोड़ देने को भी तैयार थे । सबकी अवस्था ऐसी नहीं थी । अमेरिकी समाज के ऊपरी तबकों के लिए जीवन कभी इतना आरामदेह नहीं रहा था । अमेरिका के सबसे अमीर परिवार पिछले चालीस सालों से मौज उड़ा रहे हैं । जहां अधिकतर लोगों की आमदनी में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हो रही वहीं सबसे धनी दस फ़ीसद लोग अमीरी की बाढ़ से मुटाये जा रहे हैं । 1983 से 2019 के बीच की निजी संपत्ति में इजाफ़े का 86 फ़ीसद इनके ही नसीब में गया और नीचे के 80 फ़ीसद लोगों के हिस्से महज पांच फ़ीसद संपत्ति का इजाफ़ा आया । ऊपरी दस फ़ीसद में भी अधिकांश लाभ एक फ़ीसद को हुआ और उसके बाद के पांच फ़ीसद लोगों को समस्त लाभ का एक तिहाई ही हासिल हुआ । आमदनी का भी यही किस्सा रहा । एक फ़ीसद लोग नयी आय का एक तिहाई हड़प गये और ऊपरी दस फ़ीसद ने नयी आय का लगभग 70 फ़ीसद पाया ।
कहने का मतलब कि 1980 के बाद आर्थिक हालात में बेहतरी तो आयी लेकिन उसके प्रत्यक्ष लाभ उन्हें ही मिले जो पहले से ही अमीर थे । कोई भी मानेगा कि इसमें बुनियादी रूप से कुछ गड़बड़ है । इतने अधिक संसाधनों और संपत्ति वाले समाज में ऐसा कैसे हो रहा है कि आबादी का बहुत ही छोटा ऊपरी तबका सब कुछ हड़पे जा रहा है जबकि करोड़ो लोगों के लिए जीवन भरण पोषण का संग्राम बन गया है । मुख्य धारा की मीडिया के वाचाल प्रवक्ताओं के पास इस स्थिति की व्याख्या दो तरह की है । एक तो वे इसके लिए व्यक्तियों की काहिली को जिम्मेदार ठहराते हैं । उनको लगता है कि खुशहाल जिंदगी और व्यक्ति के बीच बाधा कड़ी मेहनत करने की अनिच्छा है । इस बेरोजगारी के लिए किसी और को दोष देने का कोई तुक नहीं है । दूसरे वे इसके लिए सरकार को दोषी ठहराते हैं । उनका यह कहना है कि सामाजिक समस्याओं के पैदा होने की वजह सरकार द्वारा बाजार में बेवजह हस्तक्षेप है । इसके ही कारण बाजार अपना काम ठीक से नहीं कर पाता । अगर कोई काम करना चाहे तो बाजार में रोजगार की कमी नहीं है । अगर किसी के अंदर खास कौशल है तो बाजार उसे पहचान कर उसे सम्मानित करेगा । धन कमाने का अगर कोई तरीका उनके दिमाग में है तो बैंक उन्हें व्यवसाय हेतु कर्ज देकर धनी होने का अवसर उपलब्ध करायेगा । बाजार अपने आप पूर्ण रोजगार पैदा करता है और लोगों की प्रतिभा को मान देता है । सरकार उसे अपनी तरह चलने की आजादी नहीं देती । राजनेता और निहित स्वार्थी तत्व किसी भी उद्यमशील पहल को तमाम किस्म के नियमों के जाल में जकड़ लेते हैं । ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाता है जो लोगों को परजीवी बनाती हैं । सरहदों के आर पार सामानों की अबाध आवाजाही पर रोक लगायी जाती है । समाधान यह है कि बाजार से सरकार दूर हटे और उसे अपना जादू दिखाने दे ।
इन दोनों तर्कों में साझा बात यह है कि गरीबी, बेरोजगारी, असुरक्षा और हताशा के लिए पूंजीवाद को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता । लोगों को असुरक्षा और शक्तिहीनता में डालने की बजाय बाजार को आजादी और मौके की जगह घोषित किया जाता है । दावे के मुताबिक इसी के भीतर लोग अपने जीवन और प्रतिभा के बारे में फैसला लेते हैं और यथोचित काम खोजते हैं । यहां सभी फैसले आजाद होकर किये जाते हैं । अगर जिंदगी में खुशहाली नहीं है तो उसके लिए व्यवस्था जिम्मेदार नहीं क्योंकि उसका निर्माण लोगों के फैसलों से होता है । लोग अगर काम करते हैं तो उनकी पहल और प्रतिभा का मान मिलता है और अगर काम नहीं करते तो उसका नतीजा भुगतना पड़ता है । इसलिए उनकी गरीबी के लिए या तो वे खुद जिम्मेदार हैं या कोई बाहरी हस्तक्षेप । खूब आसानी से समझा जा सकता है कि ये तर्क विजेताओं के हैं । आखिर उनके हित में ही तो यह व्यवस्था काम करती है । इस तर्क के मुताबिक कोई अगर अमीर है तो अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत न कि अपनी वर्गीय सुविधा के कारण । उनकी संपत्ति उनकी प्रतिभा और कौशल का परिचायक है । उत्पीड़न और शोषण का कोई अस्तित्व नहीं । जो है वह चुनाव और अवसर का खेल है । पिछले कुछ दशकों से लोगों की परेशानी की इस व्याख्या को कोई चुनौती नहीं देता रहा है । टेलीविजन और पाठ्य पुस्तकों में समाज की कार्यपद्धति के बारे में जो कुछ बताया जाता था उसे मंजूर कर लेने के अलावे कोई रास्ता ही नहीं बचा था । बाजार की मूर्तिपूजा के कोलाहल में सभी आवाजें ही दब गयी थीं ।
लेकिन विगत कुछ सालों से लोग इन तर्कों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं । मार्गरेट थैचर ने जब विकल्पहीनता की बात कही थी उसके बाद अब वह विश्वास पहली बार डांवाडोल हो रहा है । राजनेता अब पहले की तरह मुक्त बाजार और मुक्त व्यापार की तारीफ़ों के पुल नहीं बांध पा रहे हैं । बाजार को काबू करने की जगह अब बहस उसकी मौजूदगी की हद के बारे में हो रही है । समाजवाद को सार्वजनिक बातचीत में वर्जित कर दिया गया था लेकिन अब राजनीतिक वातावरण में उसके चर्चे हैं । एक अनुमान के मुताबिक आधे अमेरिकी युवा इस समय समाजवाद के पक्ष में हैं । थैचर को जवाब के बतौर समाजवाद की बात अब हवाओं में है । लोगों को महसूस हो रहा है कि उनकी समस्याओं की जड़ कोई अकेला दुकेला राजनेता नहीं बल्कि यह व्यवस्था और उसकी कार्यपद्धति है ।
उनका अंदाजा सही है । समस्या तो व्यवस्था है । अगर हालात की बेहतरी के लिए कुछ करना है तो इस व्यवस्था की कार्यपद्धति को समझना होगा । इस सिलसिले में उन्होंने कुछ बातों को सूत्रवत व्यक्त किया है । पहली बात कि पूंजीवाद व्यक्तियों का समूह नहीं है बल्कि इसके तहत व्यक्तियों को सामाजिक वर्गों में बांटा जाता है । अलग अलग वर्गों के लोग अलग अलग आर्थिक हालात का सामना करते हैं । वर्गों में लोगों की मौजूदगी इससे तय होती है कि उनके पास जमीन, कारखाना, बैंक, होटल आदि उत्पादन के साधन हैं या नहीं । जिनके पास ये साधन नहीं होते वे अपनी आजीविका के लिए इन साधनों के मालिकों यानी पूंजीपतियों के पास काम करते हैं । इस तरह पूंजीवाद में अधिकांश लोग कामगारों में बदल जाते हैं और उनके पास पूंजीपतियों के हाथों अपनी मेहनत बेचने के अलावे कोई मार्ग नहीं रह जाता जिससे तैयार माल और सेवाओं को पूंजीपति बेचता है । दोनों को बाजार में बेचना पड़ता है लेकिन उनकी बिक्री में भारी अंतर होता है । इसका मतलब कि उनके हित अलग अलग होते हैं । पूंजीपति अधिकतम मुनाफ़ा हासिल करना चाहता है जिसके लिए उसे हमेशा कामगारों से युद्धरत रहना होता है । प्रत्येक मालिक की यह कोशिश रहती है कि सस्ती से सस्ती लागत पर उसका माल तैयार हो । इसके लिए वह कामगारों की पगार बहुत कम रखना और बदले में अधिक से अधिक काम कराना चाहता है । उसकी यह कोशिश कामगारों की इच्छा के विरुद्ध होती है । वह तो पगार कम रखना चाहता है जबकि कामगार अधिक से अधिक पगार पाना चाहते हैं । मालिक काम तेजी से पूरा कराना चाहता है जबकि कामगार उसकी रफ़्तार कम रखना चाहते हैं । मालिक के शक्तिशाली होने के कारण कामगारों को उनकी शर्त मजबूरन माननी पड़ती है । पूंजीपतियों द्वारा शोषण की वजह यह नहीं होती कि वे बुरे या लालची होते हैं बल्कि बाजार में जिस होड़ का उन्हें सामना करना पड़ता है उसके दबाव में वे ऐसा करते हैं । अगर कोई कम लागत में वस्तु नहीं बनाता तो उसके ग्राहक टूट जायेंगे । इससे बचने के लिए वह कीमत बहुत घटा देता है । अब अगर उसकी लागत भी कम नहीं होगी तो उसे घाटा उठाना पड़ेगा । इसलिए वह पगार में घटोत्तरी करता है । किसी भी व्यवसाय के बाजार में टिके रहने के लिए यह जरूरी होता है । इसका लालच से कोई लेना देना नहीं होता । इसी वजह से पूंजीवाद अकूत संपत्ति और अपार दरिद्रता को एक साथ जन्म देता है । उसकी संपत्ति से एकांगी समृद्धि का जन्म होता है । उत्पादकता बढ़ने के साथ अगर पगार भी बढ़े और काम का समय घट जाये तो कामगार की हालत बेहतर होगी लेकिन मुक्त बाजार में यह सम्भव नहीं है । उत्पादकता बढ़ने से हासिल लाभ कामगारों के पास नहीं पहुंचते । मालिक या तो उसका फिर से निवेश करता है या अपने हिस्सेदारों को बांट देता है या अपनी जेब के हवाले करता है । संपदा बढ़ने के बावजूद कामगार की पगार में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होती, उसका रोजगार असुरक्षित रहता है, उसे अधिक समय तक काम करना पड़ता है और सेहत गंवानी पड़ती है । इसी वजह से विषमता भी बढ़ती चली जाती है । मालिक और कामगार को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है लेकिन वे समान नहीं होते । मालिक के मुकाबले कामगार हमेशा मजबूर रहता है । उनके पास इतनी बचत ही नहीं होती कि वे काम करने से इनकार कर सकें । उन्हें काम से हटाये जाने की आशंका हमेशा बनी रहती है । इससे पार पाने का एकमात्र उपाय उनकी आपसी एकता है । अलग अलग कामगारों के हित तभी सुरक्षित होंगे जब वे सामूहिक संगठनों का निर्माण करें । यह सीख आज भी उतना ही कारगर है जितना दो सौ साल पहले थी ।
इन बातों को स्पष्ट करने के बाद लेखक ने पूंजीवाद को परिभाषित करने की कोशिश की है । यह एक खास तरह की आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निश्चित आबादी के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खास तरह से उत्पादित किया जाता है लेकिन यही एकमात्र व्यवस्था नहीं रही है । इसके अतिरिक्त दासता और सामंतवाद भी आर्थिक व्यवस्था के अन्य रूप रहे हैं । इन अन्य व्यवस्थाओं से पूंजीवाद का अंतर बाजार पर निर्भरता से पैदा होता है । पूंजीवादी समाज में अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए बाजार की शरण में जाते हैं । रोटी, कपड़ा या मकान जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी खरीद बिक्री का सहारा लेना पड़ता है । इन्हें बनाने का विकल्प उनसे छिन चुका है । बाजार आधारित इस व्यवस्था की कुछ मूलभूत विशेषता होती है । सबसे पहली बात कि उत्पादन अपने उपभोग के लिए नहीं बल्कि बाजार में खरीद बिक्री के लिए किया जाता है । स्वाभाविक रूप से बिक्री किसी और को ही होगी । इसके कारण उत्पादन के सभी पक्षों पर गहरा असर पड़ता है । आर्थिक फैसले लेने वालों को सामान के खरीदार खोजने पर सारा ध्यान लगाना पड़ता है । वस्तु या सेवा की गुणवत्ता या अपने लिए उपयोगिता से उनको कोई मतलब नहीं रह जाता । खरीदार की चाहत का ही मूल्य महत्व रह जाता है ।
इसी बात को एक और तरीके से भी कहा जा सकता है कि पूंजीवाद में रोजगार का रूप पगारजीवी श्रम का हो जाता है । मानव इतिहास के लिए यह बात नयी है क्योंकि अधिकांश समय तक अधिकतर मनुष्य स्वरोजगारी रहे हैं । किसान या दस्तकार के रूप में वे अपने खेत या कार्यशाला में काम करते रहे । पूंजीवाद में यह आत्मनिर्भरता अपवाद है दूसरों के लिए ही काम नियम है । मालिक के निर्देश पर साझा सहमति से तय समय तक और तय भरपाई की दर पर काम करना होता है । घंटे की दर से मिलने वाली रकम को पगार या मजदूरी कहते हैं । इसका मतलब है कि जहां काम करना है उस जगह पर मालिक का ही अधिकार रहता है । वे ही तय करते हैं कि कितने लोगों को काम पर रखना है और किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है । इन्हें पूंजीपति और उनकी संपदा को ही पूंजी कहा जाता है । पूंजीवादी व्यवस्था के लिए ये तीनों ही तत्व जरूरी हैं । इन सबके जरूरी होने के बावजूद निजी स्वामित्व ही इसकी जान है । पगारजीवी श्रम इससे पहले की व्यवस्थाओं में भी मौजूद रहा था तथा व्यापार और विनिमय भी होता रहा था लेकिन इनकी मौजूदगी समूचे समाज के मुकाबले बहुत कम थी । आम तौर पर खेती से होने वाली पैदावार में कुछ जोड़ने के लिए लोग श्रम करके पगार पा जाते थे । पगार पर ही पूरी तरह निर्भर लोगों की तादाद बेहद कम थी । इसी तरह व्यापार भी सदियों से मौजूद था लेकिन जीवित रहने के लिए विनिमय पर ही पूरी तरह निर्भरता बहुत कम लोगों की थी । बाजार में वही सामान पहुंचता था जो बुनियादी उपभोग से बचा रह जाता था । उत्पादन का लक्ष्य बाजार में विक्रेय सामग्री का निर्माण नहीं था । जो कुछ बनता वह निजी उपभोग के लिए होता था । मतलब कि पगारजीवी श्रम, व्यापार या विनिमय की मौजूदगी से ही पूंजीवाद का अस्तित्व साबित नहीं होता । ये सब तो पूंजीवाद से पहले से मौजूद रहा है । पूंजीवाद में ये आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में आ गये । उत्पादन और वितरण का संगठन इनके ही लिहाज से होने लगा ।
पगारजीवी श्रम और व्यापार पूंजीवाद के अभिलक्षण तभी बने जब वे समूचे अर्थतंत्र के नाभिक बन गये । ऐसा तभी हो पाया जब उत्पादन के साधनों तक अधिकांश लोगों की पहुंच को समाप्त कर दिया गया । इतिहास में अब तक अधिकतर लोगों का जीवन अपनी जमीन पर बीतता रहा था और जमीन के टुकड़ों पर अलग अलग परिवारों के अधिकार को सामाजिक मान्यता प्राप्त थी । जमीन पर जब तक उनका अधिकार था वे अपने उपभोग के लिए फसल उगाते थे । उन्हें बाजार में बेचने या पगार पर काम करने की जरूरत ही नहीं थी । बाजार में लेन देन भी होता था और कभी कभी वे पगार पर काम भी कर लिया करते थे । इससे उनको अतिरिक्त आमदनी और उपभोग्य वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती थी । उत्पादन के साधनों पर अधिकार होने से वे बाजार की ताकतों को काबू में रखे हुए थे ।
ज्यों ही मनुष्य को उत्पादन से उसके साधनों से अलगा दिया जाता है, जमीन और पूंजी तक उनकी पहुंच नहीं रह जाती उनके आर्थिक पुनरुत्पादन के हालात बदल जाते हैं । अब वे जीने के लिए अपनी फसलों या दस्तकारी पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भी अब अपने उपभोग की वस्तुओं को बाजार से खरीदना पड़ता है । इस खरीदारी के लिए उन्हें धन उपार्जित करने का तरीका खोजना पड़ता है । धन की प्राप्ति के लिए उन्हें उत्पादन के साधनों के मालिकान यानी पूंजीपतियों के पास काम करना पड़ता है । कहने का तात्पर्य यह भी है कि पूंजीवाद के साथ ही खास तरह की वर्ग संरचना का भी आगमन होता है । इसमें उत्पादन के बुनियादी साधनों पर कब्जा जमाये लोगों का छोटा समूह एक ओर होता है जिन्हें पूंजीपति कहा जाता है । दूसरी ओर विशाल बहुसंख्या होती है जिनके पास इन पूंजीपतियों से रोजगार मांगने के अलावे कोई चारा नहीं होता । इसी समूह को मजदूर वर्ग कहा जाता है । इसी वर्ग व्यवस्था के चलते सभी लोग बाजार पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं । इन दोनों वर्गों के निर्माण से बाजार समूचे समाज में व्याप्त हो जाता है ।
व्यापक आबादी से उत्पादन के साधन छीनकर दो मामलों में बाजार का निर्माण होता है । रोजगार की खोज के कारण श्रम बाजार पैदा होता है । पूंजी के मालिकान किसी वस्तु के उत्पादन के लिए इस बाजार श्रमिक ला सकते हैं । दूसरी ओर ये श्रमिक अपने उपभोग के लिए वस्तुओं की खरीदारी करते हैं तो उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का बाजार भी बन जाता है । इससे पहले यह बाजार नहीं था क्योंकि लोग निजी उपभोग के लिए अपने ही उत्पादन के साधनों पर निर्भर थे । इन दोनों मामलों में बाजार का अस्तित्व पहले या तो था ही नहीं या बहुत ही कम था । इस बाजार के हाशिये पर होने का कारण निजी संपत्ति का अभाव था और अधिकांश आबादी को जमीन से खदेड़कर मुट्ठी भर लोग उत्पादन और उपभोग के फैसले लेने का अधिकार हथियाकर अर्थतंत्र के नियंता बन जाते हैं ।
स्पष्ट है कि पूंजीवादी व्यवस्था में अधिकांश लोगों को दो वर्गों में बांट दिया जाता है । उत्पादन पर पूंजीपतियों का नियंत्रण हो जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए मजदूरों को नियुक्त करते हैं और उन्हें बाजार में माल के बतौर बेचते हैं । इस बिक्री से दोनों को आमदनी होती है । इस आमदनी की प्रक्रिया को समझाने के लिए लेखक ने मार्क्स के अर्थशास्त्र का सहारा लिया है ।