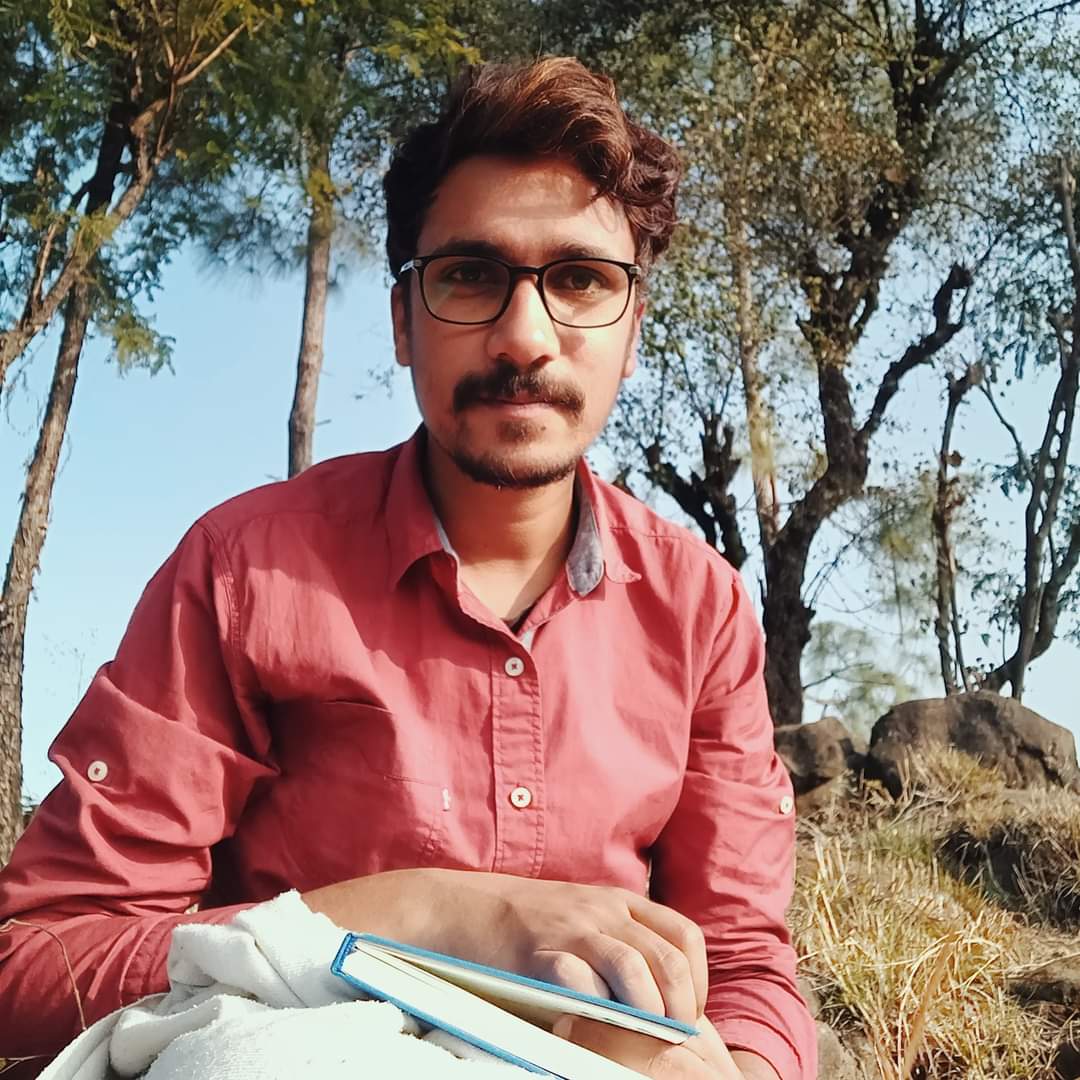(समकालीन जनमत की प्रबन्ध संपादक और जन संस्कृति मंच, उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीना राय का जीवन लम्बे समय तक विविध साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक हलचलों का गवाह रहा है. एक अध्यापक और प्रधानाचार्य के रूप में ग्रामीण हिन्दुस्तान की शिक्षा-व्यवस्था की चुनौतियों से लेकर सांस्कृतिक संकुल प्रकाशन के संचालन, साहित्यिक-सांस्कृतिक आयोजनों में सक्रिय रूप से पुस्तक, पोस्टर प्रदर्शनी के आयोजन और देश-समाज-राजनीति की बहसों से सक्रिय सम्बद्धता के उनके अनुभवों के संस्मरणों की श्रृंखला हम समकालीन जनमत के पाठकों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं. -सं.)
बचपन
एक बार गाजीपुर सर्कस लगा था। हम लोग मौसी को खिचड़ी नहाने चलने के लिए मना तो लिए लेकिन उनकी एक शर्त थी कि अगर लौटते समय भी तुम लोग बस से न आकर पैदल ही आओगी तो हम चलेंगे वरना नहीं। हम लोग उनकी शर्त मान लिए और खिचड़ी नहाने पैदल चल दिए। चित्तनाथ घाट नहाने के बाद बाजार गए। सभी लोग कुछ न कुछ सामान खरीदे उसके बाद मौसी से कहे कि सर्कस देखने चलो न। फिर हम लोगों को गाजीपुर इसके लिए कोई नहीं आने देगा। मौसी पहले तो कहीं कि पैसा नहीं है। जब सुनी कि सर्कस के उनके भी टिकट का पैसा हमीं लोग देंगे तो एक बार तो सर्कस देखने के लिए तैयार हो गईं। फिर पता नहीं क्यों कहने लगीं कि हमें अभी और भी बाजार करना है। तुम लोग सर्कस देखकर यहीं आ जाना मैं यहीं बैठी रहूंगी। हम लोग बहुत कोशिश किए लेकिन मौसी सर्कस देखने नहीं गईं और तीन घंटे दुकान पर बैठी रहीं। हम लोग सर्कस देखकर आए और मौसी के साथ बस स्टैंड गए। इतनी देर हो चुकी थी कि मौसी बस से लौटने के लिए तैयार हो गयी थीं। हां, उनका बस का भाड़ा हम लोगों को देना पड़ा था।
गरमी के दिन में जैसे ही स्कूल बंद होता था, चाचा सपरिवार गांव आ जाते थे। फिर नीरजा सुषमा और मैं बगीचे में सुबह चाय पीकर चले जाते थे। पूरे पचबखरी का बगीचा एक ही जगह था। हर घर से कोई न कोई रहता ही था। हम सभी ओल्हा पताई भी खूब खेलते थे। सबसे पहले सुरेश चाचा का बगीचा, फिर छांगुर काका का, उसके बाद बबुआ भइया का, फिर हम लोगों का, अंत में विजय भइया का। ऐसे ही टेका वाली बारी में भी क्रमश: सुरेश चाचा, छांगुर काका, विजय भइया, हमारा और अंत में बबुआ भइया का। बबुआ भइया का रोहनियवा आम सबसे पहले पकता था। सुरेश चाचा का लोढ़ियवा, छांगुर काका का बिछियवा, हमलोगों का सोनरियवा और विजय भइया का सुगउवा फेमस था। इसके अलावा करियई, करियवा, घीवहिया, सढ़ियवा, पिटहवा, मलदहिया, बइरियवा, झोपियवा आम भी था। दिन भर बगीचे में ही बीतता था। नीरजा पेड़ पर नहीं चढ़ पाती थी। सुषमा सीधे तने वाले (तरकुल जैसे) पेड़ पर बड़ी तेजी से चढ़ जाती, मैं नहीं चढ़ पाती। मैं टहनियां पकड़कर ऊंचाई तक चढ़ लेती थी। मुन्ना भइया खाना लेकर आते थे। मुन्ना भइया कभी कभी हम लोगों को दोपहर में नंगे पैर कसरत कराते थे। छांगुर काका के बिछियवा आम के पास की घास बहुत कड़ी थी। उसी पर या सामने खेत में लेफ्ट, राइट कराते। फिर जबतक पीछे मुड़ न बोलें हमलोग आगे बढ़ते रहते। फिर लौट कर खाना खाते थे। खाने में घर से रोटी सब्जी और मिर्चें का अचार आता था। उस समय छांगुर काका के यहां से राधिका दीदी की लड़की बृन्दा (गर्मी की छुट्टी में आ ही जाती थी) भी हमलोगों के खाना खाते समय रोज आ जाया करती थी। फिर सब्जी का आलू मसलकर मिर्चें का अचार भी उसी में मिला देते थे। तीखा होने से सब्जी कम नहीं पड़ती थी, लेकिन रोटी रोज कम पड़ जाय। जिसकी पूर्ति आम खाकर हो जाता कश्ती थी। मुन्ना भइया जब तक बगीचे में रहते हमलोग टेका वाली बारी में रहते। शाम को सबलोग साथ ही घर जाते। अगर अंधेरा हो जाय तो मुन्ना भइया नेटुअवा बाबा की बात कर हमलोगों को डराते भी थे। फिर उनकी शिकायत अशोक भइया से करके उनको मार भी खिलवाते थे हमलोग। फिर उनसे हमलोग मार खाएं। ये खेल की तरह चलता रहता था।
मेरा परिवार मध्यम किसान परिवार था। किसान को आर्थिक दिक्कत तो रहती ही है। लेकिन मां हमको कपड़े वगैरह ठीक ही दिलवाती थी। भरसक कोई कमी नहीं होने देती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई बंदिशें बढ़ने लगीं। आठवीं की परीक्षा देते ही पीरियड भी शुरु हो गया। अब तो स्कूल और स्कूल के बाद घर। पीरियड के लिए कपड़ा भी मुश्किल से मिलता था। भाभी लोगों को भी जरुरत होती ही थी। मां कुछ पुरानी साड़ी और बाबू की फटी धोती, लुंगी आदि रखी थी उससे काम चल जा रहा था। स्कूल टाइम मतलब हाई स्कूल तक किसी तरह बीता। पुराना कपड़ा भी अब नहीं मिल पा रहा था। समाज में इसको इतना छिपा कर रखने की मान्यता थी जैसे कोई अपराध कर दिया हो। तीन दिन तक अछूत बना दिया जाता। किसी को छूते नहीं थे। मायके में तो फिर भी रसोई में चले जाते थे लेकिन भाभी लोग तीन दिन खाना नहीं बनाती थीं। किसी किसी के यहां तो बिस्तर पर सोने नहीं देते थे। जमीन में सोना पड़ता था। जाड़े के दिन में ऐसे लोगों के लिए एक कंबल अलग रहता था। जो अछूत की तरह घर के किसी कोने में रखा रहता था। खैर ये मेरे यहां नहीं था, हां चद्दर और रजाई/कंबल का कवर तीन दिन के बाद धोना पड़ता था। गांव में पीरियड में कपड़े की जगह राखी का उपयोग भी करने की बात सुनी थी। लेकिन पूछ नहीं सकते थे कि बेइज्जती होगी। उस समय जब छोटे बच्चे कहीं बाहर लैट्रिन करते थे तो उस पर राख डाल दिया जाता था। राख डालने से सफाई आसानी से हो जाती थी। फिर मैं लुंगी के मुलायम कपड़े के छोटे छोटे पैड के आकार के पैकेट बना लेते और दूधगाड़ा की राखी को गेहूं झारने वाले झरने से चालकर,उस पैकेट में भर कर, पैकेट का मुंह सूई धागे से सिलकर बंद कर देते और यही पैकेट पीरियड होने पर हम कपड़े की जगह लेते थे। शुरू में तो दिक्कत नहीं होती थी। चूंकि राख ब्लड सोख लेता था उसके बाद पूरा पैकेट कड़ा हो जाता था जिससे उसके अगल बगल का चमड़ा छिल जाता था। चलने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन मजबूरी थी। धीरे धीरे आदत बन गई थी। बाद में कभी कभी पुराना कपड़ा मिल जाता था। तो उस बार पीरियड का समय आराम से कट जाता था। बाद में मां ने पुराने कपड़े और पुरानी रुई की व्यवस्था कर लिया था।