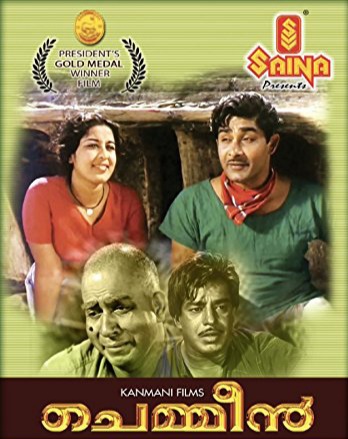वर्चस्वशाली समाज के विचार से शिक्षण की प्रविधि ही नहीं, उसकी भाषा और यहाँ तक कि वर्णमाला तक को भेद दिया करते हैं. वर्चस्वशाली विचार सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों तरह से शिक्षार्थियों को अपनी जद में लेने की कूबत रखते हैं. वर्चस्वशाली समाज के प्रतीकों की पहली शुरुआत माँ के दूध और ठोस शुरुआत वर्णमाला से शुरू हो जाती है.
विद्यालय या पाठशालाएं कोई निरापद व्यवस्था नहीं होती हैं. और हो भी नहीं सकतीं. समाज से इनका गहरा जुड़ाव रहता है. समाज की रवायत से शिशु पाठशाला से लेकर विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक प्रभावित होते हैं (और करते हैं) क्योंकि विद्यार्थी और शिक्षक के साथ-साथ पाठ्य सामग्री का मानस कहीं न कहीं प्रभावशाली समाज की मान्यताओं, विचारों और आग्रहों-दुराग्रहों से निर्मित होता है. ये सारी प्रवृत्तियां शिक्षण संस्थाओं में होने वाले आचरणों पर दबाव डालती हैं. समाज के प्रभु वर्गों की मान्यताओं का असर किसी न रूप में शिक्षण संस्थानों के अन्दर और बाहर घटित होती क्रूरताओं पर अवश्य पड़ता है. शिक्षा समाज मनोविज्ञान के विद्वान इस दिशा में कार्य कर रहे हैं.
भारत की प्राथमिक पाठशालाओं की दीवारों पर एक लोकप्रिय युक्ति पढ़ने को मिलती है – ‘ज्ञानार्थ आइए और सेवार्थ जाइये’. हमारे देश के साथ-साथ दुनिया के दूसरे देशों की शिक्षा का भी यही उद्देश्य है. यह ध्येय वाक्य भारतीय संविधान से प्रभावित है. लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में इस ध्येय वाक्य की महत्त्वपूर्ण भूमिका है. जिस तरह का ज्ञान विद्यार्थी पाते हैं, वैसा ही आचरण वे अपने सार्वजानिक जीवन में करते हैं. इसलिए विचारणीय है कि जो कुछ शिक्षण संस्थाओं में घटित होता आ रहा है, क्या वह सब इस ध्येय वाक्य के अनुकूल है?
शिक्षण संस्थाओं के अतिरिक्त एक दूसरा माध्यम सोशल मीडिया भी है, जहाँ से विद्यार्थी विभिन्न तथ्यों को हासिल करते हैं. युवाओं का शिक्षण संस्थाओं और सोशल मीडिया से गहरा नाता है. ज्ञान, प्रेम और नफरत की अनुभूति फैलाने में इनकी ऊर्जा इन्हें सबसे महत्तवपूर्ण बनाती है. अभी कुछ दिनों पहले पंजाब में एक दलित युवा की हत्या, आर्यन खान विरोधी टिप्पणी और दीपावली को एक खास तबके की परंपरा के पर्व के प्रचार-प्रसार में युवाओं की भूमिका सर्वोच्च रूप में दर्ज हुई. युवाओं का रुझान मानवतावादी न होकर लिंग, धर्म, जाति और वर्ग से निर्मित होता नजर आता है. ऐसे में शिक्षण संस्थाओं का ध्येय वाक्य (‘ज्ञानार्थ आइए और सेवार्थ जाइये’) और लोक कल्याणकारी राज्य के साथ-साथ भारतीय समाज की भूमिका भी प्रश्नांकित हो जाती है.
किसी भी देश की तरह भारत के विद्यालय भी वृहत समाज का सूक्ष्म रूपक हैं. समाज की विरूपताएं शिक्षण संस्थाओं में प्रतिलक्षित होती ही हैं. आजादी के समय स्वदेशी और सरकारी शिक्षण संस्थाएं आज़ादी के मतवालों का गढ़ हुआ करती थीं. उस समय के शिक्षण परिसरों में आज़ादी के ख़याल और ख्वाब बुने जाते थे. स्वस्थ समाज के लिए संगठन बनते थे. अर्थात समाज के मिजाज का असर दूसरी संस्थाओं की तरह शिक्षण संस्थाओं पर हमेशा से पड़ता आया है. इसलिए आज भी समाज के फांक और विभाजन के तमाम कारकों की उपस्थिति प्राथमिक पाठशालाओं से लेकर उच्च तकनीकी संस्थाओं तक में पाई जा रही हैं. समाज में उपस्थित ऊंच-नीच की मर्यादाएं शिक्षण संस्थाओं का भी सच हैं. ताज़ा उदाहरण आई.आई.टी. मुंबई का है, जहाँ प्रिंस नाम के एक दलित विद्यार्थी को आई.आई.टी. मुंबई प्रशासन द्वारा ऑनलाइन फीस जमा न कर पाने के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया. बाद में बम्बई उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से उसे वहां प्रवेश मिल पाया. इन दिनों ऐसे कई उदाहरण सामने आये हैं, जिससे पता चलता है कि डिजिटल होती व्यवस्था ने इस महादेश के वंचित तबके को हाशिये पर डालकर एक प्रकार का डिजिटल सामाजिक विभाजन निर्मित किया है. और इससे वंचनाओं का विस्तार हुआ है. यही कारण है कि शिक्षण संस्थाओं में आने वाले दलित, आदिवासी और पिछड़े तबके के विद्यार्थियों का अनुभव अगड़ी जमात से आये विद्यार्थियों से काफी हद तक मुख्तलिफ होता है.
ऐसा इसलिए है, क्योंकि हर विद्यार्थी का सामाजिक यथार्थ एक दूसरे से काफी अलग है. इस तरह भारतीय समाज के विद्यालयों की कक्षाएं, व्यवस्था और परिसर अलग-अलग सामाजिक सच्चाई और अनुभव वाले लोगों से आबाद हैं. यह अलगाव स्वाभाविक है. व्यवस्था को इस हकीकत को स्वीकार करके निदान की ओर बढ़ना चाहिए. निजी शिक्षण संस्थाओं में इस तरह का अंतर कम है. मगर वहाँ भी विद्यार्थियों के सांस्कृतिक धरातल का अंतर कहीं बहुत साफ तो कहीं छिपे या महीन रूप में विद्यमान मिलता है. मगर शिक्षण संस्थाएं अलग-अलग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले हर तरह के विद्यार्थियों के साथ एक सा ही व्यवहार करती हैं. विद्यार्थियों को एक से आचरण का अभ्यस्त बनाने के लिए इन संस्थाओं द्वारा कई कदम उठाये जाते हैं, जैसे उन्हें एक समान ड्रेस, समान शिक्षण, मूल्यांकन के समान मानकों और एक सी अनुशासन व्यवस्था में ढलने के लिए बाध्य किया जाता है. अलग-अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों को एक समान ग्रेड पॉइंट पर तौला जाता है. गरीब और पिछड़े तबके से आने वाले विद्यार्थी जब इन मानकों पर खरा नहीं उतर पाते तो उन्हें मानसिक अवसाद का सामना करना पड़ता है. और इस तरह समान बनाने वाले प्रहसन का अंत अत्यंत भयावह तरीके से होता है. कई बार इस कोशिश में समता स्थापित करने वाली चादर दरक जाती है. विशेष तबके से आने वाले बच्चों की विशिष्टता का मजाक इस तरह उड़ाया जाता है – ‘कमजोर तबके के बच्चे संसाधन ही नहीं, बुद्धि, विवेक और समझदारी में भी कमजोर होते हैं.’
शिक्षण संस्थाओं द्वारा ऐसा व्यवहार संभवतः इसलिए होता है, क्योंकि वे समाज में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संसाधनों के अंतर को स्वीकार नहीं कर पाते हैं. साथ ही इन संसाधनों से प्राप्त सहूलियतों की जमीन की अनदेखी करते हैं. प्रकृति की हर चीज निराली और खुद में काफी अलग है. अलगाव से प्रकृति का रंग निखरता है. इसी से अलग-अलग जाति समूहों का निर्माण होता है. इस मामले में हमारी शिक्षण संस्थाएं उल्टी गंगा बहाती जान पड़ती हैं. सामाजिक विभेद और स्तरीकरण से उत्पन्न हुई वंचनाओं को शिक्षण संस्थाओं द्वारा नकारा जाता है और ज्ञान की जोत जगाने वाली संस्थाओं की ओर से यह जताया जाता है कि विभन्न प्रकार की अस्मिताओं और वंचनाओं को सहने वाले विद्यार्थी पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आकर अपनी भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विशिष्टता के तमाम तंतुओं को त्याग कर एक सा बर्ताव करेंगे. हालांकि यह ऐसा ख्वाब है, जो अभी तक सच होता नहीं दिख रहा. समय-समय पर इस मान्यता के ख़राब परिणाम जरूर सामने आते रहे हैं.
पाठ्यक्रम किसी भी शिक्षा संस्थान का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते हैं. इसी के माध्यम से विद्यालय और विद्यार्थी, दोनों का भविष्य बनता है, और कभी-कभी बिगड़ता भी है. पाठ्यक्रमों के आधार पर ही प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होता है और बाद में सफल आवेदकों का नियोजन भी होता है. इसीलिए इसे ऐसा होना चाहिए जिसमें समाज के हर तबके से आने वाले शिक्षार्थी के ज्ञान और अनुभव को उपयोग हो सके ताकि वह अलगाव को महसूस न करे और पढ़ाई जाने वाली चीज अपनी सी लगे. लेकिन क्या ऐसा है? हमारी शिक्षण संस्थाएं कुछ इस तरह से अभिकल्पित की गई हैं कि पाठ्यक्रमों का स्वरूप सर्व समावेशी नहीं है. इसके अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली किताबें भारतीय समाज की विविधताओं की नुमायन्दगी नहीं कर पातीं. इन पाठ्यपुस्तकों के लोकतान्त्रिक हुए बगैर विद्यार्थी भी लोकतान्त्रिक मूल्यों वाले नहीं ही सकते, क्योंकि उनकी सोच-विचार को खाद-पानी और ऑक्सीजन यहीं से हासिल होता है.
पाठशालाओं और विद्यालयों में आने वाले विद्यार्थी घर, माँ-बाप, भाई-बहन और अड़ोस-पड़ोस में जिस भाषा संस्कृति, ज्ञान और व्यवहार को सीखते हैं, वह इन शिक्षण संस्थानों में व्यवहृत नहीं होती है. इससे विद्यार्थियों को दो अलग-अलग दुनिया के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ता है, जिसमें वे हर बार सफल नहीं हो पाते और वे अवसाद का शिकार हो जाते हैं. शिक्षण संस्थानों ने माना है कि इस तरह की समस्या है और इसके समाधान के लिए उन्होंने काउंसिलिंग केंद्र की स्थापना की है. कहीं-कहीं अभिभावकों को समझाया जाता है कि वे विद्यालय जैसा माहौल घर पर दें. इस तरह हमारे नौनिहालों का घर भी उनसे छीना जाता है.
असहज पाठ्यक्रम तमाम असहजताओं को जन्म देते हैं, जिनमें से कुछ पर बात कर लेना जरूरी है. किताबें पाठ्यक्रमों का जरूरी हिस्सा हुआ करती हैं. ये विद्यार्थियों की समझ विकसित करने में मदद करती हैं. इनका असर विद्यार्थी से होते हुए समाज के भविष्य पर पड़ता है. उदाहरण के लिए देवनागरी के वर्ण और अक्षर सर्वसमावेशी नहीं हैं. इसमें त से तलवार, य से यज्ञ और र से रथ पढ़ाया जाता है. तलवार, यज्ञ और रथ एक खास तबके को आत्मविश्वास से भले भर देते हों, मगर समाज के बड़े तबके के आत्मविश्वास का हरण अवश्य कर लेते हैं. छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक में तमाम खामियां हैं. पाठशालाओं से लेकर उच्च कक्षाओं में अभी तक वह पाठ्यक्रम आत्मसात नहीं हो पाया है, जो लैंगिक विभेद, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, थर्ड जेंडर और शोषित-वंचित तबके से आने वाले विद्यार्थी को आत्मविश्वास से लैस करता हो. इन पाठ्यक्रमों को सत्यापित और प्रत्यक्ष बनाने में उपयोग में आने वाली किताबें इन तबकों से आने वाले विद्यार्थियों को अँधेरे से भर देती हैं. क्योंकि किताबों में औरतों को या तो असहाय या वीर दिखाया जाता है. वास्तविक औरत का किताबों के पन्नों में आना अभी बाकी है. जिन्दा औरत किताब के पन्नों में कैद औरत से बहुत आगे निकल चुकी है. और किताब की औरत अभी भी पुरुष के पीछे चल रही है या तलवार भांज रही है. दिव्यांग और एलजीबीटीक्यू का प्रतिनिधित्व और आन्दोलन समाज में चाहे जितना हो, मगर वे किताबों के किरदार या तो बन नहीं पाए हैं और जहाँ कहीं बने भी हैं तो बड़े असहाय और मोहताज़ किस्म के. लोकतंत्र को मजबूत बनाने में जितनी हिस्सेदारी वंचितों, दलितों और आदिवासियों की है उतनी किसी और की नहीं फिर भी स्कूल की किताबें इन्हें गन्दा, आलसी और नशा करने वाला बताती हैं. संघर्षशील समाज का वास्तव दिखाने में किताबें असफल साबित हुई हैं.
हम एक महादेश के निवासी हैं. हम धर्म, जाति और अलग-अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं. यह विविधता हमें सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से समृद्ध, विशिष्ट बनाती है. हमारी विरासत इस विविधता का हासिल है. इतने वैविध्यपूर्ण और विशिष्ट विरासत को पाठ्यक्रमों में भी दिखाई देना चाहिए. परन्तु ऐसा नहीं है. देखना गौरतलब है कि इसमें अल्संख्यकों को कैसे दिखाया जाता है. पाठ्यक्रमों और किताबों में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों को अन्य के भाव और कभी-कभी आक्रान्ता के रूप में दिखाया जाता है. कक्षाओं में अध्यापक और विद्यार्थी उन्ही असंतुलित वास्तविकताओं को लेकर जाते हैं, जो विद्यालय के बाहर के आचरण में उपस्थित होता है. शिक्षण संस्थान तमाम असंतुलनों को समाप्त करने की जगह उनके अभ्यास के केंद्र बन कर रह गए हैं. इसीलिए इतिहास की किताबों और पाठ्यक्रमों पर फेरबदल का सबसे अधिक दबाव है. ऐसा इसलिए है क्योंकि समाज ही शिक्षण संस्थाओं को जन्म देते हैं. शिक्षा केन्द्रों की वास्तविकता अगर समाज की वास्तविकता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं. बस इससे यही दो बातें सामने आती हैं. पहला यह कि शिक्षालय अब भी समाज को दिशा दिखाने की जगह, उसी से दिशा ले रहे है हैं. दूसरा यह कि समाज कुछ खास लोगों के द्वारा संचालित हो रहा है, जो बहुसंस्कृति को पसंद नहीं करते. और ऐसा हमारे महादेश और दुनिया के कुछ दूसरे देशों में एक साथ हो रहा है. इसलिए पाठ्यक्रमों और किताबों पर वर्चस्वादी ताकतों के प्रभाव की समस्या राष्ट्रीय और वैश्विक, दोनों एक साथ है.
पाठ्यक्रम और किताबें खास तरह की शुचितावादी दृष्टि के दबाव से गुजर रही हैं, जिसके कारण इनके पृष्ठों पर सामाजिक बुराइयों के उल्लेख और अंतर्विरोध के लिए कोई जगह नहीं है, ताकि विद्यार्थियों को इन बुराइयों और अंतर्विरोधों से दूर रखा जा सके. यही कारण है कि कुछ हाशिये से आये बच्चे समाज और शिक्षण संस्थानों के परिवेश में कोई अंतर नहीं पाते और वे दोनों जगह एक समान उपेक्षा महसूस करते हैं. तमाम बच्चे इस अहसास में जीने के अभ्यस्त हो चुके हैं कि शिक्षालयों का सकारात्मक बदलाव से कोई सीधा रिश्ता नहीं है.
विद्यालयों और पाठशालाओं में जो पढ़ाया जाता है, उसका विद्यार्थियों के मानस पर अप्रत्यक्ष प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है. इन प्रभावों से विद्यार्थियों में जो आग्रह (दुराग्रह) पनपते हैं, वह ऐसे लेंस का काम करते हैं, जिनसे वे आसपास की घटनाओं को देखते और समझते हैं. इन्हीं आग्रहों से वे स्वयं के द्वारा दूसरों के खिलाफ किये गए दुर्व्यवहारों सही ठहरा पाते हैं.
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 (National Curriculum Framework-2005) की ओर से भारतीय विद्यालयों की अध्यापन प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन करने का प्रयास किया गया. विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली वह किताबें, जो सामाजिक और राजनीति विज्ञान की थीं, वह कुछ मायनों में अच्छी थीं. इन किताबों ने समाज की स्याह सच्चाइयों को रेखांकित किया और दलितों व वंचितों के साहित्य को शामिल करके हाशिये की आवाज को पाठ का हिस्सा बनाया. किन्तु ये किताबें पूरी तरह से निरापद नहीं कही जा सकती हैं. क्योंकि इन किताबों में दलितों और आदिवासियों के त्याग को एक खास रंग देने के उद्देश्य से प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है, उद्धरण के रूप में एकलव्य द्वारा गुरुदक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य को अंगूठा दान वाले प्रकरण को त्याग और श्रेष्ठ मूल्य के रूप में उत्सवधर्मी तरीके से दिखाया गया है. किताब में यह प्रकरण प्रसंशात्मक तरीके से दर्ज़ हुआ है, जबकि इसकी अवहेलना होनी चाहिए थी. क्योंकि ऐसे प्रसंगों के सम्मान से समाज में पहले से व्याप्त असमानताओं को बल मिलता है, मगर ऐसा होता नहीं दिख रहा. किताबों के पन्ने ऐसे तमाम आख्यानों से भरे पड़े हैं. इन पन्नों से उत्पन्न विषमता का अध्ययन होना चाहिए. इस प्रकरण से सहज कल्पना की जा सकती है कि किसे त्याग करना और किसे त्याग का लाभ लेना है. जाहिर सी बात है इस तरह की कथाएं असमानता और हिंसा को महिमामंडित करती हैं. ऐसे आख्यान पाठशालाओं और विद्यालयों में प्रशिक्षित हो रहे कोमल मस्तिष्कों में एक तरह की बायनरी की फसल तैयार करते हैं. साथ ही कोमल मस्तिष्कों को गुप्त और कभी-कभी प्रत्यक्ष रूप से हिंसा के लिए तैयार करते हैं. एक बार विचार अवश्य किया जाना चाहिए कि पाठशालाओं की प्रार्थनाएं, पाठ, और गौरवगाथाएं कही नफ़रत और हिंसा को बल तो नहीं दे रहीं. जरूरत पड़ने पर शिक्षण संस्थाओं के उन पन्नों को एक बार जरूर पलट लेना चाहिए जो नफरत और हिंसा के रंग में रंगे हुए है.