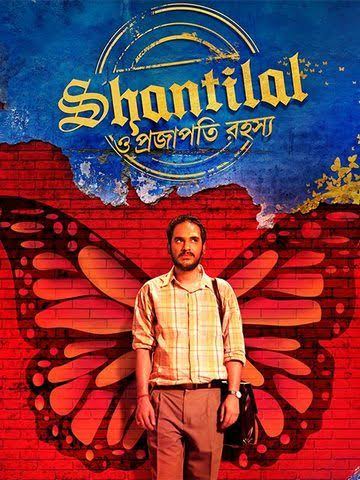कौशल किशोर
‘इस बुरे वक्त को
बुरा कहना ही पड़ेगा कवि को।
जिंदा रहने के लिए
लिखनी ही पड़ेंगी कविताएँ
दमनकारी ताकतों के खिलाफ
उनके कैदखानों में जगहें कम पड़ जाने तक।’
परिमल के लिए कविता लिखना ज़िंदा रहने की शर्त है और दमनकारी ताकतों के खिलाफ संघर्ष भी है। इस तरह कविता बर्बरताओं के विरुद्ध बेहतर की आकांक्षा के लिए वरवर राव के संघर्ष से भावनात्मक रूप से जुड़ती हैं, वहीं उसके भीतर ‘दुनिया भर को प्यार करने’ की अदम्य आकांक्षा है। इसमें प्रेम है तो अन्याय का प्रतिकार भी है। कविता का मनुष्य तमाम विपरीतताओं से संघर्ष करता है। उनका भरोसा यूँ व्यक्त होता है: ‘मुझे यकीन है कविता!/कि जिंदगी के हर उतार-चढ़ाव में/तुम यूँ ही सदा/मेरा साथ देती रहोगी।’ प्रेम और प्रतिरोध से मिलकर ही इनकी कविता का व्यक्तित्व बनता है।
धान कूटती हुई औरतें
धान के साथ-साथ
कूटती हैं अपने दुख
अपनी तकलीफ
और अपने संताप को भी।
चावल के सफेद दानों में बदलते देख
उनकी आँखें
खुशी से फैल जाती हैं।
महुआ बीनती लड़कियाँ परेशान हैं।
जब महुआओं का वक्त बीत जाएगा
लहलहाएंगे पलाश
खूब-खूब उगलेंगे अंगारे
और पूरा का पूरा जंगल/शोलों में नहा जाएगा
महुओं में छिपाकर
अब पत्थर भी बीनने लगी हैं!
आपका मिजाज
आप की हस्ती
आपकी औकात
आपकी नस्ल
कुछ भी तो छुपी नहीं रह पाती उनसे।
और आपकी संपूर्णता बरकरार रखने में
सहायक है वे।
प्रवीण परिमल की नजर गाँव में आ रहे बदलाव पर है। यह पूंजीवादी आधुनिकता और संस्कृति की वजह से हो रहा है। ‘एक रिटायर्ड आदमी की वसीयत’ में गांव का जो वर्तमान रूप है, उसमें रहना और जीना मुश्किल है। ऐसे में शहर से उम्मीद है। वहीं, ‘शहर की बदबू’ में यही बात शहर के अंदर दिखती है। ये कविताएँ गांव और शहर के बीच बँटे और फँसे आदमी के द्वंद को व्यक्त करती हैं।
प्रवीण परिमल की कविताएँ
1. लिखनी ही पड़ेंगी कविताएँ
( वरवर राव के संघर्षों को याद करते हुए )
यह उसका जुर्म ही तो है
जो उसने रच डाली हैं कविताएँ
संवेदनहीन तानाशाहों के विरोध में।
शोषितों, दलितों, वंचितों के पक्ष में
आवाज़ें बुलंद करना
गुनाह नहीं है तो और क्या है!
जनांदोलनों की भट्ठियों में
संघर्षों की फूँकें मारना
अक्षम्य अपराध ही तो है!
– ऐसा सोचता है राजा
और डरता है
ऐसी कविताओं से।
इंक़लाब लानेवाले शब्दों से
डरती है निर्दय सरकार भी।
दिखाई पड़ने लगती है
उसकी कुर्सी ख़तरे में
और वाजिब सवालों से बचने के लिए
करने लगती है उपाय।
लगाए जाते हैं अवांछित इल्ज़ाम
कलमकारों पर
और क़ैद कर लिया जाता है एक कवि
क्रांति के बीज बोने के अपराध में।
यद्यपि जानता है राजा भी
कि बहुत देर तक
क़ैद नहीं की जा सकती हैं
लोकतांत्रिक आवाज़ें ।
समय कितना बुरा है!
इस बुरे वक़्त को
बुरा कहना ही पड़ेगा कवि को।
ज़िंदा रहने के लिए
लिखनी ही पड़ेंगी कविताएँ
दमनकारी ताकतों के ख़िलाफ
उनके क़ैदखानों में जगहें कम पड़ जाने तक।
2. महुए बीनती हुई लड़कियाँ
हर साल की तरह
इस साल भी टपक रहे हैं महुए !
एक अजीब-सी गंध फैली है चारो ओर।
सुबह-सुबह
अब दिखाई देंगी
महुए बीनती हुई लड़कियाँ
कच्ची उम्र की !
मैं सोचता हूँ
महुए बीनती हुई लड़कियाँ
लड़कियाँ होती हैं
या मजबूरी की कहानियाँ।
याद आते हैं मुझे
महुए बीनती हुई लड़कियों के समूह।
चुन-चुन कर महुए
पूरी लगन के साथ
करती हैं इकट्ठा लड़कियाँ
मानो महुओं की शक्ल में
बिखरे पड़े हों उनके सपने ।
सचमुच
महुए बीनती हुई लड़कियाँ
महज महुए नहीं बीनतीं…
बीनती हैं
भविष्य के लिए सपने भी ।
टपक रहे हैं महुए
बीनती जा रही हैं लड़कियाँ !
महुओं का ढेर क्रमशः बड़ा होता जा रहा है।
महुए बीनती हुई लड़कियाँ जानती हैं
इसी ढेर से निकलेगा
कटोरी भर बासी भात
कुछ सूखी रोटियाँ
चुटकी भर नमक
और पेट भर पानी।
कि ढेर जितना ऊँचा और बड़ा हो
उतना ही अच्छा है इनके लिए ।
कहाँ- कहाँ पहुँचते हैं
उनके बीने महुए
क्या – क्या होता है महुओं के साथ
महुए बीनती हुई लड़कियों को
कुछ भी पता नहीं।
महुए बीनती हुई लड़कियाँ जानती हैं
तो सिर्फ इतना
कि महुए से बनती हैं रोटियाँ
जिससे भरते हैं पेट
दुधमुँहें भाई- बहनों के
लाचार माँओं के
वृद्ध पिताओं के।
दिहाड़ी में मिले हुए महुए
बेचती हैं लड़कियाँ
बनिए की दुकान पर
लाती हैं बदले में गुड़ और नमक
थोड़ी चाय की पत्ती भी।
डंडी मारकर इतराता है बनिया
लेने में किलो का तीन पाव
और देने में तीन पाव का सेर !
महुए जाते हैं साहूकार के गोदामों में
करते हैं इंतज़ार सही वक़्त का
और कमाते हैं एक का कितना
साहूकार के लिए
महुए बीनती हुई लड़कियाँ नहीं जानतीं।
मुनाफ़े की रक़म
तिजोरी-बंद करते हुए
एक पल के लिए भी
नहीं याद करता है साहूकार
महुए बीनती हुई
इन लड़कियों को।
महुए बीनती हुई लड़कियाँ
महुए की ही तरह
किस दिन टपक जाएँगी
बाबूसाहेब के दिमाग़ में
लड़कियाँ नहीं जानतीं ।
लड़कियाँ फिर भी बीनती हैं महुए ।
महुए से चुआयी जाती है दारू
जिसे पीते हुए
नहीं पहचान पाते बाबूसाहेब
या उनका हितैषी दारोगा
या उनका रिश्तेदार मंत्री
कि उसमें महुए का रस कितना है
और लड़कियों के जीवन का रस कितना ।
लड़कियाँ जानती हैं
जानवर आजकल दोपाए हो गए हैं ।
दारोगा आज फिर शिकार पर आया है।
बाबूसाहेब की हवेली पर ठहरा है दारोगा
दारोगा अक्सर हवेली पर ही ठहरता है !
पैग- दर- पैग रंगीन होती है रात
भेड़ियों के मुँह से टपकता है लार
मुर्ग- मुसल्लम और ‘अंग्रेजी’ तो बहुत हुई
अब ‘देसी डिश’ की बारी है ।
जंगल में छूटते हैं
बाबूसाहेब के पालतू शेर ।
कच्ची उम्र की हिरणियाँ
दहशत से दुबकी हैं ।
दारोगा हवेली में बैठे- बैठे ही
शिकार करता है
उसके शिकार करने का यही ढंग है ।
दरअसल दारोगा सियार होता है
और सियार कभी खुद शिकार नहीं करता ।
महुए बीनती हुई लड़कियों पर शामत आई है !
बाबूसाहेब का बैठकखाना
जंगल में बदल चुका है ।
दीवारों पर टँगी
लकड़ी की कृत्रिम गर्दन में ठुँकी
बारहसिंघों के सीगों में तनाव व्याप्त है ।
दीवारों पर टँगी हुई खाल से निकलकर
बिस्तर पर आ गए हैं चीते
आँखों में विचित्र- सी चमक लिए हुए !
अजगर की देह
कुछ लपेटकर
उसे मरोड़ने को आतुर है ।
जंगली सुअर
दाँत पजा रहे हैं।
महुए बीनने वाली लड़कियाँ भयभीत हैं
कि किसी भी वक़्त
वे बनाई जा सकती हैं
नीचे की ज़मीन
जिस पर
पेड़ बनकर खड़े हो जाएँगे बाबूसाहेब
या उनका कोई मेहमान
और टपकते रहेंगे महुए–
टप्- टप् …
रात भर !
बाबूसाहेब के बैठकखाने से
मुस्कुराते हुए जाते हैं भेड़िए
गुर्राते हुए निकलते हैं सुअर
दहाड़ते हुए भागते हैं चीते
और कराहती हुई जाती हैं हिरणियाँ !
और ऐसे ही एक दिन
महुए बीननेवाली लड़कियाँ
बनती हैं अखबारों की सुर्खियाँ
ख़ुश होते हैं पत्रकार और फोटोग्राफर
लहराता रहता है तिरंगा संसद भवन पर
गर्म होती हैं चर्चाएँ !
भुने हुए काजू की तरह
दिनभर कुतरते हैं विपक्ष के लोग
लड़कियों के सवाल को
और महुओं के मौसम की ही तरह
बीत जाता है एक पूरा सत्र।
मुआवज़े की रक़म का
एलान करते हैं मुख्यमंत्री
ख़ुश होते हैं बिचौलिये ।
महुए बीनती हुई लड़कियाँ परेशान हैं !
जब महुओं का वक़्त बीत जाएगा
लहलहाएँगे पलाश
खूब-खूब उगलेंगे अंगारे
और पूरा का पूरा जंगल
शोलों में नहा जाएगा ।
हाँ देखो—
अब पलाश फूलने लगे हैं ।
महुए बीनती हुई लड़कियाँ
महुओं में छिपाकर
अब पत्थर भी बीनने लगी हैं !
3. धान कूटती हुई औरतें
ढेंकी में
धान कूट रही हैं औरतें!
अलसुबह
रात की काली चादर फाड़कर
सूरज के ऊपर चढ़ने से पहले
वे कूट लेना चाहती हैं
ज़रूरत भर धान।
धूप निकलते ही
देर रात तक
आँखें फोड़ते हुए
उसीने गए धान को
घड़ों से निकाल कर
सूखने के लिए
ओटे पर पसारती हैं औरतें
ऐसे, जैसे पसार रही हों वे
सुख और समृद्धि
समूची पृथ्वी के लिए।
फूस की छत से
लटक रही डोरी को पकड़कर
बनाती हैं वे अपना संतुलन
और पूरी ताकत के साथ
मारती हैं लात
ढेंकी की दुम पर
ऐसे, जैसे एक ही वार में
वे कुचल देना चाह रही हों
अपने दुर्दिन के साँप को।
बैलों के खूँटों पर लौटने से पहले
सूखकर खनखनाते हुए
धान के दानों को
बड़े जतन से बुहारती हैं औरतें
और जमा करती हैं उन्हें
खँचिया, सूप और दउरा में।
ढेर की शक्ल में
अपनी मेहनत का ईनाम देख
भीतर तक
भीग जाती हैं औरतें।
रंभाती हुई गाय की आवाज़ पर
बछड़े की रस्सी खोलती हुई
औरतों के स्तनों में भी
अनायास उतर आता है दूध।
थनों को अच्छी तरह फेनाने के बाद
बछड़े को पकड़कर
गाय के सामने ले आती हैं औरतें
और दुलराती हैं ऐसे,
जैसे दुलरा रही हों वे
पूरी सृष्टि को।
अपने आदमी के हाथों से
दूध- भरी बाल्टी लेकर
देर तक निहारती हैं औरतें,
जैसे हिसाब लगा रही हों
कि पास-पड़ोस के घरों में
बेचने के बाद
उनके बच्चों के हिस्से में
दूध की कितनी मात्रा आएगी।
धान कूटती हुई औरतें
धान के साथ-साथ
कूटती हैं अपने दुख
अपनी तकलीफ
और अपने संताप को भी।
धान को
चावल के सफेद दानों में बदलते देख
उनकी आँखें
खुशी से फैल जाती हैं।
कल्पना में ही
उन्हें दिखाई देने लगता है
आँच पर चढ़ा
खदकता हुआ भात
जिसकी प्रतीक्षा में
उनके बच्चे
अभी भी
लेदरा- कथरी में दुबके पड़े हैं
खाली पेट को
दोनों हाथों से दबाए हुए।
धरती का सीना फाड़कर
उनके आदमी
उगाते हैं धान के जिन दानों को
कूटते वक़्त
उन दानों पर भी
रहम नहीं करतीं ये औरतें।
ढेंकी में धान कूटती हुई
आत्मविश्वास से भरी ये औरतें
कितनी सुंदर लग रही हैं —
बिल्कुल मेरी माँ और दादी जैसी!
4. जंगल से लौटकर
उसके दादा ने
इसके दादा को रटवाया —
‘क’ से ‘कहार’ !
‘च’ से ‘चमार’ !!
इसके पिता ने
उसके पिता को समझाया —
‘भ’ से ‘भाईचारा’!
‘स’ से ‘सरोकार’!!
जंगल से लौटकर
उनसबको,
इसने सिखलाया —
‘क’ से ‘कटार’!
‘ग’ से ‘गँड़ासा’!!
‘ब’ से ‘बंदूक’!!!
5. हाथी
ग़नीमत है–
पेड़-पौधे और नदियाँ
धरती पर होती हैं,
अंबर पर नहीं!
यदि होते वहाँ भी पेड़- पौधे,
यदि होतीं वहाँ भी नदियाँ–
निस्संदेह, बस जातीं वहां भी आबादियाँ!
फिर तो, हाथी वहाँ भी पहुँच जाते।
बेशर्मी से नोचते पत्तियाँ, डालियाँ
मनमानी पूर्वक करते खिलवाड़
नदियों के जल से
और चिढ़ानेवाली मुद्रा में
डकारते-पादते
बड़ी ढिठाईपूर्वक
रास्तों में मल-मूत्र त्यागते
लौट आते
अपने सुरक्षागाह तक–
स्थापित राज के नियमों की
धज्जियाँ उड़ाते!
हाथी, अब अत्यंत महत्वाकांक्षी हो गए हैं!
उनके करतब,
अब सिर्फ सर्कस तक ही
सीमित नहीं रहे।
सड़क से संसद तक–
कुछ भी अछूता नहीं रहा
अब उनसे!
ऐरावत कहलाने की होड़ में
आबादियों को जंगलों में
तब्दील करने की साजिश में,
जुटे हैं हाथी!
कहते हैं–
पगला जाते हैं जब हाथी,
किसी को नहीं पहचानते।
रौंद देते हैं, खेत के खेत
नष्ट कर देते हैं, बाग के बाग
उखाड़ फेंकते हैं, वृक्ष के वृक्ष
और ध्वस्त कर देते हैं, मकान के मकान!
अपनी हवस के लिए–
हाथी, कुछ भी कर सकते हैं,
कुछ भी!!
6. मोची
स्टेशनों के बाहर
या बस – पड़ावों के क़रीब
या चौक – बाज़ारों की मुख्य सड़कों के किनारे
अक्सर बैठे मिल ही जाते हैं
मुफ़लिसी के ये रखवाले !
अपने शहर से लेकर
देश की राजधानी तक मैंने आज़माया है
हर जगह
इन अदने – से लड़ाकुओं को मैंने पाया है।
आप कहेंगे
मोचियों को मैं लड़ाकू क्यों कह रहा हूँ!?
इंसानियत की नज़र से यदि देखें
तो पाएँगे आप भी
कि ये मोची
अपनी लड़ाई के साथ -साथ
लड़ते हैं
मेरी और आपकी लड़ाई भी।
उनकी अपनी ग़रीबी
और मज़बूरियों के साथ
उन्हें लड़ते तो आपने भी देखा होगा
मगर क्या आपकी अपनी लड़ाई
उनके द्वारा लड़ा जाना
महसूसा है आपने?
कभी सोचा है
मध्यवर्गीय आबरू के
इन पहरेदारों के बारे में ?
फटे हुए जूते
टूटी हुई चप्पलें मरम्मत कराते वक़्त
एक पल के लिए भी नहीं सोचते होंगे आप
कि कितने करीने से मरम्मत करते हैं वे
फटे हुए जूतों के साथ – साथ
आपकी फटी हुई अस्मिता
और आपके दरके हुए विश्वास को
और टूटी हुई चप्पलों के साथ – साथ
आपकी टूटी हुई ज़िंदगी को
आपके बिखरे हुए इरादों को
और आपके डिगे हुए संकल्पों को।
आपके फटे हुए जूते सीकर
वे सी देते हैं
आपकी फटी हुई ज़िंदगी को
और आपको पता तक नहीं चलता।
जूतों के भीतर नए तल्ले डालकर
कीलों की चुभन से वे आपको बचाते हैं
कीलें, जो कभी महँगाई की मार के रूप में चुभती हैं
तो कभी ज़माने की चाल के रूप में।
दरके हुए सोलों में पैबंद लगाकर
ढक देते हैं वे आपकी ग़रीबी
आपकी मज़बूरियों को
और संभाल लेते हैं
आपके ढहते हुए इरादों को।
इस तरह
बना देते हैं वे
आपको वक़्त से लड़ने के क़ाबिल
तलवों के अग्रभाग में
‘लेमनचूस’ की शक्लवाली
सुरक्षात्मक कीलें लगाकर।
जानते हैं वे
चमड़े की तुलना में
लोहा कम एवं देर से घिसता है!
कितनी आसानी से
वे आपको
चमड़े से लोहे में बदल देते हैं
और आपको पता तक नहीं चलता।
बदरंग जूतों पर
पॉलिश की चमक चढ़ाते हुए
फ़क़त जूते ही नहीं चमकाते वे
चमकाते हैं आपकी बेडौल ज़िंदगी
आपके ऐंठे हुए इरादों को भी।
पुराने, टूटे हुए फीतों को बदलकर
नएपन के एहसास से
भर देते हैं वे
आपके व्यक्तित्व को।
जूतों पर जमी धूल झाड़कर
रखते हैं वे आपको तरोताज़ा
और जमी हुई कीचड़ों को पोंछकर
याद दिलाते हैं वे
आपको आपके जीवन का असली रंग।
यह आप समझते हैं
कि वे
टूटी हुई चप्पलें भर मरम्मत करते हैं
मगर मैं जानता हूँ
कि मरम्मत करते हैं वे
आपकी चरमराती हुई
आर्थिक स्थिति को भी।
मोम से रगड़कर
वे पहले धागों को बनाते हैं
मजबूत और टिकाऊ
फिर सीते हैं आपके जूते
उन धागों से
ताकि आपकी हक़ीक़त
आसानी से दुनिया पर उजागर न हो सके।
मरम्मत करते वक़्त
आपके जूतों के नंबरों पर ध्यान नहीं देते वे।
आपका पैर कितना बड़ा
या कितना छोटा है
इससे कोई मतलब नहीं उन्हें
आपका पैर किस हद तक सुरक्षित रहेगा
और पैरों से लगे आप
कहाँ तक चल पाएँगे
यही शामिल रहता है उनकी चिंता में।
मात्र जूता देखकर ही
वे आपके सारे अनुभवों को जान लेते हैं ।
कहाँ-कहाँ
कितनी चोटें
कितने घाव झेले हैं आपने
जूते में ही
आपके संघर्ष की
पूरी कहानी पढ़ लेते हैं वे।
मरम्मत करते वक़्त
जूतों से आपके मोजे निकालकर
एक किनारे रख देते हैं वे
बहुत ही संभालकर
सिकुड़े हुए ही।
उसे फैलाकर
सबके सामने
आपकी नुमाइश नहीं करते।
आपके मोजे
उंगलियों के पास से फटे होंगे
जानते हैं वे।
मोजों के ऊपरी हिस्से की एलास्टिक
अपना अस्तित्व खो चुकी हैं
और आपने
रबर-बैंड के सहारे
अपना वजूद संभाल रखा है
पता है उन्हें।
मोजे कितने पुराने
कितने जर्जर हो चुके हैं
आँखों से देखकर तो आप भी जान लेते होंगे
वे तो नाथुनों में घुसती हुई बास
उसकी गंध भर से पहचान लेते हैं
कि आपने पसीना बहाया है
तो कितना।
आपकी धमनियों में बहता हुआ रक्त
कितना गर्म है
कितनी ऊष्मा है उसमें
मोजे के स्पर्श मात्र से ही
जान लेते हैं वे।
एक ओर
हल्की घिसी हुई एड़ियों से ही
जान लेते हैं वे
कि आप बाएँ पैर पर ज़्यादा ज़ोर डालते हैं
या दाएँ पैर पर।
जीवन में आप
आहिस्ता-आहिस्ता घिसटते रहे हैं
या दौड़कर चलने के आदी रहे हैं।
कितने दिनों तक ये जूते
आपको काटते रहे हैं
और आपकी चाल
ज़माने से मेल क्यों नहीं खा रही है।
जूतों पर पड़ी खरोचों से ही
वे जान लेते हैं
कि अभी-अभी आप
चिकनी मिट्टी से होकर चले आ रहे हैं
या रेतीले रास्तों से
कँटीली झाड़ियों से गुज़रकर आए हैं
या पहाड़ी रास्तों से।
तारकोल की सड़कों के किनारे बैठे- बैठे ही
हर प्रकार के रास्तों का अनुभव हो जाता है उन्हें।
जूते ही उनके लिए स्लेट हैं
जूते ही उनके लिए किताबें हैं
और जूते ही उनके लिए ब्लैकबोर्ड!
स्कूल या कॉलेज की डिग्रियाँ हासिल नहीं हैं उन्हें
मगर वे आपकी चाल
आपके जूते की शक्ल देखकर ही बता सकते हैं
कि आप भले मानुष हैं
या बुरे।
आपका मिजाज़
आपकी हस्ती
आपकी औक़ात
आपकी नस्ल
कुछ भी तो छुपी नहीं रह पाती उनसे।
बिना जूतों के आप पूर्ण नहीं कहाते
और आपकी संपूर्णता बरक़रार रखने में
सहायक हैं वे!
7. बूढ़ा रिक्शावाला जब मुस्कुराता है
बूढ़ा रिक्शावाला जब मुस्कुराता है
आदमी भीतर तक चनक जाता है
यदि उसकी मुस्कुराहट का मर्म समझ ले।
उसकी मुस्कुराहट का सही अर्थ समझना
ठीक वैसा ही दुष्कर है
जैसा कि ‘मोनालिसा’ को समझ पाना।
हवा में तीर मारने जैसा
आसान नहीं है यह।
चक्र पर नाचती हुई
मछली की आँख है उसकी मुस्कुराहट
जिसे अर्जुन जैसा कुशल धनुर्धर ही
बेध सकता है।
तवायफ़ों
या नेताओं की तरह
उसकी मुस्कुराहट के ‘प्रकार’ नहीं होते।
बस
एक ही अंदाज़ में मुस्कुराता है वह —
सदा, सर्वदा।
चाहे यात्रियों की गालियाँ हों
या ऑटोचालकों की फटकारें
ट्रैफिक पुलिस के डंडे हों
या बिगड़ैल विद्यार्थियों के तमाचे।
अपनी फटी – चीकटदार चादर की तरह
वह ओढ़ता नहीं किसी भी बात को।
ललाट पर चुहचुहाते
पसीने की बूँदों की तरह
पोंछकर झटक देता है वह
भीतर के आक्रोश को —
एक ख़ास और स्थायी अंदाज़ में।
बस यही वो घड़ी होती है
जब वह
महज एक रिक्शाचालक भर नहीं रह जाता
बल्कि
एक कुशल कलाकार दिखने लगता है
जिसकी मुस्कुराहट देख
आदमी भीतर तक चनक जाता है।
8. एक रिटायर्ड आदमी की वसीयत
और जब मैं मृत हो जाऊँ
मुझसे संबंधित
कोई स्मारक शिलालेख
मत बनवाना, मेरे पुत्र!
मत बनवाना।
तेरहवीं के दिन
गाँव की आख़िरी सीमा पर
मुख्य मार्ग के किनारे
मुझे निर्वासित करते हुए
तुम्हें अफ़सोस तो होगा
— मैं जानता हूँ!
परंतु उससे ज़्यादा तकलीफ
मुझे होगी
जब
शहर से आती हुई हवाएँ
मेरे क़रीब से होकर
गाँव में प्रवेश करेंगी
और मैं देखता रह जाऊँगा।
मेरा नाम
वल्द पिता का नाम
मेरी पुण्यतिथि आदि
खुदे होने के बावजूद
मुझे पहचानने की फ़ुर्सत
किसी को नहीं होगी।
मेरी स्मारक शिला में
कोई
मेरे दुख
असंतोष
अथवा असफलता की कहानी
पढ़ने नहीं जाएगा।
बहुत होगा
तो गाँव की बकरियाँ
चरने के दरम्यान
मुझमें अपनी देह रगड़कर
खुजली मिटा लेंगी।
बहुत होगा
तो फतिंगों का शिकार करते हुए
तीतर
थककर
मेरी ओट में बैठकर
सुस्ता लेंगे।
बहुत होगा
तो ……
सेवानिवृत्त होते वक़्त
कितना खुश था मैं
कि शहर के बारूदी वातावरण से दूर
ज़िंदगी के मशीनीकरण को तोड़
कब पहुँचूँ मैं अपने गाँव!
कितनी ललक थी
गाँव आने की!
सोचता था
इतने दिनों में
मेरा लंगोटिया यार जुम्मन
कैसा दिखता होगा!
उसके घर की
ईद की सेवइयों का स्वाद
आज तक नहीं भूला हूँ मैं।
वह भी तो नहीं भूला होगा
होली के रंगों से पुते
अपने चेहरे को।
रसदार पूओं की ख़ुशबू
शायद आज भी
उसके नथुनों को
बेचैन कर देती होगी।
मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ….
शाम को
जब मैं इमामबाड़े पर जाकर बैठा
तो अकेला ही रह गया।
कई लोग आए – गए
परंतु कुछ विचित्र-सी नज़रों से
देखते हुए गुज़र गए।
आज भी याद है मुझे
यह वही जगह हुआ करती थी
जहाँ
खेतों में अपनी मेहनत की बूँदे टपकाकर
थके- हारे गाँववाले
जुटा करते थे।
मगर न ‘सूरदास’ आए
न निर्गुण की टेर छिड़ी
न आल्हा- ऊदल
न भजन
न कीर्तन
न ढोल
न मंजीरा
न झाल!
अब समझ में आया…
सवेरे
नदी से लौटते वक़्त
बरहमथान का पक्का चबूतरा
क्यों खाली पड़ा था!
सलमा, सलीमा या अजमेरू
सब के सब
या तो इस तरफ़
अपनी बकरियाँ नहीं चरातीं अब
या फिर इस चबूतरे पर बैठकर
सुस्तातीं नहीं।
किसी ने बताया
कि मुहर्रम का ताज़िया भी
अब हमारे दालान तक
नहीं लाया जाता।
चना- गुड़ खिलाने
या लाठी भाँजने में
अब न तो हिंदू भाग लेते हैं,
न ही मुसलमान
रामनवमी के जुलूस में।
कौन जानता था —
मेरे पहुँचने से पहले
गाँव में
टीवी पहुँच जाएगा
और हालात ऐसे हो जाएँगे!
हफ़्ते भर हो गया है मुझे गाँव आए
मगर जुम्मन
अभी तक मिलने नहीं आया
— संदेशा भिजवाने के बावजूद।
और मेरे पहल करने पर
उसके घर का दरवाज़ा
खुला ही नहीं।
सो, बहुत भारी मन से
यह लिख रहा हूँ, मेरे पुत्र!
कि शहर के मकान वाला मेरा कमरा
ख़ाली ही रहने देना …
कभी भी लौटकर आ सकता हूँ मैं!
कवि प्रवीण परिमल
जन्म तिथि : 02.09.1961
शिक्षा: स्नातक (विज्ञान)
प्रकाशित कृतियाँ : तुममें साकार होता मैं (काव्य संकलन) / 1985
रावण ऐसे नहीं मरेगा (जनगीत संग्रह) / 2001
प्रेम का रंग नीला (काव्य संकलन) / 2021 ( प्रथम संस्करण)
प्रेम का रंग नीला (काव्य संकलन) / 2022 (द्वितीय संस्करण)
जंगल से लौटकर (कविता संग्रह ) / 2022
आगामी संकलन: धुंध में पहाड़ (कविता संग्रह) /
लहना सिंह उदास है (कविता संग्रह) / शीशे का घर (ग़ज़ल संग्रह) / हसरतों के काफ़िले (ग़ज़ल संग्रह)
निवास: फ्लैट संख्या- 4 / सी, ब्लॉक – बी ,
ब्लू सफ़ायर अपार्टमेंट,
निकट- सोहराय भवन, सहजानंद चौक, हरमू , राँची, झारखंड- 834002
सम्पर्क: 98354 10659
90319 74099
टिप्पणीकार कौशल किशोर, कवि, समीक्षक, संस्कृतिकर्मी व पत्रकार
जन्म: सुरेमनपुर (बलिया, उत्तर प्रदेश), जन संस्कृति मंच के संस्थापकों में प्रमुख.
लखनऊ से प्रकाशित त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका ‘रेवान्त’ के प्रधान संपादक।
प्रकाशित कृतियां: दो कविता संग्रह ‘वह औरत नहीं महानद थी’ तथा ‘नयी शुरुआत’। कोरोना त्रासदी पर लिखी कविताओं का संकलन ‘दर्द के काफिले’ का संपादन। वैचारिक व सांस्कृतिक लेखों का संग्रह ‘प्रतिरोध की संस्कृति’ तथा ‘शहीद भगत सिंह और पाश – अंधियारे का उजाला’ प्रकाशित। कविता के अनेक साझा संकलन में शामिल। 16 मई 2014 के बाद की कविताआों का संकलन ‘उम्मीद चिन्गारी की तरह’ और प्रेम, प्रकृति और स्त्री जीवन पर लिखी कविताओं का संकलन ‘दुनिया की सबसे सुन्दर कविता’ प्रकाशनाधीन। समकालीन कविता पर आलोचना पुस्तक की पाण्डुलिपी प्रकाशन के लिए तैयार। कुछ कविताओं का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद। कई पत्र-पत्रिकाओं में रचनाओं का प्रकाशन।
मो – 8400208031)