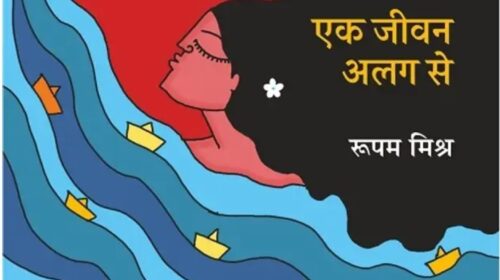रामायन राम
(संविधान निर्माता डाॅ. भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयन्ती पर भारतीय संविधान में जनता के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के निर्माण को लेकर लिखा गया लेख जनमत के पाठकों के लिए)
भारत जैसे अलोकतान्त्रिक और श्रेणीकृत आसामनता के सिद्धांत और व्यवहार पर टिके हुए समाज में एक उदार लोकतान्त्रिक संविधान का ढांचा तैयार करना बेहद कठिन और धैर्य का काम था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को जिस हड़बड़ी मे आज़ाद किया उसका अंदाजा भारत में बहुत सारे नेताओं को नहीं रहा होगा लेकिन मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन के भारत आने के बाद संविधान सभा के गठन की कार्यवाई तेज़ हो गई।
भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान के अलग अलग हिस्सों के लिए प्रस्ताव तैयार करने और सुझावों को संकलित करने के लिए विभिन्न समितियां गठित की गईं थी। उन समितियों के सुझावों को संकलित करते हुए संविधान सभा के सलाहकार बी एन राव ने एक प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया था जिसे उन्होंने संविधान सभा को 30 मई 1947 को सौंपा ।
इस प्रारंभिक मसौदे के संकलन में जिन दस्तावेजों का सहारा लिया गया था वे इस प्रकार थे – मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट 1928, जवाहर लाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया और 1931के कांग्रेस के कराची अधिवेशन से पारित भारतीय संविधान का कराची संकल्प, भारत सरकार अधिनियम 1935, तेज बहादुर सप्रू द्वारा 1945 में प्रस्तावित संवैधानिक प्रस्ताव, नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति द्वारा1945 में ही तैयार की गई रिपोर्ट, बी एन राव, के टी शाह और के एम मुंशी द्वारा तैयार मौलिक अधिकारों पर रिपोर्ट, और डॉ. अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया ज्ञापन राज्य और अल्पसंख्यक, जिसे अम्बेडकर ने संयुक्त राज्य भारत के संविधान के रूप में संविधान सभा के समक्ष मार्च 1947 में प्रस्तुत किया था।
उपरोक्त सभी दस्तावेजों के आधार पर जो प्रारंभिक मसौदा संकलित किया गया, उसे डॉ. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाले सात सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी के पास भेजा गया।
ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था इस प्रारंभिक ड्राफ्ट का पुनरीक्षण करते हुए संविधान का एक संवर्धित मसौदा संविधान सभा को सौंपना। ड्राफ्टिंग कमेटी ने यह काम अक्टूबर 1947 से लेकर फरवरी 1948 तक किया।प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई जिसमें डॉ. अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष चुना गया।
संशोधित ड्राफ्ट को प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद को सौंपा। प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत इस मसौदे पर विस्तृत बहस संविधान सभा के सदस्यों के बीच हुई।
27 अक्टूबर 1947 से लेकर 13 फरवरी 1948 तक 44 दिनों में प्रारूप समिति की हर रोज बैठक हुई जिसमें पुनरीक्षित मसौदा तैयार किया गया।
मसौदे के संशोधन और पुनर्लेखन के दौरान संशोधनों को संबंधित मंत्रालय के पास भेजा जाता था, मंत्रालयों के सुझाव और सहमति के बाद ड्राफ्ट में जरूरी बदलाव और कांट छांट की गई।
अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने बी एन राव द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट में बीस बड़े बदलाव किए जिसमें संविधान की प्रस्तावना में संशोधन और मौलिक अधिकारों की सीमा को लेकर एक सीमांकन संबंधी प्रावधान भी शामिल था। इस बीच प्रारूप समिति आए हुए सुझावों और संशोधनों पर विचार करती रही।
4 नवंबर 1948 से संविधान सभा में इस ड्राफ्ट पर बहस शुरू हुई जो ड्राफ्ट के पहले, दूसरे और तीसरे वाचन के बाद 26 नवंबर 1949 तक चली जिस तिथि को संविधान को पारित घोषित किया गया और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए। लगभग एक वर्ष तक चली इस बहस में लगभग 7500 बदलाव प्रस्तावित किए गए लेकिन संविधान सभा ने उनमें से 2500 संशोधनों को स्वीकार किया गया।
इस दौरान कई अनुच्छेदों को दुबारा लिखा गया, कुछ को पूरी तरह बाहर निकाल दिया गया। लगभग सभी बदलावों को संविधान सभा द्वारा पारित करा कर ही शामिल या बाहर किया गया।इस तरह संविधान का जो अंतिम स्वरूप निकल कर आया उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थीं।
ड्राफ्टिंग कमेटी के तरफ से डॉ. अम्बेडकर ने प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ अपने ड्राफ्ट के पक्ष में बहुत तैयारी के साथ बहसें की जिनके जरिए अम्बेडकर एक ’स्टेट्समैन’ के रूप में उभरे। डॉ. अम्बेडकर और नेहरू दोनों ही भारत को एक उदारवादी लोकतंत्र के रूप में आकार देना चाहते थे, इसलिए अम्बेडकर कांग्रेस के प्रति अपने विरोध को भूल कर और दलितों वंचितों के अधिकारों को संरक्षित करने के लक्ष्य के साथ संविधान सभा में आए थे।
1945– 46 के केंद्रीय विधान सभा के चुनावों में अम्बेडकर की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को कोई खास चुनावी सफलता हासिल नहीं हुई थी।इसलिए कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर जब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय विधान सभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा संपन्न हुआ तब कांग्रेस ने अम्बेडकर का जमकर विरोध किया था इसलिए वे महाराष्ट्र से नहीं चुके जा सके।लेकिन बंगाल से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के चुने हुए प्रतिनिधि योगेन्द्र नाथ मंडल ने मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों और अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों का समर्थन जुटा कर अम्बेडकर की जीत पक्की की और अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे।
भारत के विभाजन के बाद जिस क्षेत्र से अम्बेडकर चुन कर आए थे वह पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया जिसके कारण अम्बेडकर संविधान सभा से बाहर हो गए लेकिन अब तक संविधान निर्माण में उनकी महत्ता साबित हो चुकी थी, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें महाराष्ट्र से दुबारा चुन कर वापस बुलाया।
संविधान सभा की पहले सत्र की बैठक के दूसरे ही दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए संविधान के उद्देश्य और लक्ष्य संबंधी संकल्प का प्रस्ताव पेश किया जिसपर बोलते हुए अम्बेडकर ने अपनी असाधारण दक्षता और वक्तृता का परिचय दिया।
इसमें उन्होंने नेहरू द्वारा पेश किए गए संकल्प की आलोचना करते हुए भी संविधान सभा को एकजुट होकर देश की व्यापक जनता के हित में काम करने का आह्वान किया।
उन्होंने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचार की बात उठाते हुए कहा कि यह खेद का विषय है कि इंसानी मौलिक अधिकार जो कि हमारी सोच का अभिन्न अंग बन जाना चाहिए उसे हम संकल्प की तरह दोहरा रहे हैं।
यह भारतीय समाज के पुरातनपंथी होने का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि उपचारों के बिना अधिकार बेमानी हैं। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए जमीनों के राष्ट्रीयकरण की बात इस भाषण के दौरान उठाई और यह कहा कि बिना समाजवादी ढांचे के सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की ही नहीं जा सकती।
अम्बेडकर प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ने की बात कर रहे थे, हालांकि नेहरू ने यह कहा कि संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस पर आपत्ति हो सकती है इसलिए नीतियां समाजवादी और उदारवादी लोकतंत्र की रहें लेकिन समाजवाद शब्द न जोड़ा जाए। आगे चल कर अम्बेडकर इस बात से सहमत हो गए थे।
यह भी उल्लेखनीय है कि संविधान सभा ने अम्बेडकर द्वारा ’राज्य और अल्पसंखयक’ में प्रस्तावित प्रावधानों को भी स्वीकार नहीं किया था, न तो जमीनों और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात मानी गई , न ही अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की बात मानी गई राजनीतिक और नौकरियों में आरक्षण के सवाल को स्वीकार तो किया गया लेकिन उन रूप में नही जिस रूप में पूना समझौते में तय हुआ था।
इसके बावजूद अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों के पक्ष में अनेक प्रगतिशील प्रावधानों को लागू करवाने में अपनी भूमिका निभाई। इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका यह रही कि संविधान की प्रस्तावना में उन्होंने fraternity (बंधुत्व) शब्द जोड़ा। धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध कर उन्होंने दलित जातियों, आदिवासियों , धार्मिक अल्पसंख्यकों और स्त्रियों के लिए समान अवसर का रास्ता खोला। लेखक अशोक गोपाल ने डॉ.अम्बेडकर की जीवनी A part Apart: The life and Thought of B.R. Ambedkar में आकाश सिंह राठौर द्वारा किए गए अभिलेखीय शोध के आधार पर दावा किया है कि के 81 शब्दों में भारतीय संविधान की अदभुत और ऐतिहासिक प्रस्तावना का लेखन पूरी तरह डॉ. अम्बेडकर का व्यक्तिगत योगदान है।
संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने वाली बहसों के दौरान बहुधा नेहरू और पटेल जैसे नेता अन्य राजनैतिक व्यस्तताओं के कारण अनुपस्थित रहे। ऐसी स्थिति में अम्बेडकर ने ही बहसों का नेतृत्व किया और संशोधनों पर आने वाली बहसों का जवाब दिया और ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया। अपने पहले ही भाषण से अम्बेडकर ने यह संकेत दे दिया था कि वे अब दी हुई परिस्थिति में एक बेहतर संविधान बनाने की दिशा में कांग्रेस और संविधान सभा का सहयोग करने वाले हैं और अपनी पुरानी मांगों से थोड़ा पीछे हट कर वे अधिकतम संभव लोकतांत्रिक संविधान बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे और दलित वंचित वर्गों के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे।
अम्बेडकर ने उस भाषण में कहा कि अभी हम राजनैतिक,सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से विभाजित हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे लड़ाकू शिविरों की तरह हैं लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं और सबने मिल कर प्रयास किया तो हमें एक देश के रूप में एकजुट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अम्बेडकर द्वारा दिखाए गए आशावाद और उनकी प्रतिभा के कारण ही उन्हें संविधान सभा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं।
4 नवम्बर 1948 को अम्बेडकर ने संविधान के मसौदे को प्रस्तुत करते हुए जो भाषण दिया था वह संविधान सभा के बहसों को समझने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अम्बेडकर ने एक शक्तिशाली केंद्र की वकालत की, जिसमें उन्होंने दोहरी शासन प्रणाली और इकहरी नागरिकता के पक्ष में दलील रखी।
इसमें हर भारतीय नागरिक का अधिकार समान है चाहे वह जिस भी राज्य में रहता हो। राज्यों की स्वायतता और केंद्रीय कानूनों को लागू करने में राज्यों की संभावित शिथिलता को देखते हुए राज्य के संघीय ढांचे को एक मजबूत केंद्र के अधीन रखने की बात की।
अम्बेडकर ने इस आरोप को स्वीकार किया कि संविधान का बड़ा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इस बारे में उन्होंने कहा कि विश्व इतिहास में लोकतांत्रिक संविधानों में अलग से कोई नई चीज का होना संभव नहीं है।संविधान के मूल तत्व संपूर्ण विश्व में एक ही मानक पर आधारित हैं, इन तत्वों के कारण सभी संविधान अपने स्वरूप में एक से ही दिखाई देंगे।
प्रस्तावित संविधान पर एक आरोप यह लगा था कि इसमें भारत की प्राचीन संस्कृति राजतंत्रात्मक व्यवस्था और आत्मनिर्भर ग्राम समाज के सिद्धांतों का समावेश नहीं किया गया है। इसपर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर ग्राम समाज संकीर्णता, अंधविश्वास और सांप्रदायिकता का बसेरा हैं इसलिए अच्छा है कि संविधान में उसे आधार नहीं बनाया गया है। इस तरह अम्बेडकर के विचार सीधे तौर पर गांधी के हिंद स्वराज में व्यक्त किए गए विचारों से टकराते हैं। हालांकि नेहरू ने भी गांधी के इन विचारों को संविधान में समाहित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था।
संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए किए रक्षोपायों की आलोचना कुछ दलों के प्रतिनिधियों की ओर से की गई थी इसके जवाब में अम्बेडकर ने कहा कि “मुझे कोई शक
नहीं है कि संविधन सभा ने अल्पसंख्यकों के लिए ऐसे रक्षोपायों की व्यवस्था करके बुद्धिमत्ता का काम किया है। इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों गलत मार्ग
पर चले हैं। बहुसंख्यक के लिए अल्पसंख्यक के अस्तित्व को नकारना गलत है। इसका कोई हल खोजा जाए जो दोहरा प्रयोजन सिद्ध करे। वह हल ऐसा हो जो शुरु-शुरु में अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को माने। वह हल ऐसा हो कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों मिलकर एक हो जाएँ। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावित समाधन स्वागत योग्य है क्योंकि वह समाधन दोहरा प्रयोजन पूरा करता है। उन दुष्टों से जो अल्पसंख्यक के एमसंरक्षण के विरोध् में कट्टरता जैसी स्थिति पैदा करते हैं, मैं दो बातें कहना चाहूँॅगा। एक, अल्पसंख्यक एक ताकत है जो प्रस्पफुटित हो जाए तो राज्य के सम्पूर्ण कलेवर को उड़ा सकती है। यूरोप का इतिहास इस बात का पर्याप्त और दयनीय प्रमाण है। दूसरी, यह है कि भारत के अल्पसंख्यक अपना अस्तित्व बहुसंख्यक के हाथों सौंपने के लिए राजी हो गए हैं। …भारत में किसी भी अल्पसंख्यक ने यह बात नहीं उठाई, उन्होंने बहुसंख्यक शासन निष्ठापूर्वक स्वीकार कर लिया है जो मूलतः साम्प्रदायिक बहुसंख्यक हैं न कि राजनीतिक बहुसंख्यक। यह समझना बहुसंख्यक का कर्तव्य है कि वह अल्पसंख्यकों का शोषण न करें।अल्पसंख्यक रहेंगे अथवा लुप्त हो जाएंगे वह इसी बात पर निर्भर करेगा। ज्यों ही बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के खिलापफ भेदभाव करने की आदत को छोड़ देगा त्यों ही अल्पसंख्यक के पास अपने अस्तित्व का कोई आधर नहीं रह जाएगा। वे लुप्त हो जाएंगे।” (बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वांग्मय खंड 26)
मसौदा संविधान में मौलिक अधिकारों पर लगायी जाने वाली पाबंदियों और मूल अधिकारों के अपवादों को लेकर काफी बहस हुई। यह कहा गया कि मौलिक अधिकारों को इतने आपवादों से घेर दिया गया है कि उनका कोई मतलब नहीं रह गया है। मूल अधिकारों को पूर्ण अधिकार होना चाहिए।
इसपर अम्बेडकर ने प्रारूप समिति का पक्ष रखते हुए कहा कि किसी भी देश में और सदस्यों ने जिस अमेरिका का उदाहरण देकर पूर्ण मौलिक अधिकारों की बात कही है वहां भी ये अपवाद विहीन नहीं हैं।उन्होने कहा कि अमेरिका में उच्चतम न्यायलय ने पुलिस को यह अधिकार दे रखा है कि मौलिक अधिकार का दूरपयोग होने की दशा में वह मौलिक अधिकार पर कुछ प्रतिबन्ध आरोपित कर सकती है।
भारत के इस मसौदा संविधान में राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह जरुरी होने पर ऐसा कर सकता है। इस भाषण में अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों, केंद्र राज्य संबंधों और संविधन संशोधन के अधिकार से सम्बंधित आपत्तियों का जवाब दिया। तमाम सुझावों, संशोधनों और बहसों के बाद 26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान को राष्ट्रपति द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार किया गया।
इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय संविधान पर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व नेहरू और पटेल का गहरा नियंत्रण और प्रभाव था लेकिन बावजूद इसके अधिकतम संभव आम सहमति का ख्याल रखा गया था। इस आम सहमति को बनाने और संविधान की बहसों को सही दिशा देने में अम्बेडकर की प्रमुख भूमिका रही।
26 नवम्वर 1949 को अम्बेडकर ने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में कहा कि यह संविधान भारत के वर्तमान पीढ़ी के नेताओं के विचारों का प्रतिफल है। इसके लिए संविधान सभा को दोष नहीं दिया जा सकता। इस भाषण में अम्बेडकर ने भारत के संविधान और लोकतंत्र के सामने आने वाले खतरों के प्रति आगाह किया।
उन्होने कहा कि सिर्फ राजनैतिक लोकतंत्र से ही संतोष कर लेना काफी नहीं है हमें इसे सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना होगा अन्यथा हम एक विरोधाभास में जीते रहेंगे। सिद्धांत में तो हम लोकतंत्र को मानेंगे और व्यवहार में उसे नकारते रहेंगे। हमें यह विरोधाभास ख़त्म करना होगा वरना लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा।
बंधुत्व के सिद्धांत पर अम्बेडकर ने बहुत जोर दिया, उनका कहना था कि हज़ारों जातियों में बंटे लोग एक राष्ट्र नहीं बन सकते। राष्ट्र के लिए आज़ादी, समानता के साथ भाईचारा जरुरी है जो तब कायम होगी जब जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव ख़त्म होगा।
वर्तमान भारत में सत्ता की ओर से सामाजिक लोकतंत्र, और बंधुता के साथ साथ उदार लोकतंत्र की समूची अवधारणा पर ही हमला जारी है, आज भारतीय संविधान ही निशाने पर है, ऐसी स्थिति में भारत के संविधान के वैचारिक आधार और भारतीय लोकतंत्र के अंत:संघर्ष को समझना जरुरी है ताकि संविधान बचाने और उसे और अधिक लोकतान्त्रिक बनाने के संघर्ष को तेज़ किया जा सके।
समकालीन जनमत पत्रिका के अप्रैल 2025 के अंक में प्रकाशित।
फ़ीचर्ड इमेज गूगल से साभार