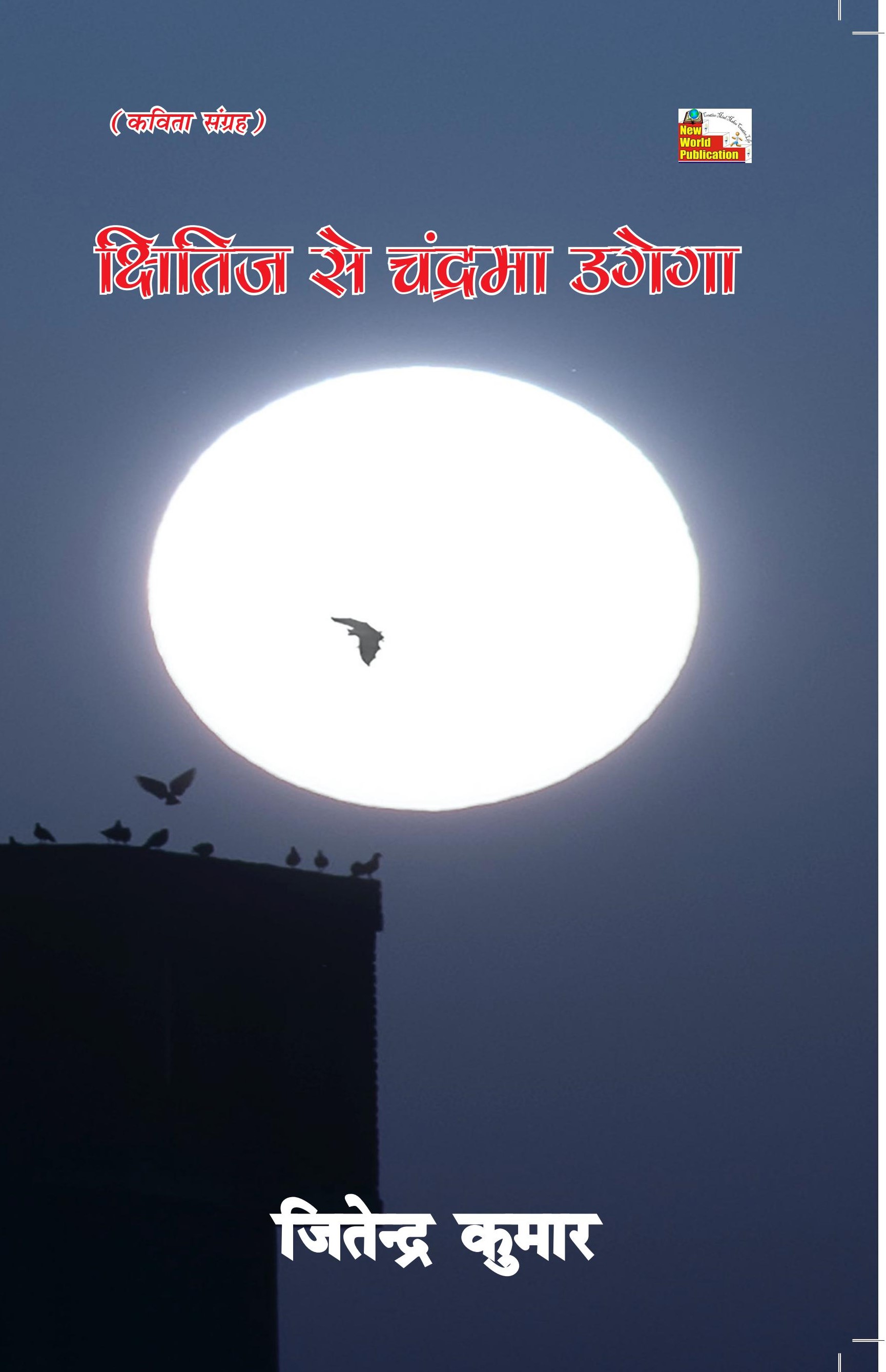निरंजन श्रोत्रिय
नेहल शाह की इन कविताओं का मूल स्वभाव विद्रोही है जो अंततः दरअसल कवि का ही है। वे किसी भी तरतीब के ख़िलाफ़ होती हैं जो जीवन को कथित रूप से व्यवस्थित बनाने का उपक्रम होती है। बेतरतीबी या कहें कि अनुशासनहीनता का यह आग्रह किसी अराजकता का नहीं, बँधे-बँधाए ढर्रे को तोड़ने का आग्रह है। उसकी शुरूआत चाहे दादा की जेब से बीड़ी निकाल कर सुट्टा मार लेने से ही क्यों न हो (महान हुनर)।
यह दिलचस्प है कि इस कथित लक्ष्मणरेखा को पार करते ही संवेदनों के साथ उत्तरदायित्वबोध का भी विस्तार हो जाता है। इस कविता में अराजकता के बीज की जनक बूढ़ी अम्मा के व्यवसाय की तह तक कवि-मन उतर जाता है और उसे ‘महान हुनर’ करार देता है।
‘संरचना’ एक महत्वपूर्ण कविता है जिसमें स्त्री-देह को लेकर व्याप्त रहस्य-रोमांच को अद्भुत प्रश्नाकुलता के साथ विन्यस्त किया गया है। कवि ने इस कविता में शब्दों का सावधान चयन किया है। हम पाते हैं कि पूरी कायनात स्त्री-देह को लेकर किसी संवेदित अनुसंधान या प्रेक्षण की पेशकश नहीं करती, बस टटोलती रहती है। जाहिर है पुरूष देह के बरक्स स्त्री देह को रहस्य के इतने कृत्रिम आवरणों से पाट देना, उसकी देह को सामाजिक मान्यताओं, रूढ़ियों और कथित संस्कारों से आबद्ध कर देना स्त्री के शोषण का ही एक मार्ग है।
कविता में महाभारत के चीरहरण प्रसंग को रेखांकित करते हुए वह एक बेहद सुलगता सवाल छोड़ जाती हैं-‘ जरा सोचिए जो कृष्ण समय पर न पहुँच पाते/ तो भी वे लोग एक स्त्री की संरचना से अधिक और क्या देख पाते?’ यह प्रश्न स्त्री देह को लेकर तमाम भ्रांतियों और दुराग्रहों को एक ही वार से काट देता है। ‘खुरदुरा मन’ कविता में विछोह की वेदना है। वियोग किसी मन की आंतरिक संरचना को किस कदर विक्षोभ से भर देता है, उसकी अदृश्य कोशाओं को विगलित कर देता है, यह अंडरटोन कविता इसका बयान है। कविता में मन के विभिन्न संस्तरों के ट्रांस्फॉर्मेशन की पड़ताल की गई है।
‘शाही पलंग’ कविता में इतिहास, सत्ता, परम्परा और नॉस्टेल्जिया का समुच्चय है। एक निर्जीव उपादान के जरिये कवि ने लम्बे समय की यात्रा की है। यहाँ पलंग राजसी सत्ता, संधि, युद्ध और तंत्र की कथा कह रहा है और इस तरह वह एक कालयात्री की तरह वर्तमान में उपस्थित है। सत्ता की तमाम कारगुजारियाँ नक्काशी के आवरण में छुपी हुई हैं जिसे उद्घाटित करना आसान नहीं। कविता को पढ़ते यह अहसास होता है गोया हम इतिहास की पुरातत्वीय धरोहर के सामने खड़े हैं।
‘घाट की देह के भीतर’ एक छोटी लेकिन सघन कविता है। यहाँ स्थिर घाट और प्रवाहित नदी के अन्तर्सम्बंधों को रेखांकित किया गया है जिन्हें संवेदनों के जरिये ही पहचाना जा सकता है। यहाँ घाट का ठहराव, उस पर होने वाले क्रिया-कलाप और उसके बरक्स बहते रहने की अनवरतता का आंतरिक आख्यान है-‘ नदी रहती है/ चिरकाल तक समुद्र के अंतस्थ में।’ ‘नदी’ कविता दरअसल इसी बहाव का विस्तार है। इसमें दर्शन का भी अक्स है-‘जितनी वह/ मिलती है गंतव्य से/ उतनी ही बाकी/ रहती है मेरे लिए।’
‘मेरे बचपन का शहर’ कविता में यादों की कसक है। नॉस्टेल्जिया के अधीन इस कविता में शहर में हो रहे बदलाव की पीड़ा है। यह पीड़ा उन अभ्यस्त संवेदनों की वजह से है जो अपने अतीत को अपने मूलस्वरूप में पाना चाहती है। प्रगति और विकास अवश्य ही समय की माँग होती है लेकिन यदि वह किसी संरचना की मूल आत्मा के विरूद्ध हो तो फिर वेदना में तब्दील हो जाती है। कोई भी कवि-मन अट्टालिकाओं और फ्लाईओवर्स से पटे शहर के भीतर एक आत्मीयता से पगी नम भूमि की खोज में ही रहता है।
कवि के लिए यह एक चमकदार लेकिन मुस्कान रहित चेहरा है। हम सभी ने कुत्तों का रोना देखा-सुना है। वे क्यों और किसके दुःख में रोते है इसका मार्मिक काव्यात्मक आख्यान है कविता- ‘कुत्ते’। कथित रूप से अपशगुन मान लिए जाने वाले रूदन के पीछे विरह, अत्याचार और अमानवीयता से उपजा दुःख है। कविता की अंतिम पंक्तियाँ दहला देती हैं-‘वे रात भर रोते रहे सभी के लिए/ जब स्वयं के लिए रोने के समय आया तो/ सुबह होने को थी।’ ‘देह केन्द्रित दुनिया’ कविता यूँ तो देह के दर्द के बारे में है लेकिन इस दर्द का संसार देह से बाहर भी है। दर्द के प्रकार, उसके संस्तर, उससे उपजी पीड़ा व्यक्ति के लिए एक अलग ही पीड़ा-दृश्य रचती है। यह किसी कवि के लिए ही संभव है कि वह दर्द की कराह को पीड़ा का गीत बना दे!
‘तुम मुझे यूँ मिले’ एक तरह से प्रेम कविता ही है जिसमें मिलने और मिलने के अधूरेपन की चित्रण है। कविता में प्रयुक्त इमेजरी इस कविता को आम प्रेम कविताओं से अलग करती है। ‘तुम मेरे लिए ही आते हो’ में भी प्रेम छितरा हुआ है। प्रेयसी ने प्रेयस की तमाम प्रेम चेष्टाओं को अपने भीतर आत्मसात् कर लिया है। इस कविता में हल्का-सा विट भी है। नेहल शाह एक उभरती हुई प्रतिभाशाली युवा कवि है जिसके भीतर विद्रोह का ताप और नवाचार की आकांक्षा एक साथ मौजूद हैं।
नेहल शाह की कविताएँ
1. महान हुनर
पता नहीं
अपराध था या नहीं
जब दादा की नज़रों से बचाकर रखे
बीड़ी के बंडल से
दूर गली में जाकर
मैंने बीड़ी का पहला कश खींचा था।
तब इल्म नहीं था
अपने भीतर की लौ का
उस दिन बीड़ी के साथ-साथ
पी गई थी मैं
अपना अहसास-ए-कमतरी
और उस दिन से
अधिक हो गई थी मैं
अधिक बड़ी
अधिक निडर
अधिक विद्रोही
अधिक बदतमीज़
अधिक गैरज़िम्मेदार
और अधिक संवेदनशील
बीड़ी के बंडल को
पूरा पी लेने की चाहत लिए
अपनी बेतकल्लुफ़ी में
छानती रही छोटी-छोटी गलियाँ
जहाँ मिली मुझे
घर के बाहर की
बेपर्दा, बेपरवाह दुनिया
यहाँ गलियाँ
नलियों से बटी-बटी
आपस में सटी-सटी
एक दूसरे के कान में
खुसफुसाती
चटखारे ले-ले कर
एक-दूसरे को एक-दूसरे के
किस्से सुनाती।
यहीं किसी संकरी गली में
मिट्टी के मकान में रहती थी
एक बूढ़ी अम्मा
जो नमीदार सूखे तेंदू पत्ते से
बीड़ी बनाती
वह पत्ते की नसें काटकर
उसमें बारीक तम्बाखू भर
उसे शंकु के आकार में
बारीकी से घुमा कर
एक महीन-सा धागा चढ़ाती
और इस तरह वह
कर गई मुझे संस्कारित
बीड़ी बनाने के ऐसे महान हुनर से
जिसे सीखने से जीवन में कभी
बेरोज़गारी नहीं आती।
2. संरचना
मैंने यह जाना कि
मनुष्य जब से मनुष्य है
तब से उसकी संरचना तय है
किन्तु
बीत जाने पर
स्त्री-देह अब भी जिज्ञासा का विषय है।
आश्चर्य है
इतनी वैज्ञानिक प्रगति हो जाने पर भी
स्त्री की संरचना को
कोई स्वीकृति नहीं मिली।
उसे अजब अचंभे-सा देखना या
अनधिकृत टटोलना
आज भी जारी है
फिर ऐसा भी नहीं
कि जो देखता, टटोलता है
वह अनभिज्ञ तबका है
या असभ्य समाज का हिस्सा।
न जाने कहाँ से आते हैं वे
घूरकर और टटोलकर
न जाने कहाँ चले जाते हैं
और एक प्रश्न छोड़ जाते हैं
क्या स्त्री का आवरण
बचा सकता है उसे
नग्न होने से किसी की नज़रों में?
यहाँ मुझे द्रोपदी चीरहरण
याद आता है
भरी सभा में जब पांडव उसे
हार गए थे जुए में
वह लज्जित हो
चीखती रही न्याय के लिए
रोकती रही खींचने में अपना आवरण
याद करती रही कृष्ण को
कृष्ण आये और बढ़ा दिया उसका चीर
भगवान जो ठहरे!
तो क्या रोक पाए थे कृष्ण उसे निर्वसन होने से
सही मायनों में?
क्या नहीं हो गई थी वह निर्वस्त्र
सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की कल्पना में?
और आज जब भी इस बात का ज़िक्र होता है
वह अनावृत हो जाती है किसी प्रेक्षागृह की तरह
हमारे ज़ेहन में
और हम कृष्ण को ढूँढते फिरते हैं
उसके आवरण के लिए
जरा सोचिए जो कृष्ण समय पर न पहुँच पाते
तो भी वे लोग एक स्त्री की संरचना से अधिक
और क्या देख पाते?
3. खुरदुरा मन
जब जा रहे थे तुम
छोड़कर मुझे
और घाव मेरे मन पर
तब पानी की निथरी सतह-सा
शांत मेरा मन
जिस पर कभी तुम्हारा अक्स
साफ दिखता था
हिल-सा गया
कुछ मटमैला
रेतीला-सा
कसमसाहट से भर गया मेरा मन।
मेरे मन में उस दिन
पहली बार दर्द हुआ
मुझे याद है
वह दर्द बहुत गीला था
आँखों से बह जाता।
समय बीतता गया
दर्द गाढ़ा होता गया
ठहरने लगा
मुश्किल से बाहर निकलता
और ठस के रह जाता
दिल में खून के थक्के की तरह
फिर दर्द जम गया
चोट में उगी पपड़ी की तरह
कुरेदो तो नया घाव बना देता
ऐसे ही कई घाव लेकर
अब खुरदुरा गया है मेरा मन
किसी पेड़ की छाल की तरह
जिसे, अब कोई नहीं सहलाता
कोई अक्स भी नहीं बनता इस पर
किन्तु अब जो भी अंकित होता है
इसकी सतह पर
वह रह जाता है हमेशा हमेशा के लिए।
सच पूछो तो
तुम्हारी चाह के विरूद्ध
मुझे ऐसा ही मन चाहिए था
खुरदुरा-सा
उबड़-खाबड़।
किन्तु ये मैं भी जानता हूँ
कि तुम चाँद से प्रेम करते हो
चाँद की तारीफ करते हो
तक क्या ये भूल जाते हो
कि खुरदुरा है चाँद का भी मन!
4. शाही पलंग
बिस्तर पर लेटे-लेटे
नींद से करवट किए
देख रही थी मैं
शाही पलंग के ऊपर बनी फ्रेम
किसी राजसी कारीगर ने
जिसे बनाया
बहुत करीने से
लगभग एक शताब्दी पहले
पलंग की श्रेष्ठ नक्कासी के साथ
इतिहास हो चुकी है
राजघराने की नींद
उनके सपने
बिन नींद की बिखरी कुछ रातें
अनगिनत कल्पनाएँ
प्रेम और विरह की यादें
संधि और युद्ध की योजनाएँ
इसके सिरहाने लगे टेक पर
एहसास है
मखमली तकियों का
जिन पर पीठ टिकाकर बैठते
महाराज, उनके पुत्र और रानियाँ
काश! कि पलंग कह सकता
उनके भेद
उस समय की कुछ कहानियाँ
किन्तु यह कुछ कहता नहीं
राज-निष्ठ है
उस राज्य के इतिहास का गवाह
नहीं जानता न्याय-अन्याय की बात
अपने कुशल पैरों पर खड़ा
जानता है देना
केवल देह को आराम
इस बात से अनभिज्ञ कि
नींद प्राकृतिक है।
कई वर्ष पहले
दादा के लिए आए
राजघराने के इस तोहफे की
मौन गादी पर बैठ
सासू बाई ने गाई लोरियाँ
अपने पुत्रों के लिए
फिर पुत्रों के पुत्रों ने
इस धरोहर को अपनाया
अब यह मेरे शयन का स्थान है
इस पर बीती हजारों रातों की तहों का
उपधान रख
मैं असंख्य नींदों के लिहाफ ओढ़
चैन से सो जाती हूँ।
5. घाट की देह के भीतर
घाट की देह के भीतर
बहती है नदी
लेकर हर भाव
घाट के जीवित मन का
कितने ही शव लेकर
वह शव नहीं होती।
बहती है नदी
घाट के भीतर तब भी
घाट सो जाते हैं जब
और कोई ध्यान नहीं होता
घाट का नदी पर।
घाट जब जीर्ण हो समाप्त होते हैं
तब बहती है नदी
समुद्र की गहराई में
बहुत आहिस्ता से
होती है शांत और गंभीर
अपने मृदु स्वभाव को जानती हुई
नदी रहती है
चिरकाल तक समुद्र के अंतस्थ में।
6. नदी
मैं देखती हूँ उसे
नित्य चलते हुए
बढ़ते हुए
गंतव्य की ओर
इच्छाओं के वेग से
जितनी वह
मिलती है गंतव्य से
उतनी ही बाकी
रहती है मेरे लिए
वह बहा ले जाती है
अतृप्ति
मन के प्रतिबिंब की
और स्वयं तृप्त रहती है
मैं देखती हूँ उसे
सदा ही भरते हुए स्वयं से
वह न तो बीतती है
न कभी रिक्त होती है।
7. मेरे बचपन का शहर
सिकुड़ गया है
मेरे बचपन का शहर
जैसे बेघर कोई बुजुर्ग
जिसे कई दिनों से
केवल आधे पेट ही मिला हो अन्न।
स्टेशन से घर पहुँचने का
पेड़ों से घिरा सुनसान रास्ता
बेतरतीब मकानों से रूँध गया है
पिता के सरकारी दफ्तर के बाहर
दूर से दिखता एक पीपल का पेड़
जो चुडैलों का ठिकाना था
अब नशेड़ियों का नया मुकाम हो गया है
यादुराव द्वारा स्थापित बावन गढ़ों में
चौगान के किले का
इस शहर का इतिहास
वीरांगना दुर्गावती के प्रताप को खंडहर कर
शक्कर नदी की धार-सा टूट रहा है।
चंद्र मोहन के बचपन की यादों को
आदर्श स्कूल के मैदान में दफन कर
गाडरवारा से ओशोधाम को नकारता हुआ
यह महेश वर्मा से महर्षि महेश की यात्रा को
लगभग भूल चुका है
नहीं याद इसे इंद्र बहादुर खरे के भोर के गीत
यह खोखले विकास की राह में दर-दर भटक रहा है
उम्र बढ़ने लगी है आशुतोष के यारों की
गले में हाथ डाल कर सड़कों पर घूमने वाला मित्र मंडल
अब मोबाइल और एक्सबॉक्स गेम्स की खुमारी में
दिख रहा है।
पलोटन गंज नहीं रहा रौबदार
बीटीआई का मैदान छोटा
डिग्री कॉलेज का ग्राउंड
तंग दिखने लगा है
गायब है चावड़ी स्थित
डॉ. भास्कर का दवाखाना
नदी मोहल्ला, झंडाचौक, गंज के बीच चीन्हे चेहरों
का मिलना दूभर हो गया है।
नहीं सुनाई देती देवी माँ के मंदिर में भक्तें
बधाई-बरातों में राई
नागपंचमी, भुजरिया, अक्ती का त्योहार
कैलेण्डर की तिथि हो चला है।
देखरेख की आस में हैं
जर्जर पुस्तकालय की बूढ़ी किताबें
काबरा उद्यान अपनी खुशहाली के
बीते दिन याद कर हताश खड़ा है
घिस चुकी हैं गालियाँ
बुजुर्ग के तंबाखू घिसते हाथों की लकीरों जैसी
कहने को शहर
स्वच्छता की दौड़ दौड़ रहा है
नहीं दिखते ट्यूशन के बहाने से
मिलते हुए कच्चे प्रेमी
अलका टॉकीज की सिंगल स्क्रीन को
नेटफ्लिक्स का बुखार
धीरेे-धीरे कमज़ोर कर रहा है
कूच कर गए हैं बड़े शहरों में
सेवानिवृत्त दिखते इस शहर के
युवा और बच्चे
झब्बर की चाट के ठेले से
झब्बर लापता है
नहीं दिखती अब कहीं
लब्दो और फुटाने बेचती अम्मा
राम मंदिर की मंगों के सिर पर
यम का दूत खड़ा है।
‘जौहार! जय राम जी की!!’ वाले शहर की
मुस्कान खो गई है
मेरे बचपन का शहर
अब बंधा-सधा-सा हो चला है।
8. कुत्ते
रात कुत्ते रो रहे थे
पता नहीं कोई असगुन था हमारे लिए
या वे हमारे किए असगुन पर रो रहे थे
कुछ घोड़े ठिठके खड़े थे
रात वे थक चुके थे
कुत्ते, घोड़ों की थकान महसूस कर रो रहे थे
बिल्लियाँ गुस्से से देख रही थीं
वे हमेशा से गुस्से से देख रही थीं
कुत्ते बिल्लियों के गुस्से से दुखी होकर रो रहे थे
रात नींद नहीं आ रही थी मुझे
मैं कविता में एक औरत के
खोए सपने और अधूरे प्रेम की बात लिख रही थी
उसके खोए सपने के बारे में
कुत्ते उस औरत के
अधूरे प्रेम और खोए सपने पर रो रहे थे।
वे रोकर मेरे पड़ोसी की नींद खराब कर रहे थे
पड़ोसी आधी रात में उठकर कुत्तों पर पत्थर बरसाने लगा
वह अपने ऊपर हुए दिनभर के अत्याचार का बदला
कुत्तों पर चुकाने लगा
अब कुत्ते पड़ोसी पर हुए अत्याचार पर रो रहे थे
वे रात भर रोते रहे सभी के लिए
जब स्वयं के लिए रोने का समय आया तो
सुबह होने को थी
कुत्ते रो-रो कर थक चुके थे
वे अब और रो नहीं सकते थे।
9. देह केन्द्रित दुनिया
दर्द में तड़पती देह
कल्पना करती है
बाहर आने की उस दर्द से
इस देह केन्द्रित दुनिया से पृथक
कोई और दुनिया नहीं अब उसके लिए
यहाँ समुद्र की तरह विस्तृत हो चुकी है
उसकी दर्द भरी देह
और आत्मा मचलती दिख रही
समुद्र मे मीठे जल की मछली की तरह
स्ट्रेचर पर आँखें बंद किये लेटी युवा स्त्री
क्राह रही है कमर दर्द से
जैसे गुनगुना रही है
दर्द की धुन
कर रही है दर्द का ध्यान
उस दर्द के आभामंडल के अभाव में
देह कुछ देख-सुन नहीं पा रही
न जगह, न आसपास का कोलाहल
न ही उसका नाम
जिसे सुनकर वह सदैव चैतन्य दिखी।
दर्द में बंधी देह
अब बन चुकी है एक अलग दुनिया
जैसे अंधकार से भरा
एक ध्वनि रहित कमरा
जहाँ नहीं है
कोई पुकार आत्मा की।
10. तुम मुझे यूँ मिले
तुम मुझे यूँ मिले
जैसे मिल जाती है कोई चीज
किसी और चीज को ढूँढते हुए
किसी अनजान पुराने संदूक में
रखकर जिसे हमेशा के लिए
भूल गया हो कोई
जैसे जीवाश्म कोई पत्ती का
जो गिर गई हो सदियों पहले किसी पेड़ से
जब दो प्रेमी दूर हो रहे हों एक-दूसरे से
जैसे कोई पुरानी अधूरी पेंटिंग
जिसके चेहरे पर बस एक परत लगाकर
कोई चित्रकार रूठ गया हो अपनी प्रेयसी से
जैसे उस मूर्ति का धड़ जो
अलग हो गया हो अपने सिर से
किसी क्रूर राजा के युद्ध में
जब यह सब हो रहा था
तब बन रही थी मेरी दृष्टि
मेरी दुनिया के रंग
मेरे विरक्त हृदय की रिक्तता
और तुम्हारा-मेरा संग।
11. तुम मेरे लिए ही आते हो
मुझे पता है
तुम मेरे लिए ही आते हो
बरसाते हो प्रेम
क्योंकि तुम जानते हो
मुझे पसंद है रंग हरा।
तुम रंगते हो
आकाश को सिन्दूरी
कि उसे देख मैं
बस सोचूँ तुमको ही
तुम धूप सुनहरी करते हो
क्यांेकि
तुम देखना चाहते हो
उसके रंग में रंग मेरा
पर मैं बता दूँ तुम्हें
कि ये रंग
भर लिए हैं मैंने
मन में कहीं
रौंप दी है कलम कोई
जिससे फूट रही है
कोपल नयी
तुम्हारे प्रेम की
और अब तुम्हें मुझे यूँ ही
हर वक्त रिझाने की जरूरत नहीं।
कवयित्री नेहल शाह, जन्मः 31 मई 1982 को गाडरवारा (मप्र) में। शिक्षाः बीपीटी, एमपीटी (कार्डियोथोरेसिक), पी-एच.डी. (स्वास्थ्य विज्ञान)
सृजनः विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, ब्लॉग्स में कविताएँ प्रकाशित, पारंपरिक कलाओं जैसे
मांडना, मधुबनी, मिथिला, आदिवासी और वारसी कलाओं में रूचि।
सम्प्रतिः भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र में फिजियोथेरेपिस्ट। सम्पर्कः 34, गायत्री विहार, रामेश्वरम एक्सटेंशन के पास, बागमुगलिया,
भोपाल-462 043
ई-मेलः nehalravirajshah@gmail.com
मोबाइलः 9424442993
टिप्पणीकार निरंजन श्रोत्रिय ‘अभिनव शब्द शिल्पी सम्मान’ से सम्मानित प्रतिष्ठित कवि,अनुवादक , निबंधकार और कहानीकार हैं. साहित्य संस्कृति की मासिक पत्रिका ‘समावर्तन ‘ के संपादक . युवा कविता के पाँच संचयनों ‘युवा द्वादश’ का संपादन और शासकीय महाविद्यालय, आरौन, मध्यप्रदेश में प्राचार्य रह चुके हैं. संप्रति : शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुना में वनस्पति शास्त्र के प्राध्यापक।
संपर्क: niranjanshrotriya@gmail.com