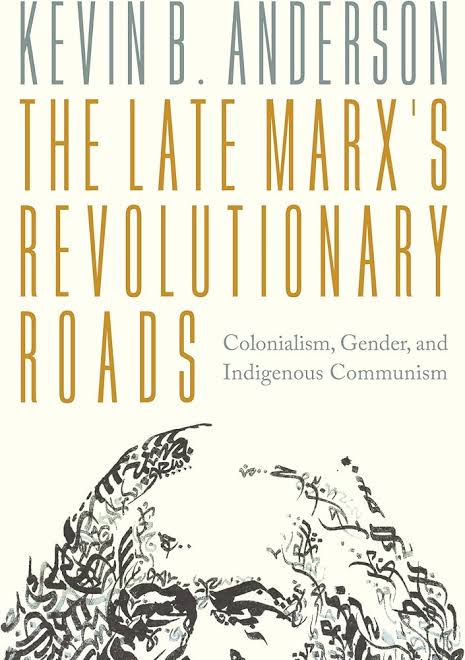2025 में वर्सो से केविन बी एंडरसन की किताब ‘द लेट मार्क्स’ रेवोल्यूशनरी रोड्स: कोलोनियलिज्म, जेंडर, ऐंड इंडिजेनस कम्युनिज्म’ का प्रकाशन हुआ । मार्क्स ने दो बार क्रांति की भविष्यवाणी की थी । पहली बार आयरलैंड में और दूसरी बार रूस में । पूंजी के छपने के दो साल बाद उन्हें आयरलैंड पर अपनी राय में संशोधन की जरूरत महसूस हुई । पहले उन्हें ब्रिटेन के मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी ताकत पर भरोसा था और उम्मीद थी कि इससे आयरलैंड भी प्रभावित होगा । बाद में उन्हें आयरलैंड के खेतिहर समाज में इसके बीज नजर आये । उन्हें राष्ट्रवादी फ़ेनियन आंदोलन पर भी भरोसा था जिसके कारण इंग्लैंड के शासक कमजोर होते । फिर फ़्रांस के क्रांतिकारी विचारों का साथ होने से इंग्लैंड में क्रांति होनी समझ आयी क्योंकि वही वास्तविक रूप से उद्योगीकृत देश था । इसके बारह साल बाद 1882 में घोषणापत्र की भूमिका लिखते हुए उन्हें रूसी किसानों में इसकी आशा पैदा हुई । वहां देहातों में सामूहिक संपत्ति साम्यवादी समाज की ओर ले जाती हुई भी महसूस हुई । इस क्रांति को पश्चिमी यूरोप की सर्वहारा क्रांतियों से भी जुड़ना था ताकि दोनों एक दूसरे के लिए पूरक की भूमिका निभा सकें । इस तरह रूस को यूरोपीय क्रांति की चिंगारी सुलगानी थी । इससे पहले वे रूस को यूरोपीय राजनीति में प्रतिक्रिया का गढ़ मानते रहे थे ।
लेखक ने 1869 से 1882 के मार्क्स को परवर्ती मार्क्स कहा है । इस दौर के लेखन में उन्हें उपनिवेशवाद, सामुदायिक संपत्ति और सामाजिक विद्रोह के मुद्दे प्रमुख रूप से नजर आये । साथ ही स्त्री समस्या संबंधी उनकी टीपें भी इसी दौर की हैं । लेखक ने इस किताब के लिए उस सामग्री पर विचार नहीं किया जिनके आधार पर एंगेल्स ने पूंजी के शेष दो खंडों को तैयार किया था । आम तौर पर इस दौर को मार्क्स के विशेषज्ञों ने महत्व नहीं दिया है । इस दौर में उन्हें शरीर से बीमार और कुछ नये इलाकों में घुसपैठ की कोशिश करने वाले के रूप में ही समझा जाता रहा है । देहांत के बाद उनकी जो कुछ लिखाई मिली भी उसके आधार पर एंगेल्स ने पूंजी के दोनों खंड ही तैयार करने पर पूरा ध्यान लगा दिया । शेष सामग्री के संपादन से बाद में 1844 की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां और जर्मन विचारधारा तथा ग्रुंड्रिस जैसी कुछ मशहूर किताबें तैयार हुईं । इस सामान्य प्रवृत्ति का अपवाद मोर्गन संबंधी उनकी विस्तृत टीपें थीं जिनके आधार पर परिवार, निजी संपत्ति और राजसत्ता के उदय पर एंगेल्स ने अपनी किताब लिखी । इस किताब के बारे में एंडरसन का मानना है कि एंगेल्स अपनी किताब में जेंडर और परिवार के मामले में मार्क्स की ऊंचाई को नहीं छू सके । साथ ही वे इसका रिश्ता उपनिवेशवाद और गैर पश्चिमी समाजों से भी नहीं जोड़ सके । 1895 में उनके निधन के बाद दूसरे इंटरनेशनल के लोगों ने मार्क्स के लेखन को सामने लाने की जगह उनके बारे में अपनी समझ को ही प्रचारित करने पर ध्यान देते रहे । इसका अपवाद अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत रहा लेकिन उसमें भी कार्ल काउत्सकी ने कुछ जरूरी बातें छोड़ दीं । उनकी चिट्ठियों को छपाते समय उनमें से भी वे सभी अंश संपादित कर दिये गये जिनमें जर्मन समाजवादियों की आलोचना थी ।
रूसी क्रांति के बाद सरकार ने संस्थान खोलकर मार्क्स के लेखन को छापने का फैसला किया । इसके मुखिया डेविड रियाज़ानोव ने मार्क्स-एंगेल्स समग्र को तैयार किया जिसमें पूंजी के सभी मसौदे, अन्य किताबें, लेख और चिट्ठियों को शामिल किया गया । इसमें भी 1857 के आर्थिक संकट, यूरोपीय इतिहास पर टीपों और गणित की पांडुलिपियों को नहीं शामिल किया गया । इस सामग्री को वे छापने लायक नहीं मान रहे थे लेकिन आखिरी समय तक शोधरत मार्क्स को सामने लाने वाली जीवनियों के उपयोग लायक मान रहे थे । भूगर्भ विज्ञान पर भी उन्होंने एक किताब की योजना अध्याय दर अध्याय दर्ज की थी । मोर्गन की किताब के आधार पर उन्होंने अपने हस्तलेख में 98 पृष्ठ 63 साल की उम्र में लिखे थे । आम तौर पर उनके लिखे एक पृष्ठ से छापे के ढाई पृष्ठ तैयार होते थे । इस पांडुलिपि को रियाज़ानोव ने भी महत्व का समझा । इसके बावजूद उन्हें समग्र में शामिल नहीं किया । रियाज़ानोव ने मार्क्स की टीपों में से एक हिस्से को जिक्र लायक भी नहीं समझा । 1879 से 1882 के बीच मार्क्स ने उपनिवेशवाद से प्रभावित इंडोनेशिया, लैटिन अमेरिका, आस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, मिस्र और भारत जैसे समाजों के बारे में विस्तार से नोट लिये थे । एक नोटबुक तो केवल भारत के बारे में थी । इस देश ने साम्राज्यवाद विरोधी एशियाई आंदोलन में जैसी भूमिका निभायी उसे रूस की नयी सरकार का समर्थन भी मिला था । इसके बावजूद रियाज़ानोव ने उस पर ध्यान नहीं दिया ।
उन्होंने परवर्ती मार्क्स के बारे में यही छवि बनायी कि बाद का उनका लेखन कुछ खास मूल्यवान नहीं है । मार्क्स की जो जीवनी उन्होंने लिखी उसमें भी यही नजरिया है । एंगेल्स की तरह ही वे भी पूंजी के लेखन में आगे न बढ़ने की शिकायत करते हैं । इसकी वजह उन्होंने मार्क्स की शारीरिक के साथ ही मानसिक सेहत की खराबी बतायी । दिमाग पर जोर पड़ने की वजह से 1878 के बाद पूंजी संबंधी किसी भी काम को भविष्य के लिए परे रख देने के तथ्य का उन्होंने उल्लेख किया है । साथ ही यह भी कहा कि मार्क्स ने इसके बावजूद टीपें दर्ज कीं । मार्क्स के प्रथम जीवनी लेखक फ़्रांज़ मेहरिंग ने भी मार्क्स के आखिरी दिनों को धीमी मौत कहा था ।
उनके जीवन के अंतिम वर्षों के बारे में एंगेल्स और रियाज़ानोव जैसे लोगों की राय बाद के अनेक दशकों तक आम राय बनी रही । मार्क्स के विरोधियों समेत उनके अध्येताओं में भी इस तथ्य पर पूरी सहमति बनी रही । 1942 में रियाज़ानोव का निधन हो गया लेकिन उनके काम की बदौलत ही आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियों के साथ जर्मन विचारधारा और ग्रुंड्रिस जैसे ग्रंथ तैयार हो सके । इसके बावजूद परवर्ती मार्क्स की उपेक्षा हुई । रियाज़ानोव ने ही कहा था कि मार्क्स की नोटबुकों से उनके जैसे अनथक शोधकर्ता की व्यापक रुचि का पता चलता है । फिर भी एंगेल्स समेत तमाम संपादकों ने पूंजी पर ही ध्यान केंद्रित रखा । उनकी सोच में वर्ग की महत्ता दिखाने के चक्कर में अन्य सवालों की अनदेखी हुई । इसके कारण उत्तर औपनिवेशिकता तथा अनुपनिवेशन के विद्वानों ने मार्क्स की तथाकथित सैद्धांतिक संकीर्णता पर हमले किये । लेखक ने एक किताब लिखकर पहले ही इस मोर्चे पर मार्क्स के चिंतन को उभारने की कोशिश की थी । यह किताब उपनिवेशों के बारे में मार्क्स के विचारों पर लिखी उसी पहली किताब की अगली कड़ी है ।
मार्क्स ने परवर्ती दिनों में जिन मुद्दों पर शोध किये और लिखा वे आज भारी रुचि का विषय हैं । इनसे उनके बौद्धिक श्रम का भी सबूत मिलता है । मसलन 1869 से उन्होंने रूसी सीखनी शुरू की और 1979 तक वे रूसी भाषा की किताबों से जर्मन में सीधे नोट लेने लगे । उन्होंने मक्सिम कोवालेव्सकी की भारत, अल्जीरिया और लैटिन अमेरिका के उपनिवेशित होने से पहले और औपनिवेशिक दौर के कुलों और गांवों की सामाजिक संरचना के बारे में लिखी किताब से नोट लिये । मोर्गन की किताव से उन्होंने तमाम प्राचीन समाजों में नातेदारी और जेंडर के जटिल संबंधों के बारे में दर्ज किया । यह अध्ययन भी राजनीतिक अर्थशास्त्र की तरह ही पर्याप्त सघन, कड़ा और श्रमसाध्य था । उनकी इन रुचियों के प्रति अध्येताओं की उपेक्षा से मार्क्स के शोधों की सीमाओं की जगह उनके अध्येताओं की यूरोप केंद्रीयता ही उजागर होती है । गैर पश्चिमी समाजों के बारे में मार्क्स के इस शोध का महत्व तो कम नहीं होता, उससे पता चलता है कि अगर वे जीवित रहते तो ‘पूंजी’ में भी इन समाजों की उपस्थिति बढ़ती । राया दुनायेव्सकाया का कहना है कि पूंजी के पहले खंड में जो जगह इंग्लैंड को मिली, अगर मार्क्स जीवित रहते तो वही जगह दूसरे और तीसरे खंडों में रूस और अमेरिका को मिली होती । इसी तरह मार्क्स के एक और अध्येता का कहना है कि ‘पूंजी’ के आगामी खंडों में यूरोपेतर समाजों की उपस्थिति का कारण यह भी होता कि पूंजी का प्रसार इन समाजों में लगातार हो रहा था और मार्क्स पूंजी के इस वैश्विक प्रसार के विरोध की रणनीति पर सोच रहे थे ।
2024 में मार्क्स की इन पांडुलिपियों का प्रकाशन हुआ । इनमें प्राचीन रोम के साथ ही इंडोनेशिया और मिस्र के बारे में टिप्पणियां हैं । मजेदार बात कि वे रोम के साथ भारत का भी जिक्र करते हैं । इन दोनों कृषक समाजों की कोई तुलना उनके दिमाग में रही होगी या इनके अध्ययन में कोई आपसी रिश्ता जरूर रहा होगा । इसके साथ ही रूसी खेतिहर समाज के बारे में भी लिखा गया है । रूस की सामग्री का तो पता नहीं था लेकिन रूसी क्रांतिकारियों के साथ उनकी चिट्ठी पत्री के सबूत सुरक्षित हैं । इसी तरह रूसी में कम्युनिस्ट घोषणापत्र की छपाई के मौके पर एंगेल्स द्वारा लिखी भूमिका भी मिलती है । इसी तरह आयरलैंड के बारे में पत्र और अन्य दस्तावेज भी सुरक्षित बचे हैं ।
किताब में जिन नोटबुकों का अध्ययन किया गया है वे ग्रुंड्रिस और आर्थिक दार्शनिक पांडुलिपियों के मुकाबले अधिक अव्यवस्थित हैं । जिन किताबों को वे पढ़ रहे थे उनका सार या उनके उद्धरण इनमें दर्ज हैं । लेकिन इनसे मार्क्स के चिंतन का भी पता चलता है । अनेक जगहों पर मार्क्स ने अपनी राय भी दर्ज की है । जिन किताबों के वे पढ़ रहे थे उनके तर्कों के साथ उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष संवाद भी जारी था । अध्ययन की सामग्री से विषयों और मुद्दों को अलगाकर चुनना और उनमें रिश्ता देखने की कला भी इनसे सीखी जा सकती है । इनसे यह भी पता चलता है कि पश्चिमेतर, उपनिवेशित और प्राक पूंजीवादी समाजों में उन्हें कौन से पहलुओं पर ध्यान देना क्यों जरूरी लग रहा था और उनमें क्या संबंध समझ आ रहा था । उनके चिंतन की नयी दिशाओं में झांकने का झरोखा इनसे खुलता है ।
यह तो निश्चित तौर पर कहना मुश्किल है कि मार्क्स इन नोटबुकों के सहारे किस दिशा में जाना चाहते थे । इसका बड़ा कारण यह है कि जब तक एंगेल्स मानचेस्टर रहे तब तक दोनों के बीच के पत्र व्यवहार से मार्क्स की बौद्धिक चिंताओं का सही अनुमान मिलता है लेकिन 1869 में एंगेल्स के लंदन आ जाने के बाद उनके बीच का यह पत्राचार बंद हो गया । अब वे दोनों रोज रोज मिलने लगे और आपसी बातचीत से एक दूसरे की राय लेने लगे । इस तरह की बातचीत का कोई दस्तावेजी सबूत मिलना मुश्किल होता है । एक अन्य स्रोत मक्सिम कोवालेव्सकी हैं जिन्होंने मार्क्स को मोर्गन की किताब का पता बताया था । 1875 से 77 के दौरान दोनों लोगों के बीच लंदन में अक्सर बातचीत होती थी । 1877 में वे मास्को विश्वद्यालय में अध्यापक हो गये । उसके बाद भी उनके बीच पत्राचार जारी रहा । इन पत्रों में से मार्क्स के लिखे पत्र अब गायब हो चुके हैं । विदेश यात्रा के समय उन्होंने ये पत्र रखने के लिए जिनको दिया था उन्होंने छापामारी के डर से उन पत्रों को जला दिया । मार्क्स को लिखे कोवालेव्सकी के पत्र तो उनके कागजों में मिले लेकिन उनसे मार्क्स की सोच का अनुमान नहीं होता । ये पत्र उस समय शिक्षित रूसियों की औपचारिक भाषा फ़्रांसिसी में हैं । इनमें मार्क्स के प्रति उनकी श्रद्धा व्यक्त हुई है लेकिन मार्क्स के चिंतन की दिशा स्पष्ट नहीं होती । 1879 में कोवालेव्सकी की भारत, अल्जीरिया और अमेरिका की सामुदायिक संपत्ति के बारे में किताब छपी । इस किताब पर भी मार्क्स ने तमाम टीपें दर्ज कीं ।
बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में तीसरी दुनिया का उभार हुआ । उसी समय छपी ग्रुंड्रिस में एशियाई समाजों पर विस्तृत टीपें नजर आयीं । इसके बाद परवर्ती मार्क्स की उपेक्षा सम्भव नहीं रह गयी और इस दौर के लेखन में रुचि पैदा हुई । परवर्ती मार्क्स की नयी धारणा भी 1980 दशक के बाद इस्तेमाल होने लगी । थियोडोर शानिन ने इस दौर में रूस के साथ मार्क्स के संसर्ग पर किताब लिखी जो 1983 में छपी । रूसी सामुदायिक संपत्ति संबंधी मार्क्स के लेखन का संग्रह तो इसमें था ही, उसके बारे में आधिकारिक विद्वानों के कुछ लेख भी शामिल किये गये थे । रोजा और मार्क्स के बारे में अपनी किताब में राया दुनायेव्सकाया ने भी दक्षिणी गोलार्ध, मूलवासी समुदाय और जेंडर संबंधी मार्क्स के इस समय के लेखन का विश्लेषण किया था । इस तरह का मार्क्स का लेखन कुछ समय पहले ही प्रकाश में आया था और उसके संपादक ने यूरोप के मुकाबले एशिया, अफ़्रीका और उत्तरी अफ़्रीका पर मार्क्स की निगाह केंद्रित होने के तथ्य का उल्लेख किया था । इसके बाद मार्क्स के इस मानवशास्त्री रूप पर भी लिखा गया । इस किताब के लेखक ने भी मार्क्स के लेखन में हाशिये की मौजूदगी संबंधी अपने अध्ययन का आखिरी अध्याय मार्क्स के इसी दौर के लेखन पर केंद्रित किया था । हीथर ब्राउन ने मार्क्स और जेंडर पर अपनी किताब के दो अध्याय मार्क्स के इस परवर्ती लेखन पर केंद्रित रखे । मार्चेलो मुस्तो ने मार्क्स के इन दिनों की एक जीवनी भी लिखी है । जापानी विद्वान कोहेइ सैतो ने पारिस्थितिकी और सामुदायिक समाजों के सिलसिले में मार्क्स के इस दौर के लेखन को याद किया है । ब्राज़ीली मार्क्सवादी ज्यां तिब्ले का कहना है कि साठ साल की उम्र में मार्क्स के चिंतन में जो बदलाव आ रहा था उसका सीधा रिश्ता उपनिवेशवाद विरोधी गोलबंदी से है । इस दौर में उन्होंने यूरोप केंद्रीयता से लगभग पीछा छुड़ा ही लिया ।
मार्क्स के समग्र योगदान को समझने और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता के लिए उनके परवर्ती लेखन का महत्व अधिकाधिक विद्वान स्वीकार करने लगे हैं । गारेथ स्टेडमान जोन्स ने परवर्ती मार्क्स पर विस्तार से विचार तो किया लेकिन दक्षिणी गोलार्ध से उनके इस समय के लेखन के रिश्ते की मौलिकता को उजागर नहीं कर पाये हैं । फिर भी उनकी जीवनी ने परवर्ती मार्क्स को मार्क्स अध्ययन के चंद विशेषज्ञों की दुनिया से बाहर निकालकर समग्र मार्क्स को समझने की आवश्यकता के तहत जरूरी बना दिया है । रयुजी ससाकी ने तो मार्क्स पर लिखी किताब का तिहाई हिस्सा परवर्ती मार्क्स पर ही केंद्रित रखा है ।
एंडरसन ने जोर देकर कहा है कि इस किताब का मकसद मार्क्स के लेखन में पूंजी और वर्ग की केंद्रीयता को भंग करना नहीं है । ‘पूंजी’ का पहला खंड तो मार्क्स का महानतम ग्रंथ है जिसमें उनकी पद्धति और विश्लेषण सबसे अधिक विकसित रूप में मौजूद हैं । इसके बावजूद उसमें पूंजीवाद के खास रूपों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना उसके सामान्य लक्षणों पर दिया गया है । अमूर्तन की यह ताकत उस काम के लिए जरूरी थी जिसमें पहली बार समग्र पूंजीवादी व्यवस्था की प्रकृति, संरचना और अंतर्विरोधों को उजागर किया गया था । फिर भी कहना होगा कि उसके अलग अलग रूपों में कुछ अन्य पहलू खास भूमिका निभाते नजर आते हैं । पूंजी और श्रम की द्वंद्वात्मकता के भीतर नस्ल, जेंडर, उपनिवेशवाद और इसी तरह के पहलू यथोचित जगह नहीं बना पाते । इस विविधता को देखना तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम पूंजी के प्रतिरोध और क्रांति की सम्भावना पर विचार करते हैं । वे जोड़ते हैं कि मार्क्स कोई संकीर्ण अनुभववादी नहीं थे हालांकि उन्हें खास किस्म के मानवविज्ञानी या सांख्यिकीय आंकड़ों का सहारा लेना पड़ा था । वे तो इस मामले में हेगेल के प्रचंड आलोचक थे जो मानव मुक्ति की संपूर्णता को अमूर्त परम विचार की दुनिया में ही फलित होता देखते थे । इस आलोचना को उन्होंने प्राचीन रोमन गुलामों से लेकर अपने समय के फ़्रांसिसी क्रांतिकारियों की ठोस ऐतिहासिक दुनिया में अवस्थित करते हैं ।
इस किताब में छह अध्याय हैं । इनमें परवर्ती मार्क्स के लेखन के अलग अलग पहलुओं का विवेचन किया गया है । पहले अध्याय में सामुदायिक सामाजिक संरचनाओं का जिक्र है । इसके तहत मार्क्स ने उपनिवेशन से पहले के उत्तरी अमेरिकी हालात का विश्लेषण किया है जिसमें मूलवासी अत्यंत निजी वस्तुओं को छोड़कर अधिकांश संपत्ति का साझा इस्तेमाल करते थे । इनके साथ ही उन्होंने प्राचीन जर्मन समाज और उपनिवेशित होने से पहले के आयरलैंड का भी जिक्र किया है जहां पारम्परिक गोत्र से वर्गीय समाज का जन्म हो रहा था । साथ ही लैटिन अमेरिका के इंका और उपनिवेशित होने से पहले भारत के मुगलों का भी जिक्र है जब जमीन साझा संपत्ति थी और बहुत छोटे शासक समूह के दबदबे में वर्गों की सीढ़ी काम करती थी । उन्नीसवीं सदी के रूस में भी उन्हें सामुदायिक ग्रामीण अर्थतंत्र और स्वेच्छाचारी शासक वर्ग का मेल नजर आया । यह ऐसा समाज था जहां अभी पूंजीवाद का प्रवेश बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था । उस समय अन्य बहुतेरे समाज यूरोपीय उपनिवेशवाद के मातहत थे । उनमें सामुदायिक सामाजिकता के अवशेष तो थे लेकिन औपनिवेशिक पूंजी द्वारा थोपा हुआ व्यक्तिवाद भी प्रवेश कर रहा था ।
दूसरा अध्याय जेंडर, नातेदारी और स्त्री सबलीकरण पर केंद्रित है । मार्क्स के निधन के एक ही साल बाद एंगेल्स की परिवार वाली किताब छपी । यह किताब मोर्गन की प्राचीन समाजों वाली किताब के बारे में मार्क्स की नोटबुक पर आधारित थी । एंगेल्स का कहना था कि प्राचीन निरक्षर समाज जेंडर के मामले में समानता वाले थे । बाद में दुनिया के बहुत सारे देशों में सामाजिक वर्ग, निजी संपत्ति और राज्य के उदय के साथ अबाध पुरुष प्रभुत्व कायम हुआ । प्राचीन ग्रीस, रोम और देशी अमेरिकी समाज उनके उदाहरण थे । जेंडर के मामले में मार्क्स की टीपों में मोर्गन के साथ अन्य लेखकों का भी जिक्र था और इसके चलते जेंडर के साथ औपनिवेशिक भारत और अल्जीरिया, प्राचीन ग्रीस और रोम, देशी अमेरिकी समूहों के अतिरिक्त आयरलैंड के प्रसंग में मानवशास्त्र और सामाजिक इतिहास भी था । उन्होंने मोर्गन और अन्य मानवशास्त्रियों तथा सामाजिक इतिहासकारों की परिष्कृत व्याख्या भी की थी । मार्क्स ने साक्षरता से पहले के समाजों की जेंडर विषमता और पितृसत्ता के प्रसंग में अन्य तत्वों का भी उल्लेख किया था और उनका आदर्शीकरण करने से बचे थे । उन्होंने बाद की पितृसत्ता को एकदम ठोस नहीं माना था और स्त्री की सामाजिक सत्ता की मौजूदगी हाशिए के समाजों में पहचानी थी ।
तीसरा अध्याय ऐतिहासिक विकास की विविधता और जटिलता के बारे में है । शुरू में मार्क्स ने उत्पादन पद्धतियों के क्रमिक विकास का खाका पेश किया था जिसमें आदिम, दास, सामंती और बुर्जुआ चरण थे । ग्रुंड्रिस में उन्होंने एशियाई उत्पादन पद्धति को शामिल किया । बाद के लेखन में सामाजिक विकास के अन्य रास्तों की बात भी उन्होंने की । उन्होंने मुगल भारत के प्रसंग में यूरोपीय सामंती ढांचे को लागू करने का विरोध किया । पूंजी के फ़्रांसिसी संस्करण में उन्होंने पश्चिमी यूरोप के बाहर के समाजों के लिए विकास के भिन्न गतिपथ की बात जोड़ी । रूस के भी प्रसंग में परवर्ती लेखन में उन्होंने इस बदलाव का जिक्र किया है ।
चौथा अध्याय उपनिवेशवाद और उसके प्रतिरोध के बारे में है । इस प्रसंग में उन्होंने घोषणापत्र और भारत संबंधी न्यू यार्क ट्रिब्यून के लेखन को याद किया है जिसमें मार्क्स ने भारत और अल्जीरिया के मामले में क्रमश: ब्रिटेन और फ़्रांस के बर्बर शासन के बावजूद उन्हें आधुनिकता का वाहक बताया था । 1879 में भारत के बारे में लिखते हुए वे 1857 के सिपाही विद्रोह का उत्साह के साथ जिक्र करते हैं । साथ ही सामुदायिक सामाजिक संबंधों का जिक्र उपनिवेशवाद के प्रतिरोध की सम्भावना के बतौर करते हैं । उसी समय लैटिन अमेरिका के बारे में लिखते हुए वे स्पेनी विजेताओं द्वारा मूलवासियों के कत्लेआम तथा उनको गुलाम बनाने का उल्लेख करते हुए भी चर्च के दबाव में शोषण की कमी का जिक्र करते हैं । साथ ही वे अफ़्रीकी गुलामों की भारी आमद का भी जिक्र करते हैं । पहले वे मानते थे कि आयरलैंड की मुक्ति ब्रिटेन के मजदूर आंदोलन पर निर्भर है लेकिन अब उन्हें ब्रिटेन के मजदूर आंदोलन के भीतर उपनिवेशवाद से प्रभावित विचारों के प्रसार की भनक लगी इसलिए वे मजदूर आंदोलन के पुनर्जीवन हेतु आयरलैंड की मुक्ति को जरूरी समझने लगे ।
पांचवां अध्याय रोम, भारत और रूस के कृषक समाजों के बारे में है । इन तीनों समाजों में ग्रामीण स्तर पर समतामूलक सामुदायिक सामाजिक ढांचों में अलग अलग समय पर बिखराव आया । भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने इस ग्रामीण पंचायती व्यवस्था का बड़े पैमाने पर उन्मूलन किया । प्राचीन रोम में गणतंत्र के दौरान गुलामों के श्रम पर बड़े बागानों की व्यवस्था का उदय हुआ जिससे मुक्त किसान की आबादी घट गयी । जो लोग आजाद थे वे दासों के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे । उनका यह रुख आधुनिक नस्लवाद की तरह था जिसके कारण सामाजिक क्रांति बाधित हो गयी थी । 1870 और 1880 के रूस में पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवाद के दबाव से सामुदायिक ग्रामीण जीवन नष्ट हो रहा था । प्राचीन रोम और वर्तमान रूस में पूंजीवाद की ओर ले जाने वाले कुछ तत्व थे लेकिन पूंजीवाद से उनकी भिन्नता अधिक स्पष्ट है । उन्होंने रूस के पूंजीवाद मेंप्रवेश को अपरिहार्य मानने से इनकार किया और अन्य देशों के लिए भी वैकल्पिक रास्ते की सम्भावना देखी । यह उनकी पहले की मान्यताओं से अलग बात थी ।
आखिरी छठवें अध्याय में क्रांतिकारी बदलाव की नयी धारणाओं और पूंजीवाद के विकल्पों की बात की गयी है । मार्क्स को विकसित पूंजीवादी देशों के मजदूर वर्ग के उभार में क्रांति की उम्मीद नजर आती रही थी । फिर वे आयरलैंड की आजादी के आंदोलन से ब्रिटेन के मजदूर वर्ग की चेतना उन्नत होने की बात करने लगे थे । उन्हें मजदूर वर्ग के भीतर आयरलैंड के उपनिवेशीकरण के प्रभाव की वजह से वर्गीय चेतना मंद होने के संकेत मिल रहे थे । अयरलैंड की मुक्ति से ब्रिटेन के मजदूर वर्ग में व्याप्त इस अर्ध नस्ली आयरलैंड विरोध के कम होने की उम्मीद थी । ‘फ़्रांस में गृहयुद्ध’ तथा ‘गोथा कार्यक्रम की आलोचना’ में उन्होंने कम्युनिज्म की कुछ नयी धारणाओं को आजमाया । पहले वे राजकीय पहलू पर अधिक जोर देते थे लेकिन अब मुक्त और सहकारी श्रम की बात करने लगे । रूस के प्रसंग में तो उन्होंने ग्रामीण सामुदायिक जीवन में पूंजीवादी घुसपैठ के विरोध में होने वाली क्रांति को आधुनिक कम्युनिज्म का जनक माना बशर्ते यह उभार पश्चिमी मजदूर आंदोलन से जुड़ जाए । इसी तरह अल्जीरिया और भारत के प्रसंग में उन्होंने सामुदायिक ग्रामीण ढांचों की बात करते हुए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों का भी उल्लेख किया । क्रांति की उनकी नयी धारणा को उनके जेंडर संबंधी टीपों से भी जोड़कर देखना लेखक को अत्यंत विचारणीय लगता है ।