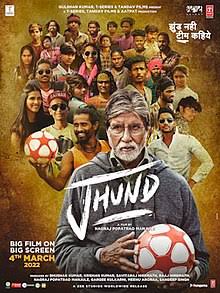(आजादी के बाद की हिन्दी कहानी में चर्चित रहे लेखक मार्कण्डेय की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर समकालीन जनमत के पाठकों के लिए प्रस्तुत है उनकी एक कहानी।)
बड़े जोर की तपन है, हरियरी का कहीं नाम न जस। बस आम-महुआ के सिर पर टोपी नुमा, थोड़े हरे पत्ते बच रहे हैं। रास्ते पर जैसे किसी ने भाड़ का बालू बिछा दिया हो। तीन मील की इस खेतार में एक भी बाग नहीं। एक भी छायादार पेड़ नहीं। प्यास लगे तो आदमी तड़प कर मर जाए।
“पानी पी लो भइया, खूब मुचेमुच्च पेट भर के, नहीं तो पियास लग जाएगी तो परानै गवा समझो।”
लोकई ने, जिसे इस स्टेशन पर ढूँढने के लिए, मुझे घंटे भर रुकना पड़ा था, और इसी कारण साढ़े ग्यारह के साढ़े बारह बज गये थे; बिस्तर सड़क पर रखकर, दुकान के सामने खड़े होते हुए कहा। मेरे बिना कहे साव ने मिठाइयों की फरमाइश करने के बाद, वह मेरी ओर देखकर एक तेल से डूबे स्टूल पर से मक्खियां उड़ाते हुए बोला, “बइठि जाओ, छहाय लो! बड़ा मरन है इस रस्ता में।”
उसने मिठाई का दोना मेरे हाथों में रख कर भट्ठी से राख लिया। पीतल की नन्हीं लोटिया को माँजकर मुझे पानी पिलाया और दो मिठाइयों के साथ चार लोटिया पानी खुद चढ़ाकर, मेरे साथ चल पड़ा। पर एक टप्पे को पार करते-करते मेरा हलक सूखने लगा। लेकिन किसी-किसी तरह, एक-एक हरी अड़ूस की झाड़ियों और ठिगने-बौने पेड़ों को गिनते, छाया की सभी आशाओं के स्थान पर, लू के थपेड़े सहते हुए, हम घर की छत के नीचे पहुँच गये थे।
काकी हदा के दौड़ीं। खटोलिया बिछाते हुए, हाथ-गोड़ धोने का पानी लाने को कहा, फिर टूटे बेने पर पानी का छिड़काव कर, चुर-मुर चुर-मुर डुलाने लगीं।
लोकई को बारह आने देने थे पर मेरे पास दस रूपये के नोट! क्या जाना था कि गाँव में पैसा गधे की सींग हो जाएगा। छब्बू बरई और मोहन साव के यहाँ से बचनुवाँ लौटा आया, पर नोट नहीं टूटा।
” लगन के दिन हैं न बचवा! बड़ा कमात बाड़े सौ। कहने के बड़े मनई हैं, खोज आओ तो एक ठो फुटहा पैसा भी न निकली ठकुराने में।”
फिर कुछ रुककर, उन्होंने पंडित के यहाँ एक आदमी भेजा, पर वहाँ भी नोट न टूटा। बुचऊ सिंह का नाम लेते हुए वे हँसने लगीं, “बड़ा चानस है, तोहरे बुचऊ का। तुम्हार नाँव सुनते ही दउड़ा आएगा, लेकिन बहुत बोलना-डोलना नहीं उसके साथ, आज-कल हुक्का-पानी बंद है।”
बुचऊ का हुक्का पानी! मैं अचम्भे में पड़ गया था। पाँच-छै बरस पहले का वह जमाना मेरे आगे नाचने लगा, जब बुचऊ भीटे से कंकड़ियाँ बटोर कर लाता और दंड बैठक करते समय, उन्हीं से गिनती करता। नन्हा, ठिगना, लकड़ी की गांठ सा आदमी, आगे के दो काले दांतो में से एक आधा हिस्सा टूटा हुआ और मिट्टी के लोने से चेहरे में घुमची की तरह, जड़ी हुई दो नन्हीं-नन्हीं आंखें। मुझे देखते ही उसके होठ दाँतों पर चढ़ जाते थे और वह हाँफ-हाँफकर होठों के किनारे आए हुए थूक के गाज को पोछता हुआ, घंटों बात करता रहता था।
“बालगंगाधर तिलिक, गोखली, मदनमोहन मौलवी, सीयारदास और जाने कितने… कँगरेसी नेता… गजब-गजब आदमी हैं भइया! उज्जर, बकुला के पंख ऐसा कपड़ा पहिनते हैं। पसेरी-पसेरी भर का खोपड़ा है। बड़े-बड़े पुलुस दरोगा कुचुर-कुचुर मुँह ताकते रह जाते हैं। मुन्सीपाल्टी वाले हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। महत्मा गन्ही के मोटर में बड़े-बड़े धनी, बोझ-बोझ भर नोट का पुलुन्दा झोंक देते हैं। औरत-मरद अपना गहना- गीठों दे देती हैं। बस एक ही बात- अंदोलन करो! सत्त पर चलो! खद्दड़ पहिनो!” और वह रुक-रुक कर बाबा की मोटी जाँघ को अँकवार में लपेट-लपेट कर तेल लगाते-लगाते हलाकान हो जाता।
हमा-सुमा के, के पूछत है उहाँ। बड़े-बड़े सेठ साहूकार के गुलाब के फूल जैसन तिरियन के कउनू तरह दरसन मिल जाता है, लेड़ी-बूची की कौन बात है?” यह चिढ़कर उस समय कहता, जब कोई गाँव का मसखरा बीच में उसे टोक कर कहता, “तुमको भी मिली थी एकाध माला क्या?”
” ले आये हैं, सुबाष बाबू की तस्वीर। जैहिन्न ऊपर लिखा है, नीचे तिरंगा लिए कपटन बने खड़े हैं। थोरिक फूलो है उनके ऊपर का गिरा हुआ। न बिसवास हो तो चल के देख लो। ”
“रक्कत हो गया है सारा मुँह।” काकी ने खयाल तोड़ दिया और पंखी रोककर वे मेरे बालों पर हाथ फेरने लगीं। “पक्का में पंखा के नीचे रहते रहते केतना सुकुवार हो गए हो। तनी लोट जाओ!” और उन्होंने एक लगदी लपेटकर, तकिया बनाते वहुए मेरे सिरहाने रख दिया। फिर गगरे से ताजा पानी लेकर पांव धोते हुए, वे बहू को पुरनकी खाँड़ का ठिल्ला बताकर कहने लगीं, “रानी के बियाह की खाँड़ है। बड़े जतन से जोगवत-जोगवत बची है, पर तोहरे कक्का के मारे रहाइस नहीं है। कभी इमले, कभी सिकेटरी, जब से ई पंचायत बनी, दुवार खनाय गया। बचनुआ एक दिन, स्कूल से लौटा था। गाँव के सब लड़के संग-संग थे। इमले महराज कहीं जाय रहे थे। बच्चा तै बच्चा, उसने जाने कैसे कह दिया, ‘रोटी, कपड़ा, तेल दो! सब लड़कों ने चिल्लाकर जवाब दिया…कुरसी छोड़ दो…वरना…’ अइसी कुछ” वे शरमा कर हँसने लगीं।
मैंने उठकर बैठते हुए कहा, “तो क्या हुआ?”
“अरे भइया इमले तो नाराज न हो गये। तुम्हारे काका से लकठा लगा दिया और बचनुवा पर ऊ ऊ मार पड़ी, वह तो संजोग कहो बुचऊ बैठा रहे दुआरे, सड़ासड़ बहस करने लगे और लोग बतावत हैं गलदोद न दिया इमले को; पर इनको क्या कहें, उनको दुआरे से उठा दिया। सुना, बेचारू रो के चले गये।”
उसी समय बचनुवा अजुरी में पैसा भरे, दौड़ा आया और मेरी चारपाई पर गिराते हुए अपनी जेब से दस रूपये का नोट निकालकर मुझे देते हुए कहने लगा, “मुझे दादा ने कहा है कि अपने भइया से कहना शाम को हमारे ही घर खाएंगे।”
“बाप रे बाप” काकी बीच में बोल उठीं।
“क्या हुआ काकी, बस इतनी-सी बात के लिए।”
काकी बोलने ही जा रही थीं कि बचनुआ ने एक हाथ उनके मुंह पर रखते हुए कहा-
“कहा है कि खसी काटेंगे…एक ही जगह बनेगा। सब लड़के जुड़ेंगे गाँव के… और… और… कहा है, पइसा दे देना… नोट भी दे देना, दस का फुटकर नहीं है।”
उसी समय काका बाहर से बिगड़ते हुए घर में घुसे, “पंचाइत के बक्से में रुपया नहीं था, कि भेज दिया उसके घर, यह बार-बार की आवा-जाही ठीक नहीं है।”
फिर कुछ नरम होते हुए, “क्यों इतनी धूप में चले आए, रुक जाते वही बजरिया में। अच्छा कुछ खा-पीकर सो रहो। और वे बाहर चले गए।
“कहो बचवा, चन्ना का रुपिया हम कइसे छुईं? यह तो जबसे कंगरेस कमेटी के लेम्बर भये, अकिलियै मारि गई इनकी, छोट-छोट बात पर लड़ा करते हैं, बस रात-दिन चन्ना, कदम-कदम पर चन्ना। जो यह बचनुआँ है न, हर महिन्ना स्कूल में एक न एक चन्ना देइ, हमरे नाको दम है, परसों मनिस्टर साहब आवै के रहें तो दिन भर लाठी-गोजी रंगत रहा, दो बजे से उसरे में खड़े-खड़े साँझ हो गयी पर नहीं आये। नन्हें-नन्हें बच्चे हकसे-पियासे घर लौट आये। जानकी के बेटौना के तभी से जर चढ़ा है… सब कहते हैं लू लग गयी है। भगवान जाने।”
काकी कहते-कहते खाना ठीक करने के लिए उठ गयीं और बचनुआँ जल्दी-जल्दी बेना डुलाने लगा।
खाना खा कर लेटा, तो हवा के तेज झोकों की साँयँ-साँयँ कुछ कम पड़ने लगी थी। लू की लपटें मिट्टी के पटौधे घर में बहुत कम लग रही थी, फिर भी काकी कई बार आती, बेना डुलाती और किवाड़ी उठँगा कर वापस चली जातीं। बचनुआँ ताखे में रखी कौड़ी को लेकर खनखनाता हुआ भागा, तो वे फिर बिगड़ीं, “बुचऊ के दालान में न जाना, नहीं तो मार पड़ेगी, तो मैं नहीं जानती।”
मैं समझ नहीं पाता था कि क्या बात है, तो बुचऊ निगाह से इतना गिर गया, आखिर यही काकी तो घंटों उससे हंसी चिबोला करती रहती थीं।
-एक गगरा पानी बबुआ… तोहरे हथवा का बड़ा मीठा लगता है।
-रख न लो भउजी। पानी ही भरा करूँगा।
बाजार से चुपके से धोती मँगानी हो, तीज-त्यौहार का सामान करना हो, उधार-बाढ़ी पैसा मँगाना हो, सबके लिए बुचऊ। यहाँ तक कि परिवार के बड़े से बड़े मौके पर, वह काम आता। परिवार की गोपनीय से गोपनीय बातें उसे मालूम रहती।
काका चन्दे के लिए एक बार बम्बई तो लौटने पर बुचऊ का किस्सा कहते-कहते लोट-पोट हो जाते। “चौपाटी पर उसे खबर मिली, कि मैं आया हूँ। बस आव न देखा ताव, कांवर कहीं एक दुकान पर पटकी और ट्राम पकड़ कर तारदेव पहुँच गया। मैं बाहर जा रहा था पर बुचऊ तो बुचऊ, बिना चाय-पानी कैसे बनी, भइया! विस्सास नहीं होता है कि तू आए हो और वह पकड़कर एक होटल ले गया। दसियो रुपए फूंक दिया। घर लौटते-लौटते सिंधुर-टिकुली से लेकर साड़ियां-जंपर, ब्लाउज, बचनुआँ के लिए कपड़ा और काकी के लिए मुंबा देवी का प्रसाद देते हुए कहने लगा, तोही लोग तो हो भैया नहीं तो हम सुराजी पाल्टी में भर्ती हो जाते। ” फिर उसने जवाहिरलाल, महात्मा गांधी सबकी छोटी-छोटी तस्वीरें काका को दी थी।
बुचऊ को अपनी एक बेटी सरधा के अलावा कोई नहीं। मेहरारू मर गई तो उसने कहा, “नार मुई घर संपत नासी, मूड़ मुड़ाय होब सन्यासी” और वह सरधा को मेरे घर छोड़कर, बम्बई चला जाता। सात-आठ महीने कमाता, फिर बहुत सारे कपड़े, गहने, सामान लेकर लौटता। गाँव में सबको सिगरेट की डिबिया और साबुन देता। गाँजा की पोटली खोलता और ऊपर से महात्मा गांधी का संदेश पिलाता।
“चमार, मुसहर, भर, पासी… सबके हाथ मिलाए से देसवा जागी। गन्हीं जी उनहीं के हैं। कहत रहे चौपाटी पर कि वही हमको सबसे पियारे हैं। उनहीं का हूँ। देश है गरीब लोग का। सुराज मिलते ही इनका राज लौट आयी।” और वह गाँव की छोटी जातियों को घूम-घूम कर आश्वासन देता है, कि “भाई तुम्हारा राज है… आंदोलन में हाथ लगाए रहो। रजिन्दर बाबू कंगरेस के मालिक हैं, उनहीं की बात मानो।”
मुझे खूब अच्छी तरह याद पड़ता है, जब वह एक दिन एक रात बिना अन्न पानी के रोता रहा था। अपनी लाल रंग की जांघिया और खाकी कमीज चरवाहे को दे दी थी। बिगुल गाँव के लड़कों को दे दिया था और जैहिंद का सुभाष बाबू वाला बिल्ला मुझे देते हुए कहने लगा था, “धरे रहना बच्चन! रजेन्नर बाबू के, जवाहिर लाल के…हाय रे नेता जीव, न भया तू एहि मौके पर” और वह खाए पिए बिना बाजार जा कर लाए हुए अखबार को नोचने लगा था।
” हम तो जाने झूठ ही उड़ा है। फिरंगिया की कोई गोटी है। कल रात सुना तो सवेरे बाजार से पर्चा लेने गए। आखीर में बटी गया देशवा।
” सरदार वल्लभ भाई कहवाँ रहे? समझात नहीं कुछ। ” और जब सवेरे सभा हुई तो सब लोग बुचऊ सिंह को सुनने के लिए उतावले हो रहे थे। गाँव के किसान कहते, भाई हम कैसे जानें कि अजाद हो गये …अंगरेज चले गये…हो ही नहीं सकता। भइया सुई की नोक भर के लिए तो महाभारत भवा, और ई सोने की चिड़िया छोड़कर जाएगा अंगरेज… ना… ना… बुचऊ सिंह कहें तो मानें। वही कहेंगे तो दिया-बत्ती होगी। नहीं तो, कौन खरचे तेल-बाती? घर की उरदी जेंगरे में डाले।”
काका ने बहुत समझाया, बहुत कहा, पर बुचऊ तख्ते पर नहीं गया। फिर जब सभा से शोर होने लगा, तो वह अपने गमछे को लपेटते हुए धीरे से तख्त पर चढ़ा। मुझे खूब याद है वह रो पड़ा था, “हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मुदा परचा में बचाय के सुना, तो सब जान पड़ा। हम तो खाली लड़ना सीखे थे… इसी से आजादी आवै वाली रही। जवहिरो लाल, गन्हियो महतमा इहै कहे थे, ‘देसवा हमरे जीव के समान है- कैसे बटी?’ का होगा, अस सुराज लेके। मुदा सरधा-भगती से परनाम करो! कुछ भवा जरूर है गड़बड़। महतमा का, जवाहिर लाल का, हिन्न का नाम लो? हमरे मन में तो अन्हियार छाय गया है।”
उसी के बाद बुचऊ बम्बई गया था, पर पता लगता था अब वह परचा खरीद कर हमारे गाँव के मुंशी जी की खोली नहीं जाता, न तो उनसे परचा पढ़वा कर सुनता है। वह काम-धंधे पर से भी हट गया है। दूध की काँवर ढोई नहीं जाती उससे। घाटी-मरहठी औरतों की कतरनी-सी जबान सहने का साहस उसमें नहीं रहा। इसीलिए वह कभी तरकारियाँ बेचता है, कभी फल और शाम को भँइसवारों के तबेले में चिलम पर फूँक देता है।
कई साल से तो सरधा को महाजन की दुकान बताकर, बम्बई जाने लगा है। एक-दो बीघे जमीन भी उसकी अपनी थी, पर वह भी धीरे-धीरे चली गयी। एक-एक करके पेड़-पालव भी उसने बेच दिये…
मेरे विचार सूत्र टूट गये। काकी ने धड़ से दरवाजा खोला और कहने लगीं, “दुलारा आजी बैठी हैं। पावलागन कर लेना बच्चन! बेचारी बहुत पूछती हैं।” मैं चारपाई पर उठ बैठा…आँगन से घाम चला गया था। बहुत शाम हो गई थी। पर बाहर होने वाली बात सुनकर, बैठा रहा..
“अरे मरकिनौना अधरमी हो गया है। चमार सियार का छुवा-छिरका खाये से अउर का हो सकत है” फिर कुछ रुककर, “ए बचवा, सुना है न!” जैसे कोई गोपनीय बात कह रही हों, “कोई घाटिन औरत राखे है बम्बई में, इसी से त कमाई-धमाई देखाती नाहीं, कहाँ आग परि गई। सब तो उहै अदमिया हैं, उहै कमइया है, ओही मुंहफुकौना के बज्जर पड़ गया।” दुलरा आजी कह चुकी थीं, अब काकी कुछ बोल रही थीं।
एक इनहूँ आदमी हैं न मइया… कंगरेस के जिलवा भर के मालिक, मुदा बात जो चाहे कर लें। भला कह तो दो, किसी का छुवा पानी पीने को। कहते हैं, ‘सिधानत मानै से, करै से अंतर है।’ एक खद्दर का कुरता-धोती धरे हैं। मिटिन में जाना होई, तो पहिन लेंगे, फिर घर लौट कर जैसे के तैसे।”
“यही धरम है, ए बचिया। सबको इतना गियान कहाँ? कहा है, ‘बाढ़ै पूत पिता के धरमें।’ बड़े बाप के बेटा है न।”
मैं बाहर निकल पड़ा, बात समझ में आ गयी। शायद वह काका का विरोध करता है। किसी नयी पार्टी में चला गया बुचऊ। मैंने सुना, दुलरा आजी आशीर्वाद वर्षा रही हैं, तो चाची की ओर देखने लगा। उनका चेहरा उतर गया था। मैंने आजी को प्रणाम किया और बाहर चला गया।
बचनुआँ कोली में से दौड़ा आया और मुझे दूर बुलाकर कहने लगा, “बुचऊ दादा बुला रहे हैं। कलवा बन गया है, कहते थे ठंडा हो रहा है। बच्चन को जल्दी से बुला लाओ।”
मैं बहुत उदास था। एक तो दिन की थकान। दूसरे, यह सारी बातें। आखिर गांव से यह अंधेरा कब जाएगा। अब तो हम जैसे सब कुछ पाकर स्वराज का सुख भोगने लगे हैं। हमारे भीतर का आदमी कहां चला गया। मैं सोचता-सोचता बुचऊ के दरवाजे पहुंच गया। वह उदास बैठा था। मुझे देख कर फिस से हंसकर रह गया। जैसे किसी गुब्बारे से हवा निकल गई हो। सरधा ने कटोरी में कलवा दिया। मैंने हाथ में लिया ही था, कि वह कहने लगी, “मैं तो समझती थी, नहीं आओगे भैया। काकी-काका ने…”
उसे देखा- बहुत चौक कर, यह कैसी हो गयी? इतनी बड़ी! कितनी सुंदर! लाल किनारे की पीली-पीली धोती पहन रखी थी उसने। झुक कर पाँव छूते-छूते उसका चेहरा लाल हो गया, मन की तहों में खराश लग गयी, इसकी शादी होनी चाहिए, पर बुचऊ की गरीबी? मैं चुप रह गया। सहसा खयाल आया, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो बुचऊ से हालचाल पूछने लगा।
“हाल-चाल के दिन लद गये बच्चन, अब तो जीव जी रहा है। समझो जितने दिन चले यह काया।” इसी बीच सरधा मिट्टी के तेल की ढेबरी दीवट पर रख गई। मैंने इधर उधर देखा लोग आ जा रहे थे पर कोई वहाँ न तो रुकता था, न बैठता था। हवा बहुत धीरे-धीरे चलने लगी थी। बुचऊ के दरवाजे की पोखरी के कारण ठंडा था। मैंने कहा, कुछ राजनीति की बताओ, दादा।”
राजनेत तो गन्ही महतमा के साथ चली गयी बच्चन! विचार नाहीं रहा अब, अउर बिना विचार की नेति कहाँ? देखा न…” वह बोलता जा रहा था। “अब काम धंधा सब में बेबिचारी आ गई। जो कुछ आग पानी हिरदय में रहा, वह बुझाय गया। हमका छोड़ा, नेता लोगों को देखा, उनका भी वही हाल। जिस कुर्सी पर बैठ गए, बस वह उनकी हो गई। अब तो कुरसी की नेति है। गन्ही महतमा का कुल काम-धाम धरा रह गया।”
“हो तो रहा है बहुत कुछ दादा।” मैंने उत्सुकता से कहा।
“क्या हो रहा है। धरम के नाव पर, जाति के नाव पर वोट उगहात हैं। ठाकुर के ठाकुर, बाम्हन के बाम्हन, कहां गई गरीबी, कहां गया छुआछूत…? अब विचार नहीं रहा, बस वोट रह गया है।
गड़बड़ तो यह है कि लोक में से बात की मरजाद उठ गयी। कहने करने में भेद हो गया। गन्हीं महतमा कहते रहे कि कउनो देश की आपन मरजाद होती है… आपन एक चरित्तर होता है, मुदा वह सब बुझ रहा है। वे आन्हर हैं, जो इसे नहीं पहचानते।
हम तो देखते हैं न परदेस में- देश में, एक-एक आदमी कहां से कहां पहुंच गया। जो एक बुराई से लड़ने की बात रही- अपने भीतर की हो या बाहर की- कुछ खोय के भी, सत्त पर, अहिनसा पर डटे रहने की बात थी- सब चली गयी।”
मैं स्तब्ध था, बुचऊ की बात सुनकर। कुछ कहते नहीं बनता था। मैंने पानी पिया, और फिर उसकी बातों में खो गया…
“वे सब आन्हर हैं बच्चन, जो देखके भी भूलते हैं। किसी देह में जब बीमारी से लड़ने की शक्ति नहीं रहती है तो चाहे जो रोग खा ले जाए, कहा नहीं जा सकता?
“अपने के देखो न! भइया दस हजार तिलक ले रहे हैं- तुम्हारी शादी के लिए। का अइसा बियाह होना चाही, पढ़े-लिखे लरिकन का। बस नौकरी मिल जाए के चाही। नहीं तो महात्मा के कहने पर कितनों ने ब्याह नहीं किया, कितने जेल गए, नौकरी-चाकरी छोड़े, स्कूल छोड़ दिए- असहजोग में, नून में, अब तो एक-एक कौड़ी छोड़ने में नानी मरती है। मुदा सब ठीक है… सब, कैसे कोई के… हमही का कहीं…हमही”, और वह खो गया था। स्वयं उसे लगा जैसे वह अपने साथ बेइमानी कर रहा है। मैंने इधर-उधर देखा, पर चारों ओर बुचऊ- वही ठूठे बाल- काँटों की तरह, आगे के दोनों काले दाँतों में, एक आध टूटा हुआ और माटी के लोंदे में बुझी हुई, दो घुमची की तरह आँखें…
घर आ गया, दहलीज में गहरा अंधेरा था पर काका की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, काकी को डांट रहे थे, “कुछ इज्जत-बात का खयाल भी है उनको, एम.ए तो पास कर लिया। मैंने गांव भर को रोक रखा है, पर वे ही जाकर उसके घर खाना खा रहे हैं। आज सब पक्का पता चल गया कि ससुरे ने नौ सौ रूपये और एक ऊँट दाना लिया है सरधवा की शादी के लिए। बेटी का बेच खाकर जिएगा। ”
चाची जैसे भौचक्की होकर रह गई थीं, “नौ सौ रूपिया और एक ऊँट दाना।”
“हाँ हाँ, पर उनकी यही हाल रही, तो हम भी कहीं के नहीं होंगे। मना करने पर भी, उसके घर चले गये, तो पूछ लेना, शायद शादी पर भी कुछ कहना हो उनको।”
मैं उलटे पाँव बाहर लौट आया और चारपाई पर लेट गया।
वह बेटी बेचता है- बेटी, और, और बुचऊ के लोंदे की तरह के मुँह में निकले डेढ़ काले दाँत, मुझे चिढ़ाते रहे- बे बिचार की नेति कहाँ? जो कुछ आग-पानी रहा… वह तो बुझ गया…”