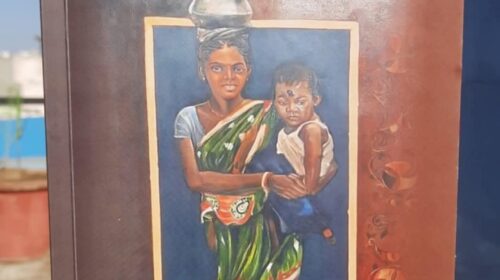रामायन राम
आज की हिंदी कविता जब अंतर्मुखी और होती जा रही है, जब कविता में खुल कर बोलना और वक्तव्य देना एक जोखिम भरा काम हो, तब प्रायः कवि आत्मकेंद्रित होकर ‘अपने निजी सच’ की प्रामाणिकता पर जोर दे रहे हैं।ऐसे में सपना चमड़िया की कविताएँअपने सहज रचनात्मक प्रतिरोध के साथ साफ़-साफ़ बात करती हैं।
सपना चमड़िया की कविताएँ
1. अनवर चाचा
चॉकलेट से भर देना चाहती हूं।
2. कश्मीर का लड़का
आज उसका सारा सामान
घर से चला गया
जैसे एक दिन वो छोड़कर
सफाचट मैंदान में मारा जायेगा।
3. गुजरात और इराक की माएँ
अभी दस दिन
रेलगाड़ी आती।
4. पैट्रोल पंप पर लड़की
नमस्ते शिल्पा
कैसी हो तुम ?
कहो शिल्पा कैसी हो तुम ।
5. नया पाठ
अभी बहुत कुछ
सीखना है मुझे
सबसे पहले कि
विदा देते हाथों में
कैसे रखा जाता है दिल ।
मेरी पत्नी घर छोड़ देती है।
6. रहमत खान
तुमने मुझे डरा ही दिया
मन हुआ
थोड़ा किनारे ले जाकर
दरयाफ्त करूं
12. राजा का क्या करें ?
राजा ने कपड़े बनवाए
राजा था
अनगिनत कपड़े थे
फिर भी मन की
मौज ।
असंख्य भूमि पर
उसके लिए कपास उगा
और जितने दिन उगा कपास
उतने दिन रोक दी गई
फसल
गेहूं, चना, बाजरा और जवार
और जो कपास उगा
एक अचरज सबने देखा,
बिल्कुल सुफैद नहीं था फूल कपास,
फूल के भीतर पड़ी थी
कुछ नीली खडी धारियाँ उदास।
मैं नहीं रच रहीं कोई
मिथक, प्रतीक
उपमा या उत्प्रेक्षा अलंकार
यह नहीं था कोई प्रयोग
या कोई अनुसंधान
मत रहना किसी सुख-सपने
में मुब्लिता दोस्त
मेरे यार
यह सिर्फ था मेरे –तुम्हारे
लिए एक सीधा पैगाम ।
भले ही बनारस के बुनकरों
में मच गया हाहाकार
पर तय हो गया कि
अब से जो कपास उगेगा
उस पर चस्पां होगा
राजा का नाम ।
और क्योंकि कुछ
स्वाभिमानी प्रजाति
बची हई थी
इस महाद्दीप में
जो किसी का नाम
नहीं ओढ़ती
उसे इस कपास
के विरोध में
उतारनी पड़ी अपनी
झीनी चदरिया ।
किसान मर रहे थे
स्त्रियाँ जूझ रही थी
इतिहासकार दफनाए जा रहे
सत्यों को
दीवानगी में अपने
पंजों और नाखूनों
से ही खोदने लगा था।
पर सब बेआवाज, बेअसर
सिर्फ राजा था, उसका फरमना था
उसकी खेती, उसका कपास
उसका कपड़ा, उसकी घरती
उसका ही आकाश था।
जो काटा जा रहा था
जो बुना जा रहा था
जो उकेरा जा रहा था
सब उसका था
उसके लिए था ।
राजा का कपड़ा सिला
कुल नीला-काला
पर यह रंग
यह काला खूबसूरत
आदिवासी का नहीं था
सुंदर काली स्त्री का
नहीं था
कोयला खदान से
निकले मजदूर का नहीं था
किसान का नहीं था
लोहार का नहीं था
रैदास का नहीं था
रोमानी रात का
नहीं था
बालों का नहीं था
काली आरतीय ऑखों का
तो बिल्कुल नहीं था।
यह काला था
जमे हुए खून का
अकड़ी हुई लाश का
फैक्ट्री से निकलते कचरे का
नदियों में घुलते जहर का
इस देश से बिदा होती
सुंदर चीजों की आह का ।
फिर भी राजा ने कपड़े बनवाए
इतना ही नहीं
उस पर
तलवार, भाला और त्रिशूल
जैसे
खड़ी धारियों वाले मोटिफ*
टंकवायें।
हम खौफजदा थे
फिर भी हम सबने
मिलकर वहीं पुराने
गीत दोहराए
जो परम्परा में हमें
मिला था
कि कोई तो आए
मजदूर, किसान
स्त्रियाँ, नौजवान
उलगूलान, तेलंगाना, नक्सलधाम
चौरी-चौरा, सन सतावन
कश्मीर,पंजाब
पहलगाम
खुदी राम बोस
या अश्फाक उल्ला खान
और भी जुड़े इसमें
कई कई नाम ।
और सब एक साथ
उठायें आलाप
मिल कर लें
तान
और कहें
राजा गन्दा है
राजा नंगा है
राजा गन्दा है
राजा नंगा है।
*मोटिफ: डिजाईन
13. सलाम, सलाम, सलाम
बिना धूप की परवाह किए
और सांवली होती हुई
विरोध में निकलने वाली
लड़कियों को सलाम ।
सुदर्शन नहीं दिखने वाले
ज़िम नहीं जाने वाले
लड़कों को सलाम।
भूख से सिकुड़ती
आँतों को सलाम
गिरते स्वास्थ्य
चमकती आँखों
को सलाम ।
इंकलाबो इंकलाब
वाले नारे को सलाम
और उन नारों पर उभरती
गले की हर एक रग को सलाम
गले से दुपट्टा फेंकने वाले
हाथों को सलाम
और बदऩजर की तरफ
उठी हुई हर तर्जनी को सलाम ।
सभा में बोले हर झूठ के
पर्दाफाश को सलाम
और सवाल पूछती हुई
हर खुली चिट्ठी को सलाम।
आधी रात को गंगा ढाबे पर
चाय पीती मेरी बेटी
की आजादी को सलाम
और लड़की को सिर्फ लड़की
की तरह देखने की
सनातनी आदत से छुटकारे
को सलाम
गुलमोहर को सलाम
और भविष्य को ताक पर
रख देने वाले
हौसलों को सलाम ।
बस्तर को बचाने की
फ्रिक को सलाम
और ना झुकने वाली
इस जवां अकड़ को सलाम ।
हिन्दू-मुस्लिम कार्ड पर
पड़ने वाले हर तमाचे
को सलाम
और सबके लिए रोटी
मांगने वाली जिद
को सलाम।
हक की बात करने
वाली हिम्मत को सलाम
इन हवाओं को सलाम
इन फिज़ाओं को सलाम
और आजादी चौक के
इन बेखौफ रातों दिन को सलाम ।
भूख की हर ऐंठन
और आँसू के हर कतरे
का हिसाब मांगने वाली
इस पढ़ाई को सलाम ।
ये सलाम सलामत रहे
ऐसी दुआ मांगने वाली हर जबां
हर इंसान को सलाम ।
पहली पंक्ति में दिखने वालों
से अंतिम पंक्ति तक की
बुलंद आवाजों को सलाम ।
14. जन-गण मन
मुझे मत मारो साहेब
कभी स्कूल गई नहीं
सच है साहेब
कि कोई नहीं गया
हमारे घर से पढ़ने-लिखने
फिर कहां सीखती
जन-गण मन
थोड़ी मोहलत दो साहेब
अगली बार आओगे
तो सीख रखूगीं
ठेकेदार से पूछूगीं
जिसने काम पर रखा,
बताया नहीं था बदमाश ने
बस इतना पूछा था
भारी तगाड़ी उठा कर
कितने माले चढ़ जाएगी
छुट्टी तो नहीं करेगी ?
सौ रूपए मिलेंगे रोज़
सौ रूपए रोज़ के साथ
कोई पर्ची नहीं पकड़ाई
जन-गण मन वाली
गांव में ?
नहीं साहेब वहां भी
रात के अँधेरे में
दखिन टोला आने वालों
में से किसी ने भी
नहीं गवाया हमसे
जन-गण-मन
सच कहते हैं साहेब
सौ रूपया रोज़
आटा, दाल, चावल,चप्पल,
तेल, लकड़ी, नमक,
हारी-बीमारी
एक बीड़ी में चार लोग
यही थोड़ी सी दुनियादारी
जाहिल हैं साहेब
माफ़ कीजिये
हम तो इसी को
जन गण मन
समझ लिए
ठेकेदार, पुलिस, मकान-मालिक
हरामज़ादी, कुतिया, साली
हमको लगा
यही हमारा देश है
यही हमारा राग
यही पेट की आग
मेरे बेटे को मत कुचलिये
बेटी को उठा मत ले जाइये
मेरे पेट से तलवार
हटाइये
मत मारिये साहेब
हम तो तब पैदा हुए थे
जब जंगल में नदियां
गाती थीं
झरने गाते थे
काले, हरे पहाड़
नाचते थे
मांदल की थाप पर
बादल के राग पर
फिर जब आप
ये सब लेने आये थे
दुःख के बादल छाये थे
तब भी हम लड़े थे
तीर से, कमान से
अपनी सुगठित
काली भुजाओं से
सौगंध खा कर
कहते हैं साहेब
तब भी हम ये नहीं गाये थे
आप आये अपना गीत गाये
पर हम तो इससे पहले से दुनिया में हैं।
मत मरिए साहेब
लाशें नहीं गाती हैं।
जी साहेब
मोबाइल है
उसमें गाना भर दीजिये
जी साहेब
आप जब भी
मिस कॉल देंगे
हम सब काम छोड़ के
जी साहेब तगाड़ी पटक देंगे
दूध पिलाते बच्चे को
झटक देंगे
रात के अँधेरे में
ठेकेदार को हटाकर
जी साहेब उसी हालत में
जी साहेब जैसे भी हो
जी सही उच्चारण से
नहीं साहब कपड़े
बाद में पहनेंगे
जी सीधे खड़े होकर
थरथराते हुए, रोते हुए, भूखे पेट
निर्वस्त्र हम
आपका गीत पहले गाएंगे।
15. औरत और फुरसत
फुरसत मेरी जान
कभी आना मेरे पास
बरसों से हम
तुम्हारी राह
देखा किए
कितनी इल्तजाएं भिजवाईं
बाबा, भईया
धर्म और सत्ता
सतयुग, द्वापर और त्रेता
हर युग में,
हर भाषा में।
कभी तो चुराया
भी तुम्हें पानी लाते
अनाज पीसते
पर हसरत
ही रही
कि
हम दोनों गलबहियां डालें,
डोले
नगरी-नगरी द्वारे-द्वारे
लांघे समुद्र के पाट
नाप आए पर्वत की ऊंचाई
और उतरे कभी
गहरी नदी के घाट
पर तुम
बेमुरव्वत
फुरसत मेरी जान
मरदाने में ही
अपना बिस्तरा लगाएं रहीं
पर काफिया और रदीफ
तो मिलता था
मेरा और तुम्हारा
औरत और फुरसत
और मैं ही रही
और मैं ही रही
तुम्हारी जन्मदायिनी भी
कि मैंने खाना पकाया
कपड़ा सुखाया
घर चमकाया
ठंड में आग सुलगाई
और
गरमी में पंखा डुलाया
कंधों पर ढोया
रिश्ते, मर्यादा
और साधे रही
खाने में नमक
ना कम, ना ज्यादा
फिर घर और
नौकरी के बीच
चक्कर घिन्नी
बनी रही
तब भी तुम रूठी रही
मैंने तुम्हारा पीछा किया
तुम निकल गईं
किसी बड़ी गाड़ी में
या
कैफे कॉफी डे में
मुझे देख मुंह फेर लिया
दूर और महंगी होती
तुम मेरे सपनों में
आती रहीं।
मैं तुम्हें फिर-फिर
रही पुकारती
फुरसत मेरी जान
आओ मेरे पास
मुझे गले से लगा लो
मेरा मुंह चूम लो
मेरी पेशानी के बल
समतल करो
मेरा जूड़ा ज़रा ढीला करो
मेरे सिर के नीचे
रखो हाथ
बेमतलब की कुछ
करो बात,
मुझे नींद आ जाए
सदियों की चाह भर जाए
सपना सच हो जाए
कि तुम यहीं रह जाओ
मेरे पास, मेरे साथ
फुरसत मेरी जान,
फुरसत मेरी जान।
16. भाषा
मैं भाषा की पहली इकाई हूँ.
कि मैंने
एक नन्हीं सी जान को
ध्वानियां पहुँचाई है.
ठंडे और गरम की
तासीर समझाई है
रिश्तों की उष्मा से
पहचान कराई है.
सुबह की ‘उठो मेरा जान’
से रात के
चन्दा मामा,आरे आवा, पारे आवा,
तक के समय की राह बनाई है।
मैंने ही जुदा-जुदा आटे के कण जोड़कर
रोटियाँ पकाई है।
सब्जी में बघार लगाई है.
वक्त पड़े पर
दरांत भी चलाई है.
सदियों पहले यह सवाल भी उठाया
कि भईया को दियो बाबुल
महला-दुमहला
और हमको दियो परदेस
कि मैंने अपनी भाषा में सांस ली है
कि मैंने उसी में प्यार किया है
उसी में रोई हूँ.
और उसी में चहकी भी हूं.
कि माँ के पेट से उसे समझा
सीखा और बरतना शुरू किया है.
मैंने उससे बहुत लिया
और बहुत कम दिया है।
लेकिन जो कुछ किया.
जैसा भी जिया
सब अपनी भाषा में किया
कि उसे मैंने ज़मीन पर रोपा
आकाश में उड़ाया
पलकों पे उतारा
दिल लगाया
माथे पर चढ़ाया
रूमाल पे काढ़ा
कि हथियार बनाया
सब अपनी भाषा में किया.
हम दोनों सहोदरा हैं।
सुख में, दुख में,
मान में, अपमान में,
एक दूसरे का हाथ थामे हुए
इसी हक से
और ज़रूरत से
और बड़े ही दुख से
उसका एक संदेशा
पढ़कर सुनाती हूँ
जो उसने भेजा है
आपके लिए
कि मैं लानत भेजती हूँ
उनपर
जिन्होंने मुझे शुद्धता के
पिंजरे में कैद रखा.
मैं नदी थी
मेरी चंचलता को
जिसने चरित्र से जोड़ा
उसे लानत भेजती हूँ.
जिसने मुझमें लिखा
नारी नरक का द्वार
और बनाई तमाम
माँ बहन की गालियां
उसे भी भरपूर लानत भेजती हूँ।
लानत भेजती हूँ उसे भी
जो अनैतिकता के कीचड़ में धसाँ
मुझमें नैतिकता में श्लोक रच
रहा था।
और उसे भी
जिसने मुझे बहुत सजा-संवार कर
मेरा बार-बार प्रदर्शन किया.
मेरा इस्तेमाल किया.
उसे तो और भी ज्यादा लानत भेजती हूँ।
जिसने मुझसे चापलूसी करवाई
और सौ बार ‘हुज़ूर’ कहलवाया
जिसने मुझसे स्वार्थ साधा
लानत उसे भी
और उसे हजार लानत
जिसने मेरी रीढ़ री हड्डी तोड़ कर झुका दी.
लेकिन मैं मरी नहीं
मैंने खुद को बदल दिया
खूब घूमी मैं
नदी-नाले झरने-पर्वत-
हाट-बाजार
घर-बाहर
स्वप्न लिए
इच्छा किए
ज़रूरत बनी
सभा की, कविता की
प्यार की, आक्रोश की
ज्ञान की, विज्ञान की
और सबसे ज्यादा तो
पली-बढ़ी सड़कों पर
हवा में मुट्ठी ताने
भरे गले से बोलती
मेरे साथ चलो
मुझे प्यार करो
मुझे रचो
मुझमें बसो
कि मैं सबूत हूँ
तुम्हारे जिन्दा होने का
और जिन्दा हो
तो मुझ में
नज़र आओ।