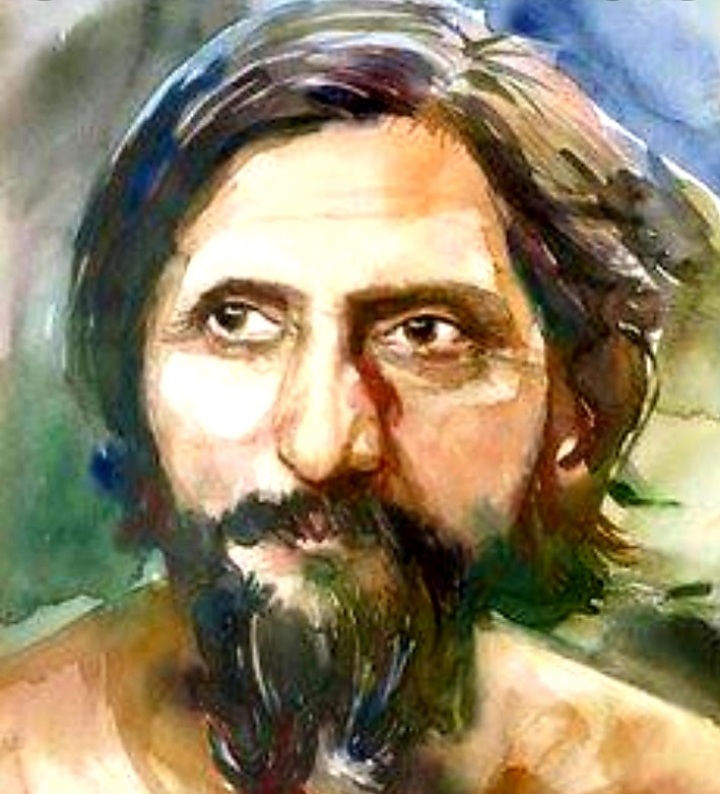तूलिका
तीर्थ यात्राओं के महात्म्य से शायद ही कोई धर्म अछूता रहा हो। अगर तीर्थ यात्रा के इर्द गिर्द की बतकही या किवदंतियों से अंदाजा लगाएँ तो इसके मुताबिक, ये यात्रा बुढ़ापा कही जाने वाली उम्र के अधिक मुफीद मानी जाती है; उम्र का वो पड़ाव जब इंसान अपनी अंतिम यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहा होता है।
ये यात्रायें भी शायद इसी तैयारी का हिस्सा मानी जाती रही होंगी। इस यात्रा की मुश्किलें इंसान को अंतिम यात्रा की मुश्किलों की तैयारी का एहसास कराती।
चूंकि अधिकाँश तीर्थ ऐसी जगहों पर होते जहां तक पहुँचने का कोई स्थाई और सुगम रास्ता नहीं होता था तो ये यात्राएं अपने भौतिक अर्थ में अंतिम यात्राओं जैसी ही पीड़ादायक मानी जातीं; फिर वह चाहे मक्का-मदीना हो या बदरीनाथ-केदारनाथ।
पर समय बदला, देश बदला, राज-काज बदला तो इन धार्मिक कही जाने वाली यात्राओं का रंग-रूप भी हर लिहाज से काफी बदल गया। खैर इसके पीछे की राजनीति और समाजशास्त्र का विवेचन तो इस क्षेत्र के विद्वान लोग ही कर सकते हैं। फिलहाल बीते सावन की कांवड़ यात्रा के आँखों देखे कुछ दृश्य:-
दृश्य-1 एक बड़ा ट्रक, बड़ा, मतलब जिसे सचमुच बड़ा कहा जाए। इसके पीछे एक किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम। जाहिर है जुलाई के महीने की दिल्ली की चिपचिपी गर्मी में राजधानी की पुरानी सड़क पर अगर ट्रैफिक जाम होगा तो इस ट्रैफिक में फंसे लोगों का ब्लड प्रेशर बढेगा और उनके भीतर-बाहर का युद्ध सरीखा शोर भी, यह सामान्य तर्कबुद्धि कहती है।
पर आश्चर्य कि आस-पास कहीं से ट्रैफिक आगे बढाने के लिए दिल्ली की सामान्य गालियों की फुहार कहीं नहीं आ रही थी, दूर-दूर तक मुझे कोई खीझता नहीं दिखा। खैर, खरामा खरामा मेरी सवारी इधर-उधर झूलती हुई उस ट्रक के पीछे तक पहुंची। मैं दायें बाएँ से जाने कितनी देर से उचक उचक कर उस ट्रक को देखने की कोशिश कर रही थी। पर वहाँ पहुँचने पर जो नज़ारा दिखा वो मेरे संवेदना या कहें मेरे आग्रहों/पूर्वाग्रहों को डिगाने वाला था।
भयानक शोर करते सराउंड साउंड वाले उस ट्रक पर लगे 5-5 फीट ऊंचे स्पीकरों के बीच में सिर झुकाए तीन-चार बच्चे बैठे थे। सब के सब बिलकुल चुप, थके, निस्तेज, उमंगहीन।
उम्र 10, 12 या अधिक से अधिक 14 बरस की। इसी हालत के, मानो अपने बचपन को कब के अलविदा कह चुके 3-4 बालक उस रेंगते से ट्रक के पीछे चल रहे थे, हाथों में 5-7 लीटर का प्लास्टिक का पानी का कैन लिए ।
सब के सब मरियल दुखी प्रेतात्माओं से। दिमाग और प्रत्यक्ष अनुभव के बीच तनाव इतना बढ़ा कि उस पल नहीं सूझा कि अब खीझूँ, रोऊँ या गुस्साऊं।
दृश्य-2 एक और ट्रक, शहर की किसी और सड़क पर। यह सड़क चौड़ी है, चिकनी है, चार पहियों से कम के वाहनों को तो कानूनन ही इस सड़क पर चलने की इजाजत नहीं है।
जाहिर है कि यह शहर ही नहीं बल्कि देश के ख़ास लोगों की ख़ास सड़क है, जिसके इर्द-गिर्द देश का राज-काज चलाने वाले खास ‘कार्यालय’ हैं।
यह ट्रक पिछली ट्रक से ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। वाहनों की मेरी बेहद सीमित जानकारी के मुताबिक शायद अपनी सजावट, उस पर लगे साउंड सिस्टम और उस पर सवार मनुष्यों के कारण।
इस ट्रक के सवारों को अगर उम्र के मुताबिक श्रेणीबद्ध करना हो तो इन्हें युवा की श्रेणी में रखा जाएगा; 18 से 25-30 के बीच। आँखों पर काला चश्मा, मुंह में गांजे की मशाल सी जलती लम्बी सिगरेट और हाथ में डंडे और किन्हीं किन्हीं के हाथों में झंडेलगे डंडे।
साउंड सिस्टम की बीट पर हाथ और शरीर हिलाते, तरह तरह की आवाजें निकालते, कई बार आतों-जातों को चिढ़ाते से दिखते, अपनी मौजूदगी को विजय स्वरूप दर्ज कराते।
इन दोनों दृश्यों में जो प्राथमिक तौर पर दिखा, वह था- हिंसा, ताकत, बदला, आज़ादी (ताकत के बल पर हासिल आज़ादी) साथ ही उतनी ही गहरी लाचारगी, असहायता और कुछ अंश में भय और ईर्ष्या भी।
न, यहाँ संस्कृति के पतन और गरीब युवाओं के युवापन को भ्रष्ट करने जैसे मध्यवर्गीय विलाप को जगह देना ऊपर के अनुभवों के साथ ईमानदारी नहीं होगी।
क्यूंकि ऐसा करते ही सहज सवाल होगा कि किसकी संस्कृति के पतन का मातम मनाया जाए? इन दृश्यों के इस सड़क पर आते ही हमारे भीतर की संस्कृति की अवधारणा के वे कौन से पन्ने हैं जो फड़फड़ाने लगते हैं?
अगर वह सबकी मजबूत सामूहिक संकृति थी, तो फिर ये जो ट्रकों पर थे उन्हें उस ‘महान’ संस्कृति को छोड़ने की जरूरत क्यूँ आन पड़ी?
ऐसा क्या था जो उनका अपना न था, जो उन्हें हासिल न था? हम कौन हैं जो पतन या उत्थान की घोषणा करते हैं; उनकी संस्कृति, सीमा आदि तय कर रहे हैं?
संस्कृति की हमारी अथॉरिटी और उनका इसे ध्वस्त करते हुए अपनी जगह को इस तरह से रीक्लेम करने की कोशिश को क्या कहेंगे?
क्या वे महज किसी राजनीति का शिकार हैं, जिन्हें अपने होने का अंदाज़ा नहीं? क्या वे महज जाल में फंसाए गए लोग हैं?
हजारों सवाल मुंह बाए खड़े हैं, परत दर परत खोलेंगे तो मामला शहर-गाँव, ऊंची-नीची जाति के द्वंद्व से होते हुए अमीर-गरीब तक पहुंचेगा!
अनगिनत सवालों की ही तरह अनगिनत भाव हैं और उन भावों पर फिर से उठते अनगिनत सवाल हैं। जैसे पहले दृश्य में उन स्पीकरों की आवाज़ों से उठी खीझ या उनके प्रति बेखयाली दोनों ही भाव क्या दिखाते हैं? इन दोनों भावों के केंद्र में कौन है?
जाहिर है यह खीझ मध्यवर्ग की है और बेख्याली के चोले में इस दृश्य को ही नज़रअंदाज करने की कोशिश करने वाले भी इसी तबके के थे।
तो क्या अब समय आ गया है कि मध्य वर्ग का बड़ा तबका इस बेख्याली वाली जमात में शामिल होना चाहता है? (इस सवाल का जवाब एक बार फिर समाजशास्त्र के अध्ययन में लगे लोगों के हवाले।)
मध्य वर्ग हालांकि अपने आप में कोई सार्वभौम कैटेगरी नहीं है पर फिर भी मोटे तौर पर इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि, वह वर्ग जो इतना कमाता है कि उसका आज का काम तो आराम से चले साथ ही बुढ़ापे का भी कामचलाऊ इंतज़ाम हो जाए।
क्या इस इंतज़ाम में दिक्कत के बावजूद भी वो ‘नज़र-अंदाज’ करने की रणनीति अपनाएगा? यह सही है कि हमारे देश के मध्य वर्ग की पहचान महज आर्थिक नहीं है, बल्कि उसकी धार्मिक, जातीय, लैंगिक स्थिति भी उसके व्यवहार को तय करती है पर वो मध्य वर्ग ही इसलिए है क्यूंकि उसकी आय उसे इस वर्ग का बनाती है।
इसके अलावा यह वही वर्ग है जो आज भी बाज़ार का केंद्र है। लग्जरी उपभोक्ता सामानों से लेकर इंश्योरेंस, टूरिज़म तक जितने सर्विस सेक्टर आपके जेहन में आ सकते हैं वे सब इसी के इर्द-गिर्द, इसी के भरोसे आकार लेते हैं। खरीद, उपयोग और उपभोग की समस्त category तक के केंद्र में यही तबका है।
उसकी भावनाएं भी उसकी आर्थिक/सामजिक स्थिति, सहूलियत और भविष्य में उसके जीवन पर असर से निर्धारित होती हैं। यहाँ भावनाओं में संवेदना भी जोड़ देना बेहतर होगा। जैसे वो खुद को इण्डिविजुअल मानता है और उसके इस मानने का नतीजा है कि वह अक्सर अकेला होता है; काम, परिवार, समाज; हर जगह।
इसी नाते शायद उसका आत्म बेहद डेलिकेट ईगो के रूप में विकसित होता है। इतना कि वो काफी तेजी से बनता, तनता और टूटता है।
शायद इन्हीं बनने, बिगड़ने, तनने और टूटने में से किसी का नतीजा था कि पहले दृश्य में उन बच्चों को देखकर मेरा आत्म चटख गया।
शायद यह आत्म इन आवाज़ों और इनके पीछे के तमाम विचारों को सुनते-गुनते (अपने अनुभव और कुछ पूर्वाग्रहों के कारण) इन्हें ‘मानवीय’ होने से एक डिग्री नीचे होने का मान चुका था पर पास पहुँच कर जब उन बच्चों की हालत को देखकर या कहें उनकी हालत से इस मध्यवर्गीय मन पर जो छवि बनी वो इन आवाजों की पूर्व छवि से बिलकुल मेल नहीं खाती थी।
यह दृश्य द्रवित करने वाला था तो उनके प्रति नफरत और हिकारत के बजाय सहानुभूति का भाव पैदा हो गया और ‘कोमल मध्यवर्गीय’ आत्म संभाल न पाया और दो बूंद बनकर आँखों से टपक पड़ा।
इसी तरह दूसरे दृश्य में जो पूर्व कल्पना थी, हकीकत उससे काफी अलग निकली। मन में बसी सभ्य और सभ्यता की छवियों से कोसों दूर यह दृश्य ताकतवर और डरावना निकला।
‘कोमल आत्म’ ने तो खुद को इस दृश्य से नफरत करने के लिए तैयार किया था पर जब दृश्य सामने आया तो हिंसा की तस्वीर थी और अब मन के भीतर एक किस्म का डर और अपमान भी जाग गया।
इस तरह से वही ‘कोमल मध्यवर्गीय आत्म’ यहाँ भी आहात हो गया। ताकत और हिंसा प्रदर्शन के वे दृश्य आँखों के सामने फिल्म बनकर लगातार चलते रहे, गुजरते रहे और यह आत्म राहत की तलाश में प्रतिक्रिया स्वरूप अपने जैसे चुनिन्दा औरों के बीच अपने पक्ष में जनमत बनाने में जुट गया।
इन दोनों दृश्यों को मिलाकर और खुद को थोड़ा इससे दूर रखकर देखें तो शायद तस्वीर थोड़ी और साफ़ हो। ‘सड़क सबकी है, ट्रैफिक में सब हैं, तो इसकी तकलीफ और फ़ायदों में सब बराबर के भागी हैं’।
ऐसा माना जाता है या माना जाना चाहिए। पर शायद ऐसा नहीं है। ट्रैफिक रोकी जाती है ताकि एक दूसरे समूह को पार करने का बराबर का रास्ता दिया जा सके पर हमेशा ऐसा नहीं होता है।
ट्रैफिक रोकी जाती है ताकि कुछ खास गाड़ियों को आगे जाने का रास्ता दिया जा सके। अम्ब्युलेंस के लिए ‘करुणा’ के नाते हमारा मन तैयार होता है।
लाल बत्तियों की सरकारी गाड़ियों के लिए जब ट्रैफिक रुकती है तो डर, स्वामिभक्ति, राजभक्ति, देशभक्ति जो कहें, के तर्क से मन संभल जाता है। जीवन-मृत्यु या राजतंत्र के मामले में मध्यवर्ग की आमतौर पर एक राय होती है पर धार्मिक जुलूसों में उसकी इंसान और नागरिक की पहचान के साथ-साथ धार्मिक पहचान भी जुड़ जाती है।
यहीं आधुनिक समाज का समूचा तर्क भ्रम और संदेह के घेरे में आ जाता है और मध्यवर्ग की आधारभूत संकल्पना में कश्म्कश शुरू हो जाती है. हमारे देश में इस अंतर्विरोध को पाटने की आधिकारिक जुगत अभी ट्रायल अवस्था में ही है।
दोनों ही दृश्यों में मौजूद चेहरों के भाव शायद महज बेचारगी या महज ताकत से लबरेज हिंस्र नहीं थे। कई बार दोनों थे, कई बार उनमें और कुछ भी शामिल था. शामिल थी- यात्रा- नई जगह जाने, देखने, उसमें होने का रोमांच, अनजानी चीजों से टकराने, अपना आत्म बल पुख्ता करने और इससे अपने होने के एहसास दिलाने का नितांत रोमांच।
शायद वो आदिम इच्छा जिसका तमाम ट्रैवेल कंपनियाँ या फिर स्पोर्ट्स सामानों और एनर्जी और सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियाँ आजकल वायदा कर रही हैं; ‘जंगल-पहाड़, डर, रोमांच सब अपने तरीके से तय करने महसूसने की आज़ादी’।
लेकिन यहाँ जिस बात की चर्चा अपेक्षित और जरुरी है वह है आज की इन धार्मिक कही जाने वाली यात्राओं से बनती ताकत और सड़कों पर धार्मिक जुलूसों की शक्ल में चलती इन लाखों इंसानी कायायों के मन मस्तिष्क में होती हलचलों और नतीजतन तेजी से बदलती सम्पूर्ण सामाजिक तस्वीर की। राजनीतिक कालक्रम से हासिल तथ्य बताते हैं कि ये यात्रा किसी सहज विकसित धार्मिक भाव का नतीजा नहीं है।
इसके पीछे के धार्मिक मन में छेड़छाड़ की गई है या साफ़-साफ़ कहें सत्ता द्वारा खिलवाड़ किया गया है। युवापन के सहज उत्साह और ‘जीत लेने’ की मूल खेल भावना को भी एक खास दिशा दी गई है, दी जा रही है।
पूंजी ने इस स्वाभाविक इच्छा को कुछ सीमित हाथों में समेटा इससे इंकार नहीं किया जा सकता है और फिर इस चालाक कोशिश के तहत इसे ताकतवर सत्ता की राजनीति ने अपने पक्ष में इस्तेमाल किया।
धार्मिकता और धार्मिक होने के भी नए मानक गढ़े गए। जहां नियमों में ढील पूर्व विधानों की तरह हेय नहीं मानी जाती, बिलकुल राष्ट्रभक्ति की तरह।
जैसे राष्ट्रभक्ति की परिभाषा इनके प्रतीकों के सार्वजनिक इस्तेमाल तक सिमट चुकी है. अगर आप आकार में बड़ा झण्डा फहराते हो, जोर-जोर से ‘भारत माता की जय’ बोलते हो या चिल्ला-चिल्ला कर पड़ोसी देश मुर्दाबाद के नारे लगाते हो तो आपको समस्त श्रेणियों के मानव और देश द्रोह के बावजूद देश भक्ति का सर्टिफिकेट आसानी से मिल सकता है।
ठीक उसी तरह अगर आप जय श्रीराम बोलते हो, काँवड़ यात्रा पर जाते हो या फिर काँवड़ यात्रियो की सेवा टहल ही कर देते हैं तो आप तमाम अनैतिक कृत्यों के बावजूद धार्मिक हिन्दू की पावन श्रेणी में आ जाएंगे. वैसे उपरोक्त दोनों श्रेणी एक दूसरे के स्थान पर भी प्रयोग में लाई जा सकती है।
यात्रा करने की मानव की आदिम प्रवृत्ति और धार्मिकता के साथ उसके जुड़ाव की इस नई तस्वीर को कैसे देखें? अब तक उदार कहां जाने वाला खेमा यह उम्मीद करता मालूम पड़ता है कि ‘ताकत के इस भ्रम का भुलावा ज्यादा देर नहीं चलेगा, और इसका नुकसान इसकी डोर थामने वाली सुप्रीम ताकतों को होगा।
जिन्हें राजधानी की सड़क के बीच में चिल्लाने का हक इस यात्रा के दौरान हासिल हुआ है उनकी महत्वाकांक्षा यहाँ से आगे भी बढ़ेगी जिसके लिए वर्चस्वशाली ताकतें कत्तई रास्ता नहीं दे सकतीं और इस तरह हताश हो हमारे ये भटके साथी अपने स्वाभाविक खेमे में आ मिलेगे’।
पर यह उम्मीद तो प्राकृतिक न्याय जैसी चीज में विश्वास करने जैसा है। जबकि जो प्राकृतिक (natural) है वह हमेशा न्यायोचित होगा ऐसा बिलकुल जरूरी नहीं होता।
‘धार्मिक होना’ और ‘यात्रा प्रवर उत्साही’ होना दोनों ही लंबे समय से सांस्कृतिक प्रैक्टिस का हिस्सा रहने के कारण एक तरह से इंसानी व्यवहार का हिस्सा हो गया है।
अपनी विकास प्रक्रिया में हर इंसान के भीतर दोनों के कुछ कुछ अंश आम तौर पर होते हैं। अगर तर्कबुद्धि से देखें तो इन्हें एक दूसरे का विरोधी भी कहा जा सकता है।
युवा उत्साही दिमाग नई चीजों के प्रति उत्सुकता से भरा होता है और साथ ही इस खोजी प्रवृत्ति से उसमें अनगिनत जलते सवालों का सैलाब उमड़ता रहता है।
जबकि धार्मिकता आम तौर पर इन सवालों से ‘हार’, उसके सामने ‘असहाय की स्थिति’ में पैदा होने वाला भाव है।
जहां इंसान अजानी ताकत के सामने अपनी परेशानियों से थक कर नतमस्तक हो जाता है। शायद इसलिए भी ऐसा है कि तीर्थ यात्राएं बुढ़ापे के दिनों की चीज मानी जाती रही हैं।
युवा तो जब घर से भागता है तो आजादी की इच्छा से भागता है न कि किसी ताकत का गुलाम बनने की इच्छा से।
इस लिहाज से युवा उत्साही कांवड़ियों के ये जत्थे अपने आप में हैरतअंगेज हकीकत हैं। हालांकि इसे अस्वाभाविक मानना स्वाभाविकपन की सीमित समझ होगी क्यूंकि अस्वाभाविक दिखने वाली घटनाओं के सिरे निश्चित रूप से बेहद सहजता से हमारी आँखों के सामने होते हैं. हमारे ही जंजाल हमारी नज़र को धुंधला देते है।
युवा कांवड़िए निकले तो उसी आदिम आज़ादी की ताकत को महसूसने थे। धार्मिकता का हथियार तो उन्हें रास्ते में थमा दिया गया, इस हथियार का असर है कि धार्मिक यात्रा से जीवन त्याग की तैयारी की भावना गायब हुई और युवापन से अजाने को जानने का उत्साह निकल गया।
इन दोनों में जो बचा वह युवावस्था की ठोस बायोलाजिकल अवस्थिति और धार्मिक जुलूसों में शामिल होने से हासिल सामाजिक बरतरी। उम्र और धार्मिकता दोनों की खोल में खतरनाक राजनीति को साधने के वाहक बने ये गरीब युवा और कभी रीझते, कभी अफनाते मूक साक्षी बने, हम!
(फीचर्ड इमेज गूगल से साभार)