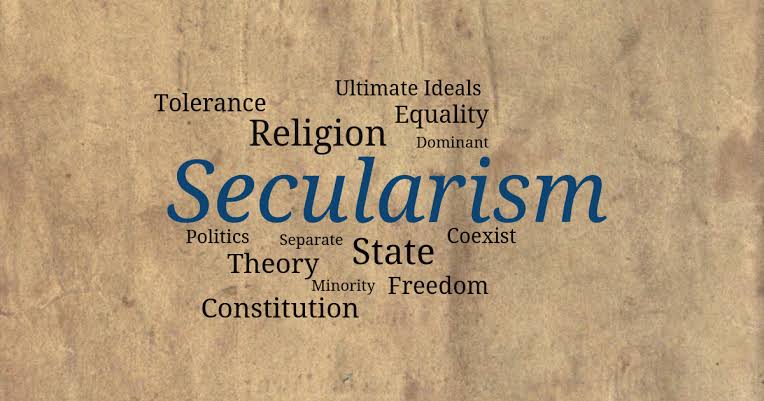कुछ समय हुआ मुझे ज़ी फाइव ओटीटी प्लेटफार्म पर पाकिस्तानी सीरीज़ ‘धूप की दीवार’ देखे हुए और इस सीरीज़ के हर एपिसोड के साथ ज़हन में कई सारी बातें आईं, जिन्हें मैं लिखना तो चाहती थी पर इस सीरीज़ ने उन सारी बातों को एक साथ जोड़कर कहने का मौका दे दिया।
कोई भी सीरीज़ देखने से पहले मैं आदतन उसकी समीक्षा पढ़ लिया करती हूँ , हालाँकि मैं देखती तो हूँ ही जो भी मुझे देखना होता है, रिव्यु से बस अपनी चॉइस के बारे में थोड़ा जान लेती हूँ। पाकिस्तानी धारावाहिकों के हिन्दुस्तान में अच्छे खासे फैन हैं और मैं यह बात अपने अनुभव से कह रही हूँ कि हाँ यह बात है ! सचमुच उनकी कहानियों में वो बात है जो आपको बाँध लेती है। जहाँ हमारे टीवी सीरिअल्स अर्से पहले ही अपना औचित्य खो चुके हैं, वहाँ पकिस्तान में काफी ऐसे सीरिअल्स बने जिनमें अच्छी कहानियाँ, अच्छी अदाकारी, अच्छी भाषा से लेकर अच्छा म्यूजिक सब कुछ मिलता है, कहने का आशय यह कि एक सम्पूर्ण मनोरंजन का एहसास है उनमें। बावजूद इन सबके फिर ऐसा क्या रहा, जिसके कारण ‘धूप की दीवार’ को वो सफलता नहीं मिली जो शायद उसे मिलनी चाहिए थी।
‘धूप की दीवार’ उमेरा अहमद की लिखी हुई सीरीज़ है। इससे पहले उमेरा का ही लिखा सीरियल ‘ज़िन्दगी गुलज़ार है’, हिन्दुस्तान में बेहद पसंद किया जा चुका है। उमेरा की लिखी किताबों पर और भी सीरिअल्स बन चुके हैं और दर्शकों द्वारा बराबर पसंद भी किये गए हैं। इस बार उमेरा एक ऐसी कहानी लेकर आती हैं, जिसका एक हिस्सा हिंदुस्तान में चल रहा है और दूसरा पकिस्तान में। ये कहानी हिन्दुस्तान में बारहवी में पढ़ रहे विशाल मल्होत्रा और पाकिस्तान में ठीक उसी उम्र और कक्षा में पढ़ रही सारा शेरअली की है। विशाल के पिता विजय और सारा के पिता शेरअली दोनों ही आर्मी में हैं, दोनों ही अपने अपने वतन की हिफाज़त करते शहीद होते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में अपने-अपने पिता की शहादत को लेकर सारा और विशाल में एक जंग छिड़ती है, जिसका लुत्फ़ दोनों ही देशों की जनता और मीडिया बराबर से उठाती दिखती है। पर कुछ ही समय में विशाल और सारा दोनों को ही ज़िन्दगी लोगों के वो चेहरे दिखाना शुरू कर देती है, जिनकी दोनों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
इस सब के बीच विशाल और सारा को इंटरनेट पर लड़ते-झगड़ते ये एहसास होता है कि दोनों ही एक गम के मारे हुए हैं। दोनों के अन्दर उठ रहे सारे सवाल बीच की सरहद के बावजूद बिलकुल एक जैसे हैं, सारी परेशानियां भी एक जैसी ही नज़र आने लगती हैं। पहले तो दोनों के परिवारों को दुश्मन से बात करना गवारा नहीं होता पर धीमे-धीमे दोनों परिवार के सदस्य आपस में घुलने लगते हैं। उन सभी के बीच सिर्फ एक रिश्ता है और वह है दर्द का रिश्ता। अपने दर्द साझा करने के लिए अपना पूरा देश होने के बाद भी दोनों परिवारों को लगता है कि उन दोनों के लिए सिर्फ वे खुद हैं और कोई भी नहीं।
कहानी आगे बढ़ती जाती है और ऐसी बहुत-सी भावनाओं को कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है जो किसी मुल्क, किसी आवाम, किसी मज़हब विशेष की नहीं बल्कि वे मानवीय हैं, सिर्फ और सिर्फ मानवीय।
आज भी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है और मज़हब के नाम पर तो रोज़ ही अब एक नयी जंग छिड़ती नज़र आती है। पर ये सब कोई नयी बात नहीं। अगर हम चाहें तो बीती शताब्दी को ही पलट कर देख लें। जंग और जंग के तबाही से किताबें, अखबार में अटे पड़े मिलेंगे। पर उन्हें कौन पढता है, सारी जानकारी तो सोशल मीडिया से ही मिलनी है। इस बीच हम शायद भूल जाते हैं कि वह एक वर्चुअल दुनिया है, उसमें बहुत कुछ मुमकिन है जो असल दुनिया में नहीं है और असल दुनिया के दर्द का वर्चुअल दुनिया में हल नहीं खोजा जा सकता। उसके लिए अनुभव ज़रूरी हैं। कोशिश करनी होगी कि हमारे सारे दर्द और उनसे निकलने की सारी कोशिशें कहीं वर्चुअल ही न हो जायें क्योंकि जी तो हम सब असल में आज भी एक मुकम्मल दुनिया में रहे हैं पर हमारे मन, दिमाग किसी वर्चुअल दुनिया के कैदी हो चुके हैं ।
जंग और जंग की तबाही की याद में दुनिया भर में जाने कितने स्मारक हैं, वो सेल्फी और सोशल मीडिया पर डालने वाली फोटो खीचने के लिए तो नहीं बनाये गए थे। उनका कुछ उद्देश्य था, पर जाने क्यों वो सब निरर्थक लगने लगता है जब मैं जंग की खबरें पढ़ती हूँ । क्या हमने दो विश्वयुद्धों से कुछ भी सीख नहीं ली ? क्या हमने हिन्दुस्तान-पकिस्तान के विभाजन से कोई सीख नहीं ली ? कैसे भूल सकते हैं कि हम करोड़ों जान का जाना ? क्या त्रासदियाँ सिर्फ हमें चंद साल जगाये रख सकती हैं? या यूँ कहा जाये की हमें जगे रहने के लिए त्रासदियों की ज़रूरत है ?
मौत जो सूनापन लाती है, उसके बारे में उन परिवारों से बेहतर कौन जान सकता है, जिन्होंने बेवक्त अपने प्रियजनों की मौतें देखीं हों, जैसे किसी भी देश की सेना के परिवार। कहीं हमें इतनी मौतों की आदत तो नहीं हो गयी है ? एक शब्द है कैजुअल्टी, किसी भी जंग में सरकारें और मीडिया इसका काफी इस्तेमाल करती है और मुझे इस शब्द से एक चिढ है एक नफरत है जो मैं धूप की दीवार देखते-देखते समझ पाई। इस शब्द का मतलब कुछ लोगों की मौत से जुड़ा है और फिर भी इसमें एक कैज़ुअल साउंड है। कम से कम इस नयी शताब्दी में इसे इतना कैज़ुअल न लिया जाता तो मैं कह पाती की हाँ हमारे ज़हन सोशल मीडिया वाली वाल्स की तरह क्षणिक नहीं हैं !
अंग्रेजी न्यूज़ साइट्स पर फिर भी इस सीरीज़ की ठीक-ठाक रिव्यु हैं पर हिंदी न्यूज़ साइट्स पर तो मुझे ढूंढने पर भी सिर्फ एक रिव्यु मिला और वह काफी बुरा था। एक बात जो उसमें लिखी गयी थी और जिससे मुझे असहमति वह है की यह वही घिसी-पिटी इंडिया-पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी है। इंडिया –पकिस्तान के बंटवारे की कहानी आज हमारे लिए घिसी -पिटी हो गयी है ? मुझे याद है कि बर्लिन के बीचों-बीच बना होलोकॉस्ट का वो स्मारक, जो इतना बड़ा है कि कभी लोग उस घटना और उसमें मरने वालों को भूल से भी भूल न पाएं और हम एक उत्तर भारतीय होकर क्या हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का विभाजन अभी से भूल चुके हैं ? हमें तो हर वक़्त में ऐसी दास्तानों की ज़रूरत है जिससे भूल कर भी हम हिन्दू-मुस्लिम दंगों की तबाही भूल न पाएं। बॉर्डर की हिफाज़त के नाम पर सालों साल इंसानों की बलि चढ़ती हैं। तो क्या हम उन्हें अपनी आदत में शामिल करते जायें ? जितने बंटवारे होते जायेंगे, जितनी सरहदें बनती जाएँगी, उनकी हिफाजत पर उतनी बलियां चढ़ती जाएँगी। क्या हम इस राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं ?
मुझे ‘धूप की दीवार’ एक सीरीज़ के तौर पर जो सन्देश देना चाहती थी, वह मोटा-मोटा कहा जाये तो यही समझ आता है। हमारे अपने देश के लोगों के बीच में अंतर तो बहुत हैं पर जोर अंतर पर न देकर अगर समानता पर दें तो शायद हम एक समाज के तौर पर विकसित होने की दिशा में बेहतर कर पाएंगे।