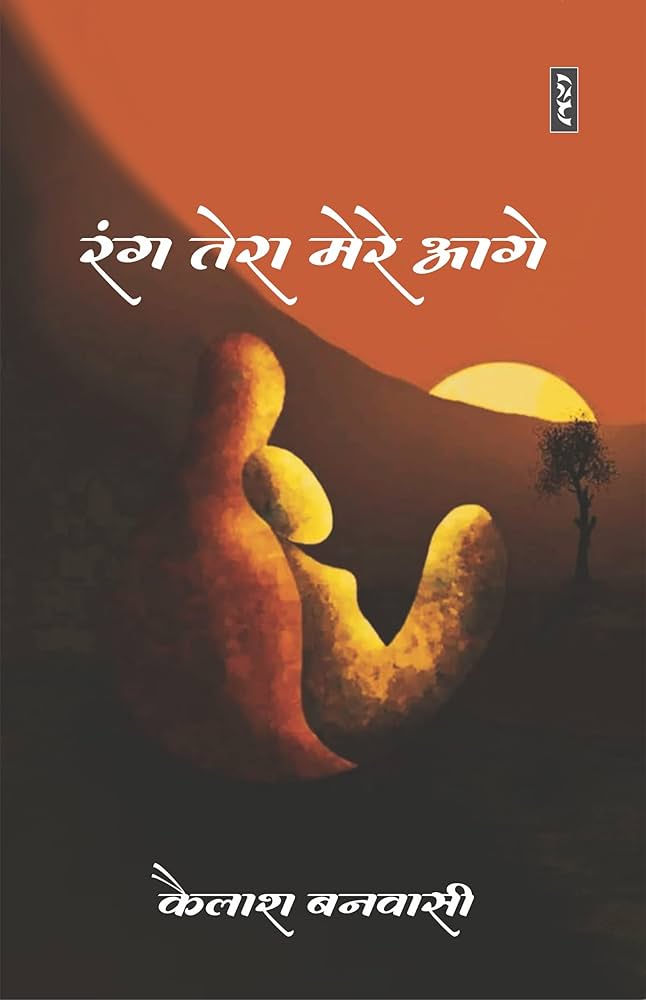आलोक कुमार श्रीवास्तव
उपन्यास, साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसमें समय-समय पर नये-नये प्रयोग होते रहते हैं और इन प्रयोगों की विशेषताओं के आधार पर उपन्यासों का वर्गीकरण भी होता रहता है।
विद्यार्थियों के लिए ये वर्गीकरण बहुत काम के होते हैं क्योंकि इनसे न केवल विधा के विकास की दिशा पता चलती है बल्कि संबंधित कृति के आलोचनात्मक अध्ययन में भी सुविधा होती है।
कभी-कभी हमारे सामने ऐसी कृतियाँ भी आ जाती हैं जिन्हें पूर्व-प्रचलित वर्गों में रखना न्यायसंगत नहीं लगता। वर्ष 2022 में सेतु प्रकाशन से प्रकाशित कैलाश बनवासी का उपन्यास ‘रंग तेरा मेरे आगे’ भी हमारे सामने ऐसी ही चुनौती पेश करता है।
यह न तो प्रेमकथा है, न ही केवल मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणपरक कृति। यह जीवन के यथार्थ के बीच में से ही पैदा हुई जटिलताओं की इकहरी रूमानी कथा है जिसका संतुलन बगैर सामाजिक परिवर्तन हुए नहीं सध सकता। यह बीजगणित का ऐसा सवाल है जिसका समीकरण समाज को ही बैठाना है।
भारतीय समाज में स्त्री-पुरुष संबंध को लेकर जो समझ और प्रचलित रूढ़ियाँ हैं, उनके चलते सहज-स्वाभाविक संबंध की अपेक्षा रखने वाले लोगों का जीवन सहज नहीं रहने पाता। फिर इस सहजता-स्वाभाविकता के रास्ते में शरीर की मनो-रासायनिक स्थितियाँ बाधा बनकर खड़ी होती हैं और यही बाधाएं विचारशील व्यक्तियों को ख़ासे ससोपंज में डाल देती हैं।
कैलाश बनवासी के उपन्यास ‘रंग तेरा मेरे आगे’ का कथानायक सुनील कुमार भी एक विचारशील व्यक्ति है – प्रगतिशील विचारों का कहानीकार और अध्यापक।
संयोगवश, उसे कुछ समय के लिए ऐसे प्रशिक्षु अध्यापकों को पढ़ाने का अवसर मिलता है जिन्होंने पत्राचार माध्यम से डी.एड. कोर्स किया है और उन्हें नियमित किए जाने के लिए पंद्रह दिनों का एक अल्पकालीन प्रशिक्षण देकर परीक्षा में शामिल कराया जाना है। उसी दरम्यान उसके जीवन में नसीम नामक एक प्रशिक्षु अध्यापिका का प्रवेश होता है, जिसके प्रति सुनील आकर्षित होने से लेकर आसक्त तक हो जाता है। इस घटना को देखने के कम से कम दो सीधे दृष्टिकोण उपन्यास में मौजूद हैं
– एक दृष्टिकोण सुनील का है और दूसरा नसीम का। सुनील वाला दृष्टिकोण प्रचलित सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से नहीं है और नसीम वाला है।
वस्तुत: इन दोनों दृष्टिकोणों का द्वंद्व ही उपन्यास का प्रस्थान-बिंदु है। एक तीसरा लोकोपवादी दृष्टिकोण भी है जो ऐसे मामलों में तमाशबीनों का रहता ही है, हालांकि वह दृष्टिकोण भी समाज में स्त्री-पुरुष संबंध को लेकर मौजूद वैचारिक द्वंद्व को ही अभिव्यक्त करता है।
प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा में लड़कियों के साथ से वंचित लड़कों के जीवन में एक ऐसा अभाव होता है, जिसकी कमी विवाह करके एक पत्नी के माध्यम से नहीं पूरी की जा सकती। अपरिचित स्त्री-पुरुष के दूसरे लोगों द्वारा तय किये गये विवाह का संबंध जैविक और सामाजिक स्तर पर तो बन जाता है लेकिन मानसिक स्तर पर इस संबंध में बहुत बड़ा गैप होता है।
पत्नी अगर पति का सम्मान करती है तो उसके पीछे एक संबंधगत मजबूरी होती है, पति भी पत्नी की इच्छा-अनिच्छा की परवाह अगर करता है तो वह भी एक संतुलन साधने की मजबूरी में ही।
प्रेम के कारण परस्पर जो सम्मान, इच्छा-अनिच्छा की जो परवाह होती है, उसकी स्वाभाविकता और वैवाहिक संबंध के कारण उत्पन्न इन्हीं चीज़ों की मजबूरी के फ़र्क को सब महसूस करते हैं। कहते नहीं। एक सामाजिक दबाव के चलते अभिव्यक्त नहीं करते। एक खोखले तने को सींचते हुए पूरा जीवन बिता देते हैं। अपने मन की बात न पति कभी पत्नी से कह पाता है, न पत्नी कभी पति से कह पाती है।
दूसरी तरफ, प्रेम की शुरुआत ही एक दूसरे से अपने मन की बात कहने से होती है। दो व्यक्तियों के बीच जो दोस्ताना बनता है, उसका आधार अभिव्यक्ति की साझेदारी ही तो होती है।
इस उपन्यास के नायक सुनील के माध्यम से कथाकार ने दोस्ती के संबंध को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। प्रशिक्षु अध्यापकों की कक्षा में सुनील आपसी संबंधों पर अपनी राय रखते हुए कहता है –
…मुझे लगता है, सबसे बड़ा और अच्छा संबंध वो होता है जिसे हम अपनी मर्ज़ी से चुनते हैं… और वो है दोस्ती का। … सम्बंधों में बड़ी चीज़ जो होनी चाहिए – अपनी आज़ादी, अपनी बात कह सकने की आज़ादी। (रंग तेरा मेरे आगे, पृ.55)
दूसरी तरफ, विवाह संस्था की आड़ में पितृसत्ता स्त्रियों की आज़ादी के ख़िलाफ खड़ी मिलती है। शायद यही कारण है कि पितृसत्ता को अपनी बात कह सकने की आजादी की जमीन पर बनी दोस्ती और उस दोस्ती के आँगन में खिला प्रेम का फूल बहुत अखरता है।
इस उपन्यास के एक प्रौढ़-परिपक्व पात्र अवधेश जी के माध्यम से कथाकार ने इस बिंदु पर भी अपना विचार रख दिया है –
विवाह नाम की संस्था ही जैसे मनुष्य की स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ है। पुरुषों के आधिपत्य और स्त्रियों को ग़ुलाम बनाकर रखने के दीर्घकालीन षड्यंत्र का नाम है पितृसत्ता। दूसरे, कई तरह की नैतिकताओं, रीति-रिवाजों के बोझ से उनके अस्तित्व के मूल प्रश्न – स्वतंत्रता, बराबरी का अधिकार – को इस क़दर कुचल डाला गया है, कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे अपना जीवन दूसरों के बनाये क़ायदे-क़ानून के लिए जी रही हैं ! अपनी कोई इच्छा या स्वतंत्रता है – इसे भूले रहने का ही पारिवारिक या नैतिक दबाव उन पर होता है। यही नहीं, यह व्यवस्था इस संस्था की आड़ में तमाम तरह के जड़ मूल्यों को बनाकर रखती है – जात-पात या ऊँच-नीच वाले मूल्य। प्रेम ही है जो इसका विरोध करता है। (रंग तेरा मेरे आगे, पृ. 290)
ऊपर दिये गये उपन्यास के दोनों उद्धरणों को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ऊपर से आपसी संबंधों का मामला दिख ज़रूर रहा है लेकिन संदर्भ के कारण यह मामला स्त्री-पुरुष संबंध पर चर्चा का है।
ध्यातव्य है कि सुनील की कक्षा के ज्यादातर प्रशिक्षु अध्यापक माँ के रिश्ते को सबसे अच्छा बताते हैं।
बहरहाल, उपन्यास के उपर्युक्त दो उद्धरणों के बारे में कहना यह है कि स्त्री-पुरुष संबंध के मामले में लेखक ने दो अलग-अलग जगहों पर क्रमश: दोस्ती और प्रेम को आदर्श आधार के तौर पर रखा है।
इसे सरल करके इस तरह समझना आसान होगा कि अगर स्त्री और पुरुष के बीच संबंध की शुरुआत दोस्ती से हो और दोस्ती का यह संबंध प्रेम के रसायन से पुष्ट हो तो इस प्रकार का संबंध एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा।
मेरी समझ में लेखक की सफलता यही है कि उसने एक बेहद जटिल दिखते संबंध में इस बात को सरलता से रख दिया है, अब आगे की जिम्मेदारी पाठक की है कि वह इसे समझे, स्वीकार करे और समाज में आगे बढ़ाए। अब दोस्ती से आगे बढ़े हुए ‘प्रेम’ पर उपन्यासकार का नज़रिया देखें। अवधेश जी ही कहते हैं –
प्रेम को उसके वास्तविक ज़मीन में देखना चाहिए… देखा जाए तो यह बड़ी क्रांति है…किसी ने कहा भी है न, कि जो प्रेम नहीं कर सकता, वह क्रांति भी नहीं कर सकता! यह सिर्फ देह से या दो जनों से जुड़ा मामला नहीं है, पूरे समाज से जुड़ा मामला है। इस रिश्ते में दुनिया भर के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या नैतिक आयाम शामिल हैं… प्रेम इन सबके बीच ही होता है, इनसे कटकर नहीं। और जो लोग इसे समाज से कटा हुआ, बिल्कुल अपना निजी मामला मानते हैं, मुझे शक है उनके प्रेम पर…। (रंग तेरा मेरे आगे, पृष्ठ 291)
अवधेश जी के मार्फत उपन्यासकार का यह नज़रिया प्रेम को जीवन के व्यापक और सम्पूर्ण संदर्भों में देखने का हिमायती है जहाँ जीवन के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नैतिक पक्ष भी उसमें शामिल हों।
इस तरह निजता के नाम पर प्रेम को गोपनीय मामला बना देने के पितृसत्तात्मक षड्यंत्र की लेखक ने अच्छी पहचान की है। प्रेम यदि सम्पूर्णता में न हो और उसे गोपनीय माना जाए तो वह या तो पाखंड होगा या सिर्फ वासना की उत्तेजना, उसे प्रेम कहना इस उदात्त भाव के साथ अन्याय ही होगा।
उपन्यास में सब कुछ जानते-समझते हुए भी सुनील का बार-बार नसीम से मिलने, बात करने का प्रयास, अपनी पत्नी वर्षा से इस प्रसंग की खुलकर चर्चा, अपने और नसीम के संबंध पर समाज (अध्यापकों, नसीम के सहकर्मियों, परिवार के सदस्यों आदि) से कुछ न छिपाने का साहस प्रेम को लेकर लेखक की इस वैचारिक धारणा की दृढ़ता का प्रमाण है।
इस प्रकार, ‘रंग तेरा मेरे आगे’ हमारे सामने स्त्री-पुरुष संबंध पर विमर्श का एक और आयाम रखता है। यह हमें स्त्री-पुरुष संबंध के मसले को एक नये कोण से देखने का अवसर देता है।
इस उपन्यास के केंद्रीय पात्र सुनील के व्यक्तित्व को बहुत ध्यान और संवेदनशीलता से देखे जाने की ज़रूरत है क्योंकि ख़ुद सुनील एक बहुत संवेदनशील इंसान है और उसके जैसे लोग अब दुनिया में बहुत कम संख्या में मिलते हैं जो मानते हैं कि व्यक्ति सिर्फ़ किसी रूटीन में ढल गया मशीन भर नहीं है।
राहत की बात यह है कि उसकी पत्नी वर्षा ने इस विषम परिस्थिति के समय में उसे पूरी संवेदनशीलता के साथ संभाला है।
इसी के साथ आप सुनील की पत्नी वर्षा के किरदार और सुनील के साथ उसके व्यवहार की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। स्वयं सुनील यह स्वीकार करता है कि वर्षा ने उसे वे सुविधाएं मुहैया करायीं जिनके अभाव में उसका यह (विवाहेतर-रूमानी!) प्रेम मुमकिन न होता।
यहाँ सोचने की एक बात यह भी है वैवाहिक-पारिवारिक जीवन में स्त्री-पुरुष संबंध की जैसी लोकतांत्रिक मिसाल वर्षा ने पेश की है, क्या सुनील वैसी मिसाल पेश करता, अगर वर्षा का ऐसा ही कोई विवाहेतर प्रेम संबंध विकसित होता?
बहरहाल, हम चर्चा सुनील के व्यक्तित्व को संवेदनशीलता से देखने की कर रहे थे, इस काम के लिए पाठक को अलग से कोई प्रयास नहीं करना होगा क्योंकि लेखक ने ही सुनील के किरदार के भीतर की रूहानियत-रूमानियत, संवेदनशीलता, सामाजिक सरोकार को कभी मशहूर शायरों की प्रासंगिक पंक्तियों के माध्यम से तो कभी महान लेखकों की अन्य रचनाओं के उल्लेख के माध्यम से प्रदर्शित किया है। ग़ालिब, जिगर, फ़ैज़, साहिर, निदा फाजली, सबा अफ़गानी, गुलज़ार आदि शायरों की ग़ज़लों के चुनिंदा अशआर उपन्यास के शिल्प को एक अलहदा मिजाज़ प्रदान करते हैं। उपन्यास का शीर्षक ही ग़ालिब के एक शे’र का अंश है, पूरा शे’र इस तरह है –
मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे
तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे
पूरे उपन्यास में सुनील की यही कोशिश रही है कि नसीम इस शे’र में कही गयी बात को समझे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इस सिलसिले में नसीम पक्के तौर पर वहां तक पहुँची है, जहां तक सुनील पहुँचा है।
इसकी वाजिब वजह भी उपन्यास में मौजूद है। सबसे पहले तो ये कि अगर नसीम वहां तक पहुँच जाए तो उपन्यास की रूह ही नहीं रहेगी
– नसीम के वहाँ तक न पहुँचने में ही सुनील की बेचैनी है, और उस बेचैनी की अभिव्यक्ति ही लेखक का उद्देश्य है। जैसा कि उपन्यास में उद्धृत निदा फाजली के इस शे’र में कहा भी गया है –
वो सितारा है चमकने दो यूँ ही आँखों में
क्या ज़रूरी है उसे जिस्म बनाकर देखो
सुनील बस नसीम का मित्रवत साहचर्य चाहता है, ये वह ज़रूरत है जो उसके अब तक के जीवन का सबसे बड़ा अभाव रही है। इस संबंध के कारण अपने मन की कशमकश और गहरे उधेड़बुन के बीच वह सोचता है –
चाह इतनी ही है कि बस उसका साथ बना रहे – किसी सच्चे दोस्त की तरह… गहरा अंतरंग… रागात्मक…भावनात्मक… वह जो एक दूसरी ही दुनिया बन जाती है – इस दुनिया के बरअक्स… इस संसार का प्रति संसार… (रंग तेरा मेरे आगे, पृष्ठ 275)
दूसरी बात ये कि सुनील और नसीम के बीच जेंडर, धर्म और वैवाहिक स्थिति का फ़र्क उनकी अनुभूतियों, उनके व्यवहार और कार्यकलापों में फ़र्क का बड़ा कारण है। स्त्री और पुरुष का अंतर, हिंदू और मुसलमान का अंतर, विवाहित और अविवाहित का अंतर… हमारे समाज के शायद ये तीन बड़े भेद हैं।
इसलिए हो सकता है कि कोई अविवाहित लड़की अपने विवाहित आशिक के दिल का हाल जान भी ले, प्रेम में अपनी स्थिति का भी उसे ज्ञान हो जाए, इसके बावजूद उसकी अभिव्यक्ति ऐसी न हो कि आशिक को इसका पता चल सके। जेंडर वाले भेद पर स्वयं कथाकार ने लिखा भी है –
एक लड़की अपने ‘लड़की’ होने को जितना समझती है, उतना एक पुरुष कभी नहीं। (रंग तेरा मेरे आगे, पृष्ठ 21) और लड़कियाँ अपने देखने को बहुत बेहतर जानती हैं। दरअसल उन्हें जैसे हमारे परिवेश ने ही इसका तगड़ा अभ्यास करा दिया है जहाँ लोग उन्हें अपने ‘पुरुष’ भाव से देखते हैं…। (रंग तेरा मेरे आगे, पृष्ठ 20)
सुनील के नसीम से लगाव का एक तार मुन्नी की याद से भी जुड़ा है और इस बात को समझने के लिए आपको उपन्यास के अड़तालीसवें परिच्छेद में जाना होगा जहाँ तीन-चार साल की नन्हीं-सी पठानिन टुरी (मुसलमान लड़की) मुन्नी है और दो-ढाई साल का शिशु सुनील, अटकन मटकन के खेल में हल्का धक्का देकर लुढ़काई जाती मुन्नी को केवल खेल में ही नहीं, ज़िंदगी में भी लुढ़का दिया गया है।
एक मुसलमान लड़की मुन्नी की मृत्यु शायद सुनील की स्मृति में जमी बैठी है, उसके साहचर्य की साध कहीं अवचेतन में दबी है और नसीम को पाकर वह साध उभर आयी है।
कैलाश बनवासी ने उपन्यास का परिवेश अपने आसपास से ही उठाया है, कहानी और वर्णन भी बिना अनुभव के इस तरह का नहीं हो सकता था, जैसा कि है।
लेखक के यही वे उपकरण हैं जिनका बेहतरीन इस्तेमाल इस उपन्यास में सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करने के लिए किया गया है। शिक्षा विभाग के उद्देश्यहीन, मूल्यहीन और भ्रष्ट हो जाने को हमारा समाज चुपचाप देखता रहा है।
यह देखना सुखद है कि उपन्यास का नायक सुनील बतौर शिक्षक यह मानता और इस बात पर अमल करता है कि पढ़ाने के लिए सिर्फ़ विषय का ज्ञान ही काफ़ी नहीं है, उसके सरोकार या उद्देश्य सबसे बढ़कर हैं।
इस सिलसिले में लेखक ने रूसी शिक्षक और शिक्षाशास्त्री वसीली सुखोम्लीन्सकी के विचारों को सुनील के अध्यापकीय मिशन में शामिल किया है। सुनील ने वसीली सुखोम्लीन्सकी के इस महत्वपूर्ण कथन को ख़ास तौर पर आत्मसात किया है कि सारे शिक्षा और चरित्र निर्माण का एक सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि मनुष्य को सौंदर्य जगत में रहना सिखाया जाए, कि वह सौंदर्य के बिना जी न सके, कि संसार का सौंदर्य स्वयं उसमें सौंदर्य का सृजन करे…। सौंदर्य का बोध होगा तो संसार में जो बहुत कुछ बदसूरत है, उसके बीच भी रहना मुमकिन होगा। लेखक ने एक जगह कहा भी है
– एक तरलता इस कठोर संसार के बीच आपको बचाकर रखती है, जितना उससे हो सकता है उतना। कि बगैर रोमान के जीवन कितना सूखा लगेगा। चूसकर फेंक दी गयी गुठली की तरह अनुपयोगी, बेकार…। (रंग तेरा मेरे आगे, पृष्ठ 25-26)
यह रोमान केवल स्त्री-पुरुष के बीच के आकर्षण तक ही सीमित नहीं है, यह रोमान व्यक्ति के अपने कामकाज से भी जुड़ता है, तभी व्यक्ति को अपना कामकाज अर्थपूर्ण लगता है और तभी व्यक्ति अपने जीवन की सार्थकता को महसूस कर पाता है।
अपने कामकाज में इस सार्थकता की खोज हर ईमानदार और संवेदनशील इंसान करता है। शिक्षा-व्यवस्था को लेकर सुनील की चिंता का कारण भी इसी सार्थकता; और अपने कामकाज के बीच जीवन के रोमान की खोज है। उपन्यास के छठे परिच्छेद में लेखक ने प्रसंगवश स्कूली शिक्षा व्यवस्था के यथार्थ और विद्यालयों में कक्षा-शिक्षण की हकीकत का करीब से देखा ब्योरा प्रस्तुत किया है। आज स्कूलों-कॉलेजों के अध्यापकों के जीवन की सच्चाई यही है कि शिक्षक बनने के लिए जो मूलभूत चरित्र और प्रवृत्ति चाहिए, वही यहाँ सिरे से नदारद है। शिक्षक की नौकरी इनके लिए, या ज्यादातर लोगों के लिए बस सरकारी नौकरी है, जिसमें इस व्यवस्था की सारी खराबियाँ समाज से, व्यवस्था से अपने आप घुसी चली आती हैं। इसे रोक पाना बेहद कठिन है। क्योंकि नीति-निर्माता और प्रशासन तंत्र उन आर्थिक, नैतिक, सामाजिक पहलुओं पर उतना ज़ोर कभी नहीं देते जितना देना चाहिए। (रंग तेरा मेरे आगे, पृष्ठ 37)
सुनील हिंदी का शिक्षक है और प्रशिक्षु अध्यापकों को पढ़ा रहा है, इस कारण भाषा-विमर्श भी इस उपन्यास में सामाजिक यथार्थ के एक पहलू के रूप में जुड़ गया है। उपन्यास के सातवें परिच्छेद का यह उद्धरण हिंदीभाषी समाज की भाषा विषयक समझ पर एक टिप्पणी की तरह है –
वह पढ़ा रहा है हिंदी। आमतौर पर ऐसी भाषा जिसमें आजकल के बच्चों में पहले जैसी रुचि नहीं होती। अधिकांश के लिए हिंदी जैसे बच्चों का खेल है, जिसमें फेल होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ भी लिखकर आखिरकार पास तो हो ही जाएंगे। हिंदी को कोर्स में बराबर रखा गया है, लेकिन उसका महत्त्व दिन पर दिन कम होता जा रहा है। उसकी तुलना में अंग्रेजी का आकर्षण कई गुना बढ़ गया है। (रंग तेरा मेरे आगे, पृष्ठ 40)
इस तथ्य के सामने उन सरकारी दावों का क्या हाल पूछा जाए जो कह रहे हैं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी माध्यम से करायी जा रही है या नयी शिक्षा नीति मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था कर रही है।
हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इस उपन्यास में जो कथावस्तु रखी गयी है उसका काल उपन्यास के प्रकाशन (2022) से लगभग पंद्रह-बीस वर्ष पहले अर्थात् लगभग सन् 2000-05 का है, फिर भी हिंदी को लेकर क्या आज भी समाज की समझ में कोई परिवर्तन हुआ है? भाषा-विमर्श को उपन्यास में शामिल करने के लिए लेखक को विशेष धन्यवाद दिया जाना चाहिए।
अंत में पुस्तक की कुछ छोटी-मोटी कमियों की बात करना भी आवश्यक लगता है। लेखक ने उपन्यास के भीतर के ‘वह’ और ‘मैं’ को गड्डमड्ड कर दिया है। सुनील के लिए कभी ‘वह’ का प्रयोग किया गया है तो कभी ‘मैं’ का। प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष के प्रयोग में लेखक सचेत नहीं रहे हैं। अगर कहीं संबंधित पात्र की डायरी या स्वगत कथन वगैरह हो तब तो ठीक है लेकिन कथाकार के नैरेशन में यह चूक बार-बार नहीं होनी चाहिए थी।
इसी तरह कुछ जगहों पर प्रूफ की गलतियां भी हैं, जैसे कि पृष्ठ 92 पर ‘प्रतिगामी’ के बदले ‘प्रगतिगामी’ छप गया है। यह प्रूफ की एक बड़ी गलती है। अगले संस्करण में इन गलतियों को सुधार लिया जाना चाहिए।
| पुस्तक : रंग तेरा मेरे आगे (उपन्यास), लेखक : कैलाश बनवासी
प्रकाशक : सेतु प्रकाशन, नोएडा प्रथम संस्करण : 2022, मूल्य : ₹325 |