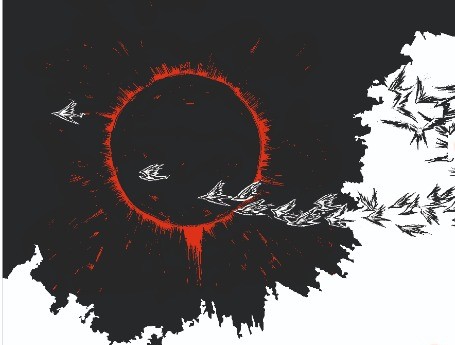समय एक प्रवाहमान धारा है फिर भी उसके अलग अलग खंड किये जाते हैं ताकि उसे पहचाना जा सके। इसके लिए उसकी विशेषता को लक्षित करना जरूरी हो जाता है। इस लिहाज से हमारे समय को विगत तीसेक साल से जारी प्रवृत्तियों का समय कहा जा सकता है। इस समय का निर्माण कुछ वैश्विक राजनीतिक बदलावों से हुआ। फिर उनके साथ ऐसे तकनीकी बदलाव भी जुड़ गये जिनकी लोकप्रियता को सामाजिक बदलावों के कारण स्थायित्व मिला। इतने सालों के बाद अब पूरी तरह से नयी दुनिया के आगमन और उसके स्थायित्व की अनुभूति होती है। वर्तमान हालात को बदलने के लिए उसे पहचानने और स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है इसलिए कोशिश इस समय को समझने के क्रम में उसकी चुनौतियों के साथ सम्भावनाओं को भी चिन्हित करने की होगी। बदलाव विछिन्न होने की जगह आपस में जुड़े हुए हैं और इसीलिए सम्भावना भी इसी किस्म की कल्पित की जा रही है।
इस मामले में सबसे पहली समस्या तो काल निर्धारण के साथ नामकरण की है। अपने वर्तमान को विगत तीस सालों की निरंतरता मानने के साथ हम इसे नवउदारवाद का समय कह सकते हैं। इसका एक सिरा आर्थिक बदलावों का है जिसकी शुरुआत थोड़ा पहले हो गयी थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जो समृद्धि नजर आयी थी उसके साथ अमेरिकी प्रभुत्व भी नाभिनालबद्ध था। इसकी अभिव्यक्ति न केवल जापान में परमाणु बम गिराकर की गयी बल्कि वैश्वीकरण के साथ जिन आर्थिक निकायों का नाम सुना गया उनकी स्थापना भी उसी समय हुई थी। स्थापना अमेरिकी धरती पर आयोजित सलाह से तो हुई ही इनमें प्रमुखता भी अमेरिका की ही थी।
अर्थशास्त्र के जनक ने संपदा को देशों के साथ जोड़कर देखा था लेकिन इन संस्थाओं का कुछ भी राष्ट्रीय नहीं था, सब कुछ वैश्विक था। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन में नाम में ही वैश्विकता थी, काम तो अमेरिकी था। इनका जो प्रमुख काम दिखायी पड़ा वह था- कर्ज देना । एकाधिक बार तो कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज दिया गया। ग्रीस और स्पेन के हालिया संकट के पहले ये कर्ज केवल गरीब देशों को दिये जाते थे। अमीर देशों के पास केवल ब्याज पहुंचता था। कर्ज की यह आर्थिकी पूंजीवाद के संकट को हल करने के लिए लायी गयी थी। देशों के भीतर कामगारों को मकान खरीदने के लिए पहले नियोक्ता संस्थाओं ने, फिर बैंकों ने जमकर कर्ज बांटे थे। इनसे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि मजदूरों के जुझारूपन में कमी आयी। कर्ज की किस्त चुकाने के लिए उनकी नियमित आय जरूरी हो गयी जिसमें हड़ताल से बाधा आ सकती थी। इस तरह पूंजीवाद की मशीन को चालू रखना मजदूरों की मजबूरी बनती गयी। विभिन्न देशों के भीतर मध्यवर्ग की मकान की आकांक्षा के जरिये इस व्यवस्था को जारी रखा गया और उनसे ब्याज वसूल कर संकट को टाला गया। इससे नियोक्ता को कार्यस्थल पर आवास मुहैया कराने की जिम्मेदारी से भी छुटकारा मिल गया। जो कामगार कभी साथ रहा करते थे वे अब बिखर गये ।
जो अनुभव राष्ट्रीय पैमाने पर मिला था उसको ही वैश्विक बनाते हुए कर्ज की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था खड़ी की गयी। इसमें कर्ज की वापसी की गारंटी के लिए देश को ही बंधक रखना पड़ा। कामगारों की तरह ही तीसरी दुनिया के गरीब देशों की प्रतिरोधक क्षमता मंद पड़ने लगी। नतीजे के बतौर उन्हें ब्याज की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी जाने लगी। सलाह वे अर्थशास्त्री देते जो बाजार में सरकारी दखल के विरोधी थे। वे सरकारों से नीति निर्माण की प्रक्रिया से कदम वापस खींचने की वकालत करने लगे। पूंजी को खुली छूट देने से ही भलाई होने की बातें समझाई जाने लगीं। जनता के पक्ष में काम करने वाली योजनाओं को व्यर्थ का खर्च बताया गया जिसे बंद कर देने से सरकार की आय बढ़ने की आशा की गयी। कल्याणकारी योजनाओं में कटौती को एकबारगी अपनाने की भी सलाह दी गयी ताकि विरोध न हो सके। यही समय था जब राज्य और सरकारी व्यवस्था को अक्षम बताने की मुहिम चल पड़ी।
इस प्रक्रिया को अर्थतंत्र का वित्तीकरण कहा गया और इसे पूंजी के लिए तो काफी लाभप्रद लेकिन जनता के लिए नुकसानदेह समझा गया। इसे उत्पादनविहीन मुनाफ़े का सबसे बड़ा स्रोत माना गया। उद्योग के लिए इसके नुकसान बहुत थे। उद्योग में पूंजी के निवेश का लाभ उत्पादित माल की बिक्री पर निर्भर होता है। इसके अतिरिक्त मजदूरों से जुड़ी बीसियों तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। औद्योगिक पूंजीवाद की इस जोखिम से मुक्त, ब्याज पर जीवित रहने वाली इस पूंजी के चलते किरायाजीवी या सूदखोर पूंजीवाद का उदय हुआ जिससे लाभ बहुत कम आबादी को मिलता था। इसने बड़े पैमाने पर तमाम किस्म की सामाजिक विषमताओं को जन्म दिया। इस विषमता ने समाज में स्थिर किस्म के विभाजन को जन्म दिया जिसके कारण संसाधनों पर कब्जा पीढ़ी दर पीढ़ी होने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। इसके कारण भी बहुतेरे लोग वर्तमान पूंजीवाद में उसी सामंतवाद की वापसी महसूस कर रहे हैं जिससे लड़ने और आजाद करने का दावा पूंजीवाद ने कभी किया था।
संस्कृति के क्षेत्र में इस नवसामंती लक्षण को अनेक रूपों में पहचाना जा सकता है। नवउदारवाद की शुरुआत से ही विज्ञापनों की दुनिया में शाही जिंदगी जीने का संदेश दिया जाता था। लम्बी सिगरेट को किंगसाइज कहा गया। आलीशान मकानों को बिक्री के लिए पेश किया जाने लगा। कीमतें भी सामाजिक विषमता के लिहाज से तय होने लगीं। तरणताल के साथ बहुमंजिला मकान बनाये जाने लगे। उत्पादित वस्तु की बिक्री से मुनाफ़ा साकार होने की मजबूरी से पूंजीवाद ने खुद को आजाद करना शुरू किया और उत्पाद को आम उपभोग की जगह खास अरबपतियों के लिहाज से ढाला जाने लगा।
आजकल हम सभी देखते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में आम की जगह खास का ध्यान रखा जाता है। इन सामानों और सुविधाओं की आकांक्षा को प्रचारित करने के लिए समूचे मीडियातंत्र को पूंजी की चाकरी में लगा दिया गया। इसका सबसे घातक उदाहरण क्रिकेट बना। उसकी लोकप्रियता को देखते हुए पूंजी ने उसका व्यवसायीकरण बड़े पैमाने पर नयी तर्ज पर किया। खिलाड़ियों की बिक्री बोली लगाकर होने लगी और इसके बेताज बादशाह ललित मोदी बने जिनके व्यक्तित्व में राजनीति, पूंजी और क्रिकेट के साथ (अरबपतियों के) भारत छोड़ो का समन्वय हो गया। आइ पी एल नामक इस श्रृंखला की टीमों के नाम देखिये और आपको अंदाजा हो जायेगा कि सामंती मूल्य किस तरह प्रचारित किये जा रहे थे। पनामा पेपर्स में नाम आने पर भी पूरी बेशर्मी के साथ विज्ञापनों की दुनिया में प्रछन्न राजनीतिक संदेश देने वाले अमिताभ बच्चन ने बिना वजह करोड़पति बनाने का व्यवसाय नहीं शुरू किया। सभी करोड़पति नहीं बन सकते थे इसलिए प्रतिदिन थोड़ा धन हासिल करने की प्रतियोगिता भी साथ ही चलती रहती थी। धर्म का धंधा बन जाना तो इसी नवाचार का सह उत्पाद है।
स्वाभाविक है कि प्रचंड सामाजिक विषमता से लोकतंत्र का क्षरण होना शुरू होता है। सामंतवाद के खात्मे के बाद से ही राजनीतिक सत्ता पर कब्जे को लेकर जनसाधारण और पूंजी के बीच लगातार टकराव रहा है। इस टकराव में जन दबाव ने हमेशा लोकतंत्र को नयी ऊर्जा दी है और उसके विपरीत जब कभी पूंजी की ताकत बढ़ी उसने लोकतंत्र की अवहेलना की है। लोकतंत्र के बारे में ऐसा समझा जाता है जैसे शासन हेतु प्रतिनिधि चुनना ही उसका सार हो लेकिन असल में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जनता का निर्णायक हस्तक्षेप उसका जीवन होता है। सबसे छोटे स्तर पर कारखाने के भीतर ट्रेड यूनियनों की मौजूदगी लोकतंत्र का ही जमीनी रूप थी। जब गरीब कामगार आम चुनाव में मतदान नहीं कर पाते थे तो नीति निर्णय की प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी इस संस्था के जरिये ही होती थी। आश्चर्य नहीं कि नवउदारवादी शासन के अमेरिकी और ब्रिटिश नेताओं (रीगन और थैचर) ने इन पर ही हमला करना सबसे जरूरी समझा। जमीनी स्तर पर एक लोकतांत्रिक संस्था के क्षरण ने धीरे धीरे ऊपर पर भी असर किया।
आज पूरी दुनिया में इस बात पर गम्भीर चिंता जाहिर की जा रही है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया लगभग समाप्त हो रही है। कानूनों के बनने या बदलने में जनता की राय का महत्व अधिकाधिक कम होता जा रहा है। कहने की जरूरत नहीं कि इस मामले में आम जनता के मुकाबले पूंजी की बढ़ती ताकत प्रत्यक्ष होती जा रही है। सारी दुनिया में वर्तमान शासकों के बरताव में जनता के हितों की निर्लज्ज उपेक्षा देखने के लिए किसी खुर्दबीन की जरूरत नहीं रह गयी है।
उनके हितों की ऐसी उपेक्षा के बावजूद नये समय के इन तानाशाहों की अद्भुत लोकप्रियता जनता में बनी हुई है। इस लोकप्रियता के निर्माण में वैश्वीकरण के अंतर्विरोधों ने उनकी भारी मदद की है। वैश्वीकरण में शुरू से जताया जा रहा था मानो पूरी दुनिया में किसी को भी किसी भी देश में जाने की अबाध छूट मिली हो। सीमाओं को लचीला बनाने की बात हो रही थी लेकिन जल्दी ही अंदाजा मिला कि आवाजाही की यह आजादी पूंजी को ही मिली हुई थी। दुनिया भर के सट्टा बाजार में बिना किसी रोकटोक के पूंजी निवेश होता था और सट्टा बाजार की तेजी को देश की समृद्धि के बतौर पेश किया जाता था। तभी से अर्थतंत्र की सेहत का प्रमुख मानक सेनसेक्स बना हुआ है। जब इस पूंजी को बिना किसी जोखिम के मुनाफ़ा मिलने में बाधा आती तो वह पलक झपकते ही गायब हो जाती है। अपने इस अति मशहूर चांचल्य से लक्ष्मी ने एक जमाने में बहुत सारे देशों में भारी तबाही मचायी थी। तमाम विकासशील देशों की मुद्रा का मूल्य पलक झपकते ही कौड़ी बराबर हो जाता था । बहरहाल पूंजी के मुक्त आवागमन के मुकाबले मनुष्यों के आवागमन पर उसी दौरान सख्ती तेज कर दी गयी थी । इस सख्ती के बावजूद विभिन्न देशों के बीच जो आवाजाही बनी उसने जिन देशों में प्रवासी श्रमिक गये उनमें तरह तरह की समस्याओं को जन्म दिया ।
कम मजदूरी देने के चक्कर में तमाम उद्योग गरीब देशों में स्थानांतरित किये गये। इसी तरह बेहतर मजदूरी के लोभ में गरीब देशों के मजदूरों ने वैध या अवैध तरीकों से अमीर देशों में जाना शुरू किया । इन दोनों प्रक्रियाओं ने खतरनाक राष्ट्रवादी उन्माद के लिए माहौल बनाया। अमीर और विकसित देशों की ओर कामगारों की जो आवक बढ़ी उसे नियंत्रित करने के लिए आव्रजन के नियमों में कड़ाई बरती जाने लगी। आम जनता में इस्लाम विरोध का उन्माद पैदा किया गया। इस तरह राष्ट्रवाद को नये ढांचे में ढाला गया जिसमें सांस्कृतिक बहिष्करण पर खासा जोर था। यूरोपीय देशों की कौन कहे, अमेरिका जैसे प्रवासियों के देश में भी यह विषाक्त हवा तेजी से बहने लगी। राष्ट्रवाद के इस नये रूप ने तानाशाह शासकों के लिए जन समर्थन जुटाने का जरूरी काम किया।
इतने विभाजनकारी समर्थन से भी काम नहीं चला तो नयी नीतियों के नुकसानदेह परिणामों से उत्पन्न विक्षोभ को काबू में करने के लिए सरकार को सख्त कानूनों से लैस करने की सिफारिश की गयी। एक ओर जनता के पक्ष में बने कानूनों को व्यापार के माहौल हेतु नुकसानदेह बेड़ी बताकर उन्हें ढीला किया गया तो दूसरी ओर सरकार के हाथ में कड़े कानूनों का डंडा पकड़ा दिया गया। इसने पूरी दुनिया में दमन की संस्थाओं और मशीनरी को अपार ताकत दे दी। शासन तंत्र ने जनता को काबू करने के इतने अधिक कारगर उपकरण इससे पहले शायद ही कभी पाये हों । हमारी आंखों के सामने हथियारों के मामले में पुलिस बल का सैन्यीकरण बड़े पैमाने पर हो रहा है। पूरी दुनिया ने अमेरिका में अश्वेतों के साथ हो रही पुलिसिया हिंसा के विरोध में फूटे हालिया जन आक्रोश के क्रम में जाना कि पुलिस नामक संस्था का जन्म ही सामुदायिक निगरानी के लिए हुआ था। मतलब कि जनता के ही धन से उसे शासकों की सेवा में लगाने और विरोध करने पर मुखबिरी और दंडित करने की इस व्यापक व्यवस्था का उदय हुआ था। शायद इसीलिए आंदोलनकारियों ने पुलिस नामक इस तंत्र को जनता के टैक्स का वह धन मुहैया कराने का विरोध किया जिसका सही उपयोग उसके विकास के लिए करना अपेक्षित होता है ।
दमन का जो नया तंत्र बना है पुलिस उसका बहुत छोटा ही अंग है। नागरिकों की निगरानी की जो विकराल व्यवस्था चतुर्दिक खड़ी की गयी है उसके निशान किसी भी शहर में चप्पे चप्पे पर नजर आते हैं । इसका पैमाना ही इतना भीषण है कि उसकी खोज खबर रखने में मनुष्य की अक्षमता के चलते कृत्रिम बुद्धि का सहारा लिया जा रहा है । मानव जीवन में नयी तकनीक के प्रवेश का यह क्षेत्र भी उत्तेजक बहस का विषय बना हुआ है ।
इस समूचे माहौल ने ऐसी शासकीय व्यवस्था को जन्म दिया है जिसको सही नाम से पुकारने में विद्वानों को अब भी संकोच हो रहा है। बहुतेरे लोग इसे पापुलिज्म नामक नयी कोटि से समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस शब्द का आगमन नवउदारवाद के समय ऐसी राजनीति को नकारात्मक तौर पर पहचानने के लिए किया जाता था जिसमें जनता को राहत देने के लिए कुछ योजनाओं का पक्ष लिया जाता था। तब इसे लोकलुभावनवाद कहा गया । अब भी इसके दक्षिण के साथ वाम स्वरूप की भी चर्चा होती है। जो लोग इस शब्द से परहेज करते हैं वे नये शासकों को सर्वसत्तावादी कह रहे हैं। लेकिन दबे सुर में ही सही, सौ साल पहले की यूरोपव्यापी राजनीतिक परिघटना का भी जिक्र शुरू हो गया है।
जो देश पिछली सदी में फ़ासीवाद का गढ़ रहे थे उनमें उनके घोषित वारिसों की राजनीतिक वापसी हो रही है। इस प्रवृत्ति की मौजूदगी बीसवीं सदी में केवल शासन के साथ ही नहीं जुड़ी रही है, जहां वे शासन में नहीं थे वहां भी फ़ासीवाद आंदोलन की शक्ल में रहा था। नये समय में भी सत्ता तो उन्हें कुछ देशों में मिली है लेकिन आंदोलन की शक्ल में इसकी मौजूदगी सर्वत्र महसूस की जा रही है। इसका सबसे मजबूत प्रमाण अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति ट्रम्प के पक्ष में सत्ताकेंद्र पर हमले की भयानक घटना है। जो लोग इस दौर में फ़ासीवाद का उभार देख रहे हैं वे भी इस बार के उसके पुनरागमन की नवीनता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात तो यही है कि पिछली बार इस विचार के विश्वासी शासकों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को उखाड़ फेंका था। उसके विपरीत इस दौर के शासक लोकतांत्रिक संस्थाओं को खारिज करने की जगह उनके जरिये ही काम कर रहे हैं। वे इन संस्थाओं के सार को समाप्त करके उनका प्रतीकवत इस्तेमाल कर रहे हैं।
प्रतीक से उन्मादी और हिंसक प्रेम सबसे अधिक राष्ट्रभक्ति के सिलसिले में देखा जा रहा है। देश की दशा जितनी ही बुरी होती जा रही है उतने ही बड़े पैमाने पर उसके प्रतीकों को जश्न में बदला जा रहा है। ऐसा केवल भारत में नहीं हो रहा है। अमेरिका में भी मागा (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) इसका ही एक खास रूप है। संकीर्ण राष्ट्रवाद का यह रूप पड़ोसी देशों से मेलजोल की जगह होड़ और ईर्ष्या को प्रोत्साहित करता है । इसमें साम्राज्यवादी राजनीति के वर्तमान केंद्र, अमेरिका से अपमानजनक नजदीकी के जरिये वैश्विक हैसियत पाने की हताश आकांक्षा है। दूसरा अंतर यह है कि पिछली बार युद्ध के चलते उन शासकों का उसी तेजी से पराभव हुआ जिस तेजी से उनका उभार हुआ था। इस बार कम से कम अपने देश में उसका उत्थान बहुत दिनों की वैचारिक तैयारी के साथ हुआ है। अन्य देशों में भी नस्लभेदी और स्त्रीद्वेषी सामाजिक हालात का उनको साथ मिला हुआ है। फ़ासीवादी प्रवृत्तियों के इस नये उभार के साथ ही पश्चिमी विद्वानों के बीच द्वितीय विश्वयुद्ध की ऐसी व्याख्या फिर से जोर पकड़ रही है जिसमें हिटलर और कम्युनिस्ट शासन को तत्कालीन हिंसा के लिए बराबर का दोषी बताया जा रहा है। कहने की जरूरत नहीं कि यह व्याख्या फ़ासीवाद के लिए हमेशा से मुफ़ीद रही है। द्वितीय विश्वयुद्ध की पराजय के बावजूद फ़ासीवाद के समर्थक समाप्त नहीं हुए थे। वे नये हालात के हिसाब से ढलकर राजनीति में मौजूद रहे और अवसर मिलने पर फिर से पुरानी प्रतिबद्धता के साथ लौट आये हैं ।
वाल्टर बेंजामिन ने कभी कहा था कि फ़ासीवादी हमले से जीवित लोगों को जितना खतरा होता है उससे अधिक खतरा अतीत यानी इतिहास को होता है। देश की महानता का झूठा आख्यान इतिहास को विकृत करके तैयार किया जाता है। ऐसे इतिहास की प्रामाणिकता के लिए शिक्षा को शिकार बनाया जाता है। वैज्ञानिक सोच और तथ्यपरक इतिहास फ़ासीवाद के लिए बाधा का काम करते हैं। बीसवीं सदी के दौरान भी ज्ञान के प्रति उपेक्षा और हिकारत का माहौल यहूदी विरोध के जरिये बनाया गया था। किताबों की होली इसी नाम पर जलायी गयी थी कि उनके लेखक यहूदी थे। न केवल इतिहास या शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक बदलाव नजर आ रहे हैं बल्कि तकनीक के साथ मीडिया के मेल ने सोशल मीडिया नामक मंच को जन्म दिया जिसने कुल मिलाकर सामाजिकता बढ़ाने की जगह झूठ फैलाने और उसे ही सत्य मान लिये जाने की ऐसी चुनौती पेश की है जिसका समाधान फिलहाल दिखायी नहीं दे रहा। इतना ही नहीं इस मंच ने पूंजीवादी मुनाफ़े के बड़े स्रोत की हैसियत प्राप्त कर ली है जिसके चलते इस किस्म के पूंजीवाद के लिए प्लेटफ़ार्म कैपिटलिज्म नामक कोटि ही चल पड़ी है । इस मामले में भी पूंजीवाद की बुनियादी वृत्ति अर्थात सामूहिक उत्पादन और निजी अधिग्रहण काम कर रही है। इनमें से कुछ मंच जैसे फ़ेसबुक तो दक्षिणपंथी राजनीति की सेवा में अपने उपयोग करने वालों के आंकड़े भी उपलब्ध कराते पकड़ा गये हैं। संगीत की दुनिया में इसी तरह यूट्यूब नामक मंच बिना किसी योगदान के सार्वजनिक उत्पादन के जरिये भारी मुनाफ़ा तो कमाता ही है, तमाम किस्म के प्रतिक्रियावादी और दक्षिणपंथी प्रचार का अड्डा भी बन गया है ।
इस इलाके में वैचारिक टकराव लगातार जारी है क्योंकि बहुतेरे लोगों को यह भी लगता है कि इन सामाजिक मंचों ने लोकतंत्र को विस्तार दिया है। समाज के अब तक उपेक्षित रहे कुछ तबकों ने इस तकनीक के इस्तेमाल से सार्वजनिक दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज करायी है। घरेलू स्त्रियों, किशोरों और अर्ध साक्षर लोगों ने इसके चलते एक किस्म का सबलीकरण हासिल किया है। इस सिलसिले में ध्यान देने की जरूरत है कि पूंजीवाद इसी तरह अपने उत्पादों के नये उपभोक्ता खोजता रहता है। टेलीविजन भी घरेलू स्त्रियों के खाली समय का इस्तेमाल योजनाबद्ध तरीके से करता था। फिलहाल वह इन तबकों के अवकाश पर भी कब्जा करके मुनाफ़ा कमाने की तकनीक खोजने और उसे प्रचारित करने में सफल हुआ है। इन क्षेत्रों में भी कामगारों का एक नया वर्ग तैयार हुआ है जिसे संगठित करने की चुनौती दरपेश है।
उद्योग के मुकाबले सेवा क्षेत्र की बढ़ोत्तरी ने मजदूरों में नये और अलग ही तरह के लोगों को प्रवेश दिया है। ये अधिकतर युवा हैं और एक जगह इकट्ठा नहीं रहते। इससे उनको एकजुट करने में समस्या तो आ रही है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ कोशिशें रूप ले रही हैं और इनमें सबसे विशाल कंपनी, अमेज़न में कामगारों के संगठन बनने शुरू भी हुए हैं । इस क्षेत्र में रोजगार की अस्थिरता के चलते श्रमिकों की स्थिति खासकर खराब रहती है। पश्चिमी देशों में कार्यरत प्रवासी मजदूरों को संगठित करने की दिशा में भी कुछ ठोस प्रयास नजर आ रहे हैं। उन देशों के वामपंथी कार्यकर्ता इस मुद्दे पर विशेष जोर दे रहे हैं। हमारे देश में भी कोरोना के दौरान लाकडाउन ने प्रवासी मजदूरों की समस्या को प्रत्यक्ष कर दिया था । बंगलोर और चेन्नई जैसे नगरों में इनको संगठित करने की कोशिश हो रही है और गाहे ब गाहे उनके छिटफुट आंदोलनों की खबरें भी बाहर आती रहती हैं ।
बेतहाशा मुनाफ़ा कमाने की पूंजीवाद की भूख ने पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचायी है । इस समय यह भी बहुत बड़े सवाल के बतौर उभरा है। इस मोर्चे पर वैचारिक तनातनी बहुत ही जोरदार स्तर पर चल रही है। जिस तरह सिगरेट पीने पर कैंसर की सम्भावना के चलते उस पर रोक लगाने की कोशिशों का विरोध करने वाले धन्नासेठों ने तम्बाकू की खेती करने वाले किसानों की ओर से अपना मोर्चा खोला उसी तरह पर्यावरण की बरबादी की जिम्मेदारी से पूंजीवाद को मुक्त करने की मुहिम भी चलती रहती है । तर्क दिया जाता है कि जबसे खेती मनुष्य के भरण पोषण का मुख्य साधन बनी तबसे ही पर्यावरण में मानव हस्तक्षेप शुरू हुआ । धरती पर जीवन की गारंटी जिस ओज़ोन परत के कारण है उसमें क्षरण की शुरुआत को भी पानी वाली फसलों की खेती के साथ जोड़कर पेश किया जाता है और इसी आधार पर धान की खेती करने वाले चीन और भारत जैसे देशों पर इसका दोष मढ़ा जाता है। जलवायु परिवर्तन से इनकार करने वालों की अगुआई करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इसे चीनी षड़यंत्र कहा तो हमारे प्रधानमंत्री ने दावा किया कि क्लाइमेट नहीं बदल रहा, हम बदल रहे हैं।
इस सिलसिले में जानकारों का यह कहना है कि औद्योगिक क्रांति से पहले जिन भी वस्तुओं का उत्पादन होता था वे प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत ही पर्यावरण में वापस मिल जाती थीं लेकिन उसके बाद से ऐसी वस्तुओं का उत्पादन शुरू हुआ जो गल पचकर नष्ट नहीं होतीं, बल्कि धरती का गला घोंटती रहती हैं। इस मामले में प्लास्टिक और कंक्रीट का उपयोग सबसे अधिक नुकसानदेह माना गया है। प्लास्टिक तो न केवल धरती के जलप्रवाह को बाधित करता है बल्कि समुद्र के भीतर सबसे स्थायी कचरा साबित हुआ है। इनके अलावे भी खेतों की रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल ने गंगा जैसी जीवनदायिनी नदी को कैंसर का सबसे बड़ा स्रोत बना दिया है। रोजमर्रा की इन चीजों के अतिरिक्त आणविक हथियारों के इस्तेमाल से होने वाली दीर्घकालीन क्षति के बारे में कोई अनुमान ही नहीं है। इन्हीं वजहों से वैज्ञानिकों का एक समुदाय इस समय को एंथ्रोपोसीन कहता है जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के बदलाव अब प्राकृतिक परिघटना के मुकाबले मनुष्य की गतिविधियों के चलते हो रहे हैं। वर्तमान समय में यह नयी पीढ़ी का सबसे गम्भीर सरोकार बन गया है। उनका मानना है कि धरती और ब्रह्मांड केवल मनुष्य के लिए नहीं हैं, सभी चीजों के साथ ही धरती पर मनुष्य रह सकता है। उसके अतिशय उपभोग की आदत ने ही हालिया कोरोना महामारी को जन्म दिया था। अगर धरती को उसका घर बने रहना है तो उसकी सुरक्षा भी उसकी जिम्मेदारी है। पर्यावरण की चेतना ने न केवल वर्तमान पूंजीवाद की सर्वभक्षी प्रवृत्ति को नंगा कर दिया है बल्कि संसाधनों पर कब्जे और उपभोग की उसकी प्रकृति को समझकर गरीब देशों ने अपना दावा पेश करना शुरू किया है। वे औपनिवेशिक काल में अपने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का इतिहास तो खंगाल रहे ही हैं, इस समय भी प्रदूषणकारी उपभोग के लिए जिम्मेदार देशों के विनाश की कीमत चुकाने से इनकार कर रहे हैं और पर्यावरणिक न्याय को अपना नारा बना रहे हैं । इसके कारण गरीब देशों के कामगारों के जीवन के संसाधन कम पड़ रहे हैं और आप्रवास पर पश्चिमी देशों ने रोक लगाकर हालत और भी खराब कर दी है ।
तीस साल पहले सोवियत संघ के पतन से ऐसी उम्मीद पैदा हुई थी कि शीतयुद्ध की समाप्ति हो गयी है। इतिहास का अंत घोषित करने वाले फ़ुकुयामा ने भी उदारवाद और लोकतंत्र के अनंत प्रसार की भविष्यवाणी की थी। आणविक और पारम्परिक हथियारों की होड़ के खत्म होने की आशा थी। लगा था कि अब होड़ मानवता की बेहतरी के लिए साधनों के निर्माण के मामले में होगी। दोनों खेमों के बीच एक जमाने में होड़ उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में होती भी थी। शिक्षा, खेल और वैज्ञानिक खोजों के मामले में उनकी होड़ से समूची मानवता को लाभ होता लेकिन दुनिया के एकध्रुवीय होते ही अमेरिका ने उन सभी कारनामों को ही अंजाम देना शुरू किया जिनकी वह अन्यथा आलोचना किया करता था । इरान-इराक और अफ़गानिस्तान के बाद लीबिया में युद्ध भड़क उठे। हथियार का एकमात्र उपयोग युद्ध में ही हो सकता है इसलिए उसके उत्पादन और बिक्री की तो बात तभी होगी जब युद्ध जारी रहें। हालिया यूक्रेन युद्ध और चीन के साथ लागडांट के बाद बहुतेरे विद्वानों को शीतयुद्ध की वापसी की भी आहट सुनायी दे रही है। इस तरह के व्यापार के साथ निजी कारपोरेट घरानों की संपत्ति में अकूत इजाफ़ा जुड़ा हुआ है क्योंकि युद्धक सामग्री की बिक्री बहुत ऊंची कीमत पर होती है। हमारे देश और पाकिस्तान के बीच हथियारों की होड़ इनके निर्माताओं के लिए बड़ी खुशी की खबर होती है। दोनों देश हथियार खरीदते हैं, मुनाफ़ा अमीर देशों को होता है और भ्रष्ट राजनेताओं को बिचौलियों की मार्फत प्रचुर धन मिलता है। हमारे देश में समय समय पर युद्धक सामग्री की खरीद के साथ विवाद उठते रहते हैं। इन विवादों ने कभी कभी कुछ नेताओं की बलि ली है लेकिन अब इस मामले में भी निर्लज्जता का ही शासन है। भ्रष्टाचार का सीधा संबंध सार्वजनिक सुविधाओं में कटौती से है। जिस धन पर टैक्स लगाकर उससे हासिल कमाई का जन कल्याण के लिए उपयोग होना था उसे विदेशों में भेज दिया जाता है या घूस के बतौर वह शासक दल के चुनाव व्यय या आलीशान कार्यालय बनाने में लग जाता है। सरकार के पास जब धन की कमी आती है तो वह इस धन पर हाथ डालने की जगह जनता की जेब पर डाका डालने का विकल्प चुनती है ।
इन सबके चलते ही पूरी दुनिया विगत तीस सालों से जबर्दस्त जनांदोलनों की रणभूमि बनी हुई है। इन आंदोलनों के मुद्दे बहुविध हैं। स्वाभाविक है कि आंदोलनों की उठान के साथ वामपंथ का भी उत्थान होता है। इस दौर के वामपंथी उत्थान की सबसे बड़ी खासियत है कि उसके साथ किसी सत्ता का साया नहीं है। इससे साधनों की कमी तो आती है लेकिन किसी सरकार के कामों की कोई जवाबदेही भी नहीं होती। नये दौर के इन वाम आंदोलनों का एक गढ़ लैटिन अमेरिका है जहां लहरों की तरह वाम उभार उठता गिरता रहता है। इस क्रम में मार्क्सवादियों के नेतृत्व में जारी यह वाम लहर अपनी सबसे बड़ी समस्या हल कर रही है। हमेशा से उस पर आरोप लगता रहा था कि मार्क्सवादी दल चुनाव की लोकतांत्रिक पद्धति के साथ सहज नहीं होते लेकिन चुनाव में हारते और जीतते हुए ये पार्टियां और इनके नेता एक नया रास्ता तैयार कर रहे हैं। याद दिलाने की जरूरत नहीं कि लैटिन अमेरिका के ही देश वेनेजुएला के शासक यूगो शावेज ने इक्कीसवीं सदी के मार्क्सवाद को विशेष बताया था। क्यूबा जैसे पुराने मार्क्सवादी देश पर कोरोना के दौरान उसके डाक्टरों के कारण ध्यान गया लेकिन यह बात अलक्षित रही कि इस समय क्यूबा में फ़िदेल और राउल के बाद की पीढ़ी का शासन है। यूरोप के ग्रीस और स्पेन जैसे देशों में वामपंथी दल जीतते हारते भी लगातार बने हुए हैं। इसी तरह अमेरिका में निरंतर वाम युवकों की तादाद बढ़ रही है और वे भी लोकतंत्र और समाजवाद के उपर्युक्त अंतर्विरोध को हल करते हुए लोकतांत्रिक समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित कर रहे हैं।
इस बारे में एक अन्य खूबी का भी जिक्र जरूरी है। अस्मिता के आंदोलनों और सवालों के साथ नये समय के वामपंथ और मार्क्सवाद का बेहद सकारात्मक संवाद बन रहा है। पूंजीवाद विरोध में संग साथ होने के चलते ऐसा केवल व्यावहारिक स्तर पर नहीं हो रहा बल्कि सैद्धांतिक स्तर पर भी हरित मार्क्सवाद और इकोसोशलिज्म जैसी नयी धारणाओं का निर्माण गम्भीरता के साथ हो रहा है। इसी तरह नारीवाद के साथ आपसी संवाद ने समूचे अर्थतंत्र में उनके वेतनरहित श्रम की भूमिका को समझने में आसानी पैदा की है। गोरे पश्चिमी देशों की अफ़्रीकी आबादी के भीतर की वैचारिक हलचल के चलते पूंजीवाद के साथ नस्लभेद के संश्रय को पहचानने में मदद मिली है और समूचे इतिहास में अफ़्रीकी अश्वेतों के श्रम की खुली लूट की भरपाई के नारे को लोकप्रिय बनाया है। उपनिवेशवाद के साथ भी नस्लभेद का रिश्ता भी इसी वजह से उजागर किया जा रहा है।
इन सवालों ने धीरे धीरे आंदोलनों से आगे आकर अकादमिक दुनिया में भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। जो आंदोलन चले उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के लिए कलात्मक रूप भी अपनाये। कला और साहित्य संस्कृति के बारे में रूढ़ धारणा से बंधे होने के कारण इन्हें देखने और रेखांकित करने में बाधा आ रही है। आशा है आगामी दिनों में यह जड़ता टूटेगी।