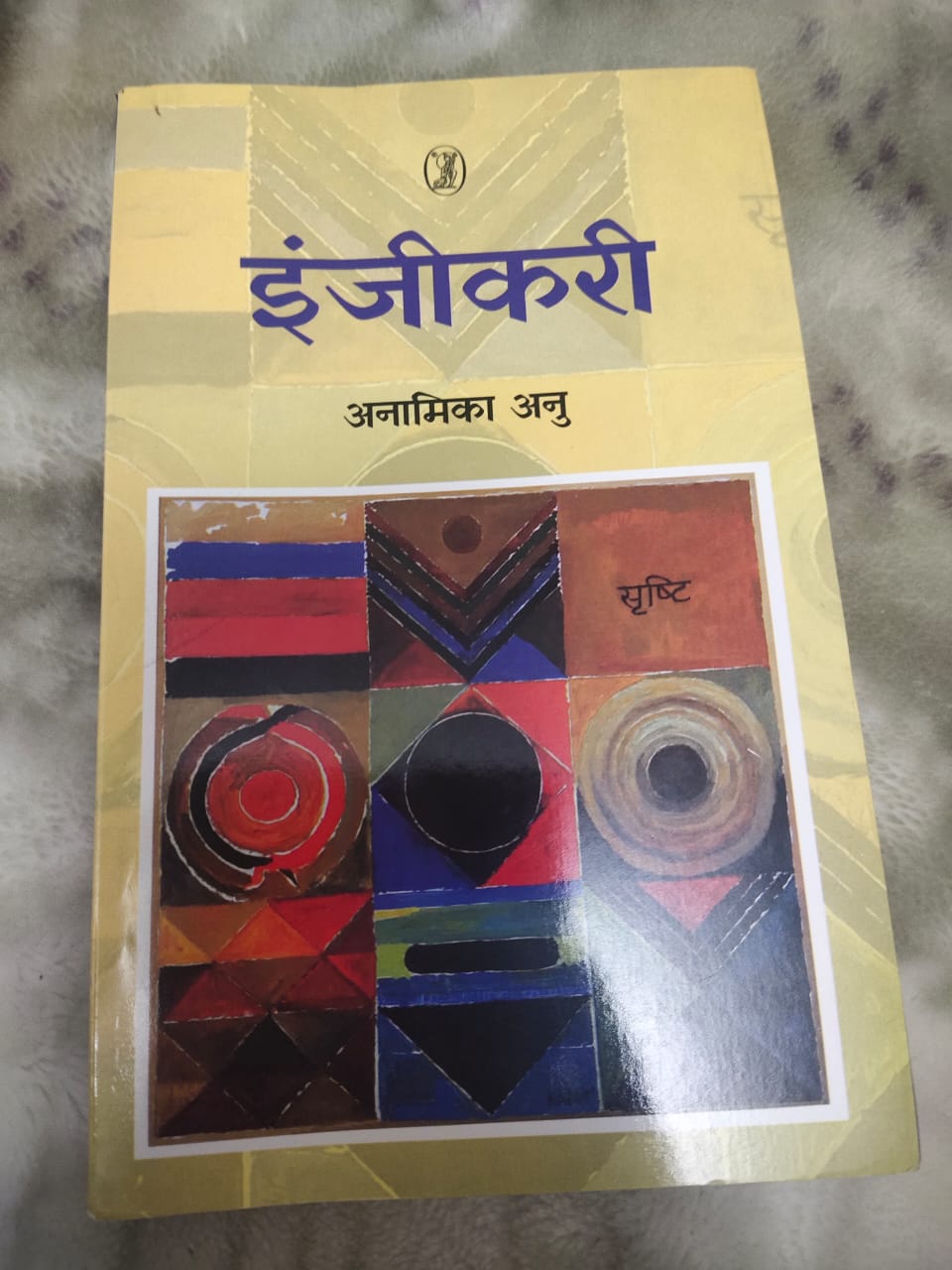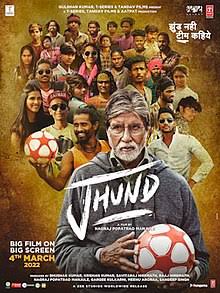‘देवी’ निराला की बहु प्रशंसित कहानी है। यह प्रशंसा इस कहानी की संवेदना को लेकर अधिक है। कोई भी रचना बड़ी तो प्रथमतः अपनी संवेदना के ही चलते होती है। लेकिन, संवेदना कोई वस्तु-निरपेक्ष भाव और विचार का संलयन नहीं बल्कि वस्तु-सापेक्ष है। जैसे उत्पीड़क और उत्पीड़ित या कष्ट देने वाले और कष्ट उठाने वाले के लिए एक ही तरह की संवेदना नहीं हो सकती। दुःख की परिस्थिति का निर्माण करने वाले या इसके लिए जिम्मेदार को लेकर वही संवेदना नहीं हो सकती जो इसके भुक्तभोगी को लेकर होगी। वह व्यक्ति हो सकता है, समूह हो सकता है, वर्ग और जाति हो सकती है, राष्ट्र हो सकता है। खैर
देवी कहानी की वस्तु संवेदना को निराला की एक अन्य रचना ‘कुल्ली भाट’ के साथ रख कर देखा जा सकता है। मामूली लोगों के जीवन और जीवन के संघर्ष में मनुष्यता के सार तत्व और उसकी विजय या अजेयता या वह जो मनुष्य होने की उच्चतम भूमि हो सकती है, उसे देख लेना, पा लेना और खुद उस अवस्था में पहुंच जाना; दोनों रचनाओं में समान है। सूत्र के रूप में जिसे मुक्तिबोध ने वाह्य का आभ्यंतरीकरण और अभ्यंतर का वाह्यीकरण कहा है। यह प्रक्रिया ऐसी होती है, कि वह सिद्धांत और व्यवहार या जीवन और मूल्य के बीच एकता बना देती है। एकता भी एक तरह से नहीं, बल्कि वह एक दूसरे में अंतर्भुक्त हो जाती है, ऐसा कि अलग-अलग करना संभव नहीं रह जाता है। रचना और रचनाकार की इस आंतरिक अन्विति को जानने के लिए भी देवी कहानी बेजोड़ है।
एक और बात जो रचना के बारे में अभी भी सत्य है, कि वह करुणा को जन्म दे या करुणा का उद्रेक करे। यह काव्य का ही सत्य नहीं है, यह साहित्य का सत्य है, और जैसे-जैसे अन्याय और मनुष्य विरोधी प्रवृतियां प्रबल होती जाती हैं, यह और बड़ा सत्य, साहित्य का होता जाता है। अगर ऐसा साहित्य अपने समय में नहीं रचा जा रहा है, तो पूर्व में रचे ऐसे साहित्य प्रासंगिक हो उठते हैं। यह पुनः लोगों के बीच अपने सत्य को लेकर जिंदा हो जाते हैं। निराला का साहित्य ऐसा साहित्य है और ‘देवी’ कहानी ऐसी रचना है।
इसी संदर्भ में एक और बात जरूरी हो जाती है, क्योंकि विमर्श का समय है यह। इसमें पूर्व के उस साहित्य को बेमानी बता दिया गया है या बताया जाता है, जो विषय के रूप में स्त्री, दलित आदि को लेकर लिखी या रची गयी हैं या सीधे रूप में गैर-दलित या पुरुष द्वारा रचे गये साहित्य को सहानुभूतिपूर्ण लेखन कहकर यह बताना, कि उसमें तो अधिकारों की बात नहीं की गयी है और यह एक प्रकार का षड्यंत्र है, छल है। और भी आक्षेप होते हैं ऐसे साहित्य पर, जैसे दयनीय दिखाना या प्रतिकार और संघर्ष न दिखाना आदि।
एक रचनाकार के पास उसकी रचनात्मक या सर्जना की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। प्रायः रचनाकार या कलाकार सत्ता की शक्ति और उसके केंद्र से दूर रहता है। अभी के समय में भले यह कम हुआ हो, उसके बावजूद साहित्य और कला की केन्द्रीय धारा अभी भी सत्ताभिमुख नहीं है। रचनाकार की यह शक्ति हमारे अपने आसपास, खुद के आसपास के और जाने-सुने सत्य को फिर से रचने में प्रकट होती है। यह पुनर्रचाव या कला उत्पाद या साहित्य संभव ही होता है रचनाकार के भीतर करुणा, दया, पीड़ा, सहानभूति की उपस्थिति से। और, यही सब मिलकर उसकी रचना का मूल्य, उसकी संवेदना बनते हैं। रचना वस्तु या विषय के रूप में दलित हो, स्त्री हो, मानव समाज का अन्य उपेक्षित वर्ग हो, हिस्सा हो, पीड़ित, सताया हुआ व्यक्ति हो, उसके सत्य को रचते हुए उसका स्प्रिचुअल मोटिफ मनुष्य के भीतर करुणा, सहानभूति जगाना ही तो होता है। उसे अधिकतम मनुष्य बनाना ही तो होता है। संवेदनशील मानव समाज और राष्ट्र निर्माण की चाहत से ही तो कोई रचनाकार ऐसा विषय या समाज का सत्य उठाता है। अन्याय के प्रति क्रोध का भाव, उसका प्रतिकार, संघर्ष तो उसी के भीतर से आता है। दूसरे, वह ऐसा सत्य रचता है जिसमें देखा जा सके कि समाज की तस्वीर को कौन बिगाड़ रहा है और इस तस्वीर के बाहर किस वर्ग, समूह को धकेल दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। अर्थात जो रचनाकार या कलाकार की असली शक्ति होती है, उसे ही दोष बताना उस तर्क प्रणाली से आता है, जिससे धर्म की सत्ताएं अपने को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल करती थीं, जैसे ब्राह्मण का शुद्ध होना, पवित्र होना या मंदिरों में प्रवेश के नियम, पूजा की विधियां आदि। यह कहना और क्या है, कि यह हमारा सत्य है, इसे हम ही कहेंगे। बहस चाहे जितना कर ले कोई, लेकिन यह तर्क प्रणाली तो वर्णवादी या ब्राह्मणवादी बहिष्कार और वर्जना की ही है। या यह वैसे ही है, जैसे आज हिंदूवादी ताकतें आंदोलनजीवी, अर्बन नक्सल, सेकुलर जैसे शब्दों को देशद्रोह के सन्दर्भ में प्रयुक्त करते हैं। साहित्य में ‘सहानुभूति’ जैसे रचना मूल्य के साथ अस्मिता विमर्श ने ऐसा ही किया है। निराला की रचनाओं को लेकर भी ऐसी बातें उठती हैं, इसलिए ‘देवी’ कहानी के संदर्भ में यह कहना पड़ा। हालांकि देवी की जाति और उसका धर्म नहीं मालूम, लेकिन उसके प्रति समाज के अग्रणी लोगों का नजरिया और रवैया वही है, जो समाज के अन्य उत्पीड़ित, उपेक्षित समूह, वर्ग को लेकर है। ‘देवी’ कहानी की संवेदना तो वहां तक फैली ही है, विस्तार लिये हुए है। कहानी में देवी का पहला शब्द चित्र यूं आता है-
“वह रास्ते के किनारे बैठी थी, एक फटी धोती पहने हुए। बाल कटे हुए। तअज्जुब की निगाह से आने-जानेवालों को देख रही थी। तमाम चेहरे पर स्याही फिरी हुई। भीतर से एक बड़ी तेज भावना निकल रही थी- ‘यह क्या है?’ उम्र पच्चीस साल से कम। दोनों स्तन खुले हुए। प्रकृति की मारों से लड़ती हुई, मुरझाकर, मुमकिन है किसी को पच्चीस साल से कुछ ज्यादा जँचे, पास एक लड़का डेढ़ साल का खेलता हुआ, संसार की स्त्रियों की एक भी भावना नहीं, उसे देखते ही मेरे बड़प्पनवाले भाव उसी में समा गये, और फिर वही छुटपन सवार हो गया। मैं उसी की चिंता करने लगा- ‘यह कौन है, हिन्दू या मुसलमान? इसके एक बच्चा भी है। पर इन दोनों का भविष्य क्या होगा? बच्चे की शिक्षा, परवरिश क्या इसी तरह रास्ते पर होगी। यह क्या सोचती होगी, ईश्वर, संसार, धर्म और मनुष्यता के संबंध में?”
देवी का यह शब्द चित्र उकेरते हुए निराला के यहां जो विचार आते हैं, उसकी प्रकृति, उसका आयाम, उसकी मंशा भी साथ में प्रकट है, उसकी अलग से व्याख्या की जरूरत नहीं। निराला के रचनात्मक संघर्ष के कारण भी इसी विचार प्रक्रिया में छिपे हैं। निराला की जो रचना दृष्टि है, वह किन ऑब्जेक्ट से बनी है या दृश्य जगत का प्रत्यक्षीकरण निराला के यहां किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, इसे भी ‘देवी’ कहानी से जाना-समझा जा सकता है। ‘कुल्ली भाट’ के साथ मिलाकर पढ़ने पर यह और स्पष्ट हो जाता है। ‘देवी’ कहानी का पहला पैराग्राफ देखा जाय-
“बारह साल तक मकड़े की तरह शब्दों का जाल बुनता हुआ मैं मक्खियाँ मारता रहा। मुझे यह ख्याल था कि मैं साहित्य की रक्षा के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रहा हूँ। इससे उसका निवेश भी सुंदर होगा और उसकी शक्ति का संचालन की ठीक-ठीक। पर लोगों को अपने फँस जाने का डर होता था, इसलिए इसका फल उल्टा हुआ।… इसलिए मेरी कद्र नहीं हुई। मुझे बराबर पेट के लाले रहे। पर फाकेमस्ती में भी मैं परियों के ख्वाब देखता रहा- इस तरह अपनी तरफ से मैं जितना लोगों को ऊँचा उठाने की कोशिश करता गया, लोग उतना मुझे उतारने पर लगे रहे और चूँकि मैं साहित्य को नरक से स्वर्ग बना रहा था, इसीलिए मेरी दुनिया भी मुझसे दूर होती गयी।… ‘दूबर होत नहीं कबहूँ पकवान के विप्र, मसान के कुकर’ की सार्थकता मैंने दूसरे मित्रों में देखी… वे पहले फटीचर थे, पर अब अमीर बन गये हैं, दोमंजिला मकान खड़ा कर लिया है, मोटर पर सैर करते हैं। मुझे देखते हैं, जैसे मेरा-उनका नौकर-मालिक का रिश्ता हो। नक्की स्वरों में कहते हैं- ‘हाँ, अच्छा आदमी है; जरा सनकी है।’ फिर बड़े गहरे पैठकर मित्र के साथ हँसते हैं। वे उतनी दूर बढ़ गये हैं, मैं जिस रास्ते पर था, उसी पर खड़ा हूँ। जिसके लिए मेरी इतनी बदनामी हुई, दुनिया से मेरा नाम उठ जाने को हुआ, जो कुछ था, चला गया, उस कविता को जीते-जी मुझे भी छोड़ देना चाहिए। जिसे लोग खुराफात समझते हैं, उसे न लिखना हो, तो लोगों की समझ की सच्ची समझ होगी? रतिशास्त्र, वनिता-विनोद, काम-कल्याण में मश्क करते कौन देर लगती है? चार किताबों की रूह छानकर करे किताब लिख दूँगा। ‘सीता’, ‘सावित्री’, ‘दमयंती’ आदि की पावन कथाएँ आँख मूँदकर लिख सकता हूँ। तब बीवी के हाथ ‘सीता’ और ‘सावित्री’ आदि देकर बगल में, ‘चौरासी आसन’ दबाने वाले दिल से नाराज न होंगे। उनकी इस भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने की कोशिश करके ही बिगड़ा हूँ। अब जरूर सँभलूँगा। राम, श्याम जो-जो थे पूजने-पुजानेवाले, सब बड़े आदमी थे। बगैर बड़प्पन की तारीफ कैसी? बिना राजा हुए राजर्षि होने की गुंजायश नहीं, न ब्राह्मण हुए बगैर ब्रह्मर्षि होने की है। वैष्यर्षि या शूद्रर्षि कोई था, इतिहास नहीं, शास्त्रों में भी प्रमाण नहीं, अर्थात नहीं हो सकता। बात यह कि बड़प्पन चाहिए। बड़ा राज्य, ऐश्वर्य, बड़े पोथे, तोप, तलवार, गोले-बारूद, बन्दूक-किर्च, रेल-तार, जंगीजहाज, टारपेडो, माइन, सबमेंरीन-गैस, पल्टन-पुलीस, अट्टालिका-उपवन आदि-आदि सब बड़े-बड़े- इतने कि वहाँ तक आँख नहीं फैलती, इसलिए कि छोटे समझें कि वे कितने छोटे हैं। चंद्र, सूर्य, वरुण, कुबेर, यम, जयन्त, इन्द्र, ब्रह्म, महेश तक बाकायदा बाहिसाब ईश्वर के यहाँ भी छोटे से बड़े तक मेल मिला हुआ है।”
निराला का यह रचनात्मक संघर्ष दरअसल नये भाव-बोध और वस्तु-संवेदना को लेकर था। कविता की भाषा खड़ी बोली अवश्य हो गयी थी, लेकिन अभी भी हिंदी समाज का जो कविता का पाठक समुदाय था वह अपने सौंदर्यबोध और वस्तु संवेदना में ब्रजभाषा की कविता का ही समर्थक था। अर्थात, मांसल सौंदर्य का प्रशंसक था। या, कविता में वह मध्यकालीन सामंती भावबोध से ग्रस्त या उसी में पड़ा हुआ था। हिंदी के व्यापक पाठक समुदाय में इसी की मांग बनी हुई थी, जिसके दबाव में खड़ी बोली में जो महाकाव्य, खंडकाव्य रचे गये, उसमें स्त्री-पुरुष संबंध में या प्रेम को लेकर किसी नये भावबोध या सौंदर्यबोध या मूल्य के लिए संघर्ष की बजाय ब्रजभाषा के साहित्य या मध्यकालीन बोध, मूल्य, नैतिकता से ही काम लिया गया। या, उसे ही कुछ राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव में मर्दवादी ओज की छौंक के साथ प्रस्तुत किया गया। इसीलिए इन महाकाव्यों और खंडकाव्यों की अंतर्वस्तु या उसके विषय पौराणिक आख्यान से लिये गये। निराला के भीतर जो रचनात्मक बेचैनी और संघर्ष था, वह इसको लेकर था। और कम या बेसी पूरी छायावादी कविता के ही भीतर था।
निराला इसमें निरंतर इसके लिए संघर्षरत रहे। स्त्री-पुरुष संबंध, प्रेम को नये भावबोध, नये सौंदर्यबोध के साथ व्यक्त करना, जिसमें ‘लिबर्टी’, ‘इक्वलिटी’ जैसे नये जीवन-मूल्य थे। जो, रोमांटिक कविता के प्राण थे। जिसे, हिंदी में छायावाद कहा गया। वह तोड़ती पत्थर जैसी कविता तो इसी के भीतर से निकलती है। यह सौंदर्यबोध तो हिंदी कविता में पहली बार आता है। इसके पहले यह है ही नहीं। और, सिर्फ स्त्री के सौंदर्य को लेकर ही नहीं, बल्कि स्त्री-पुरुष संबंध और प्रेम को लेकर भी निराला हिंदी कविता को भिन्न भूमि पर खड़ा कर देते हैं। इस मामले में अज्ञेय भले ही बाद में बड़े कवि हुए, लेकिन इसे लेकर तो निराला ही आते हैं। 1937 ईस्वी की एक कविता है ‘उक्ति’, जो इस तरह है-
“कुछ न हुआ, न हो।
मुझे विश्व का सुख, श्री, यदि केवल
पास तुम रहो!
मेरे नभ के बादल यदि न कटे-
चन्द्र रह गया ढका,
तिमिर-रात को तिरकर यदि न अटे
लेश गगन-भास का,
रहेंगे अधर हँसते, पथ पर, तुम
हाथ यदि गहो।
बहु-रस साहित्य विपुल यदि न पढ़ा-
मन्द सबों ने कहा,
मेरा काव्यानुमान यदि न बढ़ा-
ज्ञान, जहाँ का रहा,
रहे, समझ है मुझमें पूरी, तुम
कथा यदि कहो।”
1938 ईस्वी का एक गीत है, जिसकी पंक्तियां हैं-
“जैसे हम हैं वैसे ही रहें,
लिये हाथ एक दूसरे का
अतिशय सुख के सागर में बहें।
मुदें पलक, केवल देखें उर में,-
सुने सब कथा परिमल-सुर में,
जो चाहें, कहें वे, कहें।
वहाँ एक दृष्टि से अशेष प्रणय
देख रहा है जग को निर्भय,
दोनों उसकी दृढ़ लहरें सहें।
निराला के यहाँ आधुनिक भावबोध की ऐसी और भी कविताएँ हैं। कहने का आशय यह, कि ‘देवी’ कहानी के प्रारंभ में बतौर कहानी-वाचक निराला के जो विचार हैं, उसका द्वंद यही है। कविता को, साहित्य को वैयक्तिक स्वाधीन चेतना से उत्पन्न मूल्यों और सौंदर्यबोध से युक्त करना। जबकि, हिंदी के व्यापक पाठक समुदाय की मांग अभी भी मध्यकालीन सामंती भावबोध, सौन्दर्यबोध की थी। जिसे, हिंदी के ज्यादातर प्रकाशक जीवित रखे हुए थे और खड़ी बोली के कवियों से भी वे यही चाहते थे। स्त्री का मांसल सौंदर्य, बारहमासा, षडमासा, और काव्यानंद के रूप में रति-सुखानुभूति। निराला इसी को बदल देना चाहते थे। निराला के लिए बदलाव की यह चाहत औरों से अलग थी। क्योंकि, वैयक्तिक स्वाधीन चेतना या ‘लिबर्टी’, ‘इक्वलिटी’ जैसे मूल्य निराला के यहाँ वैयक्तिकता के दायरे को पार कर, समाज के भीतर प्रविष्ट हो गये। अर्थात, सामाजिक मूल्य में बदल गये। ऐतिहासिक रूप से संयुक्त परिवार और सामंती समाज की नैतिकता के खिलाफ उठी स्वाधीन पुकार या ‘स्व’, ‘इंडिविजुअल’ को मुक्त करने की चेतना, समाज की मुक्ति की तरफ बढ़ गयी। वह जगह-जगह वर्णवाद, ब्राम्हणवाद, जातिवाद से टकराने लगी। हिंदी का प्रकाशन व्यापार, चाहे अखबार हों, पत्र-पत्रिकाएं हों अभी तक बहुत हुआ, तो कुछ ऊपरी सामाजिक सुधारों को व्यक्त कर, खुद को क्रांतिकारी माने हुए थे। निराला का द्वन्द्व इसीलिए बढ़ता गया। इसे ‘कुल्ली भाट’ में जाकर ज्यादा देखा जा सकता है। उसके कई प्रकरणों में निराला के रचनात्मक संघर्ष की वजहें वर्णित हैं। एक-दो छोटे उद्धरण देखे जा सकते हैं-
“मैं बेकार था। ‘सरस्वती’ से कविता-लेख वापस आते थे। एक-आध चीज छपी थी। ‘प्रभा’ में मालूम हुआ, बड़े-बड़े आदमियों के लेख-कविताएँ छपती हैं। एक दफा ऑफिस जाकर बातचीत की, उत्तर मिला, उसमें ‘भारतीय आत्मा’, ‘राष्ट्रीय पथिक’, मैथिलीशरण गुप्त- जैसे कवियों की कविताएँ छपती हैं।”
यह भारतीय आत्मा वर्णवादी, मर्दवादी थी। निराला की भारतीय आत्मा इससे भिन्न थी। उसमें ‘दीन’ थे, ‘देवी’ थी। दूसरे यह वही साहित्य है, जिसके चलते हिंदी नवजागरण को हिंदू नवजागरण कहने की अवधारणा और पुष्ट होती है और वह कुछ हद तक ठीक भी था, क्योंकि जिसे राष्ट्रीय काव्य-चेतना, राष्ट्रीय काव्यधारा कहा गया, वह समस्याग्रस्त तो थी। खैर
‘कुल्ली भाट’ के नौवें प्रकरण का एक अंश-
“ऐसी अनेक और अड़चनें पार कीं। आचार्य द्विवेदीजी को गुरु माना; लेकिन शिक्षा अर्जुन की तरह नहीं- एकलव्य की तरह पायी।”
“… लेकिन मुझे इतना ही हर्ष है कि जीवन के उसी समय से मैं जीवन के पीछे दौड़ा था, जीव के पीछे नहीं।… जीव के पीछे पड़ने वाला बड़े-बड़े मकान, राष्ट्रचमत्कार और जादू से प्रभावित होकर जीवन से हाथ धोता है, जीवन के पीछे चलने वाला जीवन के रहस्य से अनभिज्ञ नहीं होता…।”
ऐसे और भी प्रसंग ‘कुल्ली भाट’ में हैं, जिसमें निराला का द्वंद्व और रचनात्मक संघर्ष समझ में आता है। निराला के विचार में ऐसा तत्व मौजूद था, जो तब की हिंदी प्रकाशन की दुनिया में गैर मौजूद था। देवी कहानी का पहला पैराग्राफ उन विचारों के बारे में बताता ही है। निराला भी एक-आध कोशिश करते हैं, औरों की तरह जीव के पीछे चलने की या बड़े होने के ख्याल को अपनाने की, लेकिन तब तक सत्य का ऐसा दर्शन होता है, कि निराला फिर से फाकामस्ती को प्राप्त होते हैं। निराला के साहित्य में ऐसा क्या था, जो उन्हें इस द्वंद्व और संघर्ष में ले जाता था। ‘देवी’ कहानी में ही उसका जवाब है-
” बड़े होने के खयाल से ही मेरी नसें तन गयीं और नाम मात्र के अद्भुत प्रभाव से मैं उठकर रीढ़ सीधी कर बैठ गया। सड़क की तरफ बड़े गर्व से देखा, जैसे कुछ कसर रहने पर भी बहुत कुछ बड़ा आदमी बन गया होऊँ। मेरी नजर एक स्त्री पर पड़ी।”
“… उसे देखते ही मेरे बड़प्पन वाले भाव उसी में समा गये और फिर वही छुटपन सवार हो गया” “…मेरी बड़प्पनवाली भावना को इस स्त्री के भाव ने पूरा-पूरा परास्त कर दिया।”
अर्थात, निराला की रचना-वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया में वह तत्व मौजूद है, जो उन्हें अस्वीकृत करवाता है अपने समय के बड़े प्रकाशकों या प्रायः मुख्य पत्रिकाओं में। यह तत्व क्या है, जो निराला को अस्वीकृत करवाता है। वह है, वैयक्तिक स्वाधीन चेतना या जिसे तकनीकी या पारिभाषिक या सैद्धांतिक ढंग से कहा जाता है, कि सामंती या पिछड़े समाज से पूंजीवादी समाज में संक्रमण, रूपांतरण। ‘लिबर्टी’ इसी से आया। यह ‘लिबर्टी’ है, व्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति की स्वतंत्रता किसके सापेक्ष है, तो वह है धर्म सत्ता के सापेक्ष, सामंती नैतिकता, सामंती सामाजिक मूल्य के सापेक्ष। इसमें अभी समूचे समाज और वर्ग की मुक्ति की चेतना शामिल नहीं है। लेकिन, वह भी निराला के यहाँ आ जाती है जल्दी ही। यह स्वाधीन चेतना या ‘लिबर्टी’ तर्क और विवेक के द्वार खोलती है। जिसमें प्रवेश करने के बाद मनुष्य ही नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति भी अलग दृष्टि आती है। नजरिया बदलता है और मनुष्य स्वयं का विस्तार प्रकृति की स्वतंत्रता तक करता है। निराला की कविताओं के वापस हो जाने की प्रारंभिक वजह यह थी। क्योंकि, सभी पत्रिकाओं के संपादक बने आचार्यों के यहाँ वैयक्तिक स्वाधीन चेतना नहीं आयी थी। उसको लेकर उनके पास कोई समझ नहीं थी। बाहर का ज्ञान उनके पास आ तो रहा था, लेकिन वे अभी उसे धर्मसत्ता, वर्णसत्ता के भीतर रहकर देख रहे थे और उसी के अनुकूल उसे ग्रहण कर रहे थे। निराला के यहाँ एक शब्द बहुत आता है, ‘निर्भय’। निराला के लिए यह निर्भयता है मनुष्य के मस्तिष्क में पूर्व संस्कारों या पहले से बने साँचों और विभाजनों से मुक्त हो जाने का साहस। तभी तो मनुष्य के सत्ता की एकता प्रकृति की सत्ता से स्थापित होती है। और, इस सृष्टि में मनुष्य ही एक विशिष्ट रचना है और वह किसी अन्य सत्ता के अधीन नहीं है। संपादकगण तो अभी ‘निर्भय’ हुए ही नहीं थे। आचार्यगण तो अभी ‘निर्भय’ हुए ही नहीं थे। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता तक तो अभी ‘निर्भय’ हुए ही नहीं थे। निराला सत्य और ज्ञान को लेकर ‘निर्भय’ थे। यह निर्भयता, यह स्वाधीन चेतना प्रकृति से मुड़कर मनुष्य पर आ जाती है। जहाँ ‘दीन’ है, ‘भिक्षुक’ है, कृषक है, पत्थर तोड़ती स्त्री है और इन सभी का वर्ण व्यवस्था में एक निश्चित स्थान है। मनुष्य से नीचे का दर्जा है। जबकि, आचार्यगण, संपादकगण अभी वर्ण-युक्त हैं, पत्रकारिता के व्यवसायिक घराने वर्ण-युक्त हैं। गांधी तक अभी सामंजस्य का सूत्र खोजने में लगे हैं। निराला फिर से अस्वीकृत होते हैं, लेकिन जीव के पीछे नहीं चलते, बल्कि जीवन के पीछे चलते रहते हैं।
कुल मिलाकर निराला के साहित्य में साधारण जनों का प्रवेश और उन्हें ‘देवत्व’ प्रदान करना, उन्हें अछूत बनाता है। हो सकता है, यह निराला के ऊपर विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव स्वरूप हो, लेकिन यह सिर्फ प्रभाव नहीं है, निराला स्वयं की यात्रा में भी यहाँ तक पहुंचते हैं। अब यह जो साधारण जन है, वर्ण व्यवस्था में उनकी एक जाति है। यहाँ तक कि ‘विप्लव के वीर’ बादलों का आवाहन करने वाले ‘कृषक अधीर’ की भी जाति है। इसमें अधिकांश पिछड़ी कही जाने वाली जातियाँ थीं। निराला ग्राह्य कैसे हों!!
कोई भी किसान आंदोलन कभी भी पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ग्राह्य नहीं हो पाया और आजादी के संघर्ष के बीच बनी सबसे बड़ी किसान सभा अर्थात सहजानंद सरस्वती का किसान संगठन कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ता है, कांग्रेस से नहीं। क्योंकि किसानों का यह संगठन जिन लघु, सीमांत किसानों की बात करता था, उसमें पिछड़ी जातियाँ ज्यादा आती थीं। निराला भी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ते हैं। एक कहानी ‘जान की’ में कहानी-वाचक बांदा में कम्युनिस्ट कार्यकर्ता बनकर जाता है। जाने का उद्देश्य है, संगठन का निर्माण। निराला कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं बने, लेकिन कहानी में बतौर पात्र, एक चरित्र वे बनते हैं। यह पार्टी से सहानुभूति रखने के कारण होता है। कम्युनिस्ट पार्टियों के निर्माण में ‘कैडर’ या पूर्णकालिक सदस्य बनाने के अलावा, ‘सिंपैथाइजर्स’ या सहानुभूति रखने वाले सदस्यों के निर्माण पर भी जोर होता है। दरअसल ‘सहानुभूति’ और करुणा मानवतावाद के मूल में है और मार्क्सवाद मानवतावाद की उच्चतम अवस्था कहा जाता है।
कहने का आशय यह, कि निराला की वैयक्तिक स्वाधीन चेतना, सामाजिक बराबरी या सामाजिक मुक्ति तक फैलती है, विस्तारित होती है या निराला के साहित्य में साधारण जनों का प्रवेश इसी ‘करुणा’ और ‘सहानुभूति’ से होता है। और, प्रवेश ही नहीं पाते बल्कि उनके समकालीन साहित्य में स्थापित या महाकाव्य, खंडकाव्य में स्थापित पौराणिक ‘देवजनों’ से ऊँचा स्थान पाते हैं। ‘देवी’ कहानी तो ऐसी ही कहानी है।
‘देवी’ एक पागल स्त्री है। अब इसे अगर अपना अनुभव लिखना, हो तो कैसे लिखेगी। वह गूंगी भी है, इसलिए अपना अनुभव सुना भी नहीं सकती। निराला उसकी कहानी लिखते हैं।
“मैं देख रहा था, ऊपर के धुएँ के नीचे दीपक की शिखा की तरह पगली के भीतर की परी इस संसार को छोड़कर कहीं उड़ जाने की उड़ान भर रही थी। वह सांवली थी, दुनिया की आँखों को लुभानेवाला उसमें कुछ न था, दूसरे लोग उसकी रुखाई की ओर रुख न कर सकते थे, पर मेरी आँखों को उसमें वह रूप देख पड़ा, जिसे मैं कल्पना में लाकर साहित्य में लिखता हूँ; केवल वह रूप नहीं, भाव भी।”
एक समर्थ, संवेदनशील और सचेत रचनाकार क्या कर सकता है, उसे निराला ने इतना स्पष्ट कर दिया है, कि अलग से इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं। वे आगे लिखते हैं-
“यहाँ माँ-बेटे के मनोभाव कितनी सूक्ष्म व्यञ्जना से संचारित होते थे, क्या लिखूँ! डेढ़-दो साल के कमजोर बच्चे को माँ मूक भाषा सिखा रही थी- आप जानते हैं, वह गूंगी थी। बच्चा माँ को कुछ कहकर न पुकारता था, केवल एक नजर देखता था, जिसके भाव में वह माँ को क्या कहता आप समझिए; उसकी माँ समझती थी; तो क्या वह पागल और गूंगी थी?”
“पगली का ध्यान ही मेरा ज्ञान हो गया।… उसके बच्चे में भारत का सच्चा रूप देखा, और उसमें- क्या कहूँ, क्या देखा।”
किस भारत के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है और किस भारत के लिए लड़ी जानी चाहिए! भारत की मौजूदा हालत कैसी है और उसका भविष्य क्या होगा! वह भारत जिसकी संस्कृति का झूठा गौरव गान रचा जा रहा है, वह कौन सा भारत है! और, वह भारत कौन सा है, जिसका सच्चा रूप निराला उस बच्चे में देख रहे हैं, जिसके भविष्य का निर्माण करने वाली माँ गूंगी है, पागल है, बेसहारा है, बेघर है, दीन-हीन है, सड़क पर है! राष्ट्रीय जागरण, आजादी की लड़ाई की अंतर्वस्तु और राष्ट्र निर्माण का प्रश्न निराला के यहाँ आ ही जाता है और सब कुछ के बीच में कौन सा ‘जन’ होना चाहिए, कैसे ‘जन’ का राष्ट्र होना चाहिए इसका पक्ष अस्पष्ट नहीं है, इतना स्पष्ट है, कि बिना व्याख्या भी देखा-समझा जा सकता है। हर बड़ी रचना की एक राजनीति होती है, ‘देवी’ कहानी से इसे भी जाना जा सकता है। आगे देखिए-
“देश में शुल्क लेकर शिक्षा देनेवाले बड़े-बड़े विश्वविद्यालय हैं। पर इस बच्चे का क्या होगा? इसके भी माँ है। वह देश की सहानुभूति का कितना अंश पाती है- हमारी थाली की बची रोटियाँ, जो कल तक कुत्तों को दी जाती थीं। यही, यही हमारी सच्ची दशा का चित्र है।”
जिस दशक की यह कहानी है, उस दशक में राष्ट्र निर्माण की बहस तेज हो जाती है। उसमें एक स्वर बहुत ऊंचे से साहित्य में गाया जा रहा था, गौरवशाली प्राचीन भारतीय संस्कृति का, जो एक झूठे खड़े किए गये अतीत में ही खोया था और निराला उसे यथार्थ की कठोर, खुरदुरी जमीन पर ला धरते हैं- “यही, यही हमारी सच्ची दशा का चित्र है।”
लेकिन यह जो निराला पगली के ‘बच्चे में भारत का सच्चा रूप देखा’ या जिसे वे ‘हमारी सच्ची दशा का चित्र’ कहते हैं, वह सिर्फ पगली और उसके बच्चे की स्थिति की वजह से या उसी के आधार पर कहते हैं या यह ज्यादा व्यापक किसी सामाजिक यथार्थ के आधार पर कहते हैं! देवी और उसके बच्चे की दशा के बारे में सोचते हुए निराला की नजर में बस वही दोनों हैं या करोड़ों वे भारत के जन हैं, जो गुलामी के भी भीतर गुलामी और बदतर जिंदगी जी रहे हैं! वर्ण और जाति के भेद की, छुआछूत की, अन्न के अभाव की, जमींदार के शोषण की जिंदगी जी रहे हैं। या, समाज और राष्ट्र से बहिष्कृत जिंदगी जीने वाले असंख्य जन हैं। निराला की नजर में वस्तुतः वे सभी हैं, और इसका पता उनका साहित्य ही देता है। सभी न भी पढ़े कोई तो ‘देवी’ के साथ ‘चतुरी चमार’ और ‘कुल्ली भाट’ मिलाकर पढ़ ले, पता चल जाएगा। देवी और उसके बच्चे की कहानी के कंट्रास्ट में निराला समाज के, राजनीति के विद्रूप को उभारते हैं-
“एक रोज मैंने देखा, नेता का जुलूस उसी रास्ते से जा रहा था। हजारों आदमी इकट्ठे थे। जय-जयकार से आकाश गूँज रहा था।… भीड़ में उसका बच्चा कुचल गया और रो उठा।… नेता दस हजार की थैली लेकर गरीबों के उपकार के लिए चले गये- जरूरी-जरूरी कामों में खर्च करेंगे।” व्यंग्य देखिए!
इन जरूरी कामों में देवी और उसके बच्चे का जीवन नहीं आता या उससे बाहर पड़ता है। फिर से निराला की कहानी ‘कुल्ली भाट’ याद आती है।
अब धर्मपरायण लोगों का व्यवहार देखिए और निराला क्या हैं, जानिए-
“एक दिन पगली के पास एक रामायणी समाज में कथा हो रही थी। मैंने देखा, बहुत से भक्त एकत्र थे। एतवार का दिन था। दो बजे से साहित्य-सम्राट गो. तुलसीदासजी की रामायण का पाठ शुरू हुआ, पाँच बजे समाप्त। उसमें हिंदुओं के मँजे स्वभाव को साहित्य-सम्राट गो. तुलसीदासजी ने और माँज दिया है, आप लोग जानते हैं! पाठ सुनकर, मँजकर भक्त मण्डली चली। दुबली-पतली ऐश्वर्य-श्री से रहित पगली बच्चे के साथ बैठी हुई मिली। एक ने कहा, इसी संसार में स्वर्ग और नरक देख लो। दूसरे ने कहा, कर्म के दण्ड हैं। तीसरा बोला, सकल पदारथ है जग माहीं, कर्महीन नर पावत नाहीं। सब लोग पगली को देखते, शास्त्रार्थ करते चले गये।”
हिंदुओं के मँजे स्वभाव को तुलसीदास ने और माँज दिया है। और, यह मँजा हुआ स्वभाव है क्या, तो भक्तिकाल पर मुक्तिबोध का लेख पढ़ना चाहिए इसके लिए! कई स्तरों पर मुक्तिबोध निराला के बढ़ाव हैं। हिंदुओं का मँजा हुआ स्वभाव और समझना हो, तो आज की सत्ता में बैठी हिंदूवादी सरकार का पूरा क्रिया-कलाप देख लें!
समर्थ रचनाकार अपनी रचना के माध्यम से समाज, राजनीति के चमकते रंगों के पीछे छिपी कालिमा को बाहर ला देता है। उसके भीतर के पाखंड, दिखावा, अमानवीयता को उद्घाटित कर देता है। समाज की बिगड़ी हुई तस्वीर के साथ- साथ इस तस्वीर को बिगाड़ने वालों को भी पहचानता है और उनकी असलियत को सामने लाता है। देवी और उसके बच्चे के माध्यम से निराला ने समाज के लोगों के व्यवहार की क्षुद्रता को भी व्यक्त किया है-
“मैंने हिंदू, मुसलमान, बड़े-बड़े पदाधिकारी, राजा, रईस सबको उस रास्ते में जाते समय पगली को देखते हुए देखा। पर किसी ने दिल से भी उसकी तरफ देखा, ऐसा नहीं देखा। जिन्हें अपने को देखने-दिखाने की आदत पड़ गयी है, उनकी दृष्टि में दूसरे की सिर्फ तस्वीर आती है, भाव नहीं…”
‘देखना’ निराला के यहाँ बहुत वस्तुनिष्ठ है। इसीलिए वे सामाजिक यथार्थ को उसके समूचेपन में रच पाते हैं। लेकिन इस देखने के पीछे करुणा, सहानुभूति, मानवता का भाव हो तभी वह रचना मनुष्य को बदलने की क्षमता रख पाती है। निराला ऐसे रचनाकार हैं, जिनके यहाँ अपार करुणा, सहानुभूति और मानवीयता है, इसीलिए निराला की रचनाएँ अपने भीतर प्रवेश किये को, वही नहीं रहने देती हैं, बल्कि उसे बदलने की प्रक्रिया में ले जाती हैं। यह प्रक्रिया सिर्फ पाठक के भीतर ही नहीं, खुद रचनाकार के भीतर चलती है। निराला ऐसे रचनाकार हैं और ‘देवी’ उनकी ऐसी रचना है। राष्ट्रीय आंदोलन और स्वाधीनता संघर्ष निराला की रचनाओं में अपनी तरह से आता है। ‘देवी’ कहानी के प्रसंग में वह आता है।
“दिन शहर में पल्टन का प्रदर्शन हो रहा था। पगली फुटपाथ पर बैठी थी।… सिपाही मिलिटरी ढंग से लेफ्ट-राइट, लेफ्ट-राइट दुरुस्त, दर्प से, जितना ही पृथ्वी को दहलाते हुए चल रहे थे, पगली उतना ही उन्हें देख-देखकर हँस रही थी। गोरे गम्भीर हो जाते थे।”
अंग्रेजों के शासन की शक्ति को निराला ने कैसे खोखला दिखा दिया है पगली की हँसी के द्वारा। ताकत पर निर्भर शासन का ऐसा ही रूप सामने आता है, जिसमें साधारण जन उसके भीतर का हिस्सेदार नहीं हो पाता। वह उस ताकत का, जिसका आतंक उसके सर पर है, प्रतिकार सीधे न कर पाये, लेकिन हँसकर उसके खालीपन को तो उघार ही देता है। यह काम वह साहित्य, वह रचना उतना नहीं कर सकती, जो पुराणों से चरित्रों को निकालकर, रचकर करने की कोशिश हो रही थी। उस शक्ति को उन हजारों, करोड़ों जीवित जनों में खोजना था, जिन्हें बहिष्कृत रखा गया था, उपेक्षित रखा गया था और जिनके ऊपर दोहरी गुलामी थोपी गयी थी। निराला का साहित्य यही करता है। वह उन्हीं में उस शक्ति की तलाश करता है। निराला ‘देवी’ रखते हैं कहानी का नाम। कहानी है पागल स्त्री की। जिसमें, निराला क्या देखते हैं-
“पगली का ध्यान ही मेरा ज्ञान हो गया। उसे देख कर मुझे बार-बार महाशक्ति की याद आने लगी। महाशक्ति का प्रत्यक्ष रूप संसार को इससे बढ़कर ज्ञान देने वाला और कौन सा होगा? राम, श्याम और संसार के बड़े-बड़े लोगों का स्वप्न सब इस प्रभात की किरणों में दूर हो गया। बड़ी-बड़ी सभ्यता, बड़े-बड़े शिक्षालय चूर्ण हो गये। मस्तिष्क को घेरकर केवल यही महाशक्ति अपनी महत्ता में स्थित हो गयी। उसके बच्चे में भारत का सच्चा रूप देखा, और उसमें- क्या कहूँ, क्या देखा।”
पौराणिक आख्यानों से अलग साधारण जनों में शक्ति का संधान ही निराला के साहित्य का लक्ष्य है। निराला के रचनात्मक संघर्ष का इससे सीधा संबंध है। निराला के यहां भारत इन्हीं साधारण जनों में अभिव्यक्त होता है, उसी में दिखता है, न कि किसी मिथ्या सांस्कृतिक अतीत में। हिंदी नवजागरण में निराला इसीलिए सबसे अधिक संघर्ष उठाते हैं, लेकिन ऐसा फर्क पैदा कर देते हैं, जिससे हिंदी साहित्य की आगे की दिशा तय होती है।