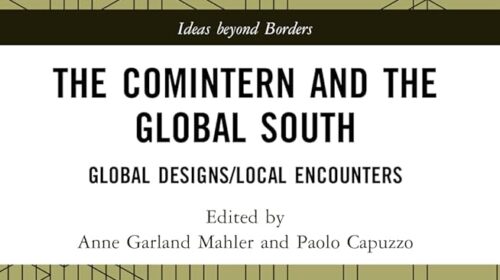निराला के जन्मदिन(बसंत पंचमी) के अवसर पर प्रस्तुत लेख
निराला के लेखन में राष्ट्र निर्माण, स्वाधीनता, धर्म, भाषा व जाति-वर्ण आदि को रचनात्मक ढंग से तो अभिव्यक्ति मिली ही है, लेकिन निराला ने अपने वैचारिक लेखन में भी इस पर खूब चिन्तन किया है। इसमें राष्ट्र निर्माण का सवाल महत्वपूर्ण है।
निराला राष्ट्र निर्माण को आधुनिक मूल्यबोध एवं दुनिया की नवीन सभ्यता के जोड़ में देखना चाहते हैं। अर्थात, निराला के समस्त चिंतन में यह बात बहुत केन्द्रीय रूप से उपस्थित मिलेगी कि भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई में संसार की नवीन सभ्यता के अनुकूल नवीन सामाजिक संगठन के निर्माण पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
निराला क्रमशः इस विचार पर पहुंचते हैं, कि भारत में धर्म, भाषा, वर्ण की जो सामाजिक-सांस्कृतिक अवस्थिति है, वह नवीन सभ्यता के मेल में नहीं है। इसीलिए निराला जातीयता, भाषा, धर्म तथा जाति-वर्ण की समस्या पर अपने लेखन में विचार करते हैं।
निराला मानते हैं, कि जाति, वर्ण, धर्म, भाषा का निर्धारण करने वाली सामाजिक शक्तियों में वह क्षमता ही नहीं है, कि वह नवीन सामाजिक संगठन का निर्माण कर सके। वे शक्तियाँ अपना स्वत्व खो चुकी हैं और प्राचीन समय में बनाये गये सामाजिक संगठन को बनाये रखने में अपनी सारी उर्जा लगा रहे हैं, जो अब भारत के नवीन निर्माण में बाधक है। इसी क्रम में वे जाति एवं वर्ण-व्यवस्था पर विचार करते हैं।
निराला हिंदी नवजागरण में इन सवालों पर विचार करने वाले अलग ही व्यक्तित्व वाले लेखक हैं। अपने समय में जाति-वर्ण पर विचार करने वाले हिंदी के विरल लेखक हैं। निराला के साथ प्रेमचंद ही हैं, जो इन समस्याओं से रूबरू होते हैं। खैर
निराला ने जिन लेखों और टिप्पणियों में जाति-वर्ण पर विचार किया है, उसमें मुख्य रूप से ‘वर्णाश्रम धर्म की वर्तमान स्थिति’, ‘वर्तमान हिंदू समाज’, ‘भारत के नवीन प्रगति में सामाजिक लक्ष्य’, ‘सामाजिक पराधीनता’, ‘हमारा समाज’, ‘हिंदू धर्म के प्राथमिक सिद्धांत’, ‘हमारे समाज का भविष्य रूप’, ‘मनुष्य गणना और जात-पाँत’, ‘हिंदुओं का जातीय संगठन’, ‘महात्माजी और हरिजन’, ‘सनातन धर्म और अछूत’, महत्वपूर्ण है।
इन लेखों और टिप्पणियों में जाति-वर्ण पर विचार करते समय निराला किसी एक निष्कर्ष पर न रहकर समय के सापेक्ष व नवीन विचारों के सम्पर्क से बदलते हैं। 1929-30 ई. के आस-पास निराला जाति-वर्ण की समस्या का जो समाधान देखते हैं, 1940 तक आते-आते वह बहुत बदल जाता है।
1920 ई. से 1930 ई. तक निराला की विश्व दृष्टि या सामाजिक दर्शन पर दो प्रभाव अधिक दिखते हैं। एक, शंकर का वैदान्तिक साम्य और दूसरा विवेकानंद का वेदान्तिक दर्शन।
यह विवेकानंद का ही प्रभाव है, जिसमें निराला यह मानते हैं, कि पराधीन या गुलाम देश में सभी शूद्र हैं। आजादी की लड़ाई की अग्रगति और भावी राष्ट्र निर्माण की बुनियादी समस्याओं का समाधान पाने के लिए निराला इन दो दर्शन या विचार के पास जाते हैं। समस्या थी, आजादी की लड़ाई के एक राष्ट्रीय स्वरूप के न होने की। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तीनों स्तरों पर एकरूपता नहीं थी। जो स्वाधीनता संघर्ष के लिए एक स्तर तक जरूरी तत्व था।
भाषा, जाति, धर्म इन तीन स्तरों पर विभाजन इस कदर था, कि वह राष्ट्रीय आंदोलन और नवीन सामाजिक प्रगति में बाधक हो रहा था। आधुनिक राष्ट्र निर्माण की दिशा में भारत की तात्कालिक स्थिति को निराला समस्याग्रस्त पाते हैं। इसी का समाधान वे वेदान्तिक साम्य में पाने जाते हैं।
जाति-वर्ण की समस्या जो बंगाल में देखकर निराला आये थे, उससे बहुत भिन्न और जटिल रूप हिंदी-उर्दू पट्टी में वे क्रमशः पाते हैं।
बंगाल में तब सामाजिक सुधार का एक चरण पूरा हो गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना के लगभग सौ साल हो चुके थे। विवेकानंद का आगमन हो चुका था। लेकिन हिंदी-उर्दू क्षेत्र में 1920 ई. के बाबा रामचंद्र के किसान आंदोलन से पहले किसी भी आंदोलन की अंतर्वस्तु में सामाजिक सुधार नहीं था। आज तक इस हिन्दी-उर्दू पट्टी में कोई सामाजिक सुधार आन्दोलन नहीं हुआ। वह महात्मा गांधी के कुछ सामाजिक सुधारों के आह्वान से क्षीण ढंग से जुड़ा रहा, लेकिन समाज में कोई अंतर वह नहीं कर पाया। इसे आजादी के पहले की हिन्दी क्षेत्र में बनी कांग्रेस की प्रान्तीय सरकारों के नेतृत्व में रहे लोगों से बखूबी समझा जा सकता है। बहरहाल
निराला हिन्दी क्षेत्र में जाति-वर्ण की समस्या के समाधान के लिए शंकर के वेदान्तिक दर्शन से प्रारंभ करते हैं। लेकिन अगले दस साल में यह दर्शन टिकता नहीं। ‘चतुरी चमार’, ‘देवी’ और ‘कुल्ली भाट’ इसके रचनात्मक प्रमाण हैं। ‘देवी’ कहानी को तो निराला के तीव्र मोहभंग की रचना के रूप में जाना जाता है।
निराला ने जाति-वर्ण की समस्या पर पहला लेख ‘वर्णाश्रम धर्म की वर्तमान स्थिति’ लिखा। यह 1929 ई. का लेख है और ‘माधुरी’, मासिक, लखनऊ में दिसंबर में छपा है। इसमें निराला लिखते हैं,
“इधर माधुरी में वर्ण व्यवस्था पर जितने लेख निकले हैं, उनमें से कोई भी लेख ऐसा नहीं, जो विवर्तित समय की मौलिकता या नवीन युग का यथार्थ तत्व समझाता हुआ वर्ण-व्यवस्था की एक विचार पुष्ट व्याख्या कर रहा हो। सब-के-सब अपनी ही धुन में लीन, अपने ही अधिकार के प्रतिपादन में नियोजित हो रहे हैं। शूद्रों के प्रति केवल सहानुभूति प्रदर्शन कर देने से ब्राह्मण-धर्म की कर्तव्यपरता समाप्त नहीं हो जाती, न ‘जाति- पाँति तोड़क मंडल’ के मंत्री संतरामजी के करार देने से इधर दो हजार वर्ष के अंदर का संसार का सर्वश्रेष्ठ विद्वान महा मेधावी त्यागीश्वर शंकर शूद्रों के यथार्थ शत्रु सिद्ध हो सकते हैं। शूद्रों के प्रति उनके अनुशासन कठोर से कठोर होने पर भी अपने समय की मर्यादा से दृढ़ संबद्ध हैं।”
यहां निराला नवीन समय के यथार्थ तत्व के सापेक्ष वर्ण व्यवस्था की व्याख्या की बात करते हैं, लेकिन शंकर के वर्ण व्यवस्था के कठोर से कठोर अनुशासन को समय की मर्यादा से दृढ़ संबद्ध भी बताते हैं।
इस समय तक निराला के भीतर भी वही अंतर्विरोध मिलते हैं, जो हिंदी नवजागरण के अंतर्विरोध थे, राष्ट्रीय आन्दोलन के अंतर्विरोध थे। भारतीयता की अवधारणा को संस्कृत के धर्मशास्त्रों और वैष्णव केन्द्रित हिन्दू दर्शन के अंतर्गत सीमित किया गया।
इस अवधारणा में औपनिवेशिक सत्ता द्वारा साम्प्रदायिक विभाजन हेतु भारतीयता की झूठी, मनगढंत अवधारणा भी जिम्मेदार थी। निराला प्रारम्भ में इसी से प्रभावित हैं लेकिन निराला उससे निकलते हैं।
आगे के एक लेख में तो निराला अंग्रेजी शासन को, जाति-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं।
निराला के साथ एक और बात थी, वह यह कि वे बांग्ला नवजागरण की उपलब्धियों से भी संबद्ध थे। इसलिए उनमें वर्ण व्यवस्था की पुरातन नैतिकता की तीखी आलोचना भी साथ-साथ मिलती है। वर्ण-व्यवस्था को उदारता के साथ न्यायोचित ठहराने की नवजागरण की प्रवृत्ति से निराला क्रमशः भिन्न होते जाते हैं।
इसी लेख में वे लिखते हैं, कि ‘जायते वर्णसंकर’ के प्रमाण से वर्ण-व्यवस्था की सार्थकता नहीं दीख पड़ती। लेकिन इसी के साथ निराला संतरामजी के ‘जाति-पाँत तोड़ो मंडल’ की आवश्यकता को भी नकारते हैं। निराला प्रस्तावित करते हैं, कि जाति-पाँति तोड़ो मंडल की जगह जाति-पाँति योजक मंडल की जरूरत है। वे लिखते हैं, कि तोड़ ही हिन्दोस्तान को तोड़ रहा है, जबकि जरूरत जोड़ने की है। हालांकि इसके बाद के अपने लेख में निराला सन्तरामजी के प्रयास को ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन के सामाजिक सुधार के साथ रखकर देखते हैं। लेकिन अपने इस लेख में शंकर को शूद्र विरोधी बताने के सन्तरामजी की बात से निराला सहज नहीं हैं। यह शंकर के वेदान्तिक साम्य के प्रति निराला का विश्वास ज्यादा गहरा होने के चलते होता है।
इस समय तक हिंदी क्षेत्र के जाति विभाजन और वर्ण व्यवस्था के निचली जातियों पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव को निराला नहीं जान पाते हैं। जाति भेद का दंश झेल रहे और वर्ण व्यवस्था की मार से पीड़ित जातियों से कोई व्यावहारिक साबका निराला का नहीं पड़ा था। लेकिन जब वह इसके संपर्क में जाते हैं, तो अपने इस समाधान की सीमा जान-समझ जाते हैं।
यद्यपि कि 1929 में यह लेख लिखते समय निराला वेदान्तिक साम्य के विचार से इस कदर प्रभावित थे, कि वह उसे सभी विचार और वाद से श्रेष्ठ बताते हैं। निराला लिखते हैं,
“भारतवर्ष को मुक्त की ओर ले जाने वाले आज तक जितने भी विचार देखने में आए हैं, वे राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक, सामाजिक किसी भी दिशा में झुकाए गए हों, वेदान्तिक विचार की समता नहीं कर सकते।… कोई वाद ऐसा नहीं, जो जाति, देश या समाज को पूर्ण स्वतंत्रता तक पहुंचा सके- जहां किसी प्रकार का विरोध न हो। भारतवर्ष की समाज-श्रृंखला उसी वेदांतिक धातु से मजबूत की गयी है।”
इसी में आगे निराला लिखते हैं, कि अगर कोई ‘वेदांत को नहीं मानता तो वह भारतीय कहलाने का दावा नहीं कर सकता।’
वेदांत संबंधी निराला के इस विचार को निरपेक्ष मान लेने से निराला को समझने में दिक्कत होगी। निराला बंगाल से हिंदी में आए थे। निराला के ऊपर विवेकानंद का प्रभाव उसमें बहुत था। उन्होंने दो लेख ही लिखे, जिसके शीर्षक हैं, ‘वेदांत केशरी स्वामी विवेकानंद’ व ‘वेदांत केसरी स्वामी विवेकानंद और भारत’। पहला लेख ‘समन्वय’, मासिक, कोलकाता में, फरवरी-मार्च 1928 ई. का छपा है और दूसरा ‘हंस’, मासिक, काशी स्वदेशांक, अक्टूबर-नवंबर 1932 ईस्वी में छपा है।
इन लेखों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि विवेकानंद द्वारा वेदांत की जो व्याख्या की गयी, शूद्र की जो व्याख्या और अवधारणा प्रस्तुत की गयी, वर्ण धर्म और हिंदू धर्म के पाखंड की जो आलोचनाएं उनके द्वारा की गयी, निराला उससे प्रभावित थे।
विवेकानंद का यह प्रभाव सिर्फ निराला तक सीमित नहीं था। राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व पर भी इसका असर था। विवेकानंद की व्याख्या से हिंदूवादियों ने भी अपने पक्ष में हिंदू धर्म को श्रेष्ठ मानने के प्रमाण जुटाये।
आशय यह, कि निराला ने भी विवेकानंद से वेदांत को श्रेष्ठ मानने के प्रमाण लिए लेकिन उनके संदर्भ अलग थे। इसमें भी निराला विवेकानंद की सीमा जानते हैं। वे लिखते हैं कि विवेकानंद के विचार ज्ञान के स्तर पर अधिक हैं, व्यवहार के स्तर पर कम। फिर भी निराला मानते हैं कि विवेकानंद के विचारों ने सामाजिक सुधार और नवीन सामाजिक संगठन के निर्माण में योग दिया। ठीक यही शंकर के वेदान्तिक साम्य को लेकर भी है। ज्ञान क्षेत्र में ही सही, वेदान्तिक दर्शन में प्रस्तुत साम्य के विचार से वे प्रभावित थे, क्योंकि इसमें सभी जातियों को भक्ति का समान अवसर दिया गया था। इसे निराला जाति-भेद के समाधान के रूप में देखते हैं। मजेदार यह है, कि निराला खुद भी यह मानते हैं कि शंकर ने बौद्ध धर्म के निचली जातियों पर बढ़ते प्रभाव को रोकने और वैष्णव धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए ऐसा किया। खैर,
निराला का वेदान्तिक झुकाव जाति भेद को समाप्त करने के लक्ष्य से ज्यादा प्रेरित है। इस लेख के आखिर में वे लिखते हैं,
“वृद्ध भारत की वृद्ध जातियों की जगह धीरे-धीरे नवीन भारत की नवीन जातियों का शुभागमन हो, इसके लिए प्रकृति ने वायुमंडल तैयार कर दिया है। यदि प्राचीन ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियां उनके उठने में सहायक न होंगी तो जातीय समर में अवश्य ही उन्हें नीचा देखना होगा।… इन्हीं की अजेय शक्ति भविष्य में भारत को स्वतंत्र करेगी।”
इसी बात को वे अपने अगले लेख
‘वर्तमान हिंदू समाज’ में आगे बढ़ाते हैं। इस लेख में निराला नई सभ्यता के अनुकूल सामाजिक-सांस्कृतिक विचार के अंतर्गत ब्रह्म समाज का विस्तार से जिक्र करते हैं। वह मानते हैं कि ब्रह्म समाज में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं था। ब्रह्म समाज ने एक स्तर पर नई सभ्यता के अनुकूल सामाजिक साम्य स्थापित करने में मदद की। इस क्रम में वे विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन के कार्यों को गिनाते हैं। इसमें सभी जातियों को समान अधिकार मिले थे। रामकृष्ण के जन्म के अवसर पर विवेकानंद सभी जातियों को एक ही पंक्ति में बैठकर प्रसाद पाने को आमंत्रित करते हैं।
निराला लिखते हैं, कि वहां वर्ण भेद नहीं है। जात-पात का झमेला यहाँ नहीं मानते। यहां पुनः निराला ‘जाति-पाँति तोड़क मंडल’ का इसी क्रम में जिक्र करते हैं। लेकिन इसमें वे संतरामजी के प्रति उदार हैं। वे लिखते हैं,
“आज जाति-पाँति तोड़क मंडल’ को स्थूल रूप से भी जाति-पाँति की आवश्यकता नहीं देख पड़ती। संतरामजी की पूरअसर बातें निष्पक्ष पाठकों के हृदय में पूरी सहानुभूत पैदा कर रही हैं। अन्त्यजों की शिक्षा-दीक्षा तथा अधिकारों की वृद्धि भी क्रमशः होती जा रही है। महात्माजी ने भी अन्यजों के लिए बहुत कुछ कहा है।”
इसके बाद फिर से वे विवेकानंद को उनके इस कथन से याद करते हैं,
“ऐ भारत के उच्च वर्ण वालों, तुम्हें देखता हूँ, तो जान पड़ता है, चित्रशाला में तस्वीरें देख रहा हूँ। तुम लोग छायामूर्तियों की तरह विलीन हो जाओ, अपने उत्तराधिकारियों को (शूद्रों को) अपनी तमाम विभूतियाँ दे दो, नया भारत जग पड़े।”
इस लेख में असवर्ण विवाह को लेकर पिछले लेख में जो असहमति निराला ने प्रकट की थी, उसमें भी बदले हुए विचार दिखते हैं। निराला लेख के आखिर में लिखते हैं,
“वर्तमान सामाजिक स्थिति पूर्ण मात्रा में उदार न होने पर भी विवाह आदि में जो उल्लंघन कहीं-कहीं देखने को मिलते हैं, वे भविष्य के ही शुभचिन्ह प्रकट कर रहे हैं। संसार की प्रगति से भारत की घनिष्ठता जितनी ही बढ़ेगी, स्वतंत्रता का ब्राह्म रूप जितना ही विकसित होगा, असवर्ण विवाह का प्रचलन भी उतना ही होता जाएगा।… वर्ण समीकरण की इस स्थिति का ज्ञान विद्या के द्वारा ही यहां के लोगों को हो सकता है। इसके साथ ही साथ नवीन भारत का रूप संगठित होता जाएगा, और यही समाज की सबसे मजबूत श्रृंखला होगी।”
1931 ई. की टिप्पणी ‘हमारे समाज का भविष्य रूप’ में निराला लिखते हैं,
“आज ब्राह्मण-विचार, पुरानी परिपाटी जितने अंशों में यहां है, देश उतने ही अंशों में पराधीन है, और नवीन मानव धर्म जितने अंशों में, उतने ही अंशों में देश स्वतंत्रता-प्रेमी।”
नवीन मानव धर्म अर्थात जिसमें जाति भेद न हो। आगे वे लिखते हैं,
“स्वतंत्रता किसी ख़ास जाति या ख़ास मनुष्य के लिए नहीं होती। यदि कोई भंगी शिक्षा के उच्च शिखर पर पहुंचे, और यथार्थ शिक्षा अर्जित करे, तो क्या उसके लिए भंगी-शब्द का प्रयोग ही रह जाएगा?… वह कौन सी वृत्ति है, जो योग्य को योग्य नहीं समझती?- अपनी महामूर्खता, महानीचता को केवल जन्मगत अधिकार के दावे पर दबा रखती है? इसी का नाश करना है। किसी मनुष्य का नहीं। तब जाति आप मर जाएगी। फिर मिठाई बेचकर राजाराम मिश्र किसी आर्ट्स के मास्टर नाई को डांट नहीं सकते। रही बात संस्कृति की, सो नाई एम.ए होकर संस्कृत नहीं हुआ और मिश्रजी मिठाई बेचते हुए सुसंस्कृत हैं, इससे बड़ी मूर्खता दूसरी हो नहीं सकती।”
निराला नवीन सामाजिक संगठन को इसी रूप में देखते हैं, अर्थात शूद्र अगर कर्म से श्रेष्ठ है, तो वह शूद्र नहीं और ब्राह्मण अगर कर्म से च्युत है, तो वह ब्राह्मण के रूप में प्राप्त सामाजिक अधिकार का हकदार नहीं।
निराला की यह बात रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा बार-बार हर अवस्था में ब्राह्मण को पूज्य बताने से उलट है। निराला ने एक टिप्पणी ही ‘अधिकार समस्या’ नाम से लिखी है। यह ‘सुधा’, अर्धमासिक, लखनऊ में 1 दिसम्बर 1933 को छपी है। इसमें वे लिखते हैं,
“अधिकारवाद भारत में महाभारत के समय से प्रबल होने लगा था, और भारत के वर्णाश्रम-धर्म के भीतरी अधिकार भी तभी से और अधिक दृढ़ होकर वर्णाधिकारों के शासन में जड़ जमा रहे थे। बौद्धयुग इन्हीं भावनाओं का विरोधकाल है। पर तब तक चूँकि देश का शासन देश ही में था, इसलिए कर्मकाण्ड के अधिकारी शासक तत्कालीन वर्ण-व्यवस्था की रक्षा के लिए तत्पर रहे थे, हम पहले लिख चुके हैं, संस्कृत-साहित्य में पुराणयुग का प्राबल्य इसका फल है- व्यास, कालिदास, श्रीहर्ष तक में इसी वर्णाश्रमधारा की पुष्टि मिलती है।”
निराला संस्कृत साहित्य के बारे में यह कहने का साहस रखने वाले लेखक हैं। जबकि, पूरा हिन्दी नवजागरण संस्कृत साहित्य के वर्णधर्म की रक्षा वाले पक्ष पर बोलता ही नहीं। निराला आगे लिखते हैं, जो उनके चिन्तन की केन्द्रीय बात है,
“पर अब वह समय नहीं रहा। अब प्रकृति ने वर्णाश्रम-धर्म के सुविशाल स्तम्भों को तोड़ते-तोड़ते पूर्ण रूप से चूर्ण कर दिया है।…अब कोई मूर्ख ही इसका अस्तित्व स्वीकार करेगा।”
इसीलिए निराला बार-बार लिखते हैं, कि ऊपर के वर्ण एक सुप्तावस्था में हैं, जो नवीन सभ्यता की बजाय पुरातन सभ्यता को बनाये रखने के भ्रम में हैं। इसीलिए निराला लिखते हैं, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण में वह शक्ति नहीं कि वह कोई नवीन सामाजिक संगठन का निर्माण कर सके। अब वर्णाश्रम धर्म ‘अपने घरों में सोते हुओं के स्वप्नों के सदृश’ ‘पहले की जागृति के संस्कार-रूप, छायादेह मात्र रह गया’ है। ‘दूसरी जागृति में वह भ्रम ही साबित होगा।’
इसके बाद निराला इसी में आगे लिखते हैं,
“जिस तरह एक ओर प्रकृति वर्णाश्रम-धर्म को तोड़ रही थी, उसी तरह दूसरी ओर वह शूद्र-शक्ति के अभ्युत्थान की तैयारी कर रही थी। अधिकार-भोग पर मनुष्य-मात्र का बराबर दावा है। जो यह समझता है, हम बड़े हैं, हम छोटे न होंगे, उसे मनुष्य कहलाने में बड़ी देर है। जो यह समझता है, बड़ा छोटा और छोटा बड़ा हो सकता है, उसे यह मानने में भी कोई आपत्ति न होगी कि शूद्र भी कर्मानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो सकते हैं। शूद्रों के इसी अधिकार पर भारत का भविष्य जातीय संगठन अवलम्बित है।…यही साम्य स्थिति की वर्तमान उद्भावना कहती है।”
नवीन सामाजिक संगठन सम्बन्धी अपने इन्हीं विचारों के सन्दर्भ में निराला राजनीतिक यथार्थ को भी जांचते हैं। वहां भी निराला अन्य हिन्दी लेखकों से भिन्न हैं। पृथक निर्वाचन को लेकर निराला की टिप्पणी ध्यान देने की है। वे लिखते हैं,
“सरकार ने राजनीति की यह बड़ी टेढ़ी मार दी है। यहीं- इसी अछूत समस्या के पास हिंदुओं की तमाम प्राचीन कमजोरियाँ एकत्र हैं।… यह पृथक- निर्वाचन- समस्या जब से खड़ी हुई तमाम राजनीति का रुख ही बदल गया। पर यह अच्छा ही हुआ। अब सुधार ठीक जड़ पर पहुंचा है।”
यह टिप्पणी ‘हिंदुओं का जातीय संगठन’ शीर्षक से 1932 नवंबर में ‘सुधा’ की संपादकीय में छपी है। इसी तरह महात्मा गांधी के अछूतोद्धार कार्यक्रम के लिए निराला अपनी दो टिप्पणी ‘महात्माजी और हरिजन’ ‘सुधा’ अर्धमासिक, लखनऊ 16 अगस्त 1933 तथा ‘सनातन धर्म और अछूत’ (वही 16 नवंबर 1933) में अपील करते हैं, कि ‘इससे सहानुभूति ही नहीं- इसकी सिद्धि के लिए जहाँ तक हो, मदद करें…।’
निराला ने ‘समाज और मनुष्य’, ‘सामाजिक व्यवस्था’ समेत कई अन्य टिप्पणियों में स्वाधीनता आंदोलन और भावी आधुनिक, नवीन राष्ट्र निर्माण के संदर्भ से जाति और वर्ण पर विचार किया है। जितने संदर्भ दिए गये, वे 1933 तक के हैं।
1933 की ही एक टिप्पणी ‘राजनीति के लिए सामाजिक योग्यता’ में निराला की भाषा का अन्दाज बहुत कुछ बयां करता है,
“हम बहुत पहले से कह रहे हैं, समाज का आमूल परिवर्तन जरूरी है।…वैश्य-शक्ति, राज-शक्ति, ब्राह्मण-शक्ति तीनों योरप को गयीं। हम इस बात को न समझकर, ब्राह्मण बनकर, भारतीय संस्कृति के एकच्छत्र सम्राट होकर भाइयों पर खोखली भारतीयता का रोब गाँठते रहें। अब उस भारतीयता से कैसा फल पैदा हुआ, वह सामने है, चखिए।”
फिर आगे लिखते हैं,
“जो ब्राह्मण और क्षत्रिय अपनी वर्णोच्चता का ढोंग भी नहीं छोड़ सकते, अपने ही घर के अंत्यजों को अधिकार नहीं दे सकते, भारतीयता के अंधेरे में प्रकाश देखने के आदी हैं, वे बिना दिये हुए कुछ पाने का विचार कैसे रखते हैं? उनकी सामाजिक नीचता ‘समाज’-शब्द को, उन्नतिशीलता के अर्थ को कैसे पुष्ट कर सकती है? हमारी राजनीतिक दुर्बलता यहीं पर है। यहीं से हमें समाज-जातीय समाज-भारतीय समाज की नींव डालनी है। उसी की मजबूती हमारे राष्ट्र की दृढ़ता है।”
निराला राजनीतिक संघर्ष के लिए नवीन सामाजिक योग्यता की बात करते हैं। समाज के आमूल परिवर्तन की बात करते हैं। इसी में वे लिखते हैं,
“जो समाज पुराना, हारा हुआ है, वह कितनी भी प्राचीन विभूतियों से युक्त हो, वह नवीन युग के लिए मृत है। उसी से पहले हमें लड़ना था, लड़कर पराश्त करना था। पराश्त कर नये समाज को सजीव और बहुजनोंवाला बनाना था। तब हम राष्ट्र का पहला सोपान तय करते। इसी समाज से राष्ट्र को बल मिलता। यही समाज राष्ट्र का समाज है। जो लोग यह तर्क उपस्थित करते हैं, कि इस तरह भ्रष्टाचार पैदा होगा(सामाजिक भ्रष्टाचार, जोर मेरा), वे मूर्ख हैं, फिर कहिए, हम फिर कहते हैं, वे मूर्ख हैं। अगर आप नहीं जानते, तो विश्वास कीजिए, वे मूर्ख हैं। जो मनुष्य देश के सभी मनुष्यों को अपने बराबर समझता है, वह अगर भ्रष्टाचार फैलाता है, तो मनुष्य की उच्चता का, सदाचार का कोई प्रमाण नहीं। ”
सामाजिक समता, समानता के विचार को आज भी कौन लोग हैं, जो उसे सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन मानते हैं! कौन लोग हैं, जो आजादी के बाद संविधान में शामिल सामाजिक बराबरी के विचार से अपार घृणा करते हैं! कौन लोग हैं, जो भारतीयता को पतित, मनुष्यविरोधी वर्णवादी मूल्यों, सनातनी मूल्यों से परिभाषित कर रहे हैं! यह जान-समझ लेने पर निराला कहाँ खड़े हैं, इसे सहज समझा जा सकता है। ऐसे लोग 1930 के दशक में पूरे जोर, दमखम से सक्रिय थे, और निराला उनसे मुखातिब थे।
निराला इसी टिप्पणी में आगे लिखते हैं,
“इसलिए तोड़़कर फेंक दीजिए जनेऊ, जिसकी आज कोई उपयोगिता नहीं, जो बड़प्पन का भ्रम पैदा करता है, और समस्वर से कहिए कि आप उतनी ही मर्यादा रखते है, जितनी आपका नीच-से-नीच पड़ोसी, चमार या भंगी रखता है। तभी आप महामनुष्य हैं। …एक समाज आपको च्युत करेगा, तो आपको दूसरा समाज मिलेगा। उसी समाज से आप साबित कर सकेंगे, आप समाज से नहीं बढ़े, समाज आपसे बढ़ा है। यहीं से राष्ट्र की वृद्धि है, शक्ति है, उत्थान है, गति है। सब सुधार, सारी शिक्षा, कुल वैमनस्य का प्रतिरोध यही है। आज का सच्चा भारतीय यही है।”
यह टिप्पणी है 1933 ई. की। 16 अगस्त, ‘सुधा’ अर्धमासिक, लखनऊ। इसके बाद निराला का वैचारिक लेखन कम होने लगता है और रचनात्मक गद्य साहित्य आता है, जिसमें उनका जाति एवं वर्ण संबंधी विचार और स्पष्ट होकर आया है। ‘देवी’, ‘चतुरी चमार’, कुल्ली भाट’ इस संदर्भ से महत्वपूर्ण है। निराला वेदांतिक दर्शन से आगे इन रचनाओं में जाते हैं। ‘कुल्ली भाट’ में कुल्ली के अछूतों के लिए खोले स्कूल में जाने के बाद नैरेटर या कथावाचक के आत्मस्वीकार से कोई गुजरे तो उसे निराला के बदले विचार को समझने में संकट नहीं होगा। खैर
जैसा कि लेख के प्रारम्भ में जिक्र हो आया है, कि निराला सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध वेदान्तिक दर्शन के ज्ञानक्षेत्र में स्थापित साम्य के विचार को अपना प्रस्थान बिंदु बनाते हैं, उससे जो संदर्भ निराला लेते हैं, उसका लक्ष्य जाति भेद का विरोध ही है।
वर्ण संबंधित निराला का जो विचार है, वह यही है कि गुलाम देश में सभी शूद्र हैं। लेकिन बाद में इसमें भी वे आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं, कि गुलामी के भीतर जो जाति की गुलामी है उसे समाप्त किए बिना नवीन सभ्यता के बराबर देश नहीं आ सकता। वे लिखते हैं,
“गुलामों की एक जाति होती है, चाहे अंग्रेजी ढंग से कह लीजिए या हिंदोस्तानी ढंग से। पर जब गुलामों के भीतर भी गुलाम जातियां निकलती रहती हैं, तब समझना चाहिए कि गुलामी के कितने पेच काटकर उससे निकलने की जरूरत है।”
निराला जाति-वर्ण पर विचार करते हुए हिंदी नवजागरण के अंतरविरोधों से बहुत आगे जाते हैं और सामाजिक एकता, साम्य के लिए जाति भेद, वर्ण विभाजन आदि को खत्म कर नवीन सभ्यता, नवीन सामाजिक संगठन बनाने पर विचार करते हैं। वे ऐसा करने वाले हिंदी के बिलकुल अलहदा लेखक, विचारक, रचनाकार हैं!