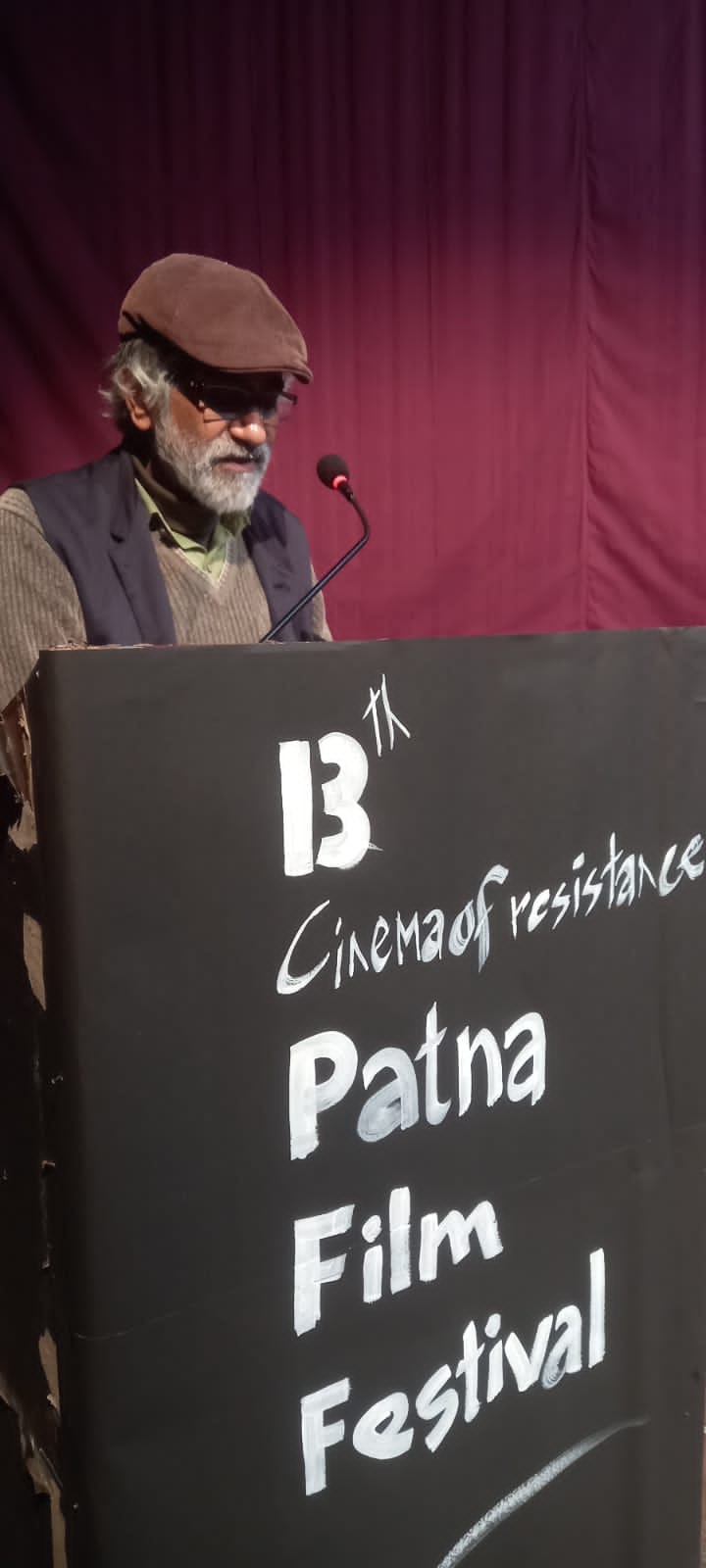निराला बंगाली जातीयता से प्रभावित थे। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस, देवेन्द्र नाथ टैगोर, रवीन्द्र नाथ टैगोर, विवेकानंद के अलावा बंगाल के इस जागरण में जितने भी लोगों ने योगदान किया, निराला उन्हें अक्सर यथा अवसर याद करते हैं।
निराला जब अपने घर उन्नाव वापस आते हैं, तो वे क्रमशः हिंदी से परिचय बढ़ाते हैं। हिन्दी में कविताएं लिखना शुरू करते हैं। हिन्दी सीखने में निराला की पत्नी मनोहरा देवी का अधिक योगदान था।
प्रारंभ में वे उन्नाव, डलमऊ, लखनऊ में ही अधिक रहते हैं। 1935 ई. के बाद प्रायः इलाहाबाद ही उनका रहना हुआ। बनारस को भी इसमें शामिल कर लिया जाए और कानपुर को ले लिया जाए, तो हिंदी का बहुतायत लेखन यहीं से हो रहा था। लेकिन निराला हिंदी में हो रहे तत्कालीन लेखन से प्रभावित नहीं होते। बल्कि, बंगाल के प्रभाव में वे अधिक रहते हैं।
रवीन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं पर निराला ‘रवीन्द्र कविता कानन’ शीर्षक से लम्बा लेख लिखते हैं। रवीन्द्र-साहित्य में बंगाली जातीयता के तत्व के साथ विश्व मानवतावाद की भावना को निराला महत्व देते हैं और इसे ही खुद के साहित्य के लिए एक लक्ष्य भी बनाते हैं।
‘रवीन्द्र कविता कानन'(1929) के अलावा ‘कविवर बिहारी और रवीन्द्र’ (मतवाला, साप्ताहिक, कलकत्ता, 24 मई, 1924), ‘दो महाकवि गो. तुलसीदास और रवीन्द्रनाथ'(मतवाला, साप्ताहिक, कलकत्ता, मार्च-अप्रैल, 1929), ‘महाकवि रवीन्द्रनाथ की कविता'(सुधा, मासिक, लखनऊ, अगस्त, 1929), ‘शेली और रवीन्द्रनाथ'(सुधा, मासिक, लखनऊ, मई, 1930), ‘शेली और रवीन्द्रनाथ का दर्शन'(सुधा, मासिक, लखनऊ, जुलाई, 1930) ‘तुलसीदास और रवीन्द्रनाथ'(सुधा, मासिक, लखनऊ, जनवरी 1931) शीर्षक लेख और टिप्पणियाँ रवीन्द्र-साहित्य के प्रति निराला के लगाव का पता देती हैं।
इसी तरह रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद पर भी निराला ने कई लेख व टिप्पणियाँ लिखी हैं। यह सभी लेख 1930-32 तक के हैं। निराला रवीन्द्र-साहित्य में पूर्व और पश्चिम की सांस्कृतिक उपलब्धियों का सुन्दर संयोजन पाते हैं। वे रवीन्द्र नाथ टैगोर को युग-प्रवर्तनकारी मानते हैं।
इसके साथ रामकृष्ण परमहंस के दर्शन और विचार में वे भेद रहित मनुष्य और उसकी मुक्ति के भाव को देखते हैं। बंगला साहित्य के उत्कर्ष पर सोचते हुए वे पाते हैं, कि ‘बंगालियों ने ज्ञान को ही अपने साहित्यिक उत्थान का मूल माना।’ इसी तरह स्त्रियों की स्वतंत्रता में वे ब्रह्म समाज का सबसे बड़ा श्रेय मानते हैं।(साहित्य का विकास, 1932)
निराला मूल्य, नैतिकता, चेतना के धरातल पर ऐसे ही तत्वों की तलाश करते हैं, जिससे हिंदी समाज की ऐसी अस्मिता बने, जो आधुनिक हो और जिसका अपना सांस्कृतिक सत्व हो।
इस सांस्कृतिक सत्व और आधुनिकता के साथ निराला इसमें विश्व मानवतावाद की भावना के होने पर भी जोर देते हैं। निराला चाहते हैं कि हिन्दी समाज इन तत्वों के साथ ही भारत की अन्य राष्ट्रीयताओं के साथ सहयोगी बन आजादी व राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे।
इसे ही निराला हिंदी जातीयता और हिन्दी की सांस्कृतिक पहचान के रूप में पाना या देखना चाहते हैं। इसमें निराला सबसे बड़ी बाधा हिन्दी समाज में व्याप्त हिन्दू वर्णवाद को पाते हैं।
1930-32 तक निराला हिन्दू वर्णवादी विभाजन का समाधान शंकर के अद्वैत या वेदांत दर्शन में खोजते हैं। इसे ही वे हिंदी जातीयता के दार्शनिक सारतत्व के रूप में रखते हैं। 1930 तक के लेखों में वे बार-बार लिखते हैं, कि पराधीन देश में सभी शूद्र हैं।
यह निराला की दार्शनिक निष्पत्ति है, जो 1940 तक जाते-जाते व्यावहारिक सामाजिक जीवन के अनुभव के सामने पीछे छूट जाती है। ‘काले कारनामे’ में वे दिखाते हैं, कि कैसे एक ही जाति-वर्ण के भीतर जमीन की मिलकियत के आधार पर सामाजिक भेदभाव का व्यवहार है।
‘बिल्लेसुर बकरिहा’ में निराला दिखाते हैं कि बिल्लेसुर ब्राह्मण हैं, लेकिन वर्ण निर्धारित पेशे से अलग काम करना पड़ता है। बिल्लेसुर बकरी तक पालते हैं और ब्राह्मणों में हेय होते हैं, लेकिन जैसे ही बिल्लेसुर धन-सम्पन्न होते हैं, वर्णगत व्यवहार से पुनः जुड़ जाते हैं। दोनों रचनाएं 1940 के आस-पास की हैं।
निराला जिस ‘वैदान्तिक साम्य’ से प्रभावित थे, वह बहुत कुछ विवेकानंद द्वारा की गयी उसकी व्याख्या पर आधारित लगती है। शंकर के वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक मूल्य ऊपरी तौर पर वर्णवाद का खण्डन करते लगते थे। निराला इसे ‘वैदान्तिक साम्य’ मानते थे।
जबकि, शंकर का यह दर्शन सनातनी वर्णवाद या बाद के विकसित वैष्णव सम्प्रदाय और वर्णवाद विरोधी बौद्ध दर्शन के बीच तालमेल बैठाकर नीचे के वर्णों को प्रभावित और आकर्षित करने की कोशिश थी। क्योंकि शंकराचार्य के समय वर्णवाद विरोधी तीव्र लहर लगभग पूरे भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद थी।
इसमें सबसे आक्रामक रूप से शैव धर्म और दर्शन ने अगुआई की। उसका प्रभाव नीचे के वर्णों पर तो था ही, क्षत्रिय वर्ण भी उसके प्रभाव में आने लगा था। खासकर इसमें शामिल नये सैनिक समुदायों और नस्लों के ऊपर। यही कारण है कि बाद में इन्हीं मध्य एशियाई और विभिन्न जनजातियों से विकसित राजपूत शासकों में प्रायः शैव मतावलम्बी मिलते हैं।
शंकर का दर्शन इसी वातावरण में वर्णवाद का एक छद्म समाधान लेकर आता है। उत्तर भारत में इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। शंकर के इस दर्शन को व्यवस्थित और लोकभाषा में, साहित्य में तुलसीदास अपने काव्य के साथ लाते हैं।
हिन्दी जातीयता के निर्माण के दार्शनिक और सांस्कृतिक मूल या आधार के लिए निराला इसीलिए बार-बार तुलसीदास और शंकर के वेदांत दर्शन के पास जाते हैं। इन दोनों ने समानता और समन्वय का जो रूप रचा, पूरा हिन्दी नवजागरण उसमें भटकता है।
खुद, निराला तब तक बंगाल के नवजागरण और जातीयता के सापेक्ष हिन्दी नवजागरण में कोई उदाहरण नहीं पाते, जो आधुनिक तात्विक आधारों को लेकर उठा हो और, जो आध्यात्मिक मूल्य के रूप में मध्यकालीन सन्त साहित्य की प्रेरणा लिए हो।
निराला सन्त साहित्य की जगह तुलसीदास के पास बार-बार जाते हैं। जबकि बंगला नवजागरण में सन्त साहित्य की प्रेरणा मुख्य है। सन्तों के यहाँ मौजूद आध्यात्मिक स्तर पर समानता के भाव से बंगला नवजागरण में मौजूद सामाजिक समानता का भाव सहज ही जुड़ जाता है।
सन्त साहित्य में वर्णवाद विरोधी भावना बेहद प्रबल है, जबकि तुलसीदास में वर्णवाद की पुनर्स्थापना ही अधिक है। वैसे भी मुगल काल में वर्णवादी सामाजिक शक्तियाँ पुनः प्रभाव और संरक्षण पाती हैं।
स्वयं, तुलसीदास काशी के ब्राह्मणों से जितना भी तिरष्कृत हुए, लेकिन जौनपुर के गवर्नर के मार्फत मुगल शासन में उनका बहुत सम्मान था।
सन्त साहित्य तथा तुलसी-साहित्य में आध्यात्मिक मूल्य में भले ही समानता दिखे, लेकिन सामाजिक आचरण और व्यवहार में बहुत अंतर है। सल्तनत काल और मुगल काल की भूमि सम्बन्धी नीतियों में अंतर इसका बड़ा कारण है।
अलाउद्दीन खिलजी ने जहाँ खुत, मुकद्दम, चौधरी जैसे मध्यस्थ भू-अधिकारों को खत्म किया तो मुगल काल में जागीरदारों और मनसबदारों के रूप में इन्हें पुनः स्थापित किया गया। वर्णवाद की ताकत यही भूमि-सम्बन्ध थे। यह एक अलग तथ्य है, लेकिन सन्त साहित्य और तुलसी-साहित्य में जो अंतर है, उसके पीछे यह महत्वपूर्ण कारक है।
लोगों को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि मुगल शासन के खिलाफ लड़कर अस्तित्व में आये या स्थापित हुए अधिकांश साम्राज्य ब्राह्मणवाद या वर्णवाद विरोधी विशिष्टता लिए होते हैं। चाहे वह जाट राज्य हो या मराठा राज्य। सिख राजत्व की भी यही विशेषता है। सतनामी राज्य भले ही कम अवधि के लिए रहा, लेकिन वह मुगल जमींदारों के खिलाफ संघर्ष के साथ तीखा वर्णवाद विरोधी चरित्र भी लिए था। दरअसल मुगल शासन में जागीरदारों, मनसबदारों और जमींदारों के खिलाफ ज्यादातर किसान जातियां संगठित होकर लड़ती हैं। यह तथ्य है कि मुगल शासन में जागीरदारों, मनसबदारों, जमींदारों में सवर्ण हिन्दू अधिक थे। औरंगजेब के समय में तो यह सर्वाधिक थे, जिस समय अधिकांश विद्रोह होते हैं, नये किसान राज्य बनते हैं। इनके गठन का दार्शनिक आधार संत साहित्य और विचार में था। अर्थात आध्यात्मिक मूल्य के रूप में समानता की प्रतिष्ठा। मुगल शासन में वर्णवादी अनुशासन पुनः प्रभावी होता है। यह जागीरदारों और मनसबदारों के सामाजिक व्यवहार में अभिव्यक्त हुआ। खैर
कहने का आशय यह है, कि निराला जब तक साहित्य के माध्यम से हिन्दी समाज को जांचते हैं, तब तक वे तुलसीदास और शंकर के वेदांत दर्शन को मुख्य मान-मूल्य बनाते हैं, लेकिन जब वे हिन्दी समाज से व्यावहारिक मेल-जोल में उतरते हैं, तो वे हिन्दी समाज के पिछड़े मूल्यों की संस्कृति के निर्माण में तुलसीदास के रामायण को जिम्मेदार बताते हैं।
‘देवी’ कहानी में वे कहते हैं कि ‘हिन्दुओं के मँजे स्वभाव को गो. तुलसीदासजी ने और माँज दिया है।’ यह कहानी 1934 की है। इसी तरह 1935 का एक लेख है, ‘हिन्दी में तर्कवाद’। इसमें वे लिखते हैं,
“हमारा साहित्य इस सिद्धांत से बहुत पीछे है। इसीलिए हमारे यहाँ तरह-तरह की बुराइयाँ हैं, तरह-तरह की रूढ़ियाँ स्थान पाये हुए हैं। तरह-तरह के प्रचार, जो यथार्थ मनुष्यता के विरोधी हैं, चलते जा रहे हैं। साहित्य में हम खड़ी बोली के रूप में भी बहुत कुछ वैसे ही हैं, जैसे पहले थे। हमारे अधिकांश जन तीरधनुष लेकर राक्षसों का नाश करते हैं…। धर्म, शिखा-सूत्र आदि की सैकड़ों रूढ़ियाँ हैं, जिनसे वास्तव में देश, साहित्य तथा भावना को क्षति पहुँचती है।”(सुधा, मासिक, लखनऊ)
अर्थात 1930 ई. के बाद निराला के चिन्तन और विचार में एक बदलाव दृष्टिगोचर होने लगता है। हिन्दी समाज और जाति को लेकर वे एक निराशा में भी जाते हैं। ‘राम की शक्तिपूजा’ में इसकी झलक है। खैर,
निराला हिन्दी जातीयता की खोज में तुलसीदास के पास बार-बार जाते हैं, तो उसमें हिन्दी नवजागरण की अंतर्वस्तु और उसकी मुख्य दिशा भी एक कारक है।
दूसरे, तुलसी-साहित्य के माध्यम से ही निराला हिन्दी भाषा-साहित्य से परिचित होते हैं। तुलसीदास और ‘वैदान्तिक साम्य’ के दर्शन पर वे जो लेख लिखते हैं, उसमें प्रायः 1920-22 के हैं, अर्थात हिन्दी जाति से परिचय का बिलकुल प्रारम्भिक समय।
मसलन, ‘तुलसीकृत रामायण में अद्वैत तत्व'(सितम्बर-अक्टूबर, 1922, ‘समन्वय’, कलकत्ता), ‘ज्ञान और भक्ति पर गोस्वामी तुलसीदास'(मई-जून, 1923, ‘समन्वय’, कलकत्ता), ‘तुलसीकृत रामायण का आदर्श'(अगस्त 1923, ‘माधुरी’, लखनऊ)। इसके बाद ‘विज्ञान और गोस्वामी तुलसीदास'(अगस्त-सितम्बर, 1927, ‘समन्वय’, कलकत्ता), ‘दो महाकवि, गो. तुलसीदास और रवीन्द्रनाथ(मार्च-अप्रैल, 1929, ‘मतवाला’ साप्ताहिक, कलकत्ता), ‘तुलसीकृत रामायण की व्यापकता'(1930, ‘सुधा’, लखनऊ), ‘तुलसीदास और रवीन्द्रनाथ'(1931, ‘सुधा’)। इसके बाद का कोई लेख नहीं है।
इन लेखों में निराला मुख्य रूप से बंगला जातीय साहित्य के बराबर हिन्दी जातीयता में साहित्यगत श्रेष्ठता की तलाश के रूप में तुलसीदास के पास जाते हैं। इसीलिए बार-बार वे तुलसीदास और रवीन्द्र नाथ टैगोर की तुलना करते हैं। लेकिन हिन्दी समाज के व्यवहार में जाने पर वे तुलसी-साहित्य के सांस्कृतिक प्रभाव को समाज के आधुनिक निर्माण के विपरीत पाते हैं।
तुलसीदास के रामायण का आदर्श बताने, गाने वाले समाज में सबसे अधिक जाति-भेद के पूजक और मानवीय करुणा से हीन हैं। दूसरे, दलित जातियों में वे कबीर-साहित्य का व्यापक असर देखते हैं। ‘चतुरी चमार’ कहानी में इसका प्रसंग है। यह कहानी 1934 की है।
इसके अलावा 1920 के आस-पास तक हिन्दी नवजागरण में सांस्कृतिक रूप से ऐसा कोई तत्व नहीं उभरता जिससे हिन्दी जातीयता को बंगला जातीय साहित्य के बराबर रखने की स्थिति हो। उसमें सामाजिक न्याय और समानता का कोई विचार हो।
फिर, जो सुधार नवजागरण काल में दिखते भी हैं वे प्रायः आचरण से सम्बंधित अधिक हैं। पाश्चात्य संस्कृति के सापेक्ष सांस्कृतिक शुद्धता का आग्रह ही मुख्य है।
पाश्चात्य संस्कृति के सापेक्ष संस्थागत सुधार हिन्दी नवजागरण का कोई तत्व नहीं बनता। प्रेमचंद ही इसमें ऐसे हैं, जिनके यहाँ संस्थागत सुधार के तत्व साहित्य का विषय बनते हैं और उसे वे बहसतलब करते हैं।
हिन्दी के अपने पहले ही उपन्यास ‘सेवासदन’ में प्रेमचंद ‘विवाह’ संस्था को आलोचना के भीतर लाते हैं तथा पाश्चात्य समाज में विवाह संस्था के भीतर आये आधुनिक और प्रगतिशील मूल्यों को अपनाने पर बल देते हैं।
संस्थागत वर्णवादी विधान पर प्रेमचंद इसलिए ज्यादा निगाह ले जा पाते हैं क्योंकि वे भूमि-सम्बन्धों को समझ जाते हैं। वर्णवादी नैतिक व्यवहार सबसे अधिक भूमि-सम्बन्धों में जीवित और कार्यरत था।
औपनिवेशिक भूमि-बन्दोबस्त और नीतियों ने मुगल शासन में रुढ़िबद्ध हुई सामाजिक व्यवहार और नैतिक आचरण को और जटिल ही बनाया। अर्थात औपनिवेशिक भू-सम्बन्धी नीति ने हिन्दी क्षेत्र में जो संस्थागत परिणाम दिये उसमें प्रायः मुगल शासन के दौर का बढ़ाव था।
यह एक दिलचस्प बात है कि 1857 के संघर्ष के बाद अपनायी गयी औपनिवेशिक साम्प्रदायिक नीति और बाद में हिन्दू साम्प्रदायिकता के आधार पर बने संगठन आरएसएस, दोनों ने मुगल शासकों को बाहरी व दुश्मन के रूप में लक्षित किया। जबकि, उसी मुगल काल में वर्णवाद सबसे अधिक मजबूत हुआ। मुगल काल में ही ‘जाति’ पुनः रुढ़िबद्ध हुई, जो, सल्तनत काल में ढीली हुई थी।
औपनिवेशिक नीतियों ने मुगलों के समय में पुनर्संगठित हुई सामाजिक संस्थाओं को और जटिल किया। इतना ही नहीं स्त्री-पुरुष सम्बन्धों में स्त्री ज्यादा कैद होती है। तंग नैतिकता निर्मित होती है।
अंग्रेज जब अपना शासन हिन्दी प्रदेश में केन्द्रित करते हैं, तो वे इस मौजूद नैतिकता को बने रहने देते हैं। दिल्ली, आगरा, मालवा और पूरा राजपुताना मुगल संस्कृति का केन्द्र था। यही हिन्दी प्रदेश का भी मुख्य हिस्सा है।
यह समझना बहुत आसान है, कि क्यों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अंग्रेजों के पिट्ठू हुए तथा क्यों महाराष्ट्र के पेशवायी संगठन होकर भी, हिन्दी प्रदेश को हिन्दूवादी राजनीति के अधिक अनुकूल पाते हैं! कहने का आशय यह, कि हिन्दी नवजागरण की यही पृष्ठभूमि थी और हिन्दी जातीयता की किसी भी आधुनिक संकल्पना को इससे टकराना था।
निराला प्रारंभ तो करते हैं इसी पृष्ठभूमि की नैतिक निर्मितियों से लेकिन बाद में जाकर वे इससे टकरा जाते हैं। प्रारम्भ में हिन्दी जातीयता की आधार निर्मितियों में निराला वैदान्तिक दर्शन से प्रभावित होते हैं और उसे ही एक तरह से स्पिरिट या हिन्दी जातीयता की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन, इसके शरीर के रूप में निराला पुरानी हिंदू वर्ण व्यवस्था के खात्मे और नये सामाजिक वर्णों के निर्माण की प्रस्तावना करते हैं। यह सब अभी विचार और दर्शन के स्तर पर ही था।
1922-23 से 30-32 तक लगभग हिन्दी जातीय पहचान के निर्माण में दर्शन तत्व पर उनका जोर अधिक है। निराला बंगाली जातीयता की निर्मिति में ब्रह्म समाज के दर्शन को मुख्य तत्व मानते हैं।
निराला मानते हैं कि ब्रह्म समाज के दर्शन ने बंगाली समाज और संस्कृति को आधुनिक भी बनाया और तेजी से जगह बनाते पाश्चात्य संस्कृति के उन प्रभावों को भी रोका, जिससे बंगाली संस्कृति की स्वतंत्र पहचान बनी रही।
ब्रह्म समाज के ही बनाये सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत वे रविंद्र नाथ टैगोर के साहित्य को रखते हैं, जिसने बंगाली राष्ट्रीयता या जातीयता को मुकम्मल रूप दिया।
ब्रह्म समाज को फैलाने में रवीन्द्र नाथ टैगोर के पिता देवेन्द्र नाथ टैगोर को निराला बड़ा श्रेय देते हैं। ब्रह्म समाज के बाद निराला रामकृष्ण परमहंस को इसका श्रेय देते हैं। लेकिन हिन्दी नवजागरण में निराला ऐसे किसी तत्व का अभाव पाते हैं, जो दर्शन के स्तर पर जातीय विशेषता लिए हो और आधुनिक मानवीय उपलब्धियों से युक्त भी हो।
इसके अभाव में निराला हिंदी जातीयता के आध्यात्मिक मूल्य के रूप में वेदांत दर्शन के पास पहुंचते हैं और उसी उसी के अनुरूप नया सामाजिक संगठन चाहते हैं।
साहित्य को, या कि कला को वे इसी ध्येय के लिए सृजित होते देखना या पाना चाहते हैं। बिना इसके हिन्दी समाज व भाषा-साहित्य का उत्थान और उसकी कोई पहचान आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में नहीं हो सकती। उसमें सुधार स्थायी नहीं होगा और हिंदी समाज दूसरी संस्कृतियों के प्रभाव में आता रहेगा। ऐसा निराला मानते या सोचते हैं या अपने स्वयं के तर्क और विवेक से इसे पाते हैं।
निराला का मानना था, कि ‘ब्रह्म समाज’ के प्रचार-प्रसार ने बंगाल के नव-शिक्षितों में बढ़ते पाश्चात्य संस्कृति के प्रभावों को रोक दिया। निराला के लिए पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव की बात जब की जाती है, तो उससे तात्पर्य वैसे प्रभावों से है, जो जातीय पहचान को विलीन करने वाली होती हैं।
आधुनिक शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय जैसे मूल्य, जो पश्चिमी समाज में जागरण से निकले थे, निराला उससे अटूट रिश्ता रखते हैं। इसके साथ निराला चाहते हैं कि पहचान इसकी अपनी जातीय हो।
इन जातीय तत्वों में क्या वरेण्य है और क्या त्याज्य या क्या अपनाया जाय और क्या छोड़ा जाय, निराला इसे हिन्दी नवजागरण में अन्यों से अलग देखते हैं।
हिन्दी नवजागरण में जिस तरह से पुराणों, वेदों, उपनिषदों के ज्ञान, विचार को धो-पोंछ कर समकालीन बनाने और उसे ही भारतीय या जातीय बताने की एक आम धारणा थी।
जिसे औपनिवेशिक सत्ता-संस्कृति ने गौरवपूर्ण बताया उसे ही लपक लेने का चलन था। निराला उससे अलग अपने तर्क-विवेक से चलते हैं। वे प्राचीन जातीय साहित्य को आधुनिक सन्दर्भ में आलोच्य बनाना चाहते हैं। जून, 1933, ‘सुधा’ में छपे लेख, ‘साहित्य और जनता’ में निराला हिन्दी समाज और साहित्यिक दोनों की इस स्थिति पर लिखते हैं,
“हमारे निन्नानबे फ़ीसदी साहित्यिकों को और सौ फ़ीसदी जनता को भगवान् श्रीरामचन्द्र पर, उनके जन्म-कर्मादि पर पूरा-पूरा विश्वास है। अतः आज यदि राम के विरोध में कोई प्रासंगिक बात की जाय, तो जनता उसे सुनने को तैयार नहीं; साहित्यिकों में केवल सुनने का धैर्य है, मत बदलने की शक्ति नहीं।”
निराला साहित्य को मत बदलने की शक्ति से युक्त देखना चाहते हैं, लेकिन हिन्दी के निन्नानबे फ़ीसदी साहित्यिकों में यह शक्ति नहीं। आगे वे लिखते हैं,
“यह अवश्य ही युगों की संचित साहित्यशक्ति का ही दौर्बल्य है। इससे जनता को कुछ हासिल हुआ, तत्व के भीतर से यह साबित नहीं होता। किसी महान भक्त से ही पूछिए, अग्नि से यज्ञ-हवि कैसे पैदा होती है, जानकीजी ऋषियों के खून से भरे घड़े से, जमीन से, कैसे निकलती हैं, महावीरजी लंका से एक ही रात में उत्तराखण्ड जाकर, सजीवन-मूरिवाला पहाड़ लेकर, रात ही-भर में लंका कैसे लौट आते हैं, तो आपको युक्तिपूर्ण, सन्तोषप्रद उत्तर कदापि प्राप्त न होगा।”
इससे यह भी पता चलता है कि तार्किकता निराला के चिंतन का प्राणतत्व है। साथ ही, तार्किकता ने ही दुनिया में तमाम पुनर्जागरण, नवजागरण को जन्म दिया। लेकिन हिन्दी नवजागरण में वह है ही नहीं। तो फिर, यह नवजागरण ज्यादातर भाषागत रूप और शैली तक ही सीमित रहा! खैर फिर आगे वे लिखते हैं,
“भारत में प्रचलित, भारतीय नाम से प्रसिद्ध आर्य-सभ्यता की उज्ज्वल श्री से मण्डित जो कुछ प्राप्त होगा, उसका अधिकांश इसी प्रकार शिरश्चरणहीन, अदृष्ट, काल्पनिक जन्तुविशेष ज्ञात होगा, जहाँ मानवीय दृष्टि की गति नहीं।”
निराला उस समय यह सब भारतीयता या भारतीय संस्कृति की हिन्दूवादी प्रस्थापनाओं के सापेक्ष लिख रहे थे। आज सत्ता पर वही तत्व काबिज हैं, जो ‘शिरश्चरणहीन’ और ‘अदृष्ट’ हैं तथा जिन्होंने हिन्दी समाज को ऐसी ही संस्कृति से ढँक दिया है।
हिन्दी धारावाहिक, सिनेमा, साहित्य में आज फिर से शिरश्चरणहीन और अदृष्ट बातों का बोलबाला है। आज कोई हिन्दी समाज की इस गति को देखकर निराला के साहित्य, चिंतन को देखे तो उसका महत्व जान सकता है और यह भी कि निराला हिन्दी की जातीय पहचान को किन आधारों पर खड़ा करना चाह रहे थे!
निराला इसी में आगे लिखते हैं, कि इन्हीं ‘बुराइयों का दूरीकरण देश का, साहित्य का सच्चा उद्धार है।’
एक अन्य लेख, साहित्य का विकास में वे लिखते हैं,
“हमारे साहित्यिकों का ज्ञान किसी धातु के बने बर्तन की तरह जड़ है, जो अपना गढ़ा हुआ स्वरूप बदल नहीं सकता।”(‘सुधा’, मासिक, लखनऊ, 1932)
जैसे-जैसे निराला हिन्दी समाज से परिचित होते हैं, वैसे-वैसे उनके सोच-विचार और धारणा में बदलाव होता है। और सबसे बढ़कर निराला बंगाल के नवजागरण की विरासत लेकर आते हैं।
निराला जिस समय बंगाल से वापस आते हैं, तब तक वहाँ नवजागरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और रवीन्द्र नाथ टैगोर का सांस्कृतिक, वैचारिक व्यक्तित्व वैश्विक महत्ता प्राप्त कर चुका था। जिसका प्रभाव कला, साहित्य, समाज, राजनीति सब पर पड़ रहा था।
बंगाल और हिन्दी समाज के भीतर के सांस्कृतिक अंतर या नवजागरण की अंतर्वस्तु के अंतर का एक प्रतीकात्मक प्रकरण कबीर को लेकर पाया जा सकता है।
प्रायः राष्ट्रीयताओं में नवजागरण की सांस्कृतिक थाती संत साहित्य है। बंगाल में इसी प्रक्रिया में कबीर को खोजा जा चुका था। हिन्दी में कबीर को लेकर हिचक है। कारण है कबीर की वर्णवाद के प्रति आक्रामकता।
1920 ई. के बाद हिन्दी का जो लघु बौद्धिक तबका बन रहा था, उसमें कबीर को लेकर एक भय है और तुलसीदास को लेकर एक मोह है। खुद निराला एक लेख में लिखते हैं, कि जिस कबीर से रवीन्द्रनाथ प्रभाव ग्रहण करते हैं, उसी कबीर को लेकर हिन्दी में आदर नहीं है। ‘साहित्य का विकास’ लेख में निराला लिखते हैं,
“कबीर एक ऐसे ऊँचे विचारवाले साहित्यिक हमारी हिन्दी में हैं, जिनका जोड़ संसार में दुर्लभ है। क्या कहीं एक अपढ़ मनुष्य इतना बड़ा ज्ञानी कवि हुआ है? हिन्दी साहित्य का ज्ञान-काण्ड यदि कबीर के साहित्य को कहें, तो अत्युक्ति न होगी। पर हिन्दी में ही कबीर का जैसा आदर होना चाहिए, नहीं हुआ। बंगाल में कबीर से बढ़कर हिन्दी का दूसरा कवि नहीं समझा जाता।…रवीन्द्रनाथ-जैसे महाकवि कबीर की प्रतिभा पर मुग्ध हैं।”
1920 ई. तक हिन्दी नवजागरण की अंतर्वस्तु में जो कुछ भी था, वह मूल्य और नैतिकता के स्तर पर वर्णवाद से मुक्त नहीं था। इसीलिए कबीर का आदर नहीं। फिर इस हिन्दी साहित्य या नवजागरण की अंतर्वस्तु क्या है, इस पर निराला लिखते हैं,
“हमारी हिन्दी में अभी छन्दों के ह्रस्व-दीर्घ की मात्राएँ गिनी जा रही हैं। भारतीयता, शालीनता और ‘पन’ के विचार से साहित्यिकों को फुरसत नहीं मिल रही।…देश ही में एक तरफ़ तमाम विश्व की भिन्न जातीय संस्कृति(Culture) अपने साहित्य में मिलाने की कोशिश हुई और हो रही है और हमारे यहाँ अभी साहित्यिक ‘भाषा कैसी होनी चाहिए’ प्रश्न नहीं हल कर सके।”
अर्थात हिंदी नवजागरण में जो साहित्य रचा जा रहा था, उसमें अपने समय के मनुष्य की कोई छवि, छाया या प्रतिबिम्ब नहीं था। उसमें ‘साहित्यिक विशालता, उदारता, स्वातन्त्र्य’ का अभाव है। वे लिखते हैं,
“हमारी हिन्दी को ऐसी ही भावना से युक्त साहित्यिकों की आवश्यकता है। सत्य की रक्षा के लिए साहित्यिक अपने प्राणों का बलिदान कर दे ! सत्य वही है, जो मनुष्य-मात्र में है। ज्ञान में हिन्दू, मुसलमान नहीं।…हिन्दी में बहुत करना है, बहुत पड़ा है, बहुत पीछे हैं हम।”(साहित्य का विकास, दिसम्बर 1932, सुधा, लखनऊ)
इसीलिए हिंदी नवजागरण को निराला भिन्न भूमि पर ले जाते हैं। वहां से वे हिन्दी की नयी, आधुनिक जातीय पहचान बनाना चाहते हैं। वे हिंदी साहित्य के चतुर्वेदिकों से बार-बार पंगा लेते हैं, उनकी चुटकी लेते हैं। अपनी हर कहानी में वे लगभग ऐसा करते हैं।
इतना ही नहीं, वह प्रेमचंद के आदर्शवाद को भी आड़े हाथों लेते हैं और यह सब वे 1930-32 तक के लेखों में बार-बार कहते हैं। यद्यपि कि प्रेमचंद के उपन्यासों में वे यथार्थ के चित्रण को मुख्य मानते हैं।
इतना ही नहीं, जयशंकर प्रसाद अपने उपन्यास में किसान समस्या तक जाते हैं, तो उसके पीछे निराला द्वारा की गयी प्रसाद की आलोचना है। वे प्रसाद के पौराणिक प्रेम को आधुनिक समस्याओं के अनुकूल नहीं पाते और उसकी आलोचना करते हैं।
निराला खुद से भी जूझते हैं। आत्मसंघर्ष और द्वन्द्व निराला के यहां जैसा है, उनके समय तक के किसी भी रचनाकार में नहीं है। इसका कारण है कि निराला साहित्य को समाज और राष्ट्र निर्माण के तत्वों से जोड़ना चाहते हैं।
इस रूप में साहित्य को उस निर्माण का सहायक बनाना चाहते हैं। क्योंकि निराला बंगाली जागरण और निर्माण में ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस, रवीन्द्रनाथ टैगोर के योगदान को देखकर आए थे। वैसा ही चाहते थे।
स्कूलों का निर्माण, आधुनिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार, नये सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण, सामाजिक स्वाधीनता हिंदी समाज में भी वे देखना चाहते थे। निराला के लेखों में यह चिंताएं व्यक्त होती हैं और कथा साहित्य में इसके सूत्र वे रचते हैं।
निराला हिंदी समाज में ऐसे तत्व को अनुपस्थित पाते थे, जिससे उसकी कोई सांस्कृतिक उन्नति हो सके। उसमें नवीनता हो, मनुष्य मात्र के मान की स्थापना हो। समानता, न्याय और बंधुत्व के मूल्य हों।
पहले निराला वेदांत दर्शन में समानता के भाव से प्रभावित थे लेकिन 1938 तक आते-आते निराला अवध के जिलों में और उसके समाज से जुड़कर उसकी गति से मिलकर एक अलग सत्य तक पहुंचते हैं।
‘कुल्ली भाट’ उसका समुच्चय है। यह रचना एक मोड़ है निराला के विचार और व्यक्तित्व में। 1941-42 तक ‘कुकुरमुत्ता’ संग्रह की कविताएं नये विचार तत्व की घोषणा हैं। हिन्दी समाज से, किसान जातियों, भूमि-सम्बन्धों से व्यावहारिक परिचय में आवाजाही के बाद निराला नयी अनुभूति, नये सत्य से गुजरते हैं। जातिवाद, भू-दासता, वर्णवाद, सामाजिक गुलामी, शोषण को देखते हैं। इसका असर एक कारक बनता है।
चतुरी चमार, देवी, श्यामा, बिल्लेसुर बकरिहा, कुल्ली भाट, काले कारनामे, चोटी की पकड़ और कुकुरमुत्ता में इसके प्रमाण मिलने लगते हैं।
1941 की एक कहानी है ‘जान की’। इसमें वे बतौर नैरेटर कम्युनिस्ट कार्यकर्ता बनकर बांदा में सामाजिक बदलाव के लिए जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि निराला कम्युनिस्ट हो गये थे, लेकिन यह पता चलता है, कि वे वेदांत दर्शन के प्रस्थान बिंदु से आगे बढ़ आये थे।
ऐसा भी नहीं है, कि निराला हिन्दी भाषा, समाज को वर्णवादी, पौराणिक नैतिकता से निकाल कर उसे आधुनिक जातीय पहचान के निर्माण के किसी मुकम्मल विचार तक पहुंच गए थे, लेकिन जो लोग यह मानते हैं कि वे अंत तक वेदांती ही रहे, वे भी सही नहीं हैं।
निराला के यहां एक विचार जो अंत तक है, वह आधुनिकता और प्रगतिशीलता है। हिन्दी जातीयता के विचार-निर्माण में यह एक बुनियादी तत्व की तरह है। इसे वे कभी नहीं छोड़ते।
उनकी एक कहानी ‘विद्या’ है, जो शायद आखिरी छपी कहानी है। इस कहानी में विद्या अंग्रेजी की छात्रा है और उसका मंगेतर संस्कृत का छात्र। दोनों में साहित्य के माध्यम से संस्कृति पर बहस होती है। विद्या नये मूल्य की भारतीयता के साथ खड़ी है और उसका मंगेतर पुराने वर्णवादी पितृसत्तात्मक मूल्य की भारतीयता के साथ।
विद्या अपनी स्थिति से पीछे नहीं हटती और उसका मंगेतर श्याम उसके साथ विवाह करने से मना कर देता है। यह कहानी सितम्बर, 1958 ई. में ‘सरस्वती’ मासिक में प्रयाग से छपी है।
निराला अपनी प्रारम्भिक कहानियों, मसलन ‘पद्मा और लिली’, ‘ज्योतिर्मयी’, ‘कमला’ आदि में भी यह दिखाते हैं कि हिन्दी समाज का जो नया मध्यवर्ग बन रहा था या जो उसका बौद्धिक भी था, वह आधुनिक रहन-सहन में पाश्चात्य रहन-सहन का नकलची है, लेकिन मूल्य और नैतिकता में वर्णवादी, पितृसत्तावादी है। समानता और न्याय को वह स्वीकार करने को तैयार नहीं है। निराला इसीलिए अपने लेखों में कहते हैं, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के पास आधुनिक समाज निर्माण की कोई शक्ति नहीं। वह स्वत्वहीन वर्ण है।
“जब ग्रीक सभ्यता का दानवी प्रवाह गत दो शताब्दियों से आने लगा दानवी माया अपने पूर्ण यौवन पर आ गयी, हिन्दुस्तान पर अँगरेजों का शासन सुदृढ़ हो गया, विज्ञान ने भौतिक करामात दिखाने प्रारम्भ कर दिये, उस समय ब्राह्मण शक्ति तो पराभूत हो ही चुकी थी, किन्तु क्षत्रिय और वैश्यशक्ति भी पूर्णतः विजित हो गयी। शिक्षा जो थी अँगरेजों के हाथ में गयी, अस्त्रविद्या अँगरेजों के अधिकार में रही(अस्त्र ही छीन लिये गये, तब वह विद्या कहाँ रह गयी? और वह क्षत्रियत्व भी विलीन हो गया), व्यवसाय-कौशल भी अँगरेजों के हाथ में। भारतवासियों के भाग्य में पड़ा शूद्रत्व।”
वे ऐसी शक्ति को उपेक्षित वर्णों में मौजूद मानते हैं। किसी भी आधुनिक निर्माण की शक्ति वे इसी वर्ण में देखते है। उनका तर्क है कि इस वर्ण की शक्ति अब तक दबी पड़ी है, उसे अवसर नहीं मिला है। उसे ही बाहर निकालने की जरूरत है।
“भारतवर्ष की तमाम सामाजिक शक्तियों का यह एकीकरण-काल शूद्रों और अन्त्यजों के उठने का प्रभातकाल है।… भारतवर्ष का यह युग शूद्रशक्ति के उत्थान का युग है। और देश का पुनरुद्धार उन्हीं के जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है।”
ऊपर के उद्धरण ‘वर्णाश्रम-धर्म की वर्तमान स्थिति’ लेख से हैं। यह लेख दिसम्बर 1929 ई. के ‘माधुरी’ में छपा है। यह मासिक पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती थी। इस लेख में निराला आजादी की लड़ाई के सन्दर्भ में सन्तराम के ‘जाति-पाति तोड़क मण्डल’ और वैदान्तिक साम्य संगठन पर विचार करते हैं।
इसी लेख में वे लिखते हैं,
“वृद्ध भारत की वृद्ध जातियों की जगह धीरे-धीरे नवीन भारत की नवीन जातियों का शुभागमन हो, इसके लिए प्रकृति ने वायुमण्डल तैयार कर दिया है। यदि प्राचीन ब्राह्मण और क्षत्रिय-जातियाँ उनके उठने में सहायक न होंगी, तो जातीय समर में अवश्य ही उन्हें नीचा देखना होगा। क्रमशः यही अन्त्यज और शूद्र, यज्ञकुण्ड से निकले हुए अदम्य क्षत्रियों की तरह, अपनी चिरकाल की प्रसुप्त प्रतिभा की नवीन स्फूर्ति से देश में एक अलौकिक जीवन का संचार करेंगे। इन्हीं की अजेय शक्ति भविष्य में भारत को स्वतन्त्र करेगी।”
महत्वपूर्ण है कि इस लेख में निराला ‘वैदान्तिक साम्य’ की यथार्थ प्रतिष्ठा के ध्येय से ही समाज का विवेचन करते हैं। इसी ध्येय की स्थापना वे साहित्य में भी चाहते हैं। इस समय तक निराला बोल्शेविक क्रान्ति और उसमें समानता के विचार को भारत के लिए अनुकूल या आवश्यक नहीं मानते। लेकिन लखनऊ से प्रकाशित ‘सुधा’ अर्धमासिक 16 जून, 1934 की सम्पादकीय टिप्पणी में इसके प्रति सकारात्मक होते हैं और लिखते हैं,
“…अब यह वैश्य-धर्म अपने तमाम विज्ञान के साथ होकर भी संसार की शान्ति को सहारा नहीं दे रहा- इसके भी दिन पूरे हो गये। नया उदाहरण रूस है, जिसने किसानों का राज्य स्थापित किया। आज संसार के बड़े-बड़े प्रायः सभी मनुष्य किसानों के युग का स्वागत कर रहे हैं। इस प्रकार, हम देखते हैं, अब वैश्य-युग भी मनुष्यों के मन से दूर हो गया है- अब किसान या मजदूरों का युग है।”
इसमें फिर आगे वे लखनऊ में रामकृष्ण मिशन तथा महात्मा गाँधी के द्वारा किसानों और मजदूरों के हित में किये प्रयासों और कार्यों की चर्चा करते हैं। यहां भी निराला बंगाल के नवजागरण के नायकों के कार्यों का उल्लेख करते हैं।
जबकि फरवरी-मार्च 1930 के कलकत्ता के ‘मारवाड़ी अग्रवाल’ मासिक पत्रिका में छपे एक लेख ‘भारत का नवीन प्रगति में सामाजिक लक्ष्य’ में बोल्शेविज़्म और साम्राज्यवाद दोनों के केन्द्र में पूंजी की प्रधानता मानते हैं। वे लिखते हैं,
“बोलशेविक चाहते हैं इम्पीरियलिज्म(साम्राज्यवाद) का नाश हो और साम्राज्यवादी चाहते हैं, बोलशेविक उनके दायरे में एक न रहे। यह सिर्फ इसलिए कि दोनों की दृष्टि में महत्ता सिर्फ पूँजी को प्राप्त है।…यहाँ तो अर्थ का संचय परार्थ के लिए, अक्षमों के लिए ही करने का विधान दिया गया है। फिर बोलशेविकों से कोई भारतीय क्यों डरे? और यहाँ बोलशेविक हों भी क्यों? क्यों साम्राज्यवाद ही रहे? यहाँ तो चारों वर्ण अपनी शक्ति का परिचय देकर, सर्वस्व का त्याग कर पूर्ण स्वतंत्र ईश की सत्ता में मिल जाना चाहते हैं, फिर कोई वाद और विवाद कैसा? भारत के समाज का यही लक्ष्य है। तमाम सुधार इसके अनुसार होने चाहिए।”
1934 की छपी उनकी दो महत्वपूर्ण कहानियों, ‘देवी’ और ‘चतुरी चमार’ में निराला के उपर्युक्त विचारों से अंतर मिलने लगता है। 1941 की कहानी ‘जान की’ का नैरेटर नायक तो सामाजिक परिवर्तन के लिए कम्युनिस्ट कार्यकर्ता बना है।
‘कुकुरमुत्ता’ संग्रह की कविताएँ बिलकुल भिन्न भूमि पर ले जाती हैं।
जून, 1932 ई. का एक लेख है ‘सामाजिक पराधीनता’। यह लखनऊ से प्रकाशित ‘सुधा’ मासिक में छपा है। इस लेख में निराला शास्त्र, पुराण, वर्ण, भारतीयता आदि पर विचार करते हैं। लेकिन पूर्व के लेखों से अलग इस लेख में वे इन सबकी कोई उदार व्याख्या या बचाव करने की बजाय इन सभी तत्वों के दोहरेपन, पाखण्ड पर बेहद आक्रामक ढंग से विचार करते हैं। जबकि 1930 के लेख ‘भारत का नवीन प्रगति में सामाजिक लक्ष्य’ में वे लिखते हैं, “अब समाज में परिवर्तन करते समय हमें किसी विषय की वृहत् व्याख्या अपने शास्त्रों से ही लेनी चाहिए।”
1932 के लेख ‘सामाजिक पराधीनता’ में निराला लिखते हैं,
“शास्त्र का एक ही विधान समाज में नहीं रहा। पर इस समय का समाज (अर्थात, हिन्दी समाज, जोर मेरा) यह मानने के लिए तैयार नहीं। बात-बात में शास्त्रों की राय लेने की जो आदत बड़े-बड़े विद्वानों तक में देख पड़ती है, वह शास्त्रीय पराधीनता है।”
फिर आगे वे लिखते हैं, “मनुष्य शास्त्रों से अपने अनुकूल विधान ही निकालता है। शास्त्रों में हर कानून की प्रतिकूलता देख पड़ती है। सच बोलना चाहिए, पर झूठ कहने के भी अवसर हैं। इस तरह के सविरोध शास्त्रों से यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपनी मेधा के अनुसार ही काम करना चाहिए।”
अपनी मेधा को निराला जाग्रत रखते हैं। तर्क, बुद्धि, विवेक को नवीन, आधुनिक समाज और राष्ट्र निर्माण की दिशा में रखते हैं और इसी के सापेक्ष बाहर-भीतर को जांचते-परखते हैं तथा अपने को बदलते हैं।
शंकर के ‘वैदान्तिक साम्य’ से प्रभावित होकर निराला वर्ण-व्यवहार को उस समय के लिए उचित मानते हैं, लेकिन आगे चलकर वे इसे किसी भी सुधार और परिवर्तन में बाधक मानने लगते हैं। ‘सामाजिक पराधीनता'(1932) लेख में निराला लिखते हैं,
“संसार में रहने वाला समाज ज्ञात या अज्ञात भाव से समस्त संसार के साथ सहयोग करता है। हमारा समाज इतना पिछड़ा हुआ, पतित और मृतकरूप हो रहा है कि वह घर ही में परस्पर सहयोग नहीं कर सकता। इसके मूल में वही प्राचीन शिक्षा है, जो एक वक्त संस्कार थी और अब कुसंस्कार”
आगे वे लिखते हैं,
“हमारे यहाँ साधुओं और गृहियों का गुरु-शिष्य सहयोग अब भी है। यह और बुरा है, क्योंकि गुरुदेव घोर कलिकाल में रहकर भी बातचीत के समय सत्ययुग से एक पग इधर नहीं रखते।”
अभी के समय के प्रवचनकारों, बाबाओं और हिन्दुत्ववादियों पर भी यह सटीक बैठता है। आगे, इसी में वे लिखते हैं,
“अधिकांश मूढ़- ‘गुरु ने जैसा घुखाया’ वाले। कुछ अल्प-शिक्षित। सब-के-सब जातीय द्वेष भड़काने वाले। इतने बड़े मायाजाल में फँसा हुआ समाज महान साधना के पश्चात ही मुक्त हो सकता है।”
हिन्दी समाज की जातीय पहचान नवीन चेतना और मूल्यों से युक्त हो, निराला इसके लिए लगातार चिंतनशील हैं और वे दर्शन के स्तर पर सभी राहों पर इसके लिए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में जब वे हिन्दी समाज की सांस्कृतिक, सांस्थानिक अवस्थिति से व्यवहार में दो-चार होते हैं, तो वे उससे टकरा जाते हैं, भिड़ जाते हैं।
इसी लेख में वे लिखते हैं,
“यह दुर्बल देश अभी किसी सभ्य देश में मुंह नहीं दिखा सकता। घर में मुसलमान-द्वेष। भिन्न जातीयता, जो हिन्दुओं में ही भरी हुई है, उसकी तो बात ही नहीं। ऐसी दशा में सबसे पहले आवश्यक है, समाज की नाव का भारतीयता के शब्दार्थ का लंगर खोल दिया जाय। तभी डांड़ चलाने की सुविधा होगी।…हिन्दी में जो लोग भारतीयता और शालीनता आदि कुछ चुने हुए शब्दों के ज़िम्मेवार हो रहे हैं, चरित्र की रक्षा कराने का ईश्वर के यहाँ से अधिकार-सा लेकर अवतीर्ण हुए हैं, उनकी महान भारतीयता उनके लेखों में ही प्रांजल है। कंगन हाथ को आरसी की जरूरत नहीं पड़ती!”
फिर आगे वे लिखते हैं
“समाज में रहन-सहन, खान-पान, विवाह आदि का कोई बँधा कानून नहीं रह सकता। यह गुलामी है।”
निराला इस गुलामी के खिलाफ सदैव संघर्षरत रहे। इस सामाजिक गुलामी को वे हिन्दी जातीयता के निर्माण की सबसे बड़ी बाधा के रूप में पहचानते हैं।
निराला हिन्दी समाज में आकर जातीयता के तत्व तलाश करते हैं। इसी प्रक्रिया में वे सांस्कृतिक सवालों से सबसे ज्यादा टकराते हैं।
जाति-भेद, वर्ण-भेद, रहन-सहन, खान-पान, विवाह जैसे समाज के संस्थानिक रूपों पर वे अधिक जोर देते हैं। बिना इस पर विचार किये समाज के सुधार और उसमें परिवर्तन की बात नहीं हो सकती थी।
निराला की चिन्ता थी, कि कैसे हिन्दी समाज में आधुनिक समय के अनुकूल नवीन रूपान्तरण हो। स्वाधीनता, समानता, न्याय और बंधुत्व के आधार पर समाज का नवीन संयोजन, संगठन हो, यह निराला का मुख्य ध्येय था।
वे जब ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, रवीन्द्र नाथ टैगोर, देवेन्द्र नाथ टैगोर पर विचार करते हैं, तो उनकी इन विशेषताओं पर वे जोर देते हैं। जैसे ब्रह्म समाज और रामकृष्ण ने सभी जाति-वर्ण के लोगों को एक साथ बैठकर खाने की व्यवस्था पर जोर दिया। बंगाल के समाज पर इसका असर पड़ा।
निराला बंगाल के नवजागरण के नायकों पर लेख लिखते समय इसे बार-बार रेखांकित करते हैं। वे लिखते हैं, कि बंगाल में अब द्विज बिना किसी दबाव के शूद्रों के साथ बैठकर एक पाँत में खाना खाते हैं। लेकिन जब वे हिन्दी समाज की व्यावहारिकता से परिचित होते हैं, तो यहाँ यह एक बड़ी सामाजिक बाधा, गुलामी के रूप में मौजूद है।
इसी तरह, अंतर्जातीय विवाह को भी निराला सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक मानते हैं। साथ ही शूद्रों और स्त्रियों की मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठा। निराला बंगाल के नवजागरण में इसे रेखांकित करते हैं। रवीन्द्र नाथ टैगोर के साहित्य पर विचार करते हुए वे इसे उभारते हैं। निराला रवीन्द्र-साहित्य में इसे आध्यात्मिक मूल्य के साथ आधुनिक मूल्य की स्थापना के बतौर देखते हैं।
इसके बराबरी में निराला को अपने समय के हिन्दी नवजागरण में कोई नहीं दिखता। इसलिए जब वे रवीन्द्र-साहित्य के बराबर हिन्दी में देखते हैं, तो तुलसीदास, सूरदास और कबीर को रखते हैं।
“बंगला में एक रवीन्द्रनाथ हैं, हिन्दी में तुलसी, सूर, कबीर तीन हैं” (‘हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में बंगाली मनोवृत्ति’ शीर्षक टिप्पणी, ‘सुधा’ अर्धमासिक, 16 जुलाई, 1934)
निराला को यहाँ रवीन्द्र-साहित्य की तुलना में हिन्दी को उच्चतर दिखाने के लिये पीछे जाना पड़ता है, मध्यकालीन समय में, जहाँ सन्तों के यहाँ मुक्ति के आध्यात्मिक सन्दर्भ ही हैं। बंगाल का नवजागरण आधुनिक भावबोध लेकर उठा, शक्ति और प्रभाव उसने अवश्य मध्यकालीन वैष्णव भक्ति से पायी।
निराला हिन्दी के जातीय पहचान को जब तक आध्यात्मिक मुक्ति और साम्य के दायरे में रखकर पाने, खोजने की कोशिश करते हैं, तब तक तुलसीदास और शंकर के वेदांत दर्शन से पार नहीं जा पाते। यह 1930-32 तक रहता है।
इसे उनके प्रबन्ध ‘तुलसीदास’ के प्रकाशन काल से जोड़कर नहीं समझना चाहिए। ‘तुलसीदास’ निराला के भीतरी या आध्यात्मिक मुक्ति से बाहरी या भौतिक, दुनियावी मुक्ति तक पहुँचने के बीच के संक्रमण काल में रचित है। अर्थात 1930-32 से 1936-38 के बीच का समय। इसी बीच वे वर्ण-धर्म, शास्त्र, पुराण और इस पर आधारित भारतीयता के प्रति वे अधिक आलोचनात्मक होने लगते हैं।
समाज के प्राचीन आदर्शों को वे अब किसी रूप में नव सृजन या नव निर्माण का मूलभूत तत्व नहीं मानते या प्रेरणा नहीं मानते। उनका मानना है, कि वह हमारे आदर्श थे, लेकिन अपने समय में थे और हम उसे उसी समय के लिए आदर्श मान सकते हैं।
आज या आधुनिक समय में हमें नये मनुष्य को गढ़ना होगा। इस मनुष्य को साहित्य में स्थापित करना होगा। इस नये मनुष्य को बनाने के लिए, नये सांस्कृतिक मूल्य स्थापित करने होंगे। इन मूल्यों में जातीय मानवीय तत्व हों, साथ ही, विश्व मानवतावाद की उपलब्धियां भी शामिल हों।
अपने इस विचार के चलते निराला वेदांत दर्शन और तुलसीदास के प्रस्थान बिंदु से 1938-40 तक एक मोड़ लेने लगते हैं। इस दौरान वे हिन्दी के साहित्य की दुनिया से बाहर निकल कर वास्तविक हिन्दी समाज में, इसके जन के बीच में चलने-फिरने, उठने-बैठने लगते हैं।
ये वास्तविक जन निराला को बदलने लगते हैं। निराला का कथा साहित्य ऐसे जन, समाज और ऐसे मनुष्यों से क्रमशः भरता जाता है। हिन्दी की जातीय पहचान को बनाने के विचार का आधार तत्व व्यवहार में आने पर बदलने लगता है। और खुद निराला बदलते हैं।
1938 ईस्वी के बाद का निराला का साहित्य इसका प्रमाण है अर्थात व्यवहार से विचार बदलता है या जिस विचार को लेकर वे समाज के उपेक्षित, वंचित, दीन-हीन, छोटे लोगों को साहित्य में रचते हैं, वे सभी निराला के विचार को बदल देते हैं।
‘कुल्ली भाट’ का विद्यालय प्रसंग हो या ‘देवी’ कहानी की अंतर्वस्तु, निराला के इस बदलाव के चिन्ह को देखा-पाया जा सकता है। ‘कुकुरमुत्ता’ की कविताओं को कोई देखे और उसमें अंतर्भुक्त आक्रामकता, उसके तेवर, तेज को कोई जांचे तो वह इस बदलाव को समझ सकता है।
हिन्दी जातीयता को हिन्दू जातीय पहचान से अलग आधुनिक तत्व, चिंतन और विचार से जोड़ने की दिशा में निराला का यह महत्वपूर्ण प्रयास होता है। निराला से ही प्रेरित राम विलास शर्मा जनवादी तत्वों और साझे सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर हिन्दुस्तानी जातीयता के निर्माण को अपनी आलोचना के केन्द्र में रखते हैं। हालांकि, राम विलास शर्मा इस जातीयता के आधार पर हिन्दी के एक प्रदेश के निर्माण पर जोर देते हैं, जबकि निराला के चिंतन में हिन्दी जातीयता का एक प्रदेश या प्रांत बनाने की बात बिलकुल नहीं है।