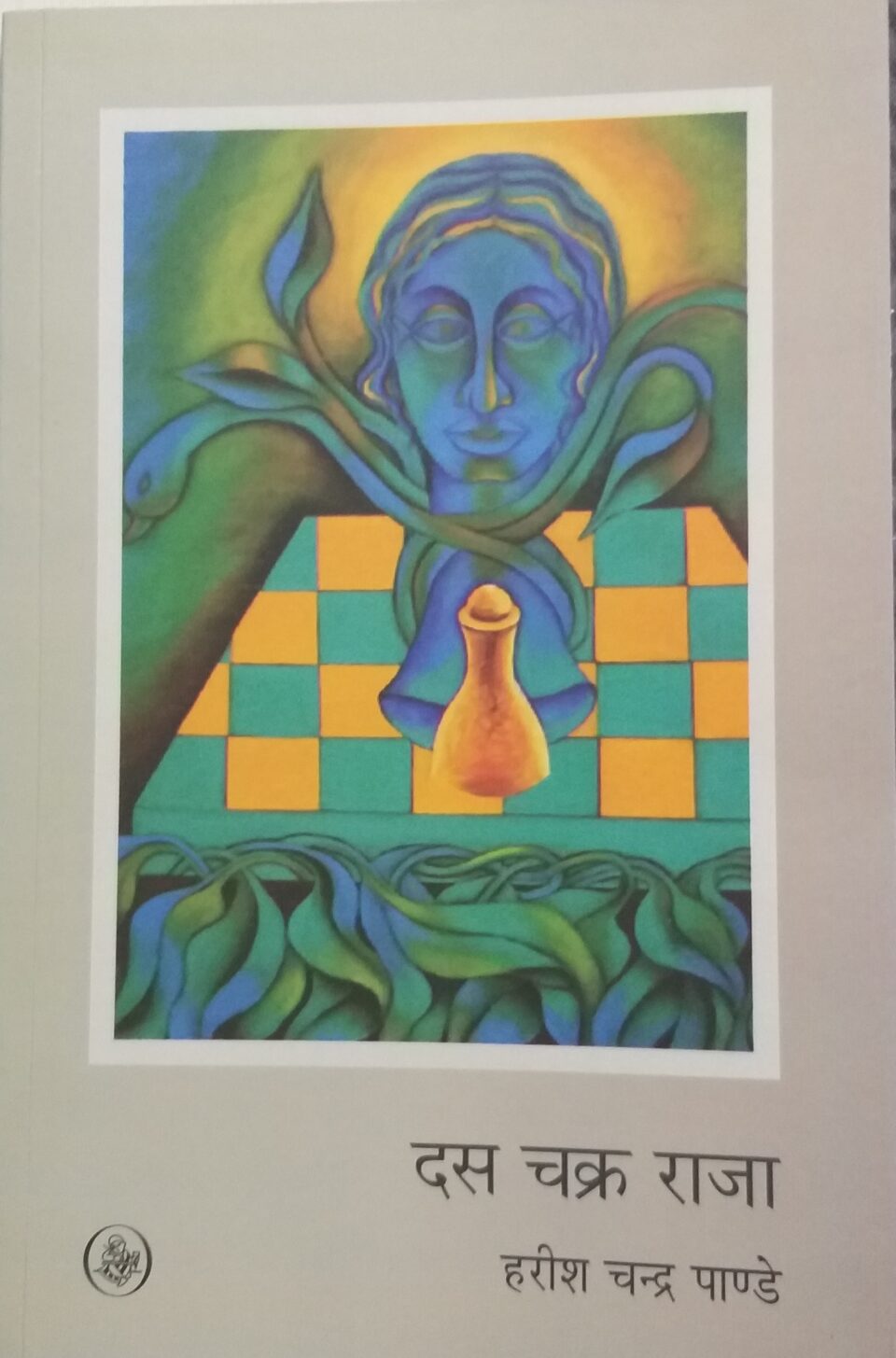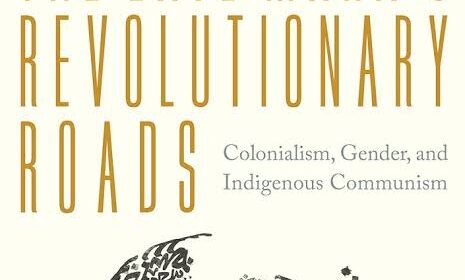हरीश चन्द्र पाण्डे एक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ‘कुछ भी मिथ्या नहीं है’, ‘एक बुरूंश कहीं खिलता है’, ‘भूमिकाएँ खत्म नहीं होतीं’, ‘असहमति’, ‘कछार कथा’ उनके चर्चा प्राप्त कविता-संग्रह हैं। समय-समय पर उन्होंने कहानियाँ भी लिखीं। यह कहानियाँ हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इन्हीं कहानियों का एक संग्रह ‘दस चक्र राजा’ नाम से प्रकाशित है। इसका पेपरबैक संस्करण 2024 में आया है। इस संग्रह में कुल उन्नीस कहानियाँ हैं। सभी कहानियाँ छोटा कथानक लिए हैं। एक बैठकी में पढ़ ली जाने वाली कहानियाँ हैं।
संग्रह की अधिकांश कहानियाँ पहाड़ के जीवन और संस्कृति को विषयवस्तु बनाती हैं। हरीश चन्द्र पाण्डे खुद अल्मोड़ा जिले के सदीगाँव नामक स्थान से हैं। उन्होंने इस संग्रह का समर्पण भी अपने अध्यापकों और गाँव के मित्रों को किया है।
संग्रह की पहली कहानी है, ‘वह फूल छूना चाहती है’। इस कहानी का मुख्य विचार पहाड़ की संस्कृति में प्रचलित रुढ़ियों, वर्जनाओं और सहज जीवन के द्वन्द्व से जुड़ा है। कहानी की मुख्य पात्र पुष्पा सामाजिक जीवन में स्त्री के ऊपर थोपी गयी वर्जनाओं को तोड़ती है। कहानी का मुख्य विचार तत्व यही है। लेकिन अपने मूल कथ्य तक पहुंचने से पहले कहानी पहाड़ के जीवन की जटिलताओं को उभारती है। सर्दी की रात का कठिन जीवन और इसका भार ढोती स्त्रियों की दिनचर्या के कई चित्र इस कहानी में उभरते हैं।
पुष्पा की माँ माहवारी के दिनों में स्त्री-वर्जनाओं का पालन कर रही है, जिसके चलते घर और चूल्हे-चौके का काम पुष्पा को करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में पुष्पा माँ के अलगाव को समझती है और खुद जब इससे गुजरती है, तो सामाजिक वर्जनाओं के इनकार तक बढ़ती है-
“पुष्पा गहरी नींद में थी कि अचानक उसे झस्स सी हुई। उसे लगा अभी-अभी वह कट कर एक द्वीप सा हो गई है। मुख्य जमीन से कटी हुई।…वह हरीतिमा छूना चाह रही थी।…वह फूलों को तोड़ना चाह रही थी…वह पानी से भरी गगरी लपक कर छूना चाह रही थी। वह सब कुछ छूना चाह रही थी जो सब इस द्वीप से त्याज्य है।”
दूसरी कहानी इस संग्रह की शीर्षक कहानी है, ‘दस चक्र राजा’। यह कहानी लोक समाज में व्याप्त अतार्किक मान्यताओं और विश्वासों का प्रत्याख्यान रचती है। मान्यता है, कि जिसके हाथों की दसों उंगलियों में चक्र होता है, वह राजा होता है। नरैण दा अपने अंगूठे के बचे चक्र को देखते रहते हैं, बाकी अंगुलियां बसूला चलाते घिस चुकी हैं-
“सुबह उठते ही सबसे पहले वह दाहिने हाथ की हथेली और अंगूठे का चक्र देखता था। एक दिन सुबह-सुबह सोबुली ने उसकी यही हथेली झटके से अपने हाथों में ले ली थी। नदी का रुख बदल गया है इसका कोई भी संकेत नहीं था हथेली पर, वह यही देख रही थी। कुछ नहीं है इनमें। सब्बल चलाने के निशान हैं, बस।”
नरैण दा अब चीड़ के पेड़ छीलने का काम करते हैं। नरैण दा और सोबुली अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन उनका जीवन रोज कमाने-खाने तक सीमित रहता है। वे खेत बनाते हैं, लेकिन बारिश में वह बह जाता है। इसके बावजूद सोबुली जीवन में विश्वास बनाये रखती हैं, और अपनी मेहनत के बल पर जीने की राह पर चलती है-
“गाँव के सामने से मोटर की सड़क निकल रही थी। काम जोरों पर था। गाड़ के पत्थर ढोये जा रहे थे, पत्थरों को तोड़ कर गिट्टी बन रही थी। औरतें पत्थर ढो रही थीं, मर्द उन्हें तोड़-तोड़ कर गिट्टियों में बदल रहे थे। सोबुली की आंखों में भी सपने तैरने लगे। इन औरतों की आंखों में ही आते हैं सपने सबसे पहले। एक सपना टूटता है तो दूसरा उगा लेती हैं। जमीन न हुई तो क्या हुआ। सोबुली भी एक दिन गाड़ से पत्थर ढोने वाली औरतों की कतार में शामिल हो गईं।”
यह कहानी भी अपने मुख्य विचार तक पहुंचने में पहाड़ के आम जीवन की कठिनाई के कई दृश्य को सामने लाती है। इसके साथ ही इन कहानियों में सांस्कृतिक विशिष्टता भी उभरती है।
हरीश चन्द्र पाण्डे ने कहानी में भी कुछ कविता का सा रचाव रखा है। चुने हुए प्रसंग छोटे और बिम्ब जैसे होते हैं। फैले हुए प्रसंग और विवरण इन कहानियों में कम हैं। कविता की भाषा का प्रायः बर्ताव लिए हुए भी, कहानी का मुख्य लक्ष्य जो होता है, वह उनकी कहानियों में मौजूद है। मसलन इसी में पहाड़ का जीवन, भूगोल, समाज और संस्कृति सब उभर आते हैं। इस लिहाज से ऊपर उल्लिखित दोनों कहानियाँ बहुत ही अच्छी हैं। हिन्दी की प्रगतिशील धारा की कहानियों के किसी भी संकलन में इन दोनों की जगह बनती है। अपने गठन और प्रभाव में भी यह कहानियाँ उम्दा हैं।
इस संग्रह की एक अन्य महत्वपूर्ण कहानी है, ‘कुंता’। कुंता तीन फीट लम्बी कद की स्त्री है और विवाह के बाद मायके में परित्यक्त जीवन जीती है। कुंता का पति दूसरी शादी कर लेता है। कुंता के ससुराल से निमंत्रण आते हैं, लेकिन वह तब तक नहीं जाती, जब तक कि उसका पति लिवाने नहीं आता। ऐसा मौका तब आता है, जब वह बूढ़ी हो जाती है। पति लिवा ले जाता है, लेकिन किसी लगाव वश नहीं, बल्कि पारलौकिक लोक मान्यताओं के डर वश। इस कहानी में एक उपेक्षित स्त्री-जीवन केन्द्र में है, जिसे लोक-वाचन की कथा-शैली में लिखा गया है।
हरीश चन्द्र पाण्डे के इस संग्रह में कई कहानियाँ हैं, जिनमें स्त्री जीवन के विभिन्न पहलुओं को, उनके जीवन में आने वाली तमाम तरह की दिक्कतों को कथावस्तु बनाया गया है। ‘प्रतीक्षा’, ‘बफर स्टेट’, ‘ढाल’ इस लिहाज से महत्वपूर्ण कहानी है। इन कहानियों में पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियाँ किन परिस्थितियों, सार्वजनिक जीवन की असुरक्षाओं से गुजरती हैं और कैसे उसमें जीवन जीने की राह निकालती हैं, इसे ही उभारा गया है। जिन कहानियों में स्त्री-जीवन मुख्य कथावस्तु नहीं है, उन कहानियों के कथानक में स्त्रियों का जीवन आ जाता है। जीवन की तमाम जिम्मेदारियों का बोझ उठाती स्त्रियाँ। ऐसी ही एक कहानी है, ‘बोहनी’। इस कहानी के परिवेश, वातावरण की बुनावट में स्त्री जीवन उभर आता है। क्योंकि कठोर श्रम केन्द्रित किसी भी परिवेश में स्त्रियाँ ज्यादा दिखेंगी। ऐसा परिवेश रचने वाले किसी भी सजग कहानीकार की दृष्टि से स्त्री ओझल नहीं हो सकती। श्रम में ज्यादा जगह घेरने वाले संवेदना में भी ज्यादा जगह पायें, यही रचनाशीलता की कसौटी होनी चाहिए। हरीश चन्द्र पाण्डे ने इसे अपनी रचनाशीलता की कसौटी बनाया है। बोहनी कहानी में परिवेश चित्रण का यह उदाहरण देखा जा सकता है-
“शुरू के व्यस्तता-भरे दिनों के बाद जब सब कुछ रूखा-रूखा-सा लगने लगा था तब नजाकत और कॉस्मेटिक से बोझिल औरतों ने नहीं वरन् जंगल की शुरुआती चढ़ाई पर चहकती चिड़ियों और इन्हीं औरतों ने उसे बासी होने से बचाया था। कभी-कभी तो वह दफ्तर के बाद इन्हीं के साथ ढलान पर उतरता। लकड़ी या घास के गट्ठरों से शरीर को बैठाता हुआ भार! धोतियाँ कमर में फैंट लगाकर बेतरतीब-सी बँधी। धवल-धवल पिंडलियों के जोड़े। गट्ठर के नीचे किनारों से बाहर झाँकते धूसर बाल…। भार के साथ ढलान पर उतरते वक्त और भी कितने सन्तुलन की जरूरत होती है, उसने यहीं देखा।”
हरीश चन्द्र पाण्डे के इस संग्रह की अधिकांश कहानियाँ श्रम आधारित समाज पर केन्द्रित हैं। एक कहानी है, ‘साथी’। इसमें साथी होटल में काम करने वाला ग्यारह-बारह साल का एक लड़का है। कहानीकार की जुबानी-
“साथी’ शब्द सुनते ही मैंने बहुत कुछ अनुमान लगा लिया था। एक आदमी मेहनती और इमानदार और साथ में वफादार भी, गरीबी उसका वर्ग चरित्र होगी। हाँ, वय की बात मैं नहीं कहता। वय कुछ भी हो सकती थी। आठ-नौ साल से लेकर साठ-पैंसठ तक के सब ‘साथी’ ही हैं।”
साथी का वर्ग चरित्र गरीबी है। साथी मेज साफ करने, खाना लगाने, बर्तन धुलने तक के सारे काम अकेले करता है। साथी हाड़-तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत का पूरा मूल्य उसको नहीं मिलता। होटल मालिक का व्यवहार भी अमानवीय। लेकिन जब एक दिन साथी चला जाता है, तो होटल मालिक कहता है,
“भाई साहब ! साथी बड़ा बदमाश निकला…भाग गया है…मैंने तो उसे हमेशा अपना ही बच्चा समझा…।”
कहानी पढ़कर कोई भी समझ जायेगा कि असल बदमाश साथी है या होटल मालिक। हरीश चन्द्र पाण्डे की कविताओं में भी यही खूबी मिलती है। सहज, सामान्य बातों, बिम्बों के भीतर से वर्ग चरित्र को उभार देना। इस संग्रह की कहानियाँ भी यहीं विशेषता लिये हैं। सहज, सामान्य कथा-प्रसंगों से कहानी अपने मूल कथ्य और विचार को पाठक के सामने ला देती है। इन कहानियों की संवेदना भी कविता की तरह आम जन, गरीब, निम्न मध्य वर्ग, उपेक्षित-पीड़ित समुदाय और स्त्री को मिलती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है कि एक कवि की लिखी कहानियाँ संवेदना के साथ शैली, शिल्प और गठन में भी पूरी तरह से सधी हुई हैं। इन कहानियों में वर्गीय सामान्य सत्य या साधारण लोगों के जीवन का सत्य प्रारूपित हुआ है। पुष्पा, नरैण दा, सोबुली, रूपाली, कुसुम, साथी आदि अपने तरह के सभी लोगों के जीवन-सत्य को धारण करते हैं। सभी अपनी स्थानीयता, बोली-भाषा, परिवेश में आसानी से पहचाने जा सकते हैं। ये कहानियाँ अपने कथ्य और शिल्प में जनवादी कथा-परम्परा से जुड़ी हैं। इन कहानियों में पठनीयता भरपूर है। पहले ही वाक्य से कहानी पाठक को अपने साथ कर लेती है।
इसी क्रम में पनाला, स्वदेश, इस पार, वेटिंग रूम, यात्रा, गड्ढा, दायरा, प्रोत्साहन, क्रमशः, वापसी, सन्धि-पत्र इस संग्रह की अन्य कहानियाँ हैं। इस संग्रह की भूमिका हिन्दी के प्रसिद्ध कहानीकार शेखर जोशी की लिखी है। आवरण चित्र वाज़्दा ख़ान का बनाया है। राजकमल पेपरबैक से प्रकाशित 120 पृष्ठ के इस संग्रह का मूल्य 199 रूपये है।